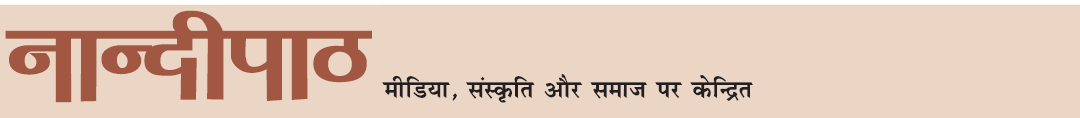संस्कृति, मीडिया और विचारधारात्मक प्रभाव
स्टुअर्ट हाल
स्टुअर्ट हाल का 10 फरवरी 2014 को निधन हो गया। उनके निधन के साथ मार्क्सवादी सांस्कृतिक अध्ययन का एक युग समाप्त हो गया। जमैका में पैदा हुए स्टुअर्ट हाल ने रेमण्ड विलियम्स और रिचर्ड होगार्ट के साथ मिलकर ‘ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़’ की शुरुआत की थी, जिसे कि बर्मिंघम स्कूल आपफ कल्चरल स्टडीज़ के नाम से जाना गया। हाल ने 1950 के दशक में प्रसिद्ध नववामपंथी पत्रिका न्यू लेफ्ट रिव्यू की भी स्थापना में केन्द्रीय भूमिका निभायी थी। पेशे से समाजशास्त्री हाल ने 1964 में होगार्ट के न्यौते पर बर्मिंघम विश्वविधालय में समकालीन सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र में काम करना शुरू किया।
हाल ने मीडिया व अन्य सांस्कृतिक माध्यमों के विश्लेषण के ग्राम्शी के वर्चस्व और अल्थूसर के विचारधारात्मक राज्य उपकरण के सिद्धान्तों का प्रयोग किया और जहाँ एक ओर अल्थूसर का अनुसरण करते हुए यह स्वीकार किया कि मीडिया वास्तव में प्रभावी विचारधारा के प्रभुत्व को पुनरुत्पादित करने का उपकरण है, वहीं अल्थूसर से अहसमत होते हुए, हाल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते कि इस विचारधारा का प्रभाव एकतरफ़ा नहीं होता है। जहाँ लोग संस्कृति के उपभोक्ता होते हैं, वहीं संस्कृति के उत्पादक भी होते हैं। हर सांस्कृतिक उत्पाद तभी प्रभावी होता है, जब लोग उसे अपनी अवस्थिति से विकूटीकृत करते हैं। इसलिए हर सांस्कृतिक उत्पादक कूटीकृत होने के बाद अपने रिसीव होने पर विकूटीकृत होता है। स्टुअर्ट हाल ने इस रूप में सांस्कृतिक अध्ययन में निर्धारणवाद का विरोध किया और एक कोडिंग/डीकोडिंग का उपयोगी सिद्धान्त दिया, जिसके कर्इ पहलुओं की निश्चित तौर पर आलोचना पेश की जा सकती है। सांस्कृतिक अध्ययन में हाल के योगदान को मान्यता देने के लिए उनके राजनीतिक विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है, जो अपनी सम्पूर्णता में नववाम के विचारों के करीब पड़ते हैं। फ़िर भी सांस्कृतिक आलोचना और विश्लेषण के मार्क्सवादी सिद्धान्त में हाल के योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस अंक में हम स्टुअर्ट हाल को श्रद्धांजलि देते हुए उनका यह महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत कर रहे हैं।
-सम्पादक
मार्क्स के अनुसार (दि जर्मन आइडियोलाजी) संस्कृति की जड़ें मनुष्य के ‘दोहरे सम्बन्ध’ में हैं, मनुष्य की प्रकृति से सम्बन्ध और अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध। मार्क्स ने यह समझाया है कि मनुष्य प्रकृति में हस्तक्षेप करता है और अपने कुछ औज़ारों तथा उपकरणों की सहायता से वह प्रकृति का उपयोग इस प्रकार से करता है कि उसके जीवन की भौतिक परिस्थितियों में कुछ वांछनीय परिवर्तन हो। मानव विकास की अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रकृति में मनुष्य का यह हस्तक्षेप श्रम के द्वारा सामाजिक दृष्टि से संगठित रहा है। अपनी भौतिक परिस्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से पुनरुत्पादित करने के लिए लोग एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, अपने साधारण औज़ारों का सामूहिक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, श्रम विभाजन के अत्यन्त प्रारम्भिक रूप का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं का विनिमय करते हैं। यही सामाजिक संगठन की शुरुआत है और मानव के इतिहास का भी। इस बिन्दु से लेकर प्रकृति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें सामाजिक हस्तक्षेप की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। निरन्तर जटिल होते जाने वाले और अधिक विस्तारित होने वाले रूपों में मानव जीवन का पुनरुत्पादन और मानव जीवन के भौतिक पहलुओं का पुनर्सृजन मूलभूत रूप में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य द्वारा प्रकृति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुकूल ढाल लेने का प्रयास उन्हीं रूपों में होता है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके सहयोगपूर्ण सम्बन्ध निर्मित कर लेते हैं, भौतिक उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाले तत्व ही अन्य प्रकार की संरचनाओं के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। इस आधारशिला से ही उत्पादन की शक्तियों और सम्बन्धों और जिस प्रकार वे सामाजिक स्तर पर संगठित किये जाते हैं – सामाजिक संरचना के और जटिल स्वरूप निर्मित होते हैं। इसके अलावा जो अन्य बातें इससे निकलती हैं वे इस प्रकार गिनायी जा सकती हैं, श्रम का विभाजन, विभिन्न प्रकार के समाजों में अन्तर की पहचान, भौतिक परिस्थितियों को बदलने के लिए कौशल और जानकारी को अपनाने के नये तौर-तरीके, सिविल और राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न स्वरूप, लोगों के विश्वास, विचार एवं सैद्धान्तिक अवधारणाएँ और भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही उनकी सामाजिक चेतना। सामाजिक विकास और मानव इतिहास की भौतिक समझदारी के लिए यही आधार है और यही बात संस्कृति की भौतिक परिभाषा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।
मार्क्स ने यह विचार प्रतिपादित किया कि सामान्य परिस्थितियों में कोर्इ भी श्रम अथवा उत्पादन नहीं हो सकता और उत्पादन पूर्वनिर्णीत परिस्थितियों में हमेशा विशेष ऐतिहासिक रूप धारण करता है। इन विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में समाज के विशेष प्रकार, सामाजिक सम्बन्ध एवं मानव संस्कृति भी एक निश्चित रूप धारण करती है। एक प्रकार का उत्पादन किसी अन्य प्रकार के उत्पादन से मूलत: भिन्न होता है। चूँकि भौतिक उत्पादन के विकास की प्रत्येक स्थिति विभिन्न प्रकार के सामाजिक सहयोग, तकनीकी एवं भौतिक उत्पादन की एक विशेष विधि और सिविल संगठन के विभिन्न रूपों को जन्म देती है, इसलिए मानव इतिहास विशिष्ट युगों में विभाजित किया जाता है। एक बार भौतिक उत्पादन और इसके अनुरूप सामाजिक संगठन के विभिन्न स्वरूप विकास की एक जटिल स्थिति पर पहुँच जाते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम गम्भीर विश्लेषण के बाद यह निश्चित करें कि विभिन्न स्तरों पर इनके सम्बन्धों की अवधारणा किस प्रकार विकसित की जा सकती है। सम्भवत: भौतिक सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन पहलू यह है कि भौतिक उत्पादन और इसके सामाजिक परिणामों के बीच सम्बन्ध निर्धारण किस प्रकार किया जाये और शेष सामाजिक परिस्थितियों के साथ इनके तालमेल के विवेचन का क्या स्वरूप हो।
हम थोड़ी ही देर में इस प्रश्न पर लौटते हैं कि लेकिन भौतिकवादी विवेचन को इस विचारधारा के अत्यन्त मूर्त पहलू को अपने में समाहित करना चाहिए। मार्क्सवादी विवेचन में यह मूर्त स्वरूप आधार (बेस) और अधिरचना (दि सुपर स्ट्रक्चर) के रूपक द्वारा व्यक्त होता है। मार्क्स के भौतिकवादी विवेचन में व्यक्ति के साथ एक और बात को जोड़ दिया गया है और वह है कि इस सम्बन्ध को निर्दिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में सोचा जाना चाहिए, इसे ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट होना चाहिए। यह दूसरी आवश्यकता ही एक ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणा को उस भौतिक विवेचन से अलग करती है जो मनुष्य के शारीरिक स्वभाव में अन्तनिर्हित है।
मार्क्स ने इसे द्वन्द्वरहित या भोंड़ा भौतिकवाद कहा है या ऐसा भौतिकवाद जो तकनीकी विकास को बहुत अधिक महत्व देता है। मार्क्स की दृष्टि में जो सम्बन्ध भौतिकवादी उत्पादन के सामाजिक सम्बन्ध को नियंत्रित करते हैं वे अत्यन्त विशिष्ट या निश्चित होते हैं। प्रत्येक विकास और चरण में प्रत्येक का अपना तौर-तरीक़ा होता है। उत्पादन की प्रत्येक पद्धति के अनुरूप सामाजिक और सांस्कृतिक अधिरचना ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट होगी। अब तक उत्पादन की प्रत्येक पद्धति ने श्रम का किसी न किसी प्रकार से शोषण करने का कोर्इ न कोर्इ तरीक़ा अपना लिया है। उत्पादन के मुख्य प्रकार, वे कितने ही जटिल, विकसित और कुशल क्यों न हों, अन्तरविरोध पर आधारित होते हैं। मार्क्स और एंगेल्स की अधिकांश कृतियों में ऐतिहासिक दृष्टि से निर्दिष्ट उन क़ानूनों और प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है जो उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही साथ उन अधिरचनाओं और विचारधारात्मक स्वरूपों पर भी गौर किया है जो समाज के भौतिकवादी विकास के अनुरूप रहे हैं। इस विवेचन में इस बात को अच्छी तरह से समझाया गया है कि भौतिक उत्पादन में श्रम का किस प्रकार से शोषण किया गया है और यह समझाया गया है कि भौतिक उत्पादन का यह गत्यात्मक प्रसारात्मक स्वरूप ऐतिहासिक दृष्टि से निर्दिष्ट था। इस विवेचन का आशय यह है कि भौतिकवादी उत्पादन को आगामी युगों में तकनीकी विकास के साथ स्वयं भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुज़रना होगा। मानव इतिहास के इस विकासक्रम में प्रत्येक अवस्था को आगे आने वाली अधिक विकसित अवस्था पीछे छोड़ देगी और इसका कारण कोर्इ बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आन्तरिक सम्बन्ध ही होगा (मार्क्स 1861)। मार्क्स का यह विवेचन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल का मुख्य प्रतिपाध विषय है।
चूँकि भौतिक उत्पादन और सामाजिक संगठन की प्रत्येक विधा ऐतिहासिक दृष्टि से नियंत्रित होती है इसलिए विभिन्न युगों के सामाजिक रूप भी एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। उत्पादन की प्रणाली को व्यक्तियों के भौतिक पुनरुत्पादन के ही रूप में ही देखना चाहिए बल्कि इन व्यक्तियों के क्रियाकलापों और जीवन के विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करने के उनके तौर-तरीकों के रूप में देखना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन को जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं वे वैसे ही हो जाते हैं और वे जैसे होते हैं वैसे ही उनका उत्पादन भी उस प्रकार का हो जाता है और इसमें दोनों ही बातें प्रभावित होती हैं, वे क्या उत्पादन करते हैं और किस प्रकार से करते हैं (मार्क्स, 1865)। उत्पादन के सामाजिक और भौतिक स्वरूप द्वारा श्रमिकों को जिस ढंग से संगठित किया गया और जिन औज़ारों से उन्होंने उत्पादन कार्य में हिस्सा लिया, पारिवारिक जीवन और सिविल समाज के किन-किन रूपों से होकर उन्हें गुज़रना पड़ा, तकनीकी विकास का कौन सा स्तर उन्होंने प्राप्त किया था और सिविल समितियों और पारिवारिक जीवन का उनका क्या स्तर था – ये सारे सम्बन्ध एक निश्चित ढाँचे की एक जीवन पद्धति को व्यक्त करते थे। इस ढाँचे से यह भी अभिव्यक्त होता था कि एक दूसरे से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों पर समग्र रूप से कैसे जिया जाता था।
संस्कृति के विवेचन में इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया है कि वह मानव अस्तित्व के एक विशेष रूप को व्यक्त करती है। उसके द्वारा एक ऐसी स्थिति का बोध होता है जिसमें कुछ निश्चित लोग निश्चित परिस्थितियों में प्रकृति के उत्पादनों को इस प्रकार से ग्रहण करते हैं कि वे उनके जीवन के अधिक से अधिक अनुकूल हों। वे श्रम पर ऐसी मोहर लगा देते हें जो पूर्ण रूप से मानवीय हो जाती है (कैपिटल)। संस्कृति की यह व्याख्या हमें उस विवेचन के निकट ले जाती है जिसे हम संस्कृति की नृतत्वशास्त्री परिभाषा के बहुत निकट पाते हैं। रेमण्ड विलियम्स का सैद्धान्तिक विवेचन (1960), टामसन द्वारा रेमण्ड विलियम्स के कार्य का संशोधन (1960) और इसके मूलभूत प्रकार्यवाद का विवेचन, सामाजिक नृतत्वशास्त्रीय लेखकों द्वारा जनजातियों की जीवन पद्धतियों का विस्तृत विवेचन – ये सभी बातें इसी परम्परा के अन्तर्गत आ जाती हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि मार्क्स और एंगेल्स ने संस्कृति शब्द का प्रयोग उसके मात्रा वर्णनात्मक अर्थ में ही नहीं किया है। मार्क्स और एंगेल्स ने संस्कृति शब्द का प्रयोग एक अधिक गतिमान और विकासात्मक अर्थ में किया है जिसके अन्तर्गत संस्कृति एक अधिक निर्णयात्मक और उत्पादक शक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। मानव संस्कृति प्रकृति पर मनुष्य के बढ़ते हुए स्वामित्व का परिणाम है। इसके माध्यम से वह प्रकृति के उपयोग को अपने उद्देश्य की दृष्टि से ढाल लेता है। यह एक प्रकार की मानवीय जानकारी है जिसको वह सामाजिक श्रम के द्वारा पूर्ण बनाता है और जो मनुष्य के उत्पादनशील ऐतिहासिक जीवन की प्रत्येक अवस्था का आधार प्रदान करती है। यह एक ऐसी जानकारी नहीं है जो कि अमूर्त तरीके से उसके मस्तिष्क में भरी हुर्इ है। इसका भौतिक स्वरूप उत्पादन में दिखायी पड़ता है और सामाजिक संगठन में इसका मूर्त स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है। व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक तकनीक के विकास के द्वारा यह भी विकास की विभिन्न स्थितियों से गुज़रती है।
जर्मन आइडियोलाजी नामक अपने ग्रंथ में मार्क्स ने निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख किया है – भौमिक परिणाम, उत्पादक शक्तियों का योग, ऐतिहासिक दृष्टि से उत्पन्न किया हुआ सम्बन्ध – व्यक्ति का प्रकृति से सम्बन्ध और एक-दूसरे से सम्बन्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नयी पीढ़ी इस सम्बन्ध को संशोधित करती है और अपने ढंग से उसे नयी दिशा और नया स्वरूप प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मनुष्य को पशु जगत से पृथक करती है। एंगेल्स ने इस प्रक्रिया में सबसे अधिक गतिशील तत्व मानवीय श्रम एवं वाणी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, चेतना की स्पष्टता का क्या आशय है, अमूर्तन की क्षमता क्या होती है और निर्णय कर सकने का क्या आशय है – इन सभी बातों ने श्रम और प्राणी दोनों को ही और भी अधिक विकास की प्रेरणा दी (लेबर इन ट्रांजिशन फ्राम एप टु मैन, एंगेल्य 1950 ए)। अपनी पुस्तक कैपिटल के एक प्रसिद्ध अंश में मार्क्स ने वास्तुकलाकारों की तुलना मधुमकिखयों से की है और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे लिखा है :
वास्तुकार किसी भी भवन को यथार्थ में निर्माण करने के पूर्व उसका ढाँचा अपने कल्पना में निर्मित करता है…। वह केवल रूप या आकार में ही परिवर्तन नहीं करता वरन वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है और उद्देश्य पूर्ति की यह इच्छा ही उसके कार्यकलापों के लिए क़ानून का निर्माण करती है (कैपिटल, पृ. 70)
इस अंश के पहले मार्क्स ने भाषा की पहचान करते हुए बताया है कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ाता है, संरक्षित रखता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है, यह एक प्रकार की व्यावहारिक चेतना है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार की इच्छा से उत्पन्न होती है (मार्क्स 1965)। बाद में मार्क्स ने इस बात को भी समझाया है कि यह संरक्षित जानकारी किस प्रकार व्यावहारिक श्रम एवं कौशल के द्वारा आधुनिक उधोग में उत्पादन की शक्ति के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और इस प्रकार पूँजी की सेवा में लगार्इ जा सकती है (कैपिटल 1, पृ. 361) । संस्कृति का अर्थ प्रकृति के उपर मनुष्य की शक्ति का संचित रूप है, जिसका श्रम के व्यवहार एवं उपकरणों द्वारा भौतिकीकरण हो जाता है और भाषा के द्वारा वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ‘दूसरी प्रकृति के रूप में पहुँचायी जाती है (देखें, वुल्पफसन 1976) ।
दि जर्मन आइडियोलाजी मार्क्स की ऐसी पुस्तक है जिसमें उन्होंने इस बात पर आग्रह किया है कि इतिहास को मानव जाति की चेतना के रूप में पढ़ा नहीं जाना चाहिए। विचार और अवधारणाओं का मस्तिष्क में उदय होता है किन्तु उन्हें भौतिक व्यवहार के रूप में समझाया जाना चाहिए और इसकी उल्टी प्रक्रिया को उचित नहीं समझा जा सकता। यह बात इस विचार के सर्वथा अनुकूल है कि संस्कृति की जानकारी और भाषा की जड़ें सामाजिक और भौतिक जीवन में विधमान रहती हैं। सामाजिक संरचना को भी मार्क्स ने स्वायत्त व्यवहारों के रूप में नहीं देखा है बल्कि एक ऐसे समग्र यथार्थ के रूप में उसका वर्णन किया जिसमें प्रत्येक वस्तु वास्तविक और सक्रिय लोगों और उनके सक्रिय व्यवहारों से उत्पन्न होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बात को कैसे समझाया जाये कि विचारों, अर्थ, मूल्य अवधारणाओं और चेतना के क्षेत्र में लोग किस प्रकार अनुभव अर्जित करते हैं जो कि उनकी वास्तविक भौतिक स्थिति के अनुरूप नहीं होती। ऐसा कैसे सम्भव होता है कि अपने जीवन और उत्पादन की यथार्थ परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न लोग किस प्रकार ग़लत चेतना निर्मित कर लेते हैं। क्या यह सोचा जा सकता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे संस्कृति को नृतत्वशास्त्रीय दृष्टि से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जा सकता है लेकिन भाषा के ही माध्यम से विकृति पैदा हो जाती है (थामसन 1960)। भाषा स्वतंत्र करने के स्थान पर बाँधने का भी काम करती है। इस प्रश्न का जवाब दि जर्मन आइडियोलाजी के उत्तरार्द्ध से प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्यों को ऐसी परिस्थितियों में रहकर काम करना होता है जिसके ऊपर उसका तनिक भी जोर नहीं चलता है। वे किसी भी तरह से अपने कार्यों के सामूहिक जनक की भूमिका अदा नहीं कर सकते।
मार्क्स ने इस बात को अच्छी तरह से समझाया है कि पूँजीवाद अब तक के मानव इतिहास में सबसे अधिक गमिमान उत्पादन का स्रोत रहा है। इसके गतिशील किन्तु इसके परस्पर विरोधी स्वभाव का परिणाम यह होता है कि उत्पादन इसके बढ़ते हुए समाजीकरण के ही द्वारा होता है अर्थात उत्पादन में श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस स्तर पर पूँजीवाद मनुष्य की उत्पादक शक्तियों के विकास और पूर्ण परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में श्रम की अन्तनिर्भरता बाज़ार के माध्यम से सम्भव हो पाती है। और बाज़ार में लोगों को बहुमुखी अन्तनिर्भरता (जिसे उसकी समाजप्रियता का आधार कहा जाता है) का अनुभव एक ऐसे तटस्थतापूर्ण परिवेश में होता है जिसमें व्यक्ति एक-दूसरे पर निर्भर ही नहीं करते बल्कि समय-समय पर उनमें संघर्ष भी होता है (मार्क्स 1973, पृ. 157)। यह एक विचित्र तथ्य है कि उत्पादन का सामाजिक स्वभाव एक ऐसी परिस्थिति में दिखायी पड़ता है जिसमें पारस्परिक उदासीनता विधमान रहती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रम का समाजीकरण और इसके विपरीत – जिसमें श्रम एक निजी सामग्री के रूप में उपस्थित होता है और जिसका शोषण किया जा सकता है तथा वस्तु विनिमय के माध्यम से बाज़ार व्यवस्था में इसको छोटे-छोटे अंशों में विभाजित भी किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत संस्कृति के विरोधी स्वरूप को समझें।
हम अनेक ऐसे समीक्षात्मक बिन्दुओं को देख सकते हैं जिनके द्वारा मार्क्स ने श्रम के सामाजिक स्वभाव और इसके निजी उपभोग को समझाया है। यह विसंगतिपूर्ण स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि बाज़ार में वस्तु विनिमय के माध्यम से उत्पादन का सामाजिक स्वभाव व्यक्ति के निजी उपभोग की सामग्री बन जाता है। बाज़ार का अस्तित्व वास्तविक है। यह किसी की कल्पना की उपज नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण अर्थ में यह अयथार्थ भी है क्योंकि यह अपनी सीमाओं के कारण उस समूचे सामाजिक सम्बन्ध को व्यक्त नहीं कर सकता जिसके ऊपर यह पूरी तरह आधारित होता है। बाज़ार एक ऐसी व्यवस्था को सूचित करता है जिसमें उत्पादन और विनिमय दोनों साथ-साथ चलते हैं लेकिन व्यवहार में ऐसा प्रतीत होता है कि विनिमय उत्पादन के ऊपर हावी हो गया है। हम यह नहीं देख पाते कि श्रम और उत्पादन एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। हम यह नहीं समझ पाते कि उत्पादन में ही श्रम का शोषण किया जाता है और बचत मूल्य को जिसको कि श्रम के द्वारा अर्जित किया जाता है उसे पूँजीपति हड़प लेता है। इन्हीं कारणों से पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत बाज़ार सम्बन्ध एक साथ ही वास्तविक और विचारधारात्मक दोनों ही हैं। वे विचारधारात्मक इसलिए हैं कि वे काल्पनिक नहीं हैं बल्कि उनका वास्तविक अस्तित्व है लेकिन जिन्हें मार्क्स ने वास्तविक सम्बन्धों का स्तर कहा है उसमें एक संरचनात्मक विसंगति दिखायी पड़ती है। हम इस सम्बन्ध में एक क़दम और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सामाजिक दृष्टि से निर्भर रहने वाला श्रम बाज़ार के क्षेत्र में स्वतंत्र और उदासीन सम्बन्धों में दिखायी पड़ता है। विचारधारात्मक सम्बन्धों के अन्तर्गत अनेक सिद्धान्तों, बिम्बों और चित्रों आदि का समावेश हो जाता है। पारिश्रमिक और कीमत, निजी ग्राहक और विक्रेता, उपभोक्ता अथवा सम्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धान्त आदि विषयों को क़ानून के अन्तर्गत रखते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों, प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र, अधिकार और कर्तव्य आदि प्रश्नों का समाधान भी विचारधारा के स्तर पर करने का प्रयास किया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक पूँजीवादी समाज के सम्बन्ध में एक जटिल क़ानूनी, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय और दार्शनिक विवेचन – इन सभी का उद्भव उन्हीं व्याप्तियों से होता है जिन पर बाज़ार का समाज और बाज़ारतंत्र आधारित होता है।
मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया है कि लोग अपने जीवन के वास्तविक सम्बन्धों को विचारधारात्मक स्तर पर जी लेते हैं। लेकिन यह विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग की होती है। पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमजीवी जिस बचत को अर्जित करता है उसका पूँजीपति अपहरण कर लेता है किन्तु बहुत ही चतुरार्इपूर्वक वह उसे मज़दूरी का नाम दे देता है। इस मज़दूरी की अवधारणा से ही विचारधारा के स्तर पर कुछ बातें उभर कर आती हैं जैसे मज़दूरी को लेकर सौदेबाजी और अर्थवाद जिसे लेनिन ने मज़दूर संघ की चेतना कहा है। इस सम्बन्ध में एक उक्ति भी प्रचलित है जो इस प्रकार है ‘एक अच्छी दिन की अच्छे काम के लिए मज़दूरी है।’ मार्क्स के अनुसार ये तत्व केवल पूँजीवाद के वर्णनात्मक विषय ही नहीं हैं बल्कि इनसे विचारधारात्मक झुकाव का पता चलता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मीडिया की क्या भूमिका होती है, इस बात पर विचार करने के पूर्व हम यह अच्छी तरह से समझ लें कि प्रभुत्वशाली विचारधारा का निर्माण किस प्रकार होता है। इस विचारधारा का दोनों वर्गों के साथ क्या सम्बन्ध होता है, पूँजी के लिए यह कौन से प्रकार्य करती है और वे कौन से ऐसे तौर-तरीके हैं जिनके माध्यम से यह व्यवस्था पूँजीवादी सम्बन्धों को बनाये रखती है।
प्रभुत्व की तीन सम्बन्धित अवधारणाएँ
अपने हाल के एक लेख में रेमण्ड विलियम्स ने (जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती विचारों में संशोधन किया है) यह विचार व्यक्त किया है, ‘किसी एक युग में व्यवहारों, अर्थों और मान्यताओं का ऐसा समूह दिखायी पड़ता है जिसे हम प्रभुत्वपूर्ण और प्रभावी कह सकते हैं – जिन्हें विशेष रूप से संगठित करके जिया जाता है। इस बात को हमें एक जड़ संरचना के रूप में नहीं वरन एक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जो अनेक बातों को अपने में शामिल कर लेती है’ (विलियम्स 1973)। अपने इस विचार की पुष्टि में विलियम्स ने शिक्षण संस्थाओं को इस प्रक्रिया के प्रमुख अभिकरणों के रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा अर्थों और मान्यताओं में से कुछ का चयन ‘ज़ोर देने के लिए किया जाता है और कुछ का परित्याग कर दिया जाता है। जो अर्थ या मान्यताएँ चयन की इस प्रक्रिया के बाहर होती हैं उनकी बार-बार व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि वे विचारधारा से रहित हो जायें या कम से कम यह इतना क्षीण हो जायें कि प्रभावी प्रभुत्वपूर्ण संस्कृति का विरोध न कर सके। विलियम्स ने वैकल्पिक अर्थ एवं व्यवहार की दो कोटियों का उल्लेख किया है। पहली कोटि में वे अवशिष्ट के रूप में आते हैं जो प्रमुख संरचना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये जा सकते क्योंकि ये अतीत से चले आ रहे होते हैं और इनका सम्बन्ध एक बीती हुर्इ व्यवस्था से होता है। ग्रामीण अतीत से सम्बन्धित विचार इस प्रकार के अवशिष्ट तत्व को ही व्यक्त करते हैं। इनके द्वारा प्रचलित संस्कृति की समीक्षा का निर्माण होता है। उभरकर आये हुए रूपों के अन्तर्गत नये व्यवहार, नये अर्थ और नयी मान्यताएँ आती हैं। संस्कृति के दोनों ही रूप (बचे हुए अथवा उभरकर पैदा हुए) आंशिक मात्रा में प्रमुख संरचना में शामिल किये जा सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि वे विचलित हो जाने वाले रूप के कारण छोड़े जा सकते हैं क्योंकि वे केन्द्रीय आग्रहों से भिन्न होते हैं।
बावजूद इसके कि रेमण्ड विलियम्स ने अनुभव और अभिप्राय पर लगातार जोर दिया है, यह कहा जा सकता है कि वह ग्राम्शी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से बहुत अधिक प्रभावित हैं। ग्राम्शी के अनुसार (1968) आधिपत्य की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब शासक वर्ग (या इस वर्ग के विभिन्न समूहों का गँठजोड़) विभिन्न अधीनस्थ समूहों को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वे इस प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों के अनुकूल अपने को ढाल लें। इतना ही नहीं इन अधीनस्थ वर्गों पर वह सम्पूर्ण सामाजिक सत्ता स्थापित कर लेता है और वह न केवल इन वर्गों को प्रभावित करता है बल्कि पूरी तरह से इनका दिशा-निर्देश भी करता है। यह दिशा-निर्देशन इतनी चतुरता के साथ किया जाता है कि अधीनस्थ वर्गों की पूरी तरह से इस बात की स्वीकृति सी मिल जाती है कि यह प्रभाव और प्रभुत्व लगातार इसी प्रकार चलता रहे।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रभाव और प्रभुत्व जोर-जबर्दस्ती और स्वीकृति इन दोनों की मिली-जुली ताक़त पर निर्भर करते हैं लेकिन इस सम्बन्ध में ग्राम्शी ने यह समझाया है कि उदारवादी पूँजीवादी राज्य में सहमति को प्राय: आगे कर दिया जाता है जबकि जोर दबाव के कवच के पीछे यह अपने को छिपा लेती है। आधिपत्य को केवल उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में प्राप्त कर लेना ही आवश्यक नहीं है बल्कि इसे राज्य एवं अधिरचना के सभी स्तरों तक सम्भव बनाना अनिवार्य है। आधिपत्य स्थापित करने के लिए अधीनस्थ वर्गों को सीमित करने के अलावा विचारधारा का सहारा लेना भी आवश्यक होता है। इसका अर्थ यह होता है कि यथार्थ की वे परिभाषाएँ जो प्रभुत्वशाली वर्गों के अनुकूल होती हैं और राज्य तथा सिविल समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत हो जाती हैं, वे ही इन अधीनस्थ वर्गों के लिए भोगे हुए यथार्थ की भाँति होती हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना के निर्माण में विचारधारा सीमेंट का काम करती है और पूरे समाज को विचारधारात्मक एकता प्रदान करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए सम्भव हो पाता है क्योंकि शासक वर्ग केवल दिशा-निर्देश एवं प्रतिषेध की क्षमता ही नहीं रखते बल्कि वे अपने इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं कि यथार्थ की परस्पर प्रतिस्पर्धी परिभाषाओं के क्षेत्रों और सभी विकल्पों को वे अपने विचार की परिधि में ले आते हैं।
शासक वर्ग ही उन संरचनात्मक एवं मानसिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं जिनके अन्तर्गत अधीनस्थ वर्गों को इस प्रकार जीवनयापन करना पड़ता है कि वे अपने ऊपर प्रभुत्व को बनाये रखने में सहायक हो सकें। ग्राम्शी ने यह स्पष्ट किया है कि विचारधारात्मक आधिपत्य को प्राप्त करने और बनाये रखने के लिए प्रचलित विचारधाराओं का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि आधिपत्य को बनाये रखने के लिए एक अकेला एकीकृत शासक वर्ग ही काफ़ी नहीं है बल्कि विभिन्न वर्गों के छोटे-छोटे टुकड़ों का गठबन्धन उसमें सहायक हो सकता है। अधिरचना के विभिन्न अभिकरणों द्वारा जिनमें परिवार, शिक्षा व्यवस्था, चर्च, मीडिया और सांस्कृतिक संगठन आ जाते हैं — आधिपत्य प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है। इसके साथ ही साथ राज्य के विभिन्न अभिकरण जैसे क़ानून, पुलिस, सेना आदि होते हैं वे भी आंशिक रूप से विचारधारा के माध्यम से ही काम करते हैं। आधिपत्य की अवधारणा के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रत्येक परिस्थिति में विधमान नहीं रहती अर्थात एक बार प्राप्त हो जाने के बाद भी इसे बनाये रखने का प्रयास करते रहना पड़ता है और ऐसा न किये जाने पर इसके खो जाने की भी आशंका रहती है। ग्राम्शी के ध्यान में इटली समाज का उदाहरण था जिसमें एक लम्बे समय तक शासक वर्ग के विभिन्न गुटों ने केवल शक्ति या जोर जबर्दस्ती के आधार पर शासन किया था और राज्य के अन्तर्गत अपनी सत्ता को क़ानूनी स्वरूप देने का कोर्इ प्रयास नहीं किया था। इससे सिद्ध यह होता है कि स्थायी आधिपत्य नाम की कोर्इ चीज़ नहीं है, इसे सक्रिय रूप से प्राप्त करके इसे सुरक्षित बनाने का प्रयास करना पड़ता है। इसके विपरीत स्थिति में यह दिखायी पड़ता है कि आधिपत्यात्मक परिस्थितियों में भी अधीनस्थ वर्गों को पूरी तरह से मिलाया नहीं जा सका है (जैसा कि मारक्यूज द्वारा लिखित वन डाइमेंशनल मैन से पता चलता है)। अधीनस्थ वर्गों का उत्पादन सम्बन्धों में वस्तुगत आधार होता है जिसके कारण सामाजिक जीवन के उनके अपने विशिष्ट रूप विकसित हो जाते हैं जो बड़े औद्योगिक घरानों के व्यवहारों और अन्य बातों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जब अधीनस्थ वर्गों के पास अपनी कोर्इ सांस्कृतिक शक्ति नहीं होती, जब वे पर्याप्त रूप से संगठित नहीं होते तो शासक वर्ग बड़े औद्योगिक घरानों की संस्कृति उनके ऊपर थोपने में सफल हो जाता है।
ग्राम्शी के द्वारा प्रतिपादित आधिपत्य की अवधारणा ने सैद्धान्तिक विवेचन के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रान्ति ला दी है और मार्क्स की दि जर्मन आइडियोलाजी में विवेचित सिद्धान्त की अपेक्षा यह अनेक दृष्टियों से अधिक विकसित प्रतीत होती है। इस अवधारणा के द्वारा ग्राम्शी ने प्रभुत्व के विचार को बहुत अधिक विस्तारित किया है। उसने इस अवधारणा को संरचना और अधिरचना के सम्बन्धों के अन्तर्गत रखा है और यह बताया है कि इन्हें बहुत अच्छी तरह से विवेचित किया जाना चाहिए ताकि किसी एक युग में जो शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो जाती हैं उनका सही-सही विश्लेषण किया जा सके (पृ. 117) । उसने शक्ति की सम्पूर्ण अवधारणा को इस प्रकार से पुनर्परिभाषित किया है कि इसके उन पहलुओं पर अच्छी तरह से प्रकाश पड़ सके जिनमें जोर जबर्दस्ती के तत्व शामिल नहीं होते हैं। उसने यह भी समझाया है कि संकीर्ण वर्ग हितों के द्वारा प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति की अपेक्षा शक्ति की अवधारणा का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत होता है। उसे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि विचारधारा न तो मनोवैज्ञानिक है और न ही नैतिक है बल्कि संरचनात्मक और ज्ञान मीमांसात्मक है।
ग्राम्शी अधिरचना के विभिन्न पहलुओं – राज्य एवं सिविल संगठनों, राजनीति एवं विचारधारा के महत्व का अनुभव करने को प्रेरित करता है और यह समझाता है कि समाजों को जोड़ने में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा विचारधारा इस बात को समझने में मदद मिलती है कि सम्पूर्ण सामाजिक, आचार-सम्बन्धी, मानसिक एवं नैतिक जीवन की प्रमुख प्रवृत्तियों को उत्पादन व्यवस्था के बिल्कुल उपयुक्त बनाया जाये। वर्ग शक्ति एवं विचारधारा की इस विस्तृत अवधारणा ने पूँजीवादी समाजों के सम्बन्ध में एक आंचलिक सिद्धान्त विकसित करने में सहायता दी है।
प्रभुत्व की तीसरी अवधारणा भी ग्राम्शी के ही द्वारा प्रेरित और विश्लेषित है, यद्यपि भौतिकवाद के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण के ऐतिहासिक पहलुओं की इसमें आलोचना की गर्इ है। अलथ्यूसर का महत्वपूर्ण लेख आइडियोलाजी एंड आइडियोलाजिकल स्टेट अपरेटस (1971)। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। इस निबन्ध में रिप्रोडक्शन या पुनरुत्पादन के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसने इन विषयों पर अभी हाल में की जाने वाली सैद्धान्तिक परिचर्चा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। संक्षेप में अलथ्यूसर के सिद्धान्त को इस प्रकार रखा जा सकता है :
उत्पादन व्यवस्था के रूप में पूँजीवाद उत्पादन की परिस्थितियों को बहुत विस्तारित रूप में पुनरुत्पादित करता है और इसमें सामाजिक सम्बन्ध भी शामिल हो जाते हैं, मुख्य रूप से श्रमशक्ति और उत्पादन के सम्बन्ध। यह स्पष्ट है कि मज़दूरी का इसमें सबसे पहले नम्बर आता है जिसके बिना श्रमशक्ति अपने को पुनरुत्पादित नहीं कर सकती और इसके बाद कुशलता का जिसके बिना श्रमशक्ति अपने को एक विकसित क्षमता के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकती। सबसे बाद में वे उपर्युक्त विचार आते हैं जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी प्रचलित व्यवस्था के नियमों के प्रति अपने को समर्पित करता है और इसके अन्तर्गत शासक वर्ग अपनी विचारधारा का प्रयोग श्रमजीवियों के शोषण और दमन के लिए करता है। विचारधारात्मक दासता के इन सभी रूपों के अन्तर्गत ही श्रमशक्ति की कुशलता का पुनरुत्पादन होता है (अलथ्यूसर 1971, पृ. 128) ।
सामाजिक पुनरुत्पादन की इस विस्तारित अवधारणा में उन सब उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए नहीं हैं। मज़दूरी के लिए श्रमशक्ति के पुनरुत्पादन में परिवार की आवश्यकता पड़ती है, कुशलता के पुनरुत्पादन के लिए शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, शासक वर्ग की विचारधारा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेने के लिए सांस्कृतिक संगठनों की आवश्यकता पड़ती है और इनके अतिरिक्त चर्च, संचार के साधन, राजनीतिक उपकरण एवं राज्य के प्रबन्धन की पद्धति इत्यादि भी इनमें शामिल हो जाती हैं। राज्य ही ऐसी संरचना है जो यह निश्चित करती है कि यह सामाजिक पुनरुत्पादन चलता रहे और (i) इसके लिए सम्पूर्ण समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है क्योंकि राज्य को तटस्थ और सभी वर्ग के दीर्घकालीन हित सुरक्षित रहें और इसका आधिपत्य बना रहे। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखते हुए अलथ्यूसर ने राज्य द्वारा प्रयुक्त सभी उपकरणों को ‘राज्य के विचारधारात्मक उपकरणों’ की संज्ञा दी है। वास्तविकता यह है कि अलथ्यूसर के साथ-साथ पौलंटाज ने भी राज्य के महत्व को अधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है और पूँजीवादी सम्बन्धों के पुनरुत्पादन में अन्य कारकों के महत्व की अपेक्षा की है। राज्य के उन तत्वों की अपेक्षा जो ज़ोर-ज़बर्दस्ती पर आधारित होते हैं, ये उपकरण मुख्य रूप से विचारधारा पर ही अवलमिबत होते हैं और उसके प्रचार-प्रसार का ही काम करते हैं। अलथ्यूसर ने इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार किया है कि शासक वर्ग प्रत्यक्ष रूप में या अपने प्रत्यक्ष हितों के संरक्षण के नाम पर शासन नहीं करता बल्कि उन सभी तत्वों और उपकरणों की सहायता लेता है जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है। जिन विभिन्न क्षेत्रों में ये उपकरण काम करते हैं उनकी विविधता और अन्तरविरोध को विचारधारा स्वयं में समाहित कर लेती है और इस कार्य में अलथ्यूसर ने सबसे गौरवपूर्ण स्थान परिवार और पाठशाला के युग्म को दिया है। उसने शासक वर्ग की विचारधारा को उन्हीं शब्दों में समझाया है जिनको पहले ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। उसने विचारधारा को ऐसे विचारों और चित्रणों का व्यवस्थित रूप बताया है जिनके माध्यम से लोग अपने अस्तित्व की वास्तविक परिस्थितियों के सम्बन्ध में एक काल्पनिक जगत में रहने लगते हैं : विचारधारा में जिस चीज़ का चित्रण होता है वह वास्तविक सम्बन्धों का नहीं होता जिनके द्वारा लोगों का जीवन संचालित होता है बल्कि काल्पनिक सम्बन्धों का होता है।
शब्दों के प्रयोग एवं सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य के मामलों में महत्वपूर्ण अन्तर के बावजूद, अलथ्यूसर ग्राम्शी के चिन्तन के बहुत निकट दिखायी पड़ते हैं (यह निकटता रीडिंग कैपिटल के अत्युत्साहपूर्ण विचारों की अपेक्षा कहीं अधिक है)। लेकिन अलथ्यूसर ने जिन दो बातों पर जोर दिया है वे महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि विचारधारा का क्षेत्र साधारण नहीं बल्कि जटिल होता है और इसमें केवल प्रमुख विचारों का ही समावेश नहीं होता बल्कि प्रमुख एवं अधीनस्थ वर्गों के विचारों का मिला-जुला प्रभाव दिखायी पड़ता है। इसलिए विचारधारात्मक उपकरणों के माध्यम से जो विचार प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें अन्तरविरोधों का अच्छा खासा चित्रण होता है। जिस दूसरी बात पर अलथ्यूसर ने जोर दिया है वह यह है कि राज्य के विचारधारात्मक उपकरण जो एकता प्राप्त करते हैं वह बहुत कष्टसाध्य होती है न कि प्रकार्यात्मक दृष्टि से बहुत सहज।
प्रभुत्वशाली पूँजीवादी व्यवस्था के लिए विचारधारा क्या करती है?
मार्क्स का अनुसरण करते हुए ग्राम्शी ने यह विचार व्यक्त किया है कि अधिरचना के दो तल होते हैं – सिविल समाज और राज्य। यह उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने इन दोनों को विचारधारात्मक रूप कहा है। ग्राम्शी ने इनके अन्तर को बहुत स्पष्टता के साथ नहीं समझाया है और यह मामला और भी जटिल इसलिए हो गया है क्योंकि विकसित पूँजीवादी समाज में इन दोनों (सिविल समाज एवं राज्य) के बीच की सीमा रेखाएँ खिसकती रहती हैं। (कृपया तुलना करें, ग्राम्शी 1968, पृ. 206 और आगे) इन दोनों के सम्बन्ध में विचारधारा के प्रश्न पर चिन्तन करते हुए पौलंटाज द्वारा प्रयुक्त दो शब्द – पृथक्करण एवं एकता के सूत्र में बाँधना – की सहायता ली जा सकती है। बाज़ार के सम्बन्धों एवं निजी अहंवादी हितों (जो सिविल समाज का मुख्य क्षेत्र है) के मामले में उत्पादक वर्ग दो रूपों में दिखायी पड़ते हैं : (अ) निजी आर्थिक इकाइयाँ जिनका उद्देश्य निजी स्तर पर धन कमाकर अपने अहं की तुष्टि करना है और (ब) जो अनेक अदृश्य अनुबंधों द्वारा बँधे हुए होते हैं और जिनमें पूँजीवादी विनियम सम्बन्धों का छिपा हुआ हाथ कहा जाता है। इसके तीन प्रभाव दिखार्इ पड़ते हैं, पहला प्रभाव इस बात में दिखायी पड़ता है कि उत्पादन की अपेक्षा विनियम पर अधिक आग्रह होता है, दूसरा प्रभाव वर्गों के व्यक्तियों के टुकड़ों में बदल जाने के रूप में दिखायी पड़ता है और तीसरा प्रभाव इस बात में दिखायी पड़ता है कि व्यक्तियों को ‘उपभोक्ताओं के निषिक्रय समूह’ में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य एवं विचारधारा की दृष्टि से राजनीतिक वर्गों एवं वर्ग सम्बन्धों को नागरिकों एवं मतदाताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ये ही नागरिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र के सदस्य के रूप में वे सामाजिक अनुबन्ध एवं अपने सामान्य एवं पारस्परिक हितों से बँधे रहते हैं। मार्क्स ने इस सामान्य हित को ‘अपने स्वार्थ साधन में लगे रहने वाले व्यक्तियों के समूह के हित’ नाम दिया है। राज्य का वर्ग स्वरूप छिपा रहता है, वर्गों का व्यक्तिगत प्रजाओं के रूप में पुनर्वितरण हो जाता है और ये व्यक्ति राज्य, राष्ट्र एवं राष्ट्रीय हित की काल्पनिक सम्बद्धता के कारण एक-दूसरे के साथ बँधे रहते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि इस यंत्र रचना के माध्यम से अनेक प्रमुख विचारधाराएँ किस प्रकार अपनी विशेष प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेती हैं।
पौलंटाज ने विचारधारा के अनेक आलोचनात्मक पहलुओं को प्रतिमानात्मक ढाँचे में रखा। पहला प्रभाव यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत विचारधारा वर्ग प्रभुत्व को छिपाये रखने का काम करती है। इसी प्रकार व्यवस्था का वर्गीय शोषण वाला रूप भी छिपा रहता है और इसकी परस्पर विरोधी आधारशिला भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाती। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की एकता शक्ति के पृथक्करण सिद्धान्त के सामने छिन्न-भिन्न हो जाती है (अलथ्यूसर 1971)। श्रमिक वर्गों के सामूहिक हितों को वर्ग के विभिन्न समूहों के आन्तरिक विरोधों के द्वारा क्षीण किया जाता है। जिस मूल्य को सार्वजनिक श्रम से उत्पादित किया जाता है उसे निजी और व्यक्तिगत ढंग से अपहरित कर लिया जाता है। उत्पादकों की आवश्यकता को उपभोक्ताओं की इच्छा कहकर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा विचारधारात्मक प्रभाव यह दिखायी पड़ता है कि इस प्रकार से प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न इकाइयों के ऊपर सुसम्बद्धता का एक काल्पनिक आवरण चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्रथम स्तर की वास्तविक एकता का स्थानान्तरण तृतीय स्तर के काल्पनिक सम्बन्धों द्वारा कर दिया जाता है। इस पद्धति के द्वारा व्यक्तियों को विभिन्न विचारधारात्मक समग्रताओं – जैसे समुदाय, राष्ट्र, लोकमत, सर्वस्वीकृति, सामान्य हित, लोक इच्छा, समाज, सामान्य उपभोक्ता में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस स्तर पर एकताओं को एक बार पुन: उत्पन्न कर दिया जाता है लेकिन ये ऐसे रूपों में होती हैं कि इनके द्वारा वर्ग सम्बन्धों एवं आर्थिक अन्तरविरोधों को अप्रतिस्पर्धी समग्रताओं के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ग्राम्शी के द्वारा विवेचित स्वीकृति एवं सुसम्बद्ध की यही प्रकार्यात्मक अवधारणा है।
आधुनिक विकसित पूँजीवादी परिस्थितयों में छिपाने वाली, टुकड़ों में विभाजित करने वाली एवं एकता के सूत्र में बाँधने वाली प्रक्रिया राज्य द्वारा अपनायी जाती है। हम इस बिन्दु पर राज्य के सम्बन्ध में मार्क्सवादी अवधारणा का विस्तृत विवेचन नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे लिए यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्ग हितों का सामान्यीकरण और सार्वभौमीकरण हो जाता है और वह सामान्य हित में परिवर्तित हो जाता है। प्रभुत्व केवल शक्ति पर ही आधारित नहीं होता बल्कि स्वीकृति एवं नेतृत्व पर भी होता है क्योंकि राज्य की मध्यस्थता के द्वारा वर्ग हितों का सामान्यीकरण हो जाता है। ग्राम्शी ने इस प्रक्रिया को ‘संरचना से होते हुए जटिल अधिरचनाओं तक पहुँचने की दिशा में एक निर्णायक कदम’ बताया है (ग्राम्शी 1968, पृ. 181)। पूँजी के लगातार विस्तार के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है क्योंकि पूँजी की ओर से राज्य ऐसी भूमिका अदा करता है जिसे एंगेल्स ने ‘आदर्श समग्र पूँजीपति’ कहा है। इस भूमिका के अन्तर्गत राज्य पूँजी के दूरगामी हितों को पूँजीपतियों के विभिन्न तबकों के तात्कालिक हितों के विरुद्ध सुरक्षित रखता है। इस मामले में शासक वर्गों के किसी भी गठबन्धन की अपेक्षा इसे (पूँजी को) अधिक स्वतंत्राता प्राप्त होती है। राज्य लेनिन द्वारा वर्णित कार्यपालिका समिति की तरह शासन करने के बजाय, वर्ग राज्य की मध्यस्थता के द्वारा शासन करता है। अपने विचारधारात्मक व्याख्यानों द्वारा राज्य इस बात में सफल हो जाता है कि वर्ग हितों को वह सामान्य हित का रूप प्रदान कर सके और जैसा कि मार्क्स ने दि जर्मन आइडियोलाजी में समझाया है कि ‘वर्ग हितों को सार्वभौमिकता का रूप प्रदान करके उन्हीं को विचारपूर्ण एवं सभी परिस्थितियों में मान्य बताकर’ प्रस्तुत किया जाता है। अपने इसी प्रकार्य के द्वारा राज्य एक ऐसी व्यवस्था आरोपित करता है जो वर्ग शोषण को क़ानूनी रूप देने में सहायक सिद्ध होती है (लेनिन 1933)। इस सम्बन्ध में एंगेल्स ने पहले ही कहा था, एक बार जब राज्य समाज के मुक़ाबले में स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है तब यह एक विचारधारा को जन्म देता है। व्यावसायिक राजनीतिकों, सार्वजनिक क़ानून के सिद्धान्तकारों और निजी क़ानून के विज्ञों के लिए आर्थिक तथ्यों के साथ विचारधारा के सम्बन्ध धूमिल पड़ जाते हैं।
अवधारणाओं और उनकी भौतिक परिस्थितियों के बीच अन्तरसम्बन्ध अधिक से अधिक जटिल होते जाते हैं और बीच की कड़ियों के कारण उनकी अस्पष्टता बहुत बढ़ जाती है (एंगेल्स, 1950)।
विचारधारात्मक प्रभावों का तीसरा क्षेत्र जिसका हमें उल्लेख करना है, वह विचारधारा के निरूपण से सम्बन्धित नहीं है बल्कि उन निरूपणों या चित्रणों के लिए वैधता या स्वीकृति प्राप्त करने से सम्बन्धित है। प्रभुत्व की जो अवधारणा ग्राम्शी ने दी है उसमें वैधता एवं स्वीकृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि इनके द्वारा ही शिक्षात्मक एवं आचार सम्बन्धी कार्य सम्पादित होते हैं और प्रभुत्वशाली वर्ग अधीनस्थ वर्गों द्वारा इन्हीं की सहायता से स्वीकृति प्राप्त करते हैं। छिपाने, टुकड़ों में विभाजित करने एवं एकता के सूत्र में बाँधने की जिस प्रक्रिया का पहले उल्लेख किया जा चुका है वह अधीनस्थ वर्गों द्वारा अपनी अधीनता को स्वीकार करने में भी दिखायी पड़ती है। किसी एक वर्ग का अन्य वर्गों पर प्रभाव इस क्षेत्र में अदृश्य सा हो जाता है, यह विचारधारात्मक प्रभाव तितर-बितर सा हो जाता है क्योंकि असंख्य निजी संकल्पों एवं सम्मतियों की भूमिका उन्हें टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं। स्वीकृति एवं सर्वसहमति की यह प्रक्रिया – जो प्रभुत्व के बिल्कुल विपरीत स्थिति का बोध कराती है – उन प्रमुख कार्यों में एक है जो प्रमुख विचारधाराओं द्वारा किये जाते हैं।
केवल इसी बिन्दु को लेकर यह प्रयत्न किया जा सकता है कि समसामयिक पूँजीवादी समाजों में संचार के साधनों की भूमिका और उसके प्रभावों का विवेचन किया जाये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मीडिया के विचारधारात्मक प्रभाव को उसका एकमात्र कार्य नहीं समझा जाना चाहिए। मीडिया के आधुनिक रूप सबसे पहले निश्चयात्मक तरीके से अठारहवीं शताब्दी में दिखायी पड़ते हैं। इसी समय इंग्लैण्ड पूँजीवादी समाज में बदल रहा था। इसी समय पहली बार एक कलात्मक या साहित्यिक कृति माल बन जाती है और साहित्यिक बाज़ार में इसे अपने विनिमय मूल्य का बोध होता है, एक ऐसी संस्कृति का जन्म होता है जिसकी जड़ें बाज़ार के सम्बन्धों में हैं : पुस्तकें, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तक विक्रेता, सचल पुस्तकालय, समीक्षण एवं समीक्षाएँ, पत्रकार और कलमघसीटू लेखक, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें और अधिक बिकने वाली घटिया पुस्तकें – इन सभी का एकाएक उद्भव हो जाता है। इसी युग में उपन्यास का उदय होता है जिसका सीधा सम्बन्ध उभरते हुए बुर्ज़ुआ के साथ है। सांस्कृतिक सम्बन्धों और उत्पादों में यह पूरा परिवर्तन एवं इनके उपभोग के प्रति बदली हुर्इ दृष्टि के कारण संस्कृति के क्षेत्र में विच्छेद दिखायी पड़ता है, सांस्कृतिक विवाद का सर्वप्रथम लक्षण दिखायी पड़ने लगता है (लोवेनयाल 1961)।
यहाँ हम मीडिया के ऐतिहासिक विकास के बारे में अधिक विस्तार के साथ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यह बतलाना आवश्यक है कि यह अगले परिवर्तन से सम्बन्धित है। यह परिवर्तन एक ग्रामीण पूँजीवादी समाज एवं उसकी संस्कृति को एक औद्योगिक नगरीय संस्कृति एवं समाज बना देता है। इस बदलाव के कारण ही परिवर्तन का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है क्योंकि इसके द्वारा ही वह भौतिक आधार एवं सामाजिक संगठन सम्भव हुआ जो परिवर्तन के दूसरे चरण के लिए आवश्यक था। इसका तृतीय चरण उस समय प्रारम्भ हुआ जब औद्योगिक पूँजीवाद का परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अहस्तक्षेप की नीति वाला पूँजीवाद, एकाधिकार वाले पूँजीवाद में परिवर्तित हो गया। यह लम्बा, असमान एवं अनेक दृष्टियों से अभी भी अपूर्ण संक्रमण्ण 1880 के दशक से प्रारम्भ होकर अभी तक चला आ रहा है। इसके निम्नलिखित तत्व उल्लेखनीय हैं – नया लोकप्रिय समाचारपत्र अपनी जड़ें जमा लेता है, इंग्लैण्ड का श्रमिक वर्ग अपने को पुन: निर्मित कर लेता है ;स्टीडमान जोन्स 1975द्ध। शहरी जीवन का विकास होता है, पूँजी का संकेन्द्रण होता है और पूँजीवादी श्रम-विभाजन अपने को पुनर्गठित कर लेता है। इसके अलावा उत्पादन और तकनीक के अभूतपूर्व प्रसार एवं सार्वजनिक बाज़ारों के विकास और विशाल पैमाने पर घरेलू उपभोग में अभिवृ(ि को भी इस परिवर्तन के प्रमुख तत्वों में गिना जाता है। इसी चरण में आधुनिक संचार साधन पूरी तरह से विकसित होकर अपनी जगह बना लेते हैं। ये संस्कृति के प्रसार के मुख्य साधन बन जाते हैं और सार्वजनिक सम्प्रेषण को अधिक से अधिक अपने में समाहित करके अपनी उपयोगिता में अभूतपूर्व अभिवृ(ि कर लेते हैं। ये सारे तत्व उन बातों से सम्बन्धित हैं जिन्हें आधुनिक एकाधिकारी पूँजीवाद की विशेषता कहा जा सकता है। विकास के परवर्ती चरणों में मीडिया आधुनिक उत्पादन प्रणाली एवं श्रमिक जीवन के केन्द्र बिन्दु में प्रवेश पा लेता है और पूँजी के पुनर्गठन में अपनी जड़ें जमा लेता है। हमें इस समय मीडिया पर विचारधारात्मक उपकरण के रूप में अपना ध्यान केनिद्रत करना है इसलिए विकास के इन पहलुओं पर अधिक विचार नहीं कर सकते।
बीसवीं शताब्दी के विकसित पूँजीवाद में मीडिया ने संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से सांस्कृतिक क्षेत्र में निर्णायक और महत्वपूर्ण नेतृत्व ग्रहण कर लिया है। आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से मीडिया के पास जितने संसाधन हैं उतने किसी भी परम्परागत अभिकरण के पास सोचे भी नहीं जा सकते। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान जटिल ढाँचा – जिसमें सार्वजनिक सूचना, अन्त:सम्प्रेषण एवं विनिमय शामिल हैं – पूरी तरह से मीडिया पर अवलमिबत है और सामाजिक जानकारी का उत्पादन एवं उपभोग इसी के माध्यम से होता है। मीडिया ने समूचे सांस्कृतिक एवं विचारधारात्मक क्षेत्र पर अपना उपनिवेश सा स्थापित कर लिया है। निम्नलिखित मामलों में मीडिया की ही सबसे बड़ी जि़म्मेदारी है : ;कद्ध वह आधार प्रदान करने में जिसके द्वारा समूह और वर्ग अन्य वर्गों के जीवन व्यवहारों, प्रयोजनों और मान्यताओं के बारे में बिम्ब बनाते हैं। ;खद्ध वैसे बिम्ब, चित्रण और विचार प्रदान करने में जिनके द्वारा सामाजिक यथार्थ को सुसम्ब( ढंग से उसकी सम्पूर्णता में समझा जा सकता है। इसे आधुनिक मीडिया के महान सांस्कृतिक कार्यों में प्रथम गिना जा सकता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक जानकारी को निर्मित कर सकते हैं और दूसरे लोगों के द्वारा भोगे हुए यथार्थ को अपनी कल्पना के सहारे अनुभव कर सकते हैं।
वर्तमान पूँजी और उत्पादन के अन्तर्गत जीवन की परिस्थितियाँ बहुत जटिल और विविधतामयी हो गर्इ हैं जिसकी वजह से समाज बहुलतापूर्ण होता जा रहा है। क्षेत्रों, वर्गों, उपवर्गों, संस्कृतियों, पड़ोस के स्थानों एवं समुदायों तथा हित-समूहों एवं अल्पसंख्यकों आदि में रहन-सहन की जो विभिन्नताएँ दिखायी पड़ती हैं उनका मीडिया में चित्रण इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें एक प्रकार का पुन:सृजन दिखायी पड़ता है। इस दृश्यमान बहुलता एवं विविधता के ही कारण ‘सामूहिक चित्रण की आवश्यकता काअनुभव किया जाता है जो पिछले युगों के विचारधारात्मक संसार की एकरूपता से बिल्कुल ही भिन्न होता है। आधुनिक मीडिया का दूसरा काम यह है कि वर्तमान जीवन की बहुलता पर बार-बार विचार करे और उन शब्दकोषों, जीवन शैलियों और विचारधाराओं की लगातार सूची प्रस्तुत करता रहे जो उसमें (मीडिया) निरूपित किये गये हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक जानकारी का वर्गीकरण किया जाता है, उनकी कोटि निर्धारित की जाती है और उन्हें व्यवस्थित रूप दिया जाता है। इसके अलावा समस्यापूर्ण सामाजिक यथार्थ के नक्शों में ;गीत्र्ज, 1964द्ध उनका संदर्भ बताया जाता है। इस सम्बन्ध में जैसा कि हैलोरन ने कहा है, ”मीडिया का प्रकार्य यह है कि वह सामाजिक यथार्थ के उन पहलुओं का चित्रण करे जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं और प्रचलित प्रवृत्तियों को नयी दशा दिखाये। यह प्रकार्य मीडिया के द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि नये दृष्टिकोण को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाये और इस मामले में विफलता को सामाजिक विचलन के रूप में देखा जाये ;हैलोरन ;सद्ध 1970द्ध। यह उल्लेखनीय है कि मीडिया जिस जानकारी को चयनित करके प्रस्तुत करता है उनका वांछित अर्थों में एवं व्याख्याओं के आधार पर मूल्यांकन करके वर्गीकरण होता है। जैसा कि हमने पहले समझाया है, कोर्इ ऐसी अकेली विचारधारा नहीं जिसमें यह सम्पूर्ण चयनित सामाजिक जानकारी समाहित की जा सके और यह भी आवश्यक होता है कि एक शासक वर्ग के जीवन के अलावा भी ऐसा संसार है जिसका चित्रण किया जाना चाहिए। इन दोनों कारकों ने इस कार्य को बड़ा ही दुरूह और जटिल बना दिया है क्योंकि इसके अन्तर्गत हमें सभी सामाजिक सम्बन्धों को उनकी वर्गीकृत योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ता है और हमें ”संसारों के बारे में न केवल जानकारी ही प्राप्त करनी पड़ती है बल्कि उन्हें समझना भी आवश्यक होता है। वोलोशिनोव का कथन है कि वर्ग और चिन्ह साथ-साथ नहीं चलते अर्थात विचारधारात्मक सम्प्रेषण के लिए एक वर्ग के लोग एक जैसे चिन्ह का ही प्रयोग नहीं करते। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न वर्गों के लोग एक ही और उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि विभिन्न प्रयोजनों को व्यक्त करने वाले चिन्ह परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और इस प्रतिच्छेदन की प्रक्रिया के ही कारण कोर्इ भी चिन्ह अपनी सशक्तता एवं गतिशीलता बनाये रखता है। जो चिन्ह सामाजिक संघर्ष के दबाव का अतिक्रमण कर देता है वह अपनी शक्ति खो बैठता है, वक एक रूपक कथा में परिवर्तित हो जाता है और वह एक जीवित सामाजिक सम्प्रेषण का विषय न होकर भाषा विज्ञान से सम्बन्धित समझदारी का विषय बन जाता है (पूर्वोक्त पृ. 23)।
इस दृष्टिकोण से मीडिया का तीसरा प्रकार्य यह है कि जिस सामग्री को चयनित और वर्गीकृत करके यह प्रस्तुत करता है उसे इस प्रकार से संगठित करके एकसाथ रख दिया जाये कि उसके द्वारा समवेत स्वर से उसी तथ्य का वाचन किया जा सके। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बहुलता के बावजूद चित्रण की एक काल्पनिक सुसम्बद्धता का निर्माण होना चाहिए। जिसे प्रदर्शित और वर्गीकृत किया गया है उसे एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना ज़रूरी होता है। यह एक ऐसा जटिल रूप होता है जिसमें वर्ग, शक्ति, शोषण और हित आदि प्रश्नों का पूरी तरह परिहार कर दिया जाता है और ऐसा करने के लिए एक सामान्य लोकमत का निर्माण किया जाता है। इस कठिन एवं समझौते पर आधारित काम के द्वारा सहमति और सर्वसम्मति की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिसके माध्यम से समस्याओं के समाहार या समाधान का प्रयास किया जाता है। सम्मतियों की सहज अभिव्यक्ति एवं विचारों के स्वतंत्र विनिमय के वातावरण में यह स्वाभाविक है कि कुछ विचार अधिक प्रबलता के साथ उभरकर आते हैं और वे व्यापक रूप से प्रचलित हो जाते हैं। क्लासिकल उदारवादी प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्त जिसके अन्तर्गत विशु( सर्वसम्मति प्राप्त की जाती है – के स्थान पर यथार्थ पर आधारित एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गर्इ है जिसमें सर्वसम्मति को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जाता है और यह उस असमानता पर आधारित होती है जिसमें एक ओर तो असंगठित जनता है और दूसरी ओर शक्ति एवं सम्मति को संगठित करने वाले केन्द्र हैं। इस प्रकार की बलात थोपी जाने वाली सर्वसम्मति को कन्सेन्सस आपफ दि बिग बटैलियन्स कहा गया है। बावजूद इस स्थिति के दूसरी सम्मतियों के लिए भी जगह बनायी जाती है और ‘अल्पसंख्यकों का दृष्टिकोण, कुछ भिन्न और विरोधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है ताकि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसके साथ अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव सम्भव हो सके। मीडिया के द्वारा विचारधारा के क्षेत्र में एकता और सुदृढ़ीकरण का जो प्रयास किया जाता है उसका सबसे आवश्यक पहलू इस प्रकार का कार्य ही है। सर्वसम्मति का निर्माण, वैधता की रचना – एक पके पकाये तैयार माल की तरह नहीं – बल्कि बतौर एक प्रक्रिया के जिसमें विचार प्रकाशन, विनिमय, विवाद एवं अनुमान आदि शामिल हैं – इस कार्य को ही मीडिया के विचारधारात्मक प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कहा जा सकता है।
अन्त में हमें इस बात पर भी विचार करना है कि इस विचारधारात्मक प्रकार्य को करने के लिए मीडिया किस संयंत्रा को अपनाता है। वर्गीय प्रजातंत्रों में मीडिया को प्रत्यक्ष रूप से आदेश नहीं दिया जा सकता ;यद्यपि ब्रिटिश ब्राडकासिटंग कारपोरेशन का राज्य के साथ सम्बन्ध बहुत स्पष्ट हैद्ध। इसके अलावा शासक वर्ग का कोर्इ हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इसे कमजोर नहीं कर सकता। जहाँ तक दैनिक प्रशासन का सम्बन्ध है, मीडिया व्यावसायिक दृष्टि से निष्पक्ष व्यवस्था के अन्तर्गत काम करता है। यह आशा की जाती है समाचार-प्रसारण अथवा राजनीतिक-आर्थिक मामलों में विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर मीडिया के ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह स्थिति ‘क़ानून का शासन की अवधारणा से मिलती है। खुल्लमखुल्ला पक्षपात किये जाने की घटनाओं को नियम नहीं बल्कि अपवाद के रूप में लिया जा सकता है। इन परिस्थितियों में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों पर प्रमुख रूप से प्रचलित विचारधारा का प्रभाव किस प्रकार दिखायी पड़ता है।
टेलीविजन को मानक उदाहरण के रूप में लेते हुए हम उन पद्धतियों में से कुछ का ही उल्लेख कर सकेंगे जिनके माध्यम से मीडिया अपने विचारधारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। जैसा कि हमने पहले बताया है, मीडिया ऐसे उपकरणों को कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से संगठित किया जाता है और जिसका उद्देश्य सन्देश एवं चिन्ह देना होता है, जो ‘प्रतीकात्मक माल कहे जा सकते हैं। इन ‘प्रतीकात्मक मालों का उत्पादन भाषा की सम्प्रेषण शक्ति के द्वारा किया जा सकता है और भाषा ऐसे शब्दों या चिन्हों का प्रयोग करती है जिनका कोर्इ अर्थ होता है। घटनाएँ, अपने आपमें कुछ भी सूचित नहीं करतीं। जब तक कि उन्हें समझने योग्य नहीं बनाया जाता तब तक उनका कोर्इ भी प्रभाव नहीं हो सकता। घटनाओं की सामाजिक बोधगम्यता इस बात पर निर्भर होती है कि वास्तविक घटनाओं को किस प्रकार प्रतीकात्मक रूपों में परिवर्तन किया जाये। यह वही प्रक्रिया है जिसके लिए इंकोडिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग हाल ;1974द्ध ने किया है जिसका अर्थ यह है कि कोड के माध्यम से घटनाओं को अर्थ प्रदान किया जाता है। घटनाओं को इनकोड या संकेतित करने के बिल्कुल ही विभिन्न तरीके होते हैं, मुख्यत: उन घटनाओं को जो समस्यापूर्ण या चिन्ताजनक होती हैं, जो हमारी सामान्य एवं दैननिदन आशाओं को èवस्त करती हैं, जो सामान्य प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में जाती हुर्इ दिखती हैं या जो किसी न किसी रूप में यथास्थिति के सम्मुख कोर्इ ख़तरा उत्पन्न कर देती हैं। संकेतों का चुनाव उस सामान्य स्पष्टीकरण पर आधारित होता है जिसे समाज स्वीकार कर लेने के लिए तैयार रहता है, जिसमें एक खास समाज की वैचारिकता प्रतिबिम्बित होती है और संकेतों का यह चयन प्रमुख एवं प्रचलित विचारधारा के ही अन्तर्गत होता है।
इस सम्बन्ध में हमें यह याद रखना चाहिए कि संकेतों का चयन करने वाले, घटनाओं का पुनरुत्पादन नहीं वरन प्रस्तुतीकरण करते हैं और ऐसा करने में वे अनेक प्रचलित अर्थों में से किसी को ही चुनते हैं। चूँकि इन अर्थों का सामान्यीकरण या सार्वभौमीकरण हो चुका होता है इसलिए ये ही बोधगम्यता के उदाहरण के रूप में रह जाते है।, ‘वे विचारपूर्ण एवं सार्वभौम रूप से वैध अवधारणाओं के रूप में स्वीकृत होते हैं। जिन शर्तों एवं व्यापितयों के कारण इन वैचारिक अवधारणाओं को सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है वे शर्तें एवं व्यापितयाँ प्रच्छन्न सी हो जाती हैं क्योंकि इनके पीछे वही प्रक्रिया काम कर रही होती है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। जो इन व्यापितयों को इनकोडिंग या संकेतीकरण के लिए प्रयोग करते हैं उनके लिए भी वे उन बातों के सारांश के रूप में ही रह जाती हैं जिन्हें हम पहले से जानते रहते हैं। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया इनकोडर्स के लिए भी सचेतन रूप में नहीं रह जाती। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यापितयाँ होती हैं और ये व्यापितयाँ परिस्थिति की प्रमुख परिभाषाओं को व्यक्त करते हैं या उनका अपवर्तन करते हैं। उस प्रत्येक घटना को वे फ़िर से रचते हैं जिसको वे मीडिया में प्रदर्शित करते हैं। वे उन पर एक निश्चित विचारधारा के अनुसार जोर देते हैं। प्राय: ही यह सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यावसायिक विचारधाराओं के द्वारा आच्छादित हो जाती है और जो कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर समाचार की उपयोगिता, उत्तेजनात्मक चित्र, आकर्षक प्रस्तुतीकरण, गरमागरम ख़बर, आदि बातों की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जाता है। इनकोडर अपने को तटस्थता की परिधि में रखता है जिससे वह प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की विचारधारात्मक विषयवस्तु से दूर दिखायी देता है। यद्यपि घटनाओं को एक जैसे ढंग से ही प्रस्तुत नहीं किया जाता फ़िर भी विचारधारा का वह आकार बहुत सीमित होता है जिससे प्रस्तुतकर्ता प्रभावित होता है। उसकी मुख्य प्रवृत्ति यह होती है कि वह प्रमुख विचारधारा के क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखे और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य दर्शक-श्रोताओं की सहमति को जीतना या अर्जित करना होता है। पहचान के इन बिन्दुओं की सहायता से वह घटनाओं की अपनी मनपसन्द प्रस्तुतियों को विश्वसनीय और सशक्त बना देता है। हमने अन्यत्रा यह दिखाने का प्रयत्न किया है ;हाल 1974 मोरले 1974द्ध कि श्रोता-दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से उनकी भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों का बोध होता है लेकिन वे प्रतिक्रियाएँ उन्हीं विचारधारात्मक संरचनाओं के अन्तर्गत नहीं हुआ करतीं जो इन प्रस्तुतियों के मूल में होती हैं। लेकिन प्रभावी सम्प्रेषण के पीछे उद्देश्य यही होता है कि मनचाही प्रस्तुतियों के लिए श्रोता-दर्शकों की सहमति या स्वीकृति प्राप्त हो जाये।
मीडिया का न केवल सभी वर्गों में प्रसार होता है बल्कि वह सामाजिक सम्प्रेषणीयता के उद्देश्य से कार्य करता है और विचारधारा के क्षेत्र में अपनी प्रभुताबनाये रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वह न केवल अपने कार्य की वैधता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है बल्कि उस वैधता को लोकप्रियता का आधार प्रदान करता है और ‘सर्वसहमति का यह आधार ही उसे वैधता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। इस कार्य में मीडिया के विभिन्न उपकरणों की स्थिति पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जैसा कि हमने पहले बताया है, इन उपकरणों पर राज्य का प्रत्यक्ष प्रभुत्व नहीं होता लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ में परोक्ष रूप से मीडिया का सम्बन्ध शासक वर्ग और इसके गठबन्धनों से होता है और इसी दृष्टि से अलथ्यूसर ने इसे विचारधारात्मक राज्य का उपकरण कहा है। इस अर्थ में मीडिया को सापेक्ष रूप में स्वायत्तता प्राप्त है। उदाहरण के लिए प्रसारण क़ानून की तरह काम करता है और राज्य की नौकरशाही की कार्यपद्धति भी इससे मिलती जुलती है। इन सभी के ऊपर ‘शक्ति के पृथक्करण का सिद्धान्त लागू होता है। कोर्इ एक वर्ग या राजनीतिक दल मीडिया को प्रत्यक्ष रूप से आदेश नहीं दे सकता क्योंकि इस प्रकार का आदेश इसकी वैधता पर कुठाराघात होगा। इससे यह सिद्ध होगा कि मीडिया की शासक वर्ग के साथ साँठ-गाँठ है। यह निर्विवाद है कि पूँजीवादी विकास की वर्तमान स्थिति में मीडिया भी राज्य के अन्य अंगों की तरह आपेक्षिक स्वायत्तता पर निर्भर है। प्रसारण या ब्राडकासिटंग के संचालन से सम्बन्धित सिद्धान्त जैसे तटस्थता, निष्पक्षता, निगर्ुटता, ‘सन्तुलन आदि का इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जा सकता है। इन्हीं के द्वारा प्रसारण की आपेक्षिक तटस्थता को प्राप्त किया जाता है ;हाल 1972द्ध। उदाहरण के लिए सन्तुलन से यह निश्चित हो जाता है कि संवाद हमेशा दो गुणों के बीच होगा और इस प्रकार श्रोता-दर्शकों को किसी भी विषय के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी वह एकतरफ़ा नहीं होगी। राजनीतिक क्षेत्र में प्रसारण संसदीय प्रजातंत्र के सारे तौर-तरीके अपनाता है, उसकी यह चेष्टा रहती है कि वह प्रजातंत्रात्मक विवाद प्रस्तुत करे। इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि मीडिया का कार्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह बहस में किसी एक पक्ष के समर्थन के लिए विषय वस्तु में तोड़-मरोड़ करे। उसकी सार्थकता तो इस बात में है कि वह बहस के किसी भी मुददे पर विरोधी मतों को निष्पक्षता से प्रस्तुत करे।
यह एक सुविदित तथ्य है कि विभिन्न राजनीतिक दल नीतिगत मामलों के किन्हीं पहलुओं पर एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं लेकिन प्रश्नों पर एकता के महत्वपूर्ण बिन्दु दिखायी पड़ते हैं। इस अन्तर्निहित एकता को ही मीडिया पुनरुत्पादित करने का प्रयास करता है, उसकी नीति तरफ़दारी की नहीं होती बल्कि राज्य के ‘यथार्थ की वास्तविक परिधि के अन्तर्गत होती है। सर्वसहमति का निर्माण करना निश्चित रूप से एक जटिल कार्य है और इस कार्य को सम्पादित करना ही मीडिया का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्रापित के लिए उसे कुछ व्याख्याओं को शामिल करना पड़ता है और कुछ को खारिज। शामिल की जाने वाली व्याख्याओं में ऐसी होती हैं जो कुल मिलाकर विवादरहित होती हैं। इसके विपरीत जिन व्याख्याओं में कुछ विवाद होता है उन्हें खारिज कर दिया जाता है। खारिज की जाने वाली व्याख्याओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार के हैं, ‘अतिवादी, ‘अविचारपूर्ण, ‘निरर्थक, ‘काल्पनिक, ‘अव्यावहारिक, आदि (देखें, हाल, दि स्ट्रक्चरिंग आपफ टापिक्स, 1975 और भी देखें करटी कारनेल और हाल 1976)।
हमें अपने आपको कुछ खास प्रक्रियाओं और विधियों तक ही सीमित रखना पड़ा है ताकि हम अपने प्रस्तावित प्रस्तावों और सुझावों का औचित्य सिद्ध कर सकें। अपने प्रतिपादित विषय को हम एक सरल ढंग से रख सकते हैं और हमारे निष्कर्ष का आधार वह सैद्धान्तिक विवेचन और विश्लेषण होगा जो हमने प्रस्तुत निबन्ध में किया है। हमारे जैसे समाजों में मीडिया का काम प्रमुख विचारधाराओं के ढाँचे में वर्गीकरण का समीक्षात्मक काम लगातार करते रहना है। यह कार्य न तो बहुत सरल है और न ही बहुत सचेतन बल्कि कहना चाहिए कि यह परस्पर विरोधी कार्य है। परस्पर विरोधी इसलिए कि जिन विभिन्न विचारधाराओं से प्रमुख क्षेत्र निर्मित होता है उनमें सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य होता है। इन विचारधाराओं में वर्ग व्यवहारों के अन्तर्गत परस्पर संघर्ष होता रहता है और इन संघर्षों का विवेचन बिना उनके अन्तरविरोधों का उल्लेख किये बग़ैर नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारधारात्मक पुनरुत्पादन का जो कार्य मीडिया को करना होता है उसमें विभिन्न प्रवृत्तियों का घात-प्रतिघात होता है। ग्राम्शी के शब्दों में यह ‘स्थायित्वरहित सन्तुलन है जो इसमें प्रदर्शित होता है। हम इसी कारण से मीडिया की प्रवृत्ति के बारे में ही कह सकते हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति इसका मुख्य तत्व है न कि इसका आनुषंगिक रूप-समाज के विचारात्मक क्षेत्र को इस तरह से प्रस्तुत करना कि इसके प्रभुत्व की संरचना व्यक्त हो जाये।
सन्दर्भ ग्रन्थ
अलथ्यूसर, एल. (1965), फ़ार मार्क्स, न्यू लेफ्ट बुक्स, (1971) ‘आइडियोलाजी एंड द स्टेट इन लेनिन एंड फ़िलासपफी एंड अदर एसेज़, न्यू लेफ्ट बुक्स।
बाथ्र्स, आर., (1967), एलीमेंटस आपफ सीमाइनोलाजी कैप।
बाटमोर, टी. एंड रूबेल एम. (1963), कार्ल मार्क्स सेलेक्टेड राइटिंग्स इन सोशियोलाजी एंड सोशल फ़िलासफी, पेंग्विन।
कोनेल, आर्इ.कुटी, एल.एंड एस.
अनुवाद: ओमप्रकाश मालवीय
(ग्रंथशिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित ‘संचार माध्यम और पूँजीवादी समाज, सम्पादक : मुरली मनोहर प्रसाद सिंह से साभार)
- नान्दीपाठ-2, जुलाई-सितम्बर 2013