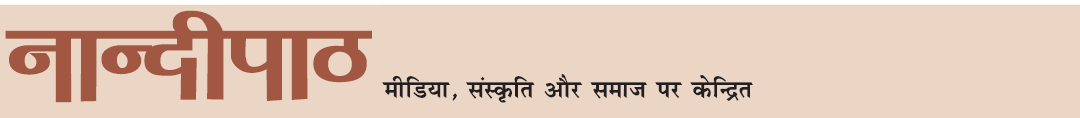आइज़ेंस्ताइन का फ़िल्म–सिद्धान्त और रचनात्मक प्रयोग
अनादि चरण
सामाजिक जीवन के यथार्थ के सौन्दर्यात्मक–कलात्मक संज्ञान की समस्याओं पर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि से चिन्तन तथा परस्पर–विरोधी अवस्थितियों के बीच टकरावों का सिलसिला पिछली पूरी शताब्दी के दौरान लगातार चलता रहा। मार्क्स और एंगेल्स के दिशा–संकेतक सूत्रों पर काफ़ी कुछ लेखन और विमर्श हुआ है। प्लेखानोव, लुनाचार्स्की, गोर्की, वोरोव्स्की, वोरोन्स्की, राल्फ फॉक्स, कॉडवेल आदि की क्लासिकी मार्क्सवादी स्थापनाओं–भाष्यों से लेकर ब्रेष्ट–लूकाच विवाद, ब्रेष्ट के द्वन्द्वात्मक थिएटर और वाल्टर बेंजामिन के कला–चिन्तन और नववामपन्थी चिन्तन की विभिन्न धाराओं–उपधाराओं तक के बारे में बहुत–कुछ लिखा–पढ़ा जाता रहा है। इस पूरे चिन्तन और विमर्श के परिमाण और गुणवत्ता पर कोई निर्णय देना या सन्तोष प्रकट करना यहाँ हमारा मन्तव्य नहीं है। हम सिर्फ़ यह कहना चाहते हैं कि इन सबकी तुलना में सेर्गेई मिखाइलोविच आइज़ेंस्ताइन (1898–1948) के कला–विषयक सैद्धान्तिक चिन्तन पर बहुत ही कम काम हुआ है।
आइज़ेंस्ताइन को महानतम फ़िल्मकारों में से एक तो सिनेमा के सभी अध्येता, सर्जक और आलोचक मानते हैं। उनकी फ़िल्म ‘बैटलशिप पोतेमकिन’ की गणना भी निर्विवाद रूप से दुनिया की अब तक की सर्वश्रेष्ठ, कालजयी फ़िल्मों में की जाती है। बुर्जुआ फ़िल्मकार और विशेषज्ञ यदि उनके चिन्तन या प्रयोग–पक्ष की चर्चा करते भी हैं तो ख़ासकर मोन्ताज के मौलिक प्रयोग के सन्दर्भ में ही करते हैं और उसे भी, सैद्धान्तिक पक्षों की अनदेखी करते हुए महज़ शिल्प–चर्चा तक सीमित कर देते हैं। बहुतेरे पश्चिमी सिनेमा–विशेषज्ञ आइज़ेंस्ताइन के प्रयोगों और चिन्तन की या तो अनदेखी करते हुए, या फिर अनर्थकारी व्याख्या करते हुए उन्हें एक ऐसे त्रासदी–नायक के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं जो जीवनपर्यन्त “कलाकार बनाम मार्क्सवादी” के उत्कट आन्तरिक तनाव का शिकार बना रहा। बुर्जुआ कलाविदों ने उनके सिनेमा के तकनीकी पहलुओं पर ख़ूब लिखा है तथा उनके सिद्धान्तों की एकांगी और मनमानी व्याख्याएँ ख़ूब की हैं। दूसरी ओर, उनके आधारभूत महत्त्व के सैद्धान्तिक अवदानों पर भी, वामपन्थी दायरे में बहुत कम चिन्तन और चर्चा हुई है।
 फिर भी, यह तथ्य तो आज स्थापित हो ही चुका है कि आइज़ेंस्ताइन सर्वहारा सिनेमा के एक महानतम सिद्धान्तकार और प्रयोगकर्ता थे। लेकिन सच सिर्फ़ इतना ही नहीं है। सच तो यह है कि कलात्मक सृजन के वैचारिक तथा ज्ञान मीमांसीय तथा सौन्दर्यात्मक पहलुओं पर, सामाजिक यथार्थ के कलात्मक संज्ञान और कलात्मक पुनसृजन के प्रश्न पर, तथा, कला की सामाजिक भूमिका के प्रश्न पर आइजे़स्ताइन का मौलिक चिन्तन कला की मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी को और सौन्दर्यशास्त्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाला है। एक विडम्बना यह भी है कि आइज़ेंस्ताइन का जो लेखन वक्तव्यों, डायरियों, पत्रों, लेखों के संकलनों और पुस्तकाकार प्रबन्धों के रूप में हमारे सामने मौजूद है, वह, बहुत अधिक लगने के बावजूद, उनके सम्पूर्ण कृतित्व का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। मास्को स्थित ‘आइज़ेंस्ताइन आर्काइव्स’ की इमारत आइज़ेंस्ताइन की डायरियों, नोट्स, प्राइवेट पेपर्स और अप्रकाशित पाण्डुलिपियों से अँटी पड़ी आज भी खड़ी है। पर आज के रूस में भला किसका ध्यान इस बहुमूल्य सम्पदा की ओर जाएगा। आइज़ेंस्ताइन की विडम्बना यह रही कि सोवियत संघ में, तीस और चालीस के दशक में कला–साहित्य–संस्कृति के क्षेत्र में यांत्रिक भौतिकवादी चिन्तन की प्रभाविता, तथा एक हद तक, सांस्कृतिक क्षेत्र में नौकरशाही की जकड़बन्दी के चलते पथान्वेषी प्रयोगों के लिए दमघोंटू माहौल था। इस माहौल में आइज़ेंस्ताइन को एकाधिक बार रूपवादी भटकाव और इतिहास की दुर्व्याख्या के आरोपों का शिकार होना पड़ा। सिनेमा में द्वन्द्ववादी पद्धति को अमल में लाने से सम्बन्धित उनके प्रयोगों पर न खुलकर विचार–विमर्श हुआ, न ही बहसें चलीं। और फिर ख्रुश्चेव–ब्रेझनेव काल आया। नई संशोधनवादी सत्ता को वर्ग–संघर्ष के उत्कट पक्षधर आइज़ेंस्ताइन के विचार भला कैसे रास आ सकते थे? सो इस दौर में आइज़ेंस्ताइन की देव–प्रतिमाएँ तो ख़ूब गढ़ी गर्इं, लेकिन उनके सैद्धान्तिक अवदानों की भरपूर अनदेखी की गई। ‘आइज़ेंस्ताइन आर्काइव्स’ के गेट पर गार्ड पहरा देते रहे और अध्येताओं का वहाँ प्रवेश वर्जित रहा।
फिर भी, यह तथ्य तो आज स्थापित हो ही चुका है कि आइज़ेंस्ताइन सर्वहारा सिनेमा के एक महानतम सिद्धान्तकार और प्रयोगकर्ता थे। लेकिन सच सिर्फ़ इतना ही नहीं है। सच तो यह है कि कलात्मक सृजन के वैचारिक तथा ज्ञान मीमांसीय तथा सौन्दर्यात्मक पहलुओं पर, सामाजिक यथार्थ के कलात्मक संज्ञान और कलात्मक पुनसृजन के प्रश्न पर, तथा, कला की सामाजिक भूमिका के प्रश्न पर आइजे़स्ताइन का मौलिक चिन्तन कला की मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी को और सौन्दर्यशास्त्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाला है। एक विडम्बना यह भी है कि आइज़ेंस्ताइन का जो लेखन वक्तव्यों, डायरियों, पत्रों, लेखों के संकलनों और पुस्तकाकार प्रबन्धों के रूप में हमारे सामने मौजूद है, वह, बहुत अधिक लगने के बावजूद, उनके सम्पूर्ण कृतित्व का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। मास्को स्थित ‘आइज़ेंस्ताइन आर्काइव्स’ की इमारत आइज़ेंस्ताइन की डायरियों, नोट्स, प्राइवेट पेपर्स और अप्रकाशित पाण्डुलिपियों से अँटी पड़ी आज भी खड़ी है। पर आज के रूस में भला किसका ध्यान इस बहुमूल्य सम्पदा की ओर जाएगा। आइज़ेंस्ताइन की विडम्बना यह रही कि सोवियत संघ में, तीस और चालीस के दशक में कला–साहित्य–संस्कृति के क्षेत्र में यांत्रिक भौतिकवादी चिन्तन की प्रभाविता, तथा एक हद तक, सांस्कृतिक क्षेत्र में नौकरशाही की जकड़बन्दी के चलते पथान्वेषी प्रयोगों के लिए दमघोंटू माहौल था। इस माहौल में आइज़ेंस्ताइन को एकाधिक बार रूपवादी भटकाव और इतिहास की दुर्व्याख्या के आरोपों का शिकार होना पड़ा। सिनेमा में द्वन्द्ववादी पद्धति को अमल में लाने से सम्बन्धित उनके प्रयोगों पर न खुलकर विचार–विमर्श हुआ, न ही बहसें चलीं। और फिर ख्रुश्चेव–ब्रेझनेव काल आया। नई संशोधनवादी सत्ता को वर्ग–संघर्ष के उत्कट पक्षधर आइज़ेंस्ताइन के विचार भला कैसे रास आ सकते थे? सो इस दौर में आइज़ेंस्ताइन की देव–प्रतिमाएँ तो ख़ूब गढ़ी गर्इं, लेकिन उनके सैद्धान्तिक अवदानों की भरपूर अनदेखी की गई। ‘आइज़ेंस्ताइन आर्काइव्स’ के गेट पर गार्ड पहरा देते रहे और अध्येताओं का वहाँ प्रवेश वर्जित रहा।
पचास वर्ष की छोटी–सी उम्र का आधा से भी अधिक हिस्सा आइज़ेंस्ताइन ने सिनेमा को दिया। उनकी महज़ छह फ़िल्में ही पूरी होकर प्रदर्शित हो सकीं। अधिकांश परियोजनाएँ अधूरी रह गर्इं। कुछ फ़िल्में तो 80–90 प्रतिशत तक बनने के बाद डिब्बाबन्द हो गर्इं। फिर भी वे एक फ़िल्मकार के साथ–साथ सिनेमा के एक चिन्तक–लेखक और शिक्षक के रूप में अनथक–अविराम काम करते रहे, तब तक, जब तक कि उनके दिल ने हमेशा के लिए धड़कना बन्द नहीं कर दिया। आइज़ेंस्ताइन का कृतित्व उस सांस्कृतिक नवजागरण के सर्जनात्मक ज्वार का शीर्ष–बिन्दु था जो बोल्शेविक क्रान्ति के बाद ऊपर उठा था, और विशेष तौर पर, तीसरे दशक के अन्त तक आलोड़ित होता रहा था। आइज़ेंस्ताइन के वैचारिक अवदानों की-आम तौर पर सर्वहारा कला, और ख़ास तौर पर सिनेमा विषयक सभी मूलभूत प्रस्थापनाओं की एक लेख में चर्चा सम्भव ही नहीं है। हम इस लेख में मुख्यत: इसी चर्चा तक सीमित रहेंगे कि चिन्तन और प्रयोग के क्षेत्र में आइज़ेंस्ताइन की मुख्य चिन्ताएँ और मुख्य सरोकार क्या थे, जीवनपर्यन्त जारी उनकी कलात्मक अन्वेषण–यात्रा के लक्ष्य क्या थे और दिशादर्शी सूत्र क्या थे तथा, उनकी वे कौन सी. मूलभूत और मौलिक स्थापनाएँ हैं जो सर्वहारा कला की सैद्धान्तिकी को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाती हैं और जिन पर सोचना हमारे लिए आगे जाने में विशेष तौर पर मददगार साबित हो सकता है?
सिनेमा की शक्ति और सम्भावनाओं की पड़ताल करती एक वैज्ञानिक इतिहास–दृष्टि
सेर्गेई आइज़ेंस्ताइन एक अकुण्ठ भौतिकवादी थे। उनका सिनेमा वर्ग–संघर्ष का सिनेमा था। अपनी भौतिकवादी विश्व–दृष्टि पर अविचल रहते हुए वे जिस प्रश्न से जीवनपर्यन्त जूझते–टकराते रहे, वह था-वस्तुगत यथार्थ के कलात्मक–सौन्दर्यात्मक संज्ञान और कलात्मक पुनर्सृजन में द्वन्द्ववादी पद्धति का प्रयोग। एक सच्चे दार्शनिक कलाकार की भाँति, हेगेल तथा कार्ल मार्क्स और लेनिन के निष्ठावान शिष्य की भाँति, आइज़ेंस्ताइन ने पद्धति के प्रश्न को हल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
सर्वहारा क्रान्ति के सन्देश को अधिकतम सम्भव प्रभावी ढंग से जन–जन तक पहुँचाने में और एक नई, श्रम–संस्कृति के निर्माण में सिनेमा की सर्वाधिक प्रभावी भूमिका को सुसंगत वैज्ञानिक आधार पर समझने की कोशिश करने वालों में आइज़ेंस्ताइन की भूमिका सर्वोपरि थी। ऐसे समवेत प्रयासों में उनके शिक्षक और वरिष्ठ साथी लेव कुलेशोव के साथ ही पुदोवकिन, दोवझेंको और वेर्तोव की भूमिका भी, निस्सन्देह, महत्त्वपूर्ण थी।
बीसवीं शताब्दी की राजनीतिक हस्तियों में लेनिन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रभावी सांस्कृतिक माध्यम के रूप से सिनेमा की महत्ता को पहचाना और बताया कि “सभी कलाओं में सिनेमा हमारे लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।“ (मार्टिन मेलर : ‘सक्सेस ऐण्ड फेल्योर ऑफ दि सोवियत सिनेमा’, ‘मार्क्सिस्ट’, वॉल्यूम–6, नं.–1, 1967, पृ. 4)। आइज़ेंस्ताइन ने इस महत्ता को पहले व्यावहारिक धरातल पर समझा और फिर सैद्धान्तिक धरातल पर। बोल्शेविक क्रान्ति ने उनके लिए तथा पुदोवकिन, दोवझेंको, तिस्से, वेर्तोव जैसे सोवियत सिनेमा की दर्ज़नों भावी हस्तियों के लिए पहली व्यावहारिक पाठशाला का काम किया। ये सभी उस समय सत्रह–अठारह साल के युवा थे जो लाल सेना के आन्दोलनात्मक प्रचार के मोर्चे पर काम कर रहे थे। मोर्चों पर न्यूज़रील की शूटिंग करते हुए और फिर इतिहास–चर्चित “एजिट–ट्रेनों” और “एजिट–स्टीमरों” में सोवियत संघ के सुदूर प्रान्तीय क्षेत्रों तक यात्रा करके थिएटर और न्यूज़रीलों के प्रदर्शन के द्वारा किसानों–मज़दूरों–सैनिकों में प्रचार करते हुए आइज़ेंस्ताइन और उनके युवा साथियों ने सिनेमा की शक्ति और प्रभाव को प्रत्यक्षत: महसूस किया।
आगे चलकर, सिनेमा की कलात्मक शक्ति के ऐतिहासिक–सामाजिक उत्सों की सैद्धान्तिक व्याख्या करते हुए आइज़ेंस्ताइन ने यह स्पष्ट किया कि वर्ग समाज के इतिहास की सर्वोन्नत मंज़िल के तौर पर, पूँजीवादी समाज में उत्पादक शक्तियों का जो अभूतपूर्व (वैज्ञानिक–तकनीकी और सांस्कृतिक–आत्मिक-दोनों ही रूपों में) विकास हुआ, उसी की एक तार्किक परिणति के रूप में सिनेमा का जन्म हुआ। ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो–टेक्नीक, फोटो–टेक्नीक आदि के क्षेत्र में, और दृष्टि की फ़िज़ियोलॉजी सम्बन्धी (जैसे एक सेकेण्ड के दसवें हिस्से तक चाक्षुष प्रभावों को संरक्षित रखने की रेटिना की क्षमता की जानकारी) नई खोजों के बग़ैर सिनेमा का विकास सम्भव नहीं था। साथ ही, पूँजीवादी उत्पादन–प्रणाली में सामूहिक उत्पादकता और सामूहिक सर्जनात्मकता की जो अनिवार्य बुनियादी भूमिका थी, उसने भी सिनेमा के उद्भव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि सिनेमा हर हाल में सामूहिक सर्जनात्मक उपक्रमों और श्रम का ही फल होता है। यह एक ऐसी कला है जिसकी उत्पादन–प्रक्रिया, उद्योगों की उत्पादन–प्रक्रिया जैसी होती है। पूँजीवादी समाज की सामाजिक आवश्यकताओं, जनान्दोलनों की व्यापक सम्भावनाओं, जीवन की गति में आई तेज़ी, विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच तथा उनके भागीदारों के बीच अन्तर्निर्भरता के व्यापक विस्तार और इतिहास–निर्माण में विशाल आम आबादी की सचेतन भूमिका ने सिनेमा के उद्भव के बुनियादी कारक उपादान की भूमिका निभाई। जिस प्रकार ‘असेम्बली–लाइन उत्पादन’ ने सर्वहारा वर्ग को संगठित होने की चेतना देने में भौतिक आधार का काम किया, उसी प्रकार सिनेमा की सामूहिक निर्माण–प्रक्रिया ने इसे वह अभिलाक्षणिक विशिष्टता प्रदान की कि यह सभी पूर्ववर्ती कलाओं का संश्लेषण करके सर्वहारा–संस्कृति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम बन सके। साथ ही, आइज़ेंस्ताइन ने यह भी स्पष्ट किया कि सिनेमा एक ओर यदि सभी पूर्ववर्ती कलाओं को संगठित–समेकित कर लेता है, तो दूसरी ओर, एक उच्चतर धरातल पर यह उनका निषेध भी है।
इसी आधार पर आइज़ेंस्ताइन का मानना था कि सर्वहारा कला का सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वोन्नत माध्यम सिनेमा है। पूँजीवाद अपने हित में इसका प्रभावी इस्तेमाल करता है, लेकिन पूँजीवादी सिनेमा अपने अनिवार्य अन्तरविरोधों से मुक्त नहीं हो सकता। व्यापक ऐतिहासिक अर्थ–सन्दर्भों में सिनेमा सर्वहारा वर्ग की कला है। सर्वहारा वर्ग ही इसकी समस्त सर्जनात्मक सम्भावनाओं को उजागर कर सकता है और उनको पूरे समाज के हित में निर्देशित कर सकता है। जीवन और चिन्तन के द्वन्द्वों को कलात्मक अभिव्यक्ति देने में सिनेमा सर्वाधिक सक्षम माध्यम है और उन्हें सचेतन तौर पर हल करने में, एक सांस्कृतिक उपकरण के तौर पर इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावी होगी।
सामाजिक–आर्थिक विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए सिनेमा के महत्त्व–प्रतिपादन के बाद, आइज़ेंस्ताइन ने एक बहुमूल्य और महत्त्वपूर्ण स्थापना यह दी कि सामाजिक श्रम–विभाजन की एक लम्बी प्रक्रिया की परिणति के तौर पर वैचारिक अमूर्त चिन्तन के गुरुत्व, और भावनाओं की आवेगात्मकता के बीच जो अलगाव विकसित हुआ है, उसे समाजवादी सामाजिक–आर्थिक संरचना के भौतिक आधार पर होने वाला, सर्वहारा कला का विकास ही दूर कर सकेगा और एकमात्र फ़िल्म–विधा ही सर्वोन्नत कला–माध्यम के रूप में, इस महासंश्लेषण में सक्षम है। आगे हम विस्तार में जाते हुए, इस महत्त्वपूर्ण स्थापना को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले ज़रूरी है कि हम मोन्ताज की उस द्वन्द्वात्मक अवधारणा पर विचार कर लें जो आइज़ेंस्ताइन का सर्वाधिक चर्चित अवदान माना जाता है और जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग में भी लागू किया।
मोन्ताज की उद्भावनापरक (ideational) द्वन्द्वात्मक अवधारणा
आइज़ेंस्ताइन ने मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद और अवबोधन (Perception) के मनोविज्ञान के आधार पर मोन्ताज का आधुनिक सिद्धान्त विकसित किया। इसकी चर्चा से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि मोन्ताज होता क्या है। मोन्ताज फ्रांसीसी शब्द ‘मोन्तेर’ (Monter) से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या ‘असेम्बल’ करना। सामान्यत: मोन्ताज का मतलब होता है-सम्पादन या अलग–अलग शॉट्स को काटकर और जोड़कर एक सुनिश्चित प्रभाव उत्पन्न करने वाला, या विचारों के अन्तर्सम्बन्धों को उद्घाटित करने वाला, या कथाक्रम को आगे बढ़ाने वाला फ़िल्म–सीक्वेंस तैयार करना। मोन्ताज की तकनीक का प्रारम्भिक विकास हमें अमेरिकी निर्देशकों एडविन पोर्टर (1870–1941) और डी.डब्ल्यू. ग्रिफिथ (1875–1948) की फ़िल्मों में देखने को मिलता है। लेकिन इसका विधिवत विकास आगे चलकर, सोवियत संघ में कुलेशोव, आइज़ेंस्ताइन और पुदोवकिन ने किया और फिर इस तकनीक को इनसे पूरी दुनिया के फ़िल्मकारों ने अलग–अलग ढंग से अपनाया और इस्तेमाल किया।
कुलेशोव पहली पीढ़ी के सुप्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक तो थे ही, लेकिन सबसे पहले, वे फ़िल्म–कला के एक महान शिक्षक थे। ‘कुलेशोव वर्कशाप’ में वे अपने छात्रों को ग्रिफिथ की फ़िल्म ‘इन्टोलरेन्स’ इतनी बार दिखलाते थे कि उसके शॉट स्ट्रक्चर्स उन्हें याद हो जाते थे और फिर कुलेशोव बहुसंस्तरीय एडीटिंग सीक्वेंसेज़ को छात्रों से सैकड़ों अलग–अलग संयोजनों में पुनर्व्यवस्थित करने को कहते थे। कुलेशोव का अगला प्रयोग और अधिक दिलचस्प था। उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता के अभिव्यक्तिहीन चेहरे के शॉट को तीन अलग–अलग, अत्यधिक अभिव्यक्तिपूर्ण शॉट्स के साथ काटकर चस्पां कर दिया-एक गर्म, भाप छोड़ते शोरबे के कटोरे के साथ, फिर ताबूत में पड़े एक स्त्री के शव के साथ, और फिर गुड़िया से खेलती एक बच्ची के साथ। दर्शकों को तीनों ‘सीक्वेंसेज़’ में अभिनेता के चेहरे पर तीन भाव दीखे-शोरबे के लिए भूख का भाव, मृत स्त्री के लिए दुख का भाव और छोटी बच्ची के लिए पितृत्वपूर्ण प्यार का भाव। इस परिघटना की, जिसे आज “कुलेशोव इफ़ेक्ट” नाम से जाना जाता है, कुलेशोव ने व्याख्या करते हुए बताया कि फ़िल्म में हर शॉट के दो मूल्य होते हैं : एक यह कि वह अपने आप में यथार्थ का फोटोग्राफ़िक बिम्ब होता है, और दूसरा मूल्य वह शॉट किसी अन्य शॉट के सानिध्य में रखे जाने पर ग्रहण कर लेता है। कुलेशोव का कहना था कि सिनेमाई महत्ता की दृष्टि से दूसरा मूल्य पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है और इसलिए, सिनेमा में दिक् और काल को सम्पादन की प्रक्रिया या मोन्ताज के मातहत होना चाहिए। इस तरह पहली बार कुलेशोव ने मोन्ताज की प्रक्रिया की एक सैद्धान्तिकी प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह एक ऐसी अभिव्यंजक प्रक्रिया होती है जहाँ असमरूपी बिम्ब परस्पर जुड़कर अनभिधात्मक या प्रतीकात्मक अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। कुलेशोव की इस अवधारणा ने उनके दो सबसे मेधावी शिष्यों को सर्वाधिक प्रभावित किया। वे थे, आइज़ेंस्ताइन और पुदोवकिन। मोन्ताज के बारे में दोनों का अवधारणात्मक चिन्तन दो दिशाओं में विकसित हुआ और कालान्तर में दोनों परस्पर–विरोधी अवस्थितियों पर जा खड़े हुए।
मोन्ताज को सामान्यत: तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : ग्राफ़िक, वर्णनात्मक (narative) और उद्भावनापरक (ideational)। वर्णनात्मक मोन्ताज में, एक अकेले विषय से जुड़े हुए, अलग–अलग स्थितिबिन्दु वाले नानाविध दृश्य और बिम्ब संयोजित किए जाते हैं। जैसे, कथाचित्रों में, किसी चरित्र या लोकेशन को कई कोणों से एक्सप्लोर किया जाता है ताकि दर्शक स्थिति–विशेष का सांगोपांग बिम्ब निर्मित कर ले। ग्राफ़िक मोन्ताज में शॉट्स को उनकी विषय–वस्तु के अनुसार नहीं बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप अथवा प्राकृतिक प्रकटन के चलते जक्स्टापोज़ किया जाता है, एक–दूसरे के साथ रखा जाता है। कुछ अवाँगार्द सिने–कृतियों में प्राय: केन्द्रीय प्रश्न यह बन जाता है कि लोगों, वस्तुओं और विविध आकृतियों आदि के विविध बिम्बों के बीच के ग्राफ़िक सम्बन्धों को दर्शक जोड़ पाते हैं अथवा नहीं। ग्राफ़िक मोन्ताज में, स्थिर स्थिति के बजाय प्राय: गति के शॉट्स के दौरान कटिंग की जाती है। इससे एक बिम्ब द्वारा दूसरे का विस्थापन सुगम हो जाता है। उद्भावनापरक मोन्ताज में दो अलग–अलग बिम्ब जुड़कर एक तीसरी चीज़ तक पहुँच जाते हैं, एक विचार तक, जिसके प्रादुर्भाव में वे सहायता करते हैं और जिसके द्वारा वे नियंत्रित–निर्देशित होते हैं।
मोन्ताज की ये तीनों श्रेणियाँ अपने शुद्ध रूप में कम ही आती हैं। जैसे, उद्भावनापरक मोन्ताज अपने संघटकों की ग्राफ़िक समरूपता के आधार से प्रस्थान करता है। इसी तरह वर्णनात्मक मोन्ताज अपने मूवमेण्ट का विवरण प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ़िक कटिंग पर निर्भर रहता है। ठीक इसी तरह, विभिन्न चीज़ों का ग्राफ़िक सहमेल एक सुनिश्चित घटना (परिणति) की दिशा में गति के विचार का निर्माण करता है। साउण्डट्रैक के आगमन ने मोन्ताज की सम्भावनाओं–प्रभावों को कई गुना बढ़ा दिया। आइज़ेंस्ताइन और पुदोवकिन ने शॉट–दर–शॉट कथा या विचार के खुलते जाने की “क्षैतिज़” (horizontal) प्रक्रिया के बरक्स “उदग्र” (vertical) मोन्ताज की सम्भावनाओं का भी हवाला दिया है। इसका आधार यह था कि ध्वनि, हर क्षण जो सुना और देखा जा रहा है, उनके बीच सम्बन्ध–स्थापन सम्भव बना देती है। सिनेमा में ध्वनि के प्रवेश के बाद फ़िल्म–बिम्ब को स्वत:स्फूर्त स्वायत्त इकाई नहीं माना जा सकता था, यह अपनी अनुवर्ती ध्वनि के साथ अन्तर्क्रिया करती थी। संवाद, संगीत, परिवेशी शोर और श्रव्य–प्रभावों के रूप में ध्वनि–सम्बन्ध इमेज–ट्रैक के सतत सहसम्बन्ध में निर्मित किए जा सकते हैं, या ये एक समान्तर संघटन और अभिकल्प (design) की रचना कर सकते हैं जो दिखाए जा रहे दृश्य को कक्षान्तरित करने का काम करे। कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि मोन्ताज एक ऐसे असाधारण उपादान के रूप में सामने आया जो अन्य कलाओं से चलचित्र को सर्वाधिक मूलभूत और गुणात्मक रूप से पृथक्कृत करता था। या यूँ कहें कि इसकी भूमिका सिने–माध्यम के आधार की बन गई। हालाँकि यह भी सच है कि कुछ फ़िल्मकारों ने अपने कथ्य को उसकी पूरी शक्ति और सौन्दर्य के साथ सम्प्रेषित करने में मोन्ताज के बजाय सिनेमा की अन्य अभिलाक्षणिकताओं का-जैसे कि इसकी प्रदीप्तता का, गतिमानता का और यथार्थ–प्रस्तुति की क्षमता का सहारा लिया। इनमें मिज़ोगुची केंजी (जापान) रॉबर्तो रोस्सेलिनी (इटली) और मिकलोस जांक्सो (हंगरी) जैसे फ़िल्मकार अग्रणी थे। बहरहाल, हम अपनी मूल चर्चा पर वापस लौटें।
मोन्ताज की उपरोक्त सारी सम्भावनाओं–क्षमताओं को समझने और उजागर करने में आइज़ेंस्ताइन की भूमिका इतनी अधिक थी कि आज बहुधा उन्हें इसके जनक के रूप में याद किया जाता है। दूसरे नम्बर पर यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह बेशक पुदोवकिन ही थे। लेकिन आइज़ेंस्ताइन और पुदोवकिन के बीच मोन्ताज को लेकर कई मूलभूत कोटि के अवधारणात्मक–सैद्धान्तिक मतभेद थे।
सबसे बुनियादी फ़र्क़ यह था कि आइज़ेंस्ताइन का मोन्ताज का सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक संघात या टकराव (conflict or collision) पर आधारित था, जबकि पुदोवकिन का सिद्धान्त संज्ञानात्मक सहयोजन या सहलग्नता (cognitive linkages) पर आधारित था। आइज़ेंस्ताइन की द्वन्द्वात्मक दृष्टि न तो यथार्थ को और न ही उसके कलात्मक पुनर्सृजन को एकाश्मी रूप में देखती थी, इसलिए वह मोन्ताज को कला में विरुद्धों की एकता और संघर्ष (unity and conflict of opposition) के रूप में देखते थे। मोन्ताज उनके लिए प्रतीति को भेदकर यथार्थ के सार तक पहुँचने की एक पद्धति थी, न कि महज़ एक फॉर्म या तकनीक। मोन्ताज के नये इस्तेमाल के द्वारा आइज़ेंस्ताइन ने फ़िल्म ‘कंस्ट्रक्ट’ करने की उस परम्परागत पद्धति पर हमला बोल दिया, जिसके द्वारा सीक्वेंसेज़ को शान्त–निर्विघ्न ढंग से सहसम्बन्धित किया जाता था। इस मायने में पुदोवकिन की पद्धति पुरानी पद्धति का विकसित रूप थी जहाँ भौतिकवादी दृष्टि तो थी लेकिन पद्धति द्वन्द्ववादी नहीं थी। अधिभूतवादी विचलन पुदोवकिन के यथार्थवाद को प्रत्यक्षवादी विचलन तक लेकर चला जाता था और आलोचनात्मक यथार्थवाद की विवरणात्मक पद्धति से निर्णायक विच्छेद न होने के चलते, समाजवादी समाज के यथार्थ के चित्रण में वह “नवनिर्मित नायक़” द्वारा पुराने नायक को विस्थापित करने तक चला जाता था और समाजवाद के अन्तरविरोधों की अनदेखी की प्रवृत्ति भी उसमें लगातार दिखाई देती थी। चौथे–पाँचवें दशक में जब सोवियत संघ में कला–साहित्य–संस्कृति के क्षेत्र में भी यांत्रिक भौतिकवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था तो पुदोवकिन को विशेष तरजीह मिली (हालाँकि एक बार उन पर भी रूपवाद का आरोप लगा था), जबकि आइज़ेंस्ताइन को शुम्यात्स्की से लेकर ज़्दानोव तक की कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
पुदोवकिन के साथ अपने विकट मतभेदों की आइज़ेंस्ताइन ने एक जगह बड़े ही दिलचस्प ढंग से चर्चा की है। उन्होंने लिखा है :
“मेरे सामने एक मुड़ा–तुड़ा पीला काग़ज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस पर एक रहस्यपूर्ण टिप्पणी अंकित है : “लिंकेज–पी” और “कॉलिज़न-ई”
यह मोन्ताज के विषय पर पी (पुदोवकिन) और ई. (मैं स्वयं) के बीच सरगर्म ज़ोर–आज़माइश का पर्याप्त संकेत है।” (आइज़ेंस्ताइन : ‘फ़िल्म फॉर्म’, मेरिडियन बुक्स, 1957, पृ. 37)
पुदोवकिन भी दर्शक के दिमाग़ में ‘कैरी–ओवर” की महत्ता पर बल देते थे, लेकिन उनका कहना था कि वस्तु–विशेष को किसी संश्लेषण के अंग के रूप में प्रस्तुत करने पर ही वह “फ़िल्मी जीवन से समृद्ध हो पाती है” या यूँ कहें कि उसका सिने–कलात्मक पुनर्सृजन हो पाता है। पुदोवकिन का कहना था कि “फ़िल्म को शूट नहीं किया जाता बल्कि सेल्युलायड की अलग–अलग पट्टियों से इसका निर्माण किया जाता है, वे (पट्टियाँ) इसका कच्चा माल होती हैं।” पुदोवकिन ने मोन्ताज का प्रतीकात्मक इस्तेमाल करने की जगह ग्रिफिथ की ही भाँति मोन्ताज का वर्णनात्मक प्रयोग किया। पुदोवकिन की फ़िल्मों में आइज़ेंस्ताइन की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक पक्ष, अन्तर्जगत का पक्ष अधिक प्रबल है। सामाजिक संघर्षों के घटना–प्रवाह का जो “एपिक ड्रामा” आइज़ेंस्ताइन की फ़िल्मों का फ़ोकस है, वह पुदोवकिन की फ़िल्मों में मानवीय भावनाओं की अन्योन्यक्रिया के लिए महज़ पृष्ठभूमि का काम करता है।
हम यूँ कह सकते हैं कि मोन्ताज की इन दो परस्पर–विरोधी अवधारणाओं में आइज़ेंस्ताइन का ज़ोर ‘थीसिस–एण्टीथीसिस’ पर था जबकि पुदोवकिन का ज़ोर ‘सिन्थेसिस’ पर था। आइज़ेंस्ताइन का ज़ोर विरुद्धों के संघर्ष पर था जबकि पुदोवकिन का ज़ोर उनकी एकता पर। गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये द्वन्द्ववाद के प्रश्न पर दो परस्पर–विरोधी अवस्थितियाँ हैं, जिनका टकराव राजनीति और दर्शन के क्षेत्र में पहले भी सामने आया है।
हेगेल की द्वन्द्ववादी पद्धति की चर्चा करते हुए और द्वन्द्ववाद भौतिकवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले लेनिन ने इस बात को स्पष्ट किया था कि किसी भी चीज़ के भीतर विपरीत तत्त्वों के बीच का संघर्ष एक चिरस्थायी परिघटना होती है जबकि उनकी एकता एक अस्थायी परिघटना। किसी भी चीज़ को जानने का मतलब होता है उसके आन्तरिक अन्तरविरोध को जानना, यानी उसके भीतर के विपरीत तत्त्वों के संघर्ष का अध्ययन करना। यानी हम ‘थीसिस–एण्टीथीसिस’ को जानने के ज़रिए ही ‘सिन्थेसिस’ को समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ को संश्लेषित, एकाश्मी रूप में देखते हुए और फिर उसके अलग–अलग अंशों को उसी सम्पूर्ण के एक अंग के रूप में देखते हुए हम उस चीज़ के वास्तविक संज्ञान तक नहीं पहुँच सकते। चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति (1966–76) के दौरान जब यह दार्शनिक बहस उठी थी तो माओ ने एक बार फिर इसे अपनी विशिष्ट शैली में स्पष्ट करते हुए बताया था कि मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद का नियम है, “एक दो में बँट जाता है, न कि यह कि, दो मिलकर एक हो जाते हैं।” अन्यत्र इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए माओ त्से–तुङ ने लिखा है :
“मार्क्सवादी दर्शन का मत है कि विपरीत तत्त्वों की एकता का नियम विश्व का बुनियादी नियम है। यह नियम समूचे विश्व में लागू होता है, चाहे प्राकृतिक जगत हो, चाहे मानव समाज हो अथवा मनुष्य की विचारधारा। किसी अन्तरविरोध में विपरीत तत्त्वों के बीच एकता भी क़ायम होती है और संघर्ष भी होता है तथा इसी से प्रेरित होकर वस्तुएँ गतिमान होती हैं और उनमें परिवर्तन होता है। अन्तरविरोध हर जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन वे अलग–अलग वस्तुओं की अलग–अलग प्रकृति के अनुरूप अलग–अलग स्वरूप वाले होते हैं। किसी घटना–विशेष तथा वस्तु–विशेष में विपरीत तत्त्वों की एकता परिस्थितियों से बँधी, अस्थायी व संक्रमणशील होती है और इसलिए सापेक्ष होती है जबकि विपरीत तत्त्वों का संघर्ष एक निरपेक्ष चीज़ होता है।” (माओ त्से–तुङ : ‘जनता के बीच के अन्तरविरोधों को सही ढंग से हल करने के बारे में’, 27 फरवरी, 1957, पहला अंग्रेज़ी पॉकेट संस्करण, पृ. 18)
समाहार के तौर पर कहा जा सकता है कि उन्नत मार्क्सवादी समझ के बावजूद, घटना–प्रवाह के या विचार–अनुभूति–प्रवाह के एकरेखीय विवरणात्मक ब्योरे पर बल देते हुए तथा आन्तरिक द्वन्द्व के ऊपर संश्लेषण पर बल देते हुए भौतिकवादी पुदोवकिन द्वन्द्ववादी पद्धति से विचलित होते हैं, जबकि आइज़ेंस्ताइन द्वन्द्वात्मक टकराव को ही कुंजीभूत कड़ी बनाकर यथार्थ के संज्ञान पर अविचल रूप से बल देते हैं।
आइज़ेंस्ताइन ने कलात्मक संज्ञान और यथार्थ के कलात्मक पुनर्सृजन के प्रश्न पर अनुभववादी पद्धति को छोड़कर दार्शनिक ढंग से सोचने की शुरुआत दरअसल तभी कर दी थी जब उन्होंने गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद महान और विवादास्पद नाट्य–निर्देशक व्सेवेलोद मेयरहोल्ड के साथ थिएटर में डिज़ाइनर और फिर निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया था। यहीं उन्होंने थिएटर की अपेक्षा सिनेमा की शक्ति को पहचाना और यथार्थ की हूबहू प्रस्तुति की प्रकृतवादी सोच से निर्णायक विच्छेद करके यथार्थवाद की उस अवधारणा की दिशा में यात्रा की शुरुआत की जो जीवन के सारभूत आन्तरिक द्वन्द्वों की शिनाख्त और पड़ताल पर तथा उनके समाधान की जनपक्षीय दिशा की समझ पर बल देती थी। यथार्थवाद की यह नई समझ अनुभूतिजन्य भावावेग के बजाय दर्शकों में एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करने पर बल देती थी। आगे हम इस बात की अलग से चर्चा करेंगे कि आइज़ेंस्ताइन, बरास्ता मेयरहोल्ड, किस प्रकार ब्रेष्ट के रंग–चिन्तन से जुड़ते हैं और उसे सिनेमा में गुणात्मक छलाँग के ज़रिए आगे ले जाते हैं जबकि पुदोवकिन स्तानिस्लाव्स्की के रंग–चिन्तन को सिनेमा की दुनिया में क्रियान्वित–विस्तारित करते प्रतीत होते हैं।
आइज़ेंस्ताइन ने 1922.23 में, थिएटर से सिनेमा की दुनिया के संक्रमण की तैयारी करते हुए, कुलेशोव के मातहत अध्ययन की शुरुआत की। मोन्ताज विषयक अपनी अवधारणाओं को उन्होंने पहली बार ‘आकर्षणों का मोन्ताज’ नामक लेख में सूत्रबद्ध किया जो कवि मयाकोव्स्की द्वारा सम्पादित पत्रिका ‘लेफ’ में प्रकाशित हुआ। यह लेख एक तरह से, आइज़ेंस्ताइन की नई कलात्मक मुहिम का सैद्धान्तिक घोषणापत्र था। इसमें उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि एजिटेशन के उद्देश्य से, दर्शकों पर सुविचारित भावनात्मक झटकों द्वारा चोट की जानी चाहिए। मोन्ताज विषयक अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि शॉट ‘अ’ और शॉट ‘ब’ को इस प्रकार अन्तर्सम्बन्धित होना चाहिए कि उनका योग ‘स’ हो जाए, लेकिन ‘स’ भी स्वयं में एक शॉट हो। यह ‘थीसिस–एण्टीथीसिस–सिन्थेसिस’ का सिनेमाई समतुल्य था। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जापानी लिपि से एक दिलचस्प सादृश्य–निरूपण प्रस्तुत किया। जापानी लेखन में कैरेक्टर्स का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि ‘कुत्ता’ के लिए प्रयुक्त कैरेक्टर को जब ‘मुँह’ के लिए प्रयुक्त कैरेक्टर से जोड़ा जाता है तो उसका नतीजा मात्र ‘कुत्ते का मुँह’ नहीं होता, बल्कि ‘भौंकने’ की नई अवधारणा अभिव्यक्त होती है। आइज़ेंस्ताइन ने मोन्ताज की तुलना एक आन्तरिक दहन इंजन के भीतर के उन विस्फोटों से की जिनके चलते कार आगे की ओर गतिमान होती है। मोन्ताज विषयक अपनी इस अवधारणा को आइज़ेंस्ताइन ने सबसे सटीक और प्रातिनिधिक ढंग से अपनी फ़िल्म ‘बैटलशिप पोतेमकिन’ में प्रस्तुत किया। लेकिन मोन्ताज की द्वन्द्वात्मक अवधारणा को व्यवहृत करने वाले इस महान ऐतिहासिक प्रयोग से पहले आइज़ेंस्ताइन अपनी पहली फ़िल्म ‘स्ट्राइक’ में इसका पूर्वरंग प्रस्तुत कर चुके थे।
प्रयोगों के दौरान अन्तरविरोधों से जूझकर आगे बढ़ती एक महान विचार–यात्रा
1924 में, प्रोलेतकुल्त थिएटर ने, जिससे जुड़कर कई नाटकों के लिए डिज़ाइनिंग और निर्देशन का काम आइज़ेंस्ताइन ने किया था, उन्हें ‘सर्वहारा अधिनायकत्व की ओर’ फ़िल्म–श्रृंखला के आठ प्रसंगों/कड़ियों में से एक के निर्देशन की ज़िम्मेदारी सौंपी। इसी का नतीजा ‘स्ट्राइक’ फ़िल्म के रूप में सामने आया जिसने सोवियत सिनेमा की दिशा बदल दी। यह फ़िल्म ज़ारकालीन रूस में मज़दूरों की एक हड़ताल की पूरी प्रक्रिया और फिर उसके क्रूर दमन को दर्शाती थी। मजूदर वर्ग की ऊर्जा और प्रचण्ड शक्ति के साथ ही शासक वर्गों के जासूसों, उकसावेबाज़ों और सशस्त्र दस्तों की भूमिका को फ़िल्म में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया था। फ़िल्म का अन्त उन दो दृश्यों के इतिहास–प्रसिद्ध अध्यारोपण से किया गया था जिनमें से एक में मज़दूरों का नरंसहार और दूसरे में एक साँड़ को जिबह किए जाते दिखाया गया था। इस फ़िल्म में पहली बार आइज़ेंस्ताइन ने मोन्ताज की अवधारणा को व्यवहार में लागू किया। अपने रंगकर्म दिनों में लिखित ‘आकर्षणों का मोन्ताज’ में उन्होंने दर्शकों के ऊपर दहलाने वाले, चमत्कारिक दृश्यों की बौछार की जो बात की थी, उससे भी दो क़दम आगे जाते हुए इस फ़िल्म में डाक्युमेण्टरी पद्धति को पूरी तरह से खरिज कर दिया गया था। फ़िल्म घटनाक्रम का सुव्यवस्थित ब्योरा प्रस्तुत करने की जगह इतिहास के प्रातिनिधिक तथ्यों के व्यवस्थित चयन से निगमित तर्क को दर्शक तक पहुँचाने की कोशिश करती है और वैयक्तिक नायक के चलन को तोड़ती हुई, पहली बार मज़दूर वर्ग को सामूहिक नायक के रूप में उपस्थित करती है। ‘स्ट्राइक’ के निर्माण और प्रदर्शन के दौर में आइज़ेंस्ताइन फ़िल्म–निर्माण के कलात्मक–तकनीकी पक्षों से भी अधिक सिनेमा को लेकर गहन दार्शनिक प्रश्नों से टकरा रहे थे और पुदोवकिन जैसे साथी सहकर्मियों से घनघोर बहस जारी थी। उस दौर को याद करते हुए बाद में उन्होंने लिखा था कि उस माहौल में मेरे पढ़ने की मेज़ पर भौतिकवादी द्वन्द्ववादियों की कृतियों ने सौन्दर्यशास्त्र की पुस्तकों को विस्थापित कर दिया था।
1925 में ‘बैटलशिप पोतेमकिन’ फ़िल्म बनी और रिलीज़ हुई। 1905 की रूसी क्रान्ति की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में सरकार ने कुछ फ़िल्मों के निर्माण का फ़ैसला लिया था जिनमें से एक की ज़िम्मेदारी आइज़ेंस्ताइन को दी गई। सिनेमा में चित्रित युद्धपोत पोतेमकिन के नौसैनिकों का विद्रोह मूलत: 1905 के क्रान्तिकारी घटना–परिदृश्य को दिखलाने वाले तमाम सीक्वेंसेज़ में से एक था। लेकिन जब पटकथा पर काम आगे बढ़ा तो आइज़ेंस्ताइन को लगा कि नौसैनिकों के विद्रोह, ओदेस्सा के मज़दूरों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया और कज़्जाकों द्वारा बर्बर दमन का पूरा घटनाक्रम अपने आप में 1905 के क्रान्ति की स्पिरिट और सारतत्त्व को प्रातिनिधिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। दूसरे, वे इतिहास का डॉक्युमेंटरी जैसा विवरणात्मक ब्योरा प्रस्तुत करने के बजाय करना भी यही चाहते थे क्योंकि उनके लेखे कलाकृति का प्रयोजन भी यही होता है। नतीजतन, पूरी फ़िल्म पोतेमकिन पर विद्रोह और ओदेस्सा की घटनाओं पर ही केन्द्रित कर दी गई।
‘बैटलशिप पोतेमकिन’ न केवल आइज़ेंस्ताइन की मोन्ताज–विषयक अवधारणाओं को मूर्त रूप देने वाली सर्वाधिक प्रातिनिधिक फ़िल्म थी, बल्कि यह उनके जीनियस की घनीभूततम और सफलतम अभिव्यक्ति भी थी। कई बार इसे दुनिया की महानतम फ़िल्म का दर्ज़ा मिला और आज भी जब कभी दुनिया के सिनेमाविद् और सिने–आलोचकगण सार्वकालिक महान फ़िल्मों की कोई सूची बनाते हैं तो उसमें ‘पोतेमकिन’ अवश्य ही शामिल होती है। फ़िल्म के प्रभाव का यह आलम था कि इण्डोनेशिया में डच युद्धपोत पर विद्रोह करने वाले नौसैनिकों ने अपने मुक़दमे के दौरान यह स्वीकार किया था कि विद्रोह की प्रेरणा उन्हें ‘बैटलशिप पोतेमकिन’ फ़िल्म से मिली थी। पूरे चौथे दशक के दौरान यूरोपीय मज़दूर आन्दोलन में इस फ़िल्म की प्रचण्ड लोकप्रियता बनी रही। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, इस फ़िल्म के कारण जापान में एक राजनीतिक संघर्ष उठ खड़ा हुआ था और इस फ़िल्म को ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को दिखाने के लिए एक नागरिक कमेटी का भी गठन किया गया था।
यह फ़िल्म न केवल जनसमुदाय की समष्टिगत शक्ति, इतिहास–निर्मात्री शक्ति और अजेयता की स्पिरिट तथा सत्तातंत्र की बर्बरता के यथार्थ को सेल्युलॉयड पर पकड़ने और प्रस्तुत करने का एक सचेत और वैज्ञानिक ढंग से सुविचारित प्रयास थी, बल्कि यह दर्शकों को एक आलोचनात्मक दृष्टि देने के साथ ही उनमें शक्तिशाली भावोद्रेक पैदा करने का भी काम कर रही थी। परम्परागत थिएटर–प्रस्तुतियों में भावनात्मक आवेग का जो वर्चस्व होता था और एपिक थिएटर–प्रस्तुतियों में वस्तुपरक तर्कणा का जो वर्चस्व होता था, उन दोनों का द्वन्द्वात्मक संश्लेषण पहली बार आइज़ेंस्ताइन ने व्यावहारिक धरातल पर ‘पोतेमकिन’ में प्रस्तुत किया और फिर इसके सिद्धान्तीकरण की दिशा में आगे क़दम बढ़ाया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
‘बैटलशिप पोतेमकिन’ में वस्तुगत और मनोगत उपादानों के कुशल द्वन्द्वात्मक सन्तुलन के पीछे सर्वोपरि कारण यह है कि फ़िल्म में, प्रारम्भिक अन्तर्बोध के बाद आइज़ेंस्ताइन ने हर तफ़सील को अत्यन्त सावधानी से नियोजित किया और पहली बार वे अपनी इस स्थापना को व्यवहारत: सिद्ध करने में सफल रहे कि मोन्ताज महज़ एक सम्पादन–तकनीक ही नहीं है। पूरी फ़िल्म में हमें शॉट्स के भीतर काउण्टरप्वाइण्ट, सभी सीक्वेंसेज़ के बीच काउण्टरप्वाइण्ट, मूड, टेम्पो, टोन, टेक्स्चर, चेहरों और जनसंकुलों का ‘काउण्टरप्वाइण्ट’ देखने को मिलते हैं। प्रत्येक टकराव एक ही बुनियादी टकराव को अभिव्यक्त करता है : ओदेस्सा में और समूचे रूस में 1905 की क्रान्ति के दौरान वर्गों का टकराव। ओदेस्सा बन्दरगाह की सीढ़ियों वाला सीक्वेंस शायद फ़िल्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सीक्वेंस है जिसमें कज़्जाकों को उन नागरिकों का क़त्लेआम करते दिखलाया गया है जो पोतेमकिन के विद्रोहियों का स्वागत करने के लिए बन्दरगाह की ओर उतरती सीढ़ियों पर एकत्र हैं। आइज़ेंस्ताइन ने प्रस्फोटों की एक श्रृंखला के रूप में मोन्ताज की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी, उसको पूरी तरह, हर पहलू से इस सीक्वेंस ने मूर्त रूप दे दिया है। भीड़ का उमड़ना, मार्च करते सफ़ेद बूटों के शॉट्स, तलवारों का चमकना, क्षणांश के लिए स्क्रीन पर चेहरों के क्लोज़–अप्स का भर जाना, एक ओर कज़्जाकों के दबाव से भीड़ का ऊपर सीढ़ियों की ओर वापस जाना और दूसरी ओर ठीक उसी समय एक बच्चागाड़ी का लम्बी सीढ़ियों पर नीचे की ओर ढुलकते जाना। परस्पर–विरोधी शॉट्स की टक्कर से सिनेमा में नई अर्थोत्पत्ति के जिस द्वन्द्ववादी मोन्ताज–सिद्धान्त का विस्तृत निरूपण आगे चलकर आइज़ेंस्ताइन ने ‘फ़िल्म सेंस’ (1942 में प्रकाशित) और ‘फ़िल्म फ़ॉर्म’ (1949 में प्रकाशित) पुस्तकों में संकलित लेखों में किया, उसका सर्वाधिक प्रतिनिधि उदाहरण वे पहले ही “ओदेस्सा की सीढ़ियों” के सीक्वेंस में प्रस्तुत कर चुके थे। इस सीक्वेंस की शक्ति तब उभरकर सामने आती है जब दर्शक का दिमाग़ अलग–अलग, स्वतंत्र शॉट्स को मिलाकर एक नया, भिन्न, अवधारणात्मक प्रभाव निर्मित कर लेता है जो उन शॉट्स के विवरणात्मक पहलू को एकदम पीछे धकेल देता है। सिनेमाई दिक् और काल के त्वरित परिचालन और उलट–पुलट से, सीढ़ियों पर क़त्लेआम तथा नीचे कज्जाक और ऊपर ज़ार की मिलिशिया के बीच सैकड़ों नागरिकों के फँसे होने का दृश्य एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण कर लेता है।
आइज़ेंस्ताइन का अगला प्रोजेक्ट ‘अक्टूबर’ फ़िल्म का निर्माण था जो 1928 में प्रदर्शित हुई। अक्टूबर–क्रान्ति की दसवीं वर्षगाँठ के आयोजन के निमित्त बनने वाली फ़िल्मों में से यह भी एक थी। क्रान्ति के इतिहास–सम्बन्धी दस्तावेज़ों की गहन छानबीन के बाद आइज़ेंस्ताइन ने जो फ़िल्म तैयार की, वह कथा–फ़िल्म के रहे–सहे ताने–बाने को भी छिन्न–भिन्न करती हुई शायद फ़िल्म–निबन्ध जैसी कोई चीज़ थी। ‘पोतेमकिन’ यदि प्रकृति से पूरी तरह एक एजिटेशनल फ़िल्म थी, तो ‘अक्टूबर’ एक सैद्धान्तिक विमर्श प्रस्तुत करती प्रोपेगैण्डा फ़िल्म थी। आइज़ेंस्ताइन ने ‘स्ट्राइक’ और ‘पोतेमकिन’ के बाद अपनी सिने–सैद्धान्तिकी को और आगे विकसित करते हुए, जानबूझकर ‘अक्टूबर’ को ‘बौद्धिक़” या “विचारधारात्मक” मोन्ताज की एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें उनकी सम्पादन–प्रक्रिया और अधिक अमूर्त हो गई। शॉट्स के बीच का सम्बन्ध–स्थापन इसमें चाक्षुष या भावनात्मक न होकर अवधारणात्मक हो गया। इस फ़िल्म की न केवल आलोचकों ने काफ़ी आलोचना की, बल्कि दर्शकों ने भी इसके काफ़ी हद तक अबूझ होने की शिकायत की। सोवियत संघ के कला–विशेषज्ञों ने और कम्युनिस्ट पार्टी के संास्कृतिक मामलों से सम्बद्ध लोगों ने भी आइज़ेंस्ताइन पर रूपवादी अतिरेक, कुलीनतावाद और सौन्दर्यवाद का आरोप लगाया। इन आलोचनाओं का आइज़ेंस्ताइन ने कोई प्रतिकार नहीं किया। उनकी केन्द्रीय चिन्ता और चिन्तन का विषय यह था कि द्वन्द्ववादी ट्रीटमेण्ट में वे विफ़ल कहाँ रहे? क्या सिनेमा जैसा सर्वोन्नत कला–माध्यम भी विचार–सम्प्रेषण या विचारधारा–निरूपण का सापेक्षत: अधिक प्रत्यक्ष और अधिक प्रभावी साधन नहीं बन सकता? इस ऊहापोह के बीच ही आइज़ेंस्ताइन ने अपनी नई फ़िल्म ‘ओल्ड ऐण्ड न्यू’ (1929) पर काम शुरू किया। यह फ़िल्म सोवियत संघ के देहातों में कृषि के सामूहिकीकरण और मशीनीकरण की मुहिम पर केन्द्रित थी। ‘पोतेमकिन’ की उग्रता, आवेगात्मकता और चुस्ती के विपरीत यह फ़िल्म शान्त और फैली हुई थी। इसकी संरचना कुछ–कुछ, एक प्रगीतात्मक कविता जैसी थी। इस फ़िल्म में पहली बार आइज़ेंस्ताइन ने अमूर्त रंग का प्रयोग किया और मूक फ़िल्म में ध्वनि के इस्तेमाल की भी कोशिश की। इस फ़िल्म को भी रूपवादी भटकाव के उन्हीं आरोपों का सामना करना पड़ा जो ‘अक्टूबर’ पर लग चुके थे। आज पुनरावलोकन करते हुए कहा जा सकता है कि फ़िल्म उत्पादन–सम्बन्धों और सामाजिक सम्बन्धों के समाजवादी रूपान्तरण, भौतिक प्रगति और जीवन–मूल्यों और जीवन–शैली के स्तर पर जारी नये–पुराने के टकराव को तो दिखलाती है, लेकिन समाजवादी संक्रमण के पूरे दौर में जारी वर्ग–संघर्ष के विविध सूक्ष्म और व्यापक रूपों पर रोशनी नहीं डालती। लेकिन इसके लिए आइज़ेंस्ताइन की विचार–दृष्टि दोषी नहीं थी। समाजवादी समाज में वर्ग–संघर्ष की निरन्तरता के बारे में स्पष्ट समझ बनने की शुरुआत ही सोवियत संघ में पाँचवें दशक के अन्त में हुई और इस प्रक्रिया को परिणति तक पहुँचाने का काम चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति (1966–67) ने किया। ‘ओल्ड ऐण्ड न्यू’ के निर्माण के समय सामान्य सोच यही हुआ करती थी कि स्वामित्व के रूप सहित उत्पादन के सम्बन्धों में बदलाव और फिर उसके बाद उत्पादक शक्तियों का विकास-समाजवादी रूपान्तरण का यही मुख्य कार्यभार है।
बहरहाल, एक बार फिर हम आइज़ेंस्ताइन की केन्द्रीय चिन्ता की ओर वापस लौटें। कला की सामाजिक भूमिका के प्रश्न पर सोचते हुए आइज़ेंस्ताइन एक सर्वोन्नत कला के रूप में फ़िल्म–विधा से अधिकतम सम्भव की उम्मीद कर रहे थे और यह भी अपेक्षा कर रहे थे कि परम्परागत वर्णनात्मकता, प्रत्यक्षता और परम्परागत प्रतीकवाद से ऊपर उठकर फ़िल्म विधा अमूर्तन तथा बिम्बात्मकता की नई ऊँचाइयों को पा लेगी और फिर सामाजिक चेतना यथार्थ के इस अति उन्नत–अति अमूर्त कलात्मक पुनर्सृजन के अवबोध के ज़रिए वास्तविक जगत का अवधारणात्मक ज्ञान प्राप्त करेगी तो वह अत्यन्त उन्नत, व्यापक और सूक्ष्म स्तर का होगा।
चिन्तन–प्रक्रिया को उद्घाटित करने वाली रहस्यमय डायरी और ‘पूँजी’ पर फ़िल्म बनाने की योजना
आइज़ेंस्ताइन की मृत्यु के बरसों बाद उनके निवास स्थान से एक डायरी मिली जिसमें स्फुट टिप्पणियों की भरमार थी। ये नोट्स, काम करते हुए, शूटिंग के बीच, सम्पादन–कक्ष में, यहाँ–वहाँ लिये गए थे। ज़्यादातर नोट्स उन वर्षों के दौरान लिये गए हैं जब आइज़ेंस्ताइन ‘अक्टूबर’ पूरी करने के बाद ‘ओल्ड ऐण्ड न्यू’ बना रहे थे, और उन पर चारों तरफ़ से आक्रमणों की बौछार हो रही थी, यानी 1927 से 1930 के बीच।
इन नोट्स से पता चलता है कि ‘अक्टूबर’ की कथित विफ़लता और अपने ऊपर लगे रूपवादी भटकाव के आरोप की पड़ताल करते हुए आइज़ेंस्ताइन इस प्रश्न से जूझ रहे थे कि आख़िरकार यथार्थवाद है क्या? क्या यह यथार्थ की तफ़सीलों का ग्राफ़िक विस्तार के साथ वर्णनात्मक चित्रण मात्र है? क्या यह वस्तुगत यथार्थ को अधिक सघन और प्रातिनिधिक बनाने के लिए कलात्मक नाटकीयता के समावेशन तथा प्रतिनिधि व्यक्तिगत नायकों का सृजन करके उनके मनोजगत की गहराइयों में उतरने की प्रविधि मात्र है? यदि अमूर्तन तथा प्रतीक–रूपक–बिम्ब आदि, कला के अपरिहार्य संघटक अवयव होते हैं तो सभी कलाओं के संश्लेषण से गठित सर्वोन्नत कला-सिनेमा में परम्परागत कथात्मकता और चाक्षुष वर्णनात्मकता के रूप के सीमान्तों का अतिक्रमण करके, क्या उन्नत धरातल के अमूर्तन में छलाँग लगाना सिनेमा के यथार्थवाद का बुनियादी कार्यभार नहीं होना चाहिए?
आइज़ेंस्ताइन ने अपनी डायरी की टिप्पणियों में लगातार, समाजवादी यथार्थवाद की इस यांत्रिक भौतिकवादी समझ का विरोध किया है कि चीज़ों का सीधा–सादा, सरल–सुगम, सम्प्रेषणीय, “शब्दश: प्रस्तुत” ब्योरा ही यथार्थवाद है और हर तरह का अमूर्तन रूपवाद के गड्ढे की ओर विपथगमन से अधिक कुछ नहीं है। सामाजिक जीवन की भौतिक अवस्थाओं के उन्नत होने तथा उन्नततर कला–विधाओं के प्रादुर्भाव के साथ ही आइज़ेंस्ताइन कलात्मक अमूर्तन की उन्नततर मंज़िलों की ओर छलाँग को जनता के सांस्कृतिक स्तरोन्नयन और कला की प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे। कला में “साधारण जीवन से अमूर्त और सामान्यीकृत बिम्बावली में छलाँग” को वे अनिवार्य मानते थे। अपनी प्रारम्भिक तीन फ़िल्मों में स्व–आविष्कृत, उद्भावनापरक मोन्ताज का ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक प्रयोग करते हुए वे क़दम–ब–क़दम आगे बढ़े। ‘स्ट्राइक’ समाज में वर्ग–संघर्ष के उद्भव–विकास और उसके रूपों पर बनी एक सुव्यवस्थित शैक्षिक फ़िल्म थी। ‘पोतेमकिन’ एक एजिटेशनल फ़िल्म थी जिसमें क्रान्ति–कथा का विवरण या उसके किसी चरित्र को व्यक्तिगत प्रतिनिधि चरित्र बनाकर उसके मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वों का चित्रण प्रस्तुत करने के बजाय पूरी क्रान्ति की एक घटना के द्वन्द्वों को द्वन्द्वात्मक मोन्ताज–शैली के प्रयोग से इस तरह प्रस्तुत किया गया था कि निर्मित बिम्ब–श्रृंखला ने उस घटना को पूरी क्रान्ति का रूपक बना दिया और बुनियादी सामाजिक अन्तरविरोधों को अनावृत्त करते हुए वर्ग–संघर्ष की ऐतिहासिक शिक्षा को एक आवेगमय आह्वान में रूपान्तरित कर दिया। कथा–फ़िल्मों के वर्णनात्मक और अभिलेखन मूलक पारम्परिक व्यवहार से टकराते हुए ‘अक्टूबर’ फ़िल्म में निस्सन्देह आइज़ेंस्ताइन एक दूसरे छोर पर जा खड़े प्रतीत होते हैं। दैनन्दिन जीवन के सिलसिलेवार चित्र प्रस्तुत करने और सामाजिक लक्ष्य को प्रतिनिधि चरित्रों/नायकों के जीवनलक्ष्य में रूपान्तरित करके उनके अन्तर्जगत के मनोवैज्ञानिक चित्रण की पद्धति के बरक्स आइज़ेंस्ताइन पूरी जनता के सामूहिक नायकत्व को और इतिहास के बुनियादी तर्क को पर्दे पर प्रक्षेपित कर देना चाहते थे तथा इस प्रक्रिया में फ़िल्म–विधा को अमूर्त, सामान्यीकृत बिम्बात्मकता की ऊँचाइयों तक ले जाना चाहते थे। इसकी तार्किक परिणति, ज़ाहिरा तौर पर इसी रूप में सामने आनी थी कि वे अर्मूत विचार के सुस्पष्ट तर्क का पक्ष लेकर कथा–सूत्र की अनिवार्यता को सिरे से खारिज कर दें। इसी का परिणाम था-‘अक्टूबर’ का निर्माण, वह पहला महान, मौलिक सिने–प्रयोग जिसमें आइज़ेंस्ताइन ने मूर्त तथ्यपरकता और कथात्मकता से पूरी तरह विच्छेद कर लिया। कहा जा सकता है कि यह एक चिन्तन–फ़िल्म थी जिसमें अक्टूबर क्रान्ति की घटनाओं को, घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि प्रमेयों की एक पूरी श्रृंखला के निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया था। स्वयं आइज़ेंस्ताइन के शब्दों में, “नाटक, कविता और बैले के बाद ‘अक्टूबर’ एक नया रूप प्रस्तुत करता है : विषय–वस्तुओं की श्रृंखला पर आधारित निबन्धों का संग्रह।“
अधिकांश पहले, महान, मौलिक प्रयोगों की ही तरह ‘अक्टूबर’ में भी बहुतेरी अनगढ़ताएँ थीं, प्रयोगों की कई नवीनताएँ अबूझ थीं, अमूर्तन कई जगह पूरी तर्क–प्रक्रिया से विलग हो गया था जो दर्शकों में विभ्रम भी पैदा करता था। लेकिन आइज़ेंस्ताइन के लेखन और सिनेमा में आद्यन्त जो अविचल भौतिकवादी जीवन–दृष्टि और द्वन्द्वात्मक पद्धति के प्रति जो हठीला आग्रह मौजूद है, वह हमें विवश करता है कि एक प्रयोग की आंशिक विफ़लता पर, यदि हम उसमें रूपवादी और हेगेलियन प्रत्ययवादी द्वन्द्ववादी विचलन दीखते हों, तो भी फ़ैसले सुनाने के बजाय आइज़ेंस्ताइन के चिन्तन के आगे और पीछे के सूत्रों को जोड़ते हुए यह जानने की कोशिश करें कि आख़िरकार सिनेमा का यह महान सिद्धान्तकार क्या कहना और करना चाहता था?
‘अक्टूबर’ की कतिपय विफ़लताओं को प्रायोगिक विफ़लताओं के रूप में स्वीकार करते हुए भी आइज़ेंस्ताइन चिन्तन की अपनी मूल दिशा पर अविचल रहे। उनकी जिस डायरी की हमने ऊपर चर्चा की है, उसके नोट्स यह मानने का पर्याप्त आधार मुहैया कराते हैं कि आरोपों–अविश्वास और ग़लतफ़हमियों से जूझ रहे आइज़ेंस्ताइन अपने तर्कों को और धारदार बना रहे थे। ‘स्ट्राइक’, ‘पोतेमकिन’ और ‘अक्टूबर’ का नये सिरे से, बार–बार, सरल, वस्तुनिष्ठ, स्पष्टवक्तृता के साथ विश्लेषण करते हुए वे अपनी चूकों की शिनाख्त कर रहे थे, इस बात की पड़ताल कर रहे थे कि ये फ़िल्में द्वन्द्वात्मक चिन्तन की शिक्षा देने में क्या भूमिका निभा सकीं और नये सिरे से इस यक्ष–प्रश्न के रूबरू खड़े हो रहे थे कि चिन्तन की प्रक्रिया का फ़िल्म में ऐसा अनुवाद आख़िरकार कैसे किया जाए कि जैसे चलते–फिरते चित्र अमूर्त विचारों को प्रकट कर रहे हों। यह सोचते हुए उनके दिमाग़ में अपनी अवधारणा को मूर्त रूप देने वाला एक अनूठा विचार आया और वह था ‘पूँजी’ का फ़िल्मांकन। डायरी के प्रारम्भ में ही यह निश्चयात्मक घोषणा है : “तो यह तय हो चुका है : हम पूँजी पर फ़िल्म बना रहे हैं : आलेख कार्ल मार्क्स का होगा। यही एकमात्र तार्किक समाधान है।” यह डायरी मिलने तक ‘पूँजी’ पर फ़िल्म बनाने की आइज़ेंस्ताइन की घोषणा को कमोबेश एक लन्तरानी, एक आधा गम्भीर आधा मज़ाकिया शिगूफा ही माना जाता था।
एक तरह के सिनेमाई निबन्ध, सिनेमा के ज़रिए वैचारिक हस्तक्षेप या सिनेमाई शोध–प्रबन्ध की रचना की महत्त्वाकांक्षा ने आइज़ेंस्ताइन को ‘पूँजी’ के फ़िल्मांकन के विचार तक पहुँचाया। इस सोच की अगली कड़ी यह थी कि परम्परागत सिनेमा की सामान्य वाचिक संरचना और कथा को क्रमश: आगे बढ़ाते हुए दृश्यबन्ध से मुक्त होने के बाद, हम अपने परिवेश की एकदम साधारण चीज़ों का नये सिरे से अन्वेषण करें, परस्पर–विरोधी सामान्य घटनाओं–क्रियाओं को इस प्रकार ‘जक्स्टापोज़’ करें कि वे एक नये अर्थसन्धान की परिणति तक जा पहुँचें और वह भी किसी घटना के माध्यम से ही चाक्षुष बिम्ब में ढलकर स्वयं को प्रकट करे। ‘पूँजी’ पर फ़िल्म बनाने की अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना के लिए कच्चा माल आइज़ेंस्ताइन ने प्राय: दैनिक पत्रों से जुटाया और साथ ही ऐसे कुछ सामान्य दृश्यों की एक सूची तैयार की, जिनके परस्पर विरोधी युग्मों का संयोजन किसी संश्लेषण की स्थिति में पहुँचकर एक सुनिश्चित अर्थ या विचार तक जा पहुँचता हो : पेरिस में युद्ध से लौटे अपाहिज सैनिक की आत्महत्या, सनकी भगवान जैसे आग़ाख़ान की उसके अनुयाइयों द्वारा भक्ति, शंघाई में भूखे मरते लोगों द्वारा विरोध स्वरूप स्वयं को कारों के आगे डाल देना आदि घटनाएँ और चर्च, स्टॉक एक्सचेंज आदि के परिचित दृश्य। इन्हीं साधारण–सी चीज़ों के सूक्ष्म ब्योरों के उद्भावनापरक मोन्ताज से अमूर्त विचारों को व्याख्या का मूर्त रूप देना, अमूर्तन के ढाँचे पर अति साधारणता को मांस–मज्जा की तरह मढ़ना और किसी एक वस्तु या दृश्य के सूत्र को पकड़कर सर्वाधिक दूरवर्ती साहचर्य के विस्फोट के ज़रिए यथार्थ के अवबोधन तथा अवधारणात्मक ज्ञान के नये–नये, उन्नत संस्तरों तक जा पहुँचना-आइज़ेंस्ताइन का यह उद्देश्य था। कथा–सूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा, सामान्यीकरणों और अमूर्तनों की बुनियादी संरचना को सहारा देने वाले एक स्तम्भ जितना ही होना चाहिए। उसे पूरे ताने–बाने का एक सूत्र मात्र होना चाहिए और ध्यानाकर्षण का केन्द्र तो कदापि नहीं बनना चाहिए। आइज़ेंस्ताइन का विचार था कि कथात्मक–नाटकीय सामग्री का भार जितना कम होगा, फ़िल्म उतना ही अधिक वैचारिक सामग्री का भार उठा सकेगी और उसकी बौद्धिक क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी।
सर्वहारा सिनेमा में बौद्धिकता/तर्कणा के गुरुत्व और भावना/अनुभूति के संवेग के बीच द्वन्द्वात्मक संश्लेषण की अवधारणा
आइज़ेंस्ताइन जब आख्यानात्मक–नाटकीय सामग्री या कथा–सूत्र की वर्णनात्मकता को सिनेमा के केन्द्रीय संघटक उपादान के स्थान से विस्थापित करके महज़ एक बैसाखी या सहारा देने वाले स्तम्भ का दर्जा देते हैं, तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि वे राजनीतिक उपदेशवाद और दर्शकों पर अपनी बौद्धिक योजना थोपने की प्रवृत्ति के शिकार होकर कला के भाव–संवेगात्मक पक्ष को और सौन्दर्यात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति के पक्ष को सिरे से खारिज कर रहे होते हैं। इसके विपरीत, आइज़ेंस्ताइन की चोट इस जड़ीभूत प्रस्तरीकृत मान्यता पर होती है कि भाव–संवेगात्मक तत्त्व किसी कलाकृति में तभी मौजूद हो सकते हैं और वह दर्शकों की सौन्दर्यात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति तभी कर सकती है, जब उसमें तथ्यों का आख्यानपरक पुनर्सृजन या किस्सागोई मौजूद हो। इसके विपरीत, विषय–वस्तुओं की श्रृंखला द्वारा प्रक्षेपित विचारों का अपना भी एक सौन्दर्यात्मक पक्ष होता है।
आइज़ेंस्ताइन बौद्धिक सिनेमा की बात करते हुए कोरे सिद्धान्तों या तर्कणा या राजनीतिक सन्देश–सम्प्रेषण की बात नहीं करते, बल्कि चाक्षुष बिम्ब–विधान की मोन्ताज पद्धति के द्वारा वस्तुओं–प्रक्रियाओं–संरचनाओं के आन्तरिक द्वन्द्वों को उद्घाटित करने की बात करते हुए और “द्वन्द्वात्मक पद्धति की चाक्षुष तकनीक” को सूत्रबद्ध करने के अपने मूल लक्ष्य को रेखांकित करते हुए, किसी भी चीज़ से ज़्यादा, आइज़ेंस्ताइन को जिस चीज़ की तलाश थी, वह थी बौद्धिकता और भावनात्मकता की, अथवा, तर्कणा और अनुभूति के द्वन्द्वात्मक संश्लेषण की। यदि ये दो चीज़ें थीसिस और एण्टी–थीसिस के रूप में कला में आती हैं तो इनकी तार्किक निष्पत्ति सिन्थेसिस के रूप में सामने आनी ही चाहिए। आइज़ेंस्ताइन लिखते हैं : “मैं सोचता हूँ कि बौद्धिक आकर्षण भावनात्मक आवेग को कभी अलग नहीं करता।” और आगे बढ़ते हुए वे तर्क के भावनात्मक आवेग की और भावनात्मक आवेग के तर्क की बात करते हैं। साथ ही, एक सच्चे भौतिकवादी द्वन्द्ववादी के समान, भावनात्मक और तार्किक तत्त्वों की एकता की बात करते हुए आइज़ेंस्ताइन उनमें स्पष्ट अन्तर की आवश्यकता पर भी पूरा बल देते हैं। वे कहते हैं कि मोन्ताज संरचना के प्रभावशाली होने की शर्त है कि वह भावनात्मक उद्गार के रहस्यमय नियम खोज निकाले। एक ओर वे ‘भावावेगों के तर्क’ की बात करते हैं और दूसरी ओर उनका मानना है कि चिन्तन ठोस–मूर्त तथ्यों के वस्तुपरक नियमों से प्रत्यक्षत: संचालित नहीं होता, बल्कि कर्ता उन तथ्यों के गहन आन्तरिक अर्थों को गहराई से महसूस करता है। यानी हर तार्किक धारणा एक सघन भावनात्मक जुड़ाव के साथ ही अस्तित्वमान होती है।
अपने विरोधियों की आलोचना करते हुए आइज़ेंस्ताइन लिखते हैं : “वे संश्लेषण (या संवाद) की एकांगी माँगों के पाप में गिर गए हैं। वे वैचारिक विश्लेषण और भावावेगात्मक संश्लेषण के बीच अन्तर्निर्भरता को भी नहीं समझते। वे वैचारिक मुक्ति देने वाले और मस्तिष्क को समृद्ध करने वाले पद्धति–शास्त्र के बजाय मार्ग–निर्देशन की उम्मीद रखते हैं।”
चिन्तन की इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, आइज़ेंस्ताइन ने विचारों के गुरुत्व और भावनाओं के आवेग के पृथक्करण और फिर सम्भाविक एकता की शानदार ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। उनका मानना था कि प्राक्वर्गीय समाज में और कमोबेश वर्ग–समाज की प्रारम्भिक अवस्थाओं तक ज्ञान का चरित्र भावावेगात्मक या अनुभूतिमूलक भी था और सामूहिक विवेक या तर्कणा के रूप में भी। जैसे–जैसे श्रम–विभाजन और समष्टि के विघटन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वैसे–वैसे ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा विलग होते गये। एक ओर शुद्ध अमूर्तन, सैद्धान्तिक दर्शन या तर्कणा और दूसरी ओर, शुद्ध भावनात्मक आवेग या अनुभूति। वर्ग–विहीनता की दिशा में गतिमान समाजवादी समाज में सर्वहारा कला का विकास कालान्तर में इस विलगाव को दूर करेगा और सर्वोन्नत कला–माध्यम के रूप में अकेली फ़िल्म–विधा ही इस महासंश्लेषण में समर्थ है।
आइज़ेंस्ताइन 1927 के बाद के जिन वर्षों में अपनी डायरी में ये टिप्पणियाँ दर्ज़ कर रहे थे, उसके ठीक बाद, 1929 के अन्त में वे पेरिस गये। वहाँ, 1930 में, अपने बहुचर्चित सॉरबोन भाषण में उन्होंने उपरोक्त प्रसंग में जो बातें कहीं, वे डायरी की सन्दर्भित टिप्पणियों की ही एक सुव्यवस्थित प्रस्तुति थीं :
“प्राचीनतम काल, जादू और धर्म के काल में ज्ञान भावनात्मक आवेग और सामूहिक विवेक दोनों था। फिर द्वैतवाद के प्रभाव में वस्तुएँ अलग–अलग हुर्इं। एक ओर निरा सैद्धान्तिक दर्शन, शुद्ध अमूर्तन था और दूसरी ओर शुद्ध भावना या आवेग। हमें अवश्य ही लौटना होगा लेकिन आदिम (धार्मिक पड़ाव की) स्थिति की ओर नहीं, बल्कि भावनात्मक और बौद्धिक तत्त्वों के सहधर्मी संश्लेषण की स्थिति में। मैं सोचता हूँ कि अकेली फ़िल्म–विधा ही इस महासंश्लेषण में सक्षम है। वही सक्षम है कि बुद्धि को उसके सक्रिय और ठोस भावनात्मक स्रोतों तक लौटा सके। वही हमारा रास्ता है और निर्दिष्ट कर्म है, जिसे हमने चुना है। वही मेरी नई फ़िल्म का प्रस्थान–बिन्दु होगा। वह फ़िल्म जो कामगारों और किसानों को द्वन्द्वात्मक चिन्तन के लिए दिशा–निर्देश करेगी। वह फ़िल्म होगी मार्क्स की ‘पूँजी’।”
स्तानिस्लाव्स्की–पुदोवकिन बनाम मेयरहोल्ड–ब्रेष्ट–आइज़ेंस्ताइन–थिएटर से सिनेमा तक दो धाराओं का टकराव और आगे का रास्ता
अब हम थिएटर और सिनेमा के क्षेत्रों के सुधीजनों के सामने सोचने के लिए कुछ विचारोत्तेजक प्रश्न उपस्थित करना चाहेंगे। यह कोई तर्कातीत अटकल या महज़ पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि यह मानने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि मोन्ताज–विषयक अवधारणात्मक वाद–विवाद में आइज़ेंस्ताइन और पुदोवकिन की जो अवस्थितियाँ थीं वे क्रमश: ब्रेष्ट की एपिक थिएटर विषयक अवस्थिति और स्तानिस्लाव्स्की की ड्रामेटिक थिएटर विषयक अविस्थिति के निकट थीं।
स्तानिस्लाव्स्की का थिएटर भी नाटक के कथात्मक ताने–बाने पर विशेष ज़ोर देता था और सामाजिक जीवन के घटना–प्रवाह को पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल करते हुए प्रतिनिधि चरित्रों के मनोजगत के द्वन्द्वों को उभारने का प्रयास करता था। इसके लिए, स्तानिस्लाव्स्की का कहना था कि अभिनेता को अभिनीत चरित्र के साथ स्वयं को सम्पूर्णत: आइडेण्टिफाई करना चाहिए। स्तानिस्लाव्स्की की ‘अंगज व्यापार विधि’ के अनुसार, क्रिया (अभिनय) अनुभूति को और फिर अनुभूति चिन्तन को जन्म देती है। अभिनेता द्वारा अनुभूत अनुभूति तीव्र–सजीव होनी चाहिए। तब फिर वह दर्शकों को भी भावावेगात्मक रूप से संक्रमित कर देगी, उनके हृदय में प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी। दर्शक अभिनेता के साथ तदनुभूति से जुड़ जाएगा। इस तरह दर्शक की भावनाओं को एक सुनिश्चित दिशा में निर्देशित करके थिएटर उसके चिन्तन को निर्देशित करेगा।
ब्रेष्ट स्तानिस्लाव्स्की के रंग–सिद्धान्त पर एकरेखीयता का, क्रमिक विकास के सिद्धान्त का आरोप लगाते हैं। ग़ौरतलब है कि वे स्तानिस्लाव्स्की के परम्परागत नाटकीय रंगमंच से जब एपिक रंगमंच की तुलना करते हैं तो एकरेखीय विकास के बरक्स मोड़ों–घुमावों से होकर विकास की बात करते हैं, कथा के क्रमिक विकास की जगह मोन्ताज की (ग़ौर करें, मोन्ताज की) बात करते हैं, अनुभूति के बरक्स विश्व–दृष्टिकोण को रखते हैं, भावना के सामने तर्कबुद्धि को रखते हैं, क्रमिक विकास के नियतत्ववाद की जगह उछालों की बात करते हैं तथा दर्शक को मंचीय व्यापार में शामिल करके उसकी सक्रियता समाप्त करने के बजाय उसे प्रेक्षक बनाए रखकर उसकी सक्रियता जगाने पर बल देते हैं। (‘दि मॉडर्न थिएटर इज़ दि एपिक थिएटर’, ब्रेष्ट ऑन थिएटर, 1974, लन्दन, पृ. 37) ब्रेष्ट मनुष्य की स्वत:र्स्फूत भावना और अन्धसहजवृत्ति को उभाड़कर जनोत्तेजक ढंग से उसे किसी पक्ष में खड़ा करने को सर्वहारा जनवादी चेतना के प्रतिकूल मानते थे, वे भावना के बजाय मनुष्य के आलोचनात्मक विवेक को जगाने पर बल देते थे। इसके लिए, उनका मानना था कि अभिनेता और बिम्ब के बीच एक निश्चित दूरी बनी रहनी चाहिए और अभिनेता को अपने द्वारा सृजित बिम्ब का “तटस्थ रहकर” अवलोकन करना चाहिए।
एलियनेशन के इस सिद्धान्त को ब्रेष्ट के “एपिक थिएटर” के दायरे के बाहर, अपने–अपने ढंग से जो लोग लागू कर रहे थे, वे थे सोवियत नाट्य निर्देशक मेयरहोल्ड और वाख्तांगोव। सच तो यह है कि ब्रेष्ट से भी कुछ पहले ही मेयरहोल्ड ने एलियनेशन की अवधारणा को रखना और प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। मेयरहोल्ड स्तानिस्लाव्स्की के शिष्य थे, लेकिन आचार्य से दूरी लेते हुए उन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि अभिनेता को चरित्र में विलीन नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि दोनों के बीच एक दूरी होनी चाहिए ताकि अभिनेता अभिनीत चरित्र के प्रति अपने रुख को भी अभिव्यक्त कर सके।
दो धाराओं की इस पूरी बहस को समझने के बाद, पुदोवकिन के ‘संज्ञानात्मक सहयोजन (cognitive linkage) का सिद्धान्त’ और आइज़ेंस्ताइन के ‘विरुद्धों के संघर्ष का सिद्धान्त’ के बीच के संघर्ष को, विवरणात्मक मोन्ताज बनाम उद्भावनापरक मोन्ताज पर बहस को एक बार फिर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भावना और अन्तर्जगत के चित्रण पर बल देने वाले पुदोवकिन सिनेमा में स्तानिस्लाव्स्की की रंग–सैद्धान्तिक धारा की अगली कड़ी हैं, जबकि बौद्धिकता पर बल देते हुए कथा–सूत्र के रैखीय क्रमिक विकास का निषेध करने वाले आइज़ेंस्ताइन सिनेमा में ब्रेष्टीय रंग–सैद्धान्तिकी को विस्तार देते हुए प्रतीत होेते हैं।
यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पुदोवकिन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिनय की ‘स्तानिस्लास्की–प्रणाली’ को, जिसे ‘अंगज व्यापार–विधि’ भी कहा जाता है, सिनेमा में लागू किया। दूसरी ओर, यह भी ग़ौरतलब है कि सिनेमा में प्रवेश करने के पहले आइज़ेंस्ताइन ने प्रोलेतकुल्त थिएटर में मेयरहोल्ड के साथ काम करते हुए उनकी नाट्य–शैली से काफ़ी कुछ सीखा। मेयरहोल्ड की रंग–सैद्धान्तिकी और ‘कुलेशोव–प्रभाव’ के अत्यन्त सर्जनात्मक संश्लेषण ने ही आइज़ेंस्ताइन के फ़िल्म–सिद्धान्त की आधारशिला तैयार की।
ऊपर चर्चित जिस लेख (‘दि मॉडर्न थिएटर इज़ दि एपिक थिएटर’) में ब्रेष्ट ने परम्परागत थिएटर से एपिक थिएटर की तुलना की है, वह लेख उन्होंने 1930 में लिखा था। उसमें वे परम्परागत थिएटर की ‘विकास’ की अवधारणा के बरक्स ‘मोन्ताज’ की अवधारणा की बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि इसके ठीक पहले 1929 में बर्लिन में ब्रेष्ट और आइज़ेंस्ताइन की मुलाक़ात हुई थी। यह समय था जब आइज़ेंस्ताइन अपनी डायरी लिखते हुए सिनेमा के ऊपर चर्चित सैद्धान्तिक प्रश्नों से टकरा रहे थे और दूसरी ओर ब्रेष्ट लगातार “एपिक थिएटर” की सैद्धान्तिकी पर काम कर रहे थे। यह जानना सिनेमा और रंगकर्म के अध्येताओं के लिए बहुत दिलचस्प होता कि अपने–अपने क्षेत्र के इन दो महान आचार्यों के बीच, जो दृष्टिकोण और अवस्थिति में एक–दूसरे के इतने निकट थे, क्या बात हुई और दोनों ने एक–दूसरे के चिन्तन की दशा–दिशा को कितना प्रभावित किया।
बहरहाल, ब्रेष्ट के थिएटर और आइज़ेंस्ताइन के सिनेमा के बीच अवधारणात्मक धरातल पर जो एक फ़र्क़ था, वह यह कि एपिक थिएटर भावना और अनुभूति की जगह तर्कबुद्धि और विश्व–दृष्टिकोण पर बल देता था जबकि आइज़ेंस्ताइन का उद्भावनापरक मोन्ताज–शैली पर केन्द्रित सिनेमा भावना और तर्कबुद्धि के द्वन्द्वात्मक संश्लेषण को सर्वहारा कला के यक्ष–प्रश्न के कुंजीभूत समाधान के रूप में देख रहा था। कहा जा सकता है कि आइज़ेंस्ताइन की सोच ब्रेष्ट की अपेक्षा द्वन्द्वात्मक रूप से अधिक सन्तुलित और उन्नत प्रतीत होती है। पर इसका कारण इन दो आचार्यों की प्रतिभा के बीच का फ़र्क़ नहीं था बल्कि यह था कि आइज़ेंस्ताइन ब्रेष्ट के मुक़ाबले अधिक उन्नत कला–विधा के क्षेत्र में काम कर रहे थे और इस नाते, अधिक उन्नत और सूक्ष्म धरातल की सैद्धान्तिक समस्याएँ उनके सामने ज़्यादा जल्दी मूर्त रूप में आकर खड़ी होनी ही थीं। दूसरे, यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमउम्र होते हुए भी आइज़ेंस्ताइन रूस की स्थितियों में मार्क्सवादी पहले बने और सामाजिक वर्ग–संघर्ष और सर्वहारा कला की पाठशालाओं में उन्हें जो घनीभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला वह ब्रेष्ट को नहीं मिला। लेकिन मुख्य बात यह है कि आइज़ेंस्ताइन बौद्धिकता और भावनात्मकता के द्वन्द्वात्मक संश्लेषण के नतीजे तक इसलिए जल्दी पहुँच सके कि अन्य सभी पूर्ववर्ती कलाओं को समाविष्ट कर लेने वाली तथा कला और विज्ञान के उन्नत संश्लेषण से निर्मित फ़िल्म विधा सर्वोन्नत कला–विधा है जो सर्वहारा संस्कृति और विचार के लिए सर्वाधिक अनुकूल है और इसी नाते, जैसाकि आइज़ेंस्ताइन ने स्वयं अपने सॉरबोन भाषण में कहा था : “…अकेली फ़िल्म–विधा ही इस महासंश्लेषण में सक्षम है। वही सक्षम है कि बुद्धि को उसके सक्रिय और ठोस भावनात्मक स्रोतों तक लौटा सके।”
दूसरा तथ्य जो ग़ौरतलब है, वह यह कि ब्रेष्ट चौथे दशक के उत्तरार्द्ध तक, भावना और तर्कबुद्धि के संश्लेषण के बारे में सोचने लगे थे और इस तरह की बातें करने लगे थे कि तर्कणा ही अनुभूति बन जाती है। “एपिक थिएटर” की अवधारणा आगे चलकर उन्हें अधूरी लगने लगी थी और वे “द्वन्द्वात्मक थिएटर” की बात करने लगे थे। यह समय था जब वे ‘कुछ चीज़ें जो स्तानिस्लाव्स्की से सीखी जा सकती हैं’ जैसे लेख लिख रहे थे। बहरहाल, यह चर्चा प्रसंगान्तर होगी। इसलिए इसे हम यहीं विराम देते हैं।
चौथा–पाँचवाँ दशक : आइज़ेंस्ताइन की अवधारणाओं में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन और कुछ प्रगति के वर्ष
पॉलिमिक्स में प्राय: ऐसा होता है कि प्रतिपक्ष से टकराते हुए एक सही अवस्थिति भी अक़सर दूसरे छोर पर जा खड़ी होती है। यह विचलन, इतिहास–पुरुषों के खण्डन–मण्डनात्मक लेखन तक में पाया जाता है।
कथा–फ़िल्मों की परम्परागत, विकासवादी विवरणात्मकता का विरोध करते हुए आइज़ेंस्ताइन ने जब अपनी मोन्ताज–शैली को विकसित किया तो एक तरह से प्रकृतवाद का विरोध करते हुए वे आलोचनात्मक यथार्थवादी परम्परा का निषेध करने के छोर तक जा पहुँचे।
दूसरी बात, आइज़ेंस्ताइन का यह सोचना सही था कि सर्वहारा सिनेमा में वह क्षमता और सम्भावना है कि वह कथा–सूत्र के पारम्परिक रूपबन्ध से मुक्त होकर जीवन के अन्तरतम लक्ष्य को अमूर्त सामान्य बिम्बावली में प्रकट कर सके। लेकिन महज़ सर्वहारा सिनेमा की इस क्षमता से यह तय नहीं हो जाता कि, समाजवादी समाज में भी, सभी सिने कृतियों से यह अपेक्षा पाली जाए। केवल समाजवादी समाज की उन्नत अवस्था में, जब मानसिक श्रम–शारीरिक श्रम के बीच का अन्तर तक मिट जाए, ऐसा हो पाएगा कि ‘दर्शन रहस्य नहीं रह जाएगा’, सिर्फ़ तभी कथात्मक सूत्र से विच्छेद कर चुका विचार–सिनेमा भी लोगों की कलात्मक–सौन्दर्यात्मक माँगों को भी पूरा कर सकेगा और सीधे अमूर्त विचार भी उन तक सम्प्रेषित कर सकेगा। समाजवाद की प्रारम्भिक अवस्थाओं की भौतिक स्थिति और जनता की चेतना के हिसाब से ‘अक्टूबर’ जैसी फ़िल्म फिर भी लम्बे समय तक उन्नत चेतना वाले दर्शकों को सम्बोधित बौद्धिक सिनेमा की श्रेणी में ही रहेगी। बेशक, ‘पोतेमकिन’ जैसी एजिटेशनल फ़िल्में आम जनता में ज़बर्दस्त रूप से लोकप्रिय होंगी लेकिन वे ‘लोकप्रिय सिनेमा’ का एकमात्र रूप नहीं हो सकतीं। स्वयं आइज़ेंस्ताइन के प्रमेय के आधार पर भी कहा जा सकता है कि ऐसी लोकप्रिय फ़िल्मों का भौतिक आधार और अनिवार्य आवश्यकता समाजवादी समाज में भी लम्बे समय तक बनी रहेगी जिनमें कथात्मक–नाटकीय सामग्री का भार अधिक हो और वैचारिक सामग्री या शिक्षामूलक सन्देश का भार कम हो।
तीसरी बात, बौद्धिकता और भावनात्मकता के द्वन्द्वात्मक संश्लेषण को लेकर। कोई भी द्वन्द्वात्मक संश्लेषण ऐसी स्थैतिक और निरपेक्ष प्रकृति का नहीं हो सकता जिसे हम सामान्य समीकरण के रूप में सभी कृतियों पर लागू कर दें। अनिवार्यत: कुछ कृतियों में बौद्धिकता का पहलू प्रधान होगा तो कुछ में भावनात्मकता का पहलू। उन्नत सामाजिक भौतिक आधार और उन्नत चेतना की बुनियादी पूर्वशर्त की मौजूदगी में ही, हम सामान्य सिने–कृति से भी यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वहाँ बौद्धिकता का भावनात्मक आवेग हो और भावना का बौद्धिक गुरुत्व, जहाँ तर्कणा एक अनुभूति हो और हर अनुभूति तर्कबुद्धिसंगत हो।
चौथी बात, जन समुदाय को नायक के रूप में प्रस्तुत करने का यह मतलब एकांगी है कि कलाकृतियों में व्यापक समूहों की गतिविधियों–क्रियाकलापों को ही प्रस्तुत किया जाए और प्रतिनिधि चरित्रों–नायकों को केन्द्र में रखकर उनके मनोजगत में चल रहे विचारों–भावनाओं के द्वन्द्व को उभारने तथा सामाजिक परिवर्तन की घटनाओं को मनोजगत के उक्त चित्रण के पृष्ठपट के रूप में प्रस्तुत करने की पद्धति का हर हाल में विरोध किया जाए। ‘इतिहास का निर्माण जनता करती है’-इस सूत्र को हृदयंगम करने के साथ ही वर्ग–समाज में नायक या नेतृत्व की भूमिका की अपरिहार्यता को भी समझना होता है। कलाकृति में जब कोई वास्तविक चरित्र या गढ़ा गया प्रतिनिधि चरित्र केन्द्रीय या महत्त्वपूर्ण पात्र के रूप में उपस्थित किया जाता है तो उसके माध्यम से भी आम दर्शक समाज–विकास की दिशा और अपने कार्यभारों के बारे में शिक्षित होता है क्योंकि उसका दिलो–दिमाग़ इस समाज में नायकों–प्रतिनिधियों से निर्देशित होने के लिए, प्रतीक–चिह्नों से उत्प्रेरित होने के लिए अनुकूलित होता है। जब तक समाजवाद की उच्चतर अवस्थाओं के उन्नत भौतिक आधार पर उसकी समष्टिगत चेतना अत्यधिक उन्नत नहीं होगी, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। इतिहास में व्यक्ति और जनता, व्यष्टि और समष्टि के द्वन्द्वात्मक अन्तर्सम्बन्धों की सही समझ के आधार पर इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। इसी लाइन पर सोचते हुए इस बात को भी समझा जा सकता है कि प्रतिनिधि चरित्रों के अन्तर्जगत के मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वों के चित्रण के माध्यम से भी हम सामाजिक जीवन के द्वन्द्वों को समझ सकते हैं क्योंकि अलग–अलग पात्रों के अन्तर्जगत के द्वन्द्व (उनकी वर्ग अवस्थिति के हिसाब से) भौतिक जगत के द्वन्द्वों के ही परावर्तित रूप होते हैं। यह कलात्मक–वैचारिक संज्ञान के मार्क्सवादी परावर्तन सिद्धान्त के सर्वथा अनुरूप है।
चौथे दशक में, यूरोप और अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद, आइज़ेंस्ताइन अपनी पूर्व मान्यताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ठोस बनाने के साथ ही उनके अतिरेकी छोरों के बारे में भी गम्भीरता से सोच रहे थे। उस समय तक पुदोवकिन, दोवझेंकों आदि दर्ज़नों निर्देशकों की सोवियत क्रान्ति और समाजवादी निर्माण के दौर पर बनी कथानक–प्रधान फ़िल्मों की जो व्यापक लोकप्रियता थी तथा ये फ़िल्में आम जनता की शिक्षा और नई समाजवादी संस्कृति के निर्माण में जो भूमिका निभा रही थीं, उन वास्तविकताओं पर आइज़ेंस्ताइन ने ग़ौर किया। ‘प्लॉट’ और कथानक की परम्पराओं को पूरी तरह खारिज करने पर तथा व्यक्तिगत नायक की जगह समूह की प्रस्तुति पर उनका जो अतिरेकपूर्ण बल था, उसे उन्होंने सुधारने की कोशिश की। 1934 में उन्होंने पुनर्विचार की अपनी प्रक्रिया को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी :
“साहित्य की नई क़िस्म की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए–विषय का नाट्यशास्त्र-सिनेमा अपने प्रारम्भिक दौरों के ज़बर्दस्त अनुभवों को कभी भुला नहीं सकता। लेकिन रास्ता अब पीछे उनकी ओर नहीं जाएगा, बल्कि आगे, हमारे मूक सिनेमेटोग्राफ़ी के दौर में जो कुछ भी सर्वोत्कृष्ट हुआ, उसके संश्लेषण की ओर, आज के तकाज़ों के साथ उसके संश्लेषण की ओर जाएगा, यह कथावस्तु और मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचारधारात्मक विश्लेषण की लाइनों पर आगे बढ़ेगा। यह समाजवाद के युग की जनता के बिम्बों के स्मारकीय संश्लेषण का दौर है-समाजवादी यथार्थवाद का दौर है।” (आइज़ेंस्ताइन : ‘फ़िल्म फॉर्म’, मेरिडियन बुक्स, 1957, पृ. 17)
पुन: 1935 में, आइज़ेंस्ताइन ने अपनी पूर्व–धारणाओं में संशोधन को इस रूप में प्रस्तुत किया :
“आन्दोलन और जनसमुदाय के अनुभव के पूर्ववर्ती सर्वसमावेशी जनसमष्टिगत बिम्ब–विधान के बाद, अब इस दौर में व्यक्तिगत वीरोचित चरित्रों को उपस्थित करने की शुरुआत करनी होगी। उनके उपस्थित होने से उन कृतियों में भी संरचनागत परिवर्तन आया है जिनमें वे प्रस्तुत हुए हैं। पूर्ववर्ती “एपिकल” गुण और उनके अभिलाक्षणिक विराट पैमाने का भी ऐसी संरचनाओं में संकुचन होने लगा है, जो शब्द के संकीर्ण–अर्थ में, वस्तुत: अधिक परम्परागत क़िस्म की नाट्य–विधा के निकटतर हैं…
यह इत्तफाक नहीं है कि ख़ास तौर पर इस अवधि के दौरान, पहली बार हमारी सिनेमेटोग्राफ़ी में व्यक्तित्वों के, और न सिर्फ़ व्यक्तित्वों के, बल्कि नेतृत्वकारी व्यक्तित्वों के : कम्युनिस्ट और बोल्शेविक नेतृत्व के अग्रणी चरित्रों के, परिष्कृत बिम्ब उपस्थित हो रहे हैं…” (उपरोक्त, पृ. 123.124)
आइज़ेंस्ताइन की इन स्फुट उक्तियों से यह भी लगता है कि कथात्मक सूत्रों, व्यक्तिगत नायकों और उनके मनोवैज्ञानिक–भावनात्मक द्वन्द्वों के चित्रण वाली, परम्परागत रूपबन्ध वाली फ़िल्मों की आवश्यकता को वे काफ़ी हद तक समाजवाद के तत्कालीन विशेष दौर की उपज अैर आवश्यकता मान रहे थे। लेकिन इतना तय है कि अपनी पूर्वस्थापना के मूल सूत्रों पर क़ायम रहते हुए, सहायक निष्कर्षों और उपप्रमेयों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।
यह इतिहास का एक तथ्य है, और आइज़ेंस्ताइन के कला–चिन्तन के खुले–अधूरे सिरों पर ग़ौर करते हुए किसी नतीजे तक पहुँचने की प्रक्रिया में इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तत्कालीन सोवियत मार्क्सवादी हलकों में व्याप्त यांत्रिक भौतिकवादी विचलन के प्रभाव में, कला–साहित्य के क्षेत्र में समाजवादी यथार्थवादी का जो अति सरल–सपाट संस्करण हावी था और मुख्य धारा पर प्रकृतवाद और प्रत्यक्षवाद की जो विच्युतियाँ हावी थीं, उनके चलते कई प्रयोगधर्मा और अन्वेषी प्रकृति के कलाकारों–लेखकों को भी समाजवाद–विरोधियों की कतारों में खड़ा कर दिया गया था या उन पर रूपवादी भटकाव की तोहमत लगा दी गई थी। यह अलग से एक गम्भीर सवाल है। इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में हावी नौकरशाही की भी एक भूमिका थी। तीसरे दशक में भी, मक्सिम गोर्की और अन्तोन मकारेंको तक को इस नौकरशाही का कोप झेलना पड़ा था, लेकिन तब इसके विरोध का प्रबल स्वर भी मौजूद था। स्तालिन की युगनिर्मात्री भूमिका और उस दौर की महान उपलब्धियों को स्वीकारते हुए भी हम माओ त्से–तुङ और चीन की पार्टी द्वारा प्रस्तुत आलोचना से अर्जित दृष्टि से यह मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। कला–साहित्य के बुनियादी मसलों पर खुली लम्बी बहसों के बाद (जैसी परम्परा सोवियत संघ में तीसरे दशक तक और फिर माओकालीन चीन में रही) विरोधी धाराओं की आलोचना और “एक्सपोज़र” के बजाय, शासकीय निर्देशों के हिसाब से सृजन, और शीर्ष नेतृत्व द्वारा आलोचना से एकबारगी सबकुछ तय कर दिए जाने की पद्धति ने भी सोवियत कला के शानदार विकास के रास्ते में कुछ अड़चनें पैदा कीं और इससे बुर्जुआओं और त्रात्स्कीपन्थियों को उल्टे–सीधे प्रचार का मौक़ा भी ख़ूब मिला। हम समझते हैं कि चीन की सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की आम कार्यदिशा के आलोक में अतीत के इस दौर का समाहार ज़रूरी है ताकि आइज़ेंस्ताइन जैसे विचारक सर्जकों के चिन्तन को सही परिप्रेक्ष्य में देखा–समझा जा सके।
चौथे दशक में आइज़ेंस्ताइन पर जब “रूपवादी” भटकाव के आरोप लग रहे थे तो ‘अक्टूबर’ के साथ ‘पोतेमकिन’ को भी इस लपेट में ले लिया गया था। छह दिनों तक चली ‘ऑल यूनियन कान्फ्रेन्स ऑफ सिनेमेटोग्राफ़िक वर्कर्स’ में जब लगातार, एक स्वर से आइज़ेंस्ताइन की आलोचना हो रही थी, तो एकमात्र लेव कुलेशोव थे जिन्होंने खुलकर उनका बचाव किया।
1935 के मध्य में आइज़ेंस्ताइन ने ‘बेझिन मीडो’ फ़िल्म पर काम शुरू किया। फ़िल्म जब पूरी होने को थी, तभी उसे रोक दिया गया। ‘प्रावदा’ में लेख लिखकर सोवियत फ़िल्म प्रोडक्शन के नये अध्यक्ष शुम्यात्स्की ने (जो कुछ ही महीनों बाद, गम्भीर आलोचना के बाद हटा दिए गए) आइज़ेंस्ताइन पर यह आरोप लगाया कि वे यथार्थ के रंगों और शौर्य से कट गए हैं और सशक्त, सरल, प्रत्यक्ष चित्रण वाली फ़िल्म बनाने के बजाय रूपवादी प्रयोगों में उलझे हुए हैं। वह अधूरी फ़िल्म कभी सामने आई ही नहीं, इसलिए अन्तिम निर्णय के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आइज़ेंस्ताइन की अन्य फ़िल्मों की आलोचनाओं की सतही यांत्रिकता के आधार पर, इस आलोचना को भी शंका की दृष्टि से अवश्य देखा जा सकता है।
रचना–कर्म का आख़िरी पड़ाव : ‘अलेक्सान्द्र नेव्स्की’ और
‘इवान दि टेरिबल’
एक फ़िल्मकार के रूप में आइज़ेंस्ताइन के छोटे से जीवन का आधे से भी अधिक हिस्सा अधूरी, स्थगित और खण्डित परियोजनाओं की त्रासद गाथा मात्र था। उनकी अधूरी फ़िल्मों के बचे–खुचे प्रिण्ट्स का यदि कभी अध्ययन हुआ तो सर्वहारा सिनेमा के अग्रवर्ती विकास की दृष्टि से, निश्चित ही, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बीच–बीच में आइज़ेंस्ताइन मायूस भी होते रहे और फ़िल्म–निर्माण से विरत होकर अध्ययन–अध्यापन–लेखन में ज़्यादातर समय लगाते रहे। इस त्रासद स्थिति का सकारात्मक पक्ष यह है कि उनका लिखा हुआ काफ़ी कुछ प्रकाशित रूप में आज हमारे सामने मौजूद है और अब भी अप्रकाशित सामग्री का विपुल भण्डार ‘आइज़ेंस्ताइन अभिलेखागार’ में पड़ा हुआ है, जिसे विश्वव्यापी सर्वहारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण–प्रबोधन के नये दौर में सामने लाया जाना है और जिसका नये सिरे से, गहन आलोचनात्मक विवेक के साथ अध्ययन किया जाना है।
पचास साल की अल्पायु में मृत्यु से पहले आइज़ेंस्ताइन ने ऐतिहासिक विषय–वस्तु पर दो भव्य फ़िल्में बनार्इं-‘अलेक्सान्द्र नेव्स्की’ और ‘इवान दि टेरिबल’ (दो खण्डों में)।
1937 में सोवियत संघ पर जर्मन फ़ासिस्ट आक्रमण का ख़तरा आसन्न था। यह भी तय ही था कि पश्चिमी साम्राज्यवादी फ़ासिस्टों के हाथों समाजवाद को नेस्तनाबूद कर दिए जाने की हार्दिक आकांक्षा रखते थे और उनसे किसी तरह के सहयोग की अपेक्षा तब तक नहीं की जा सकती थी जब तक कि स्वयं उन्हीं का अस्तित्व ख़तरे में न पड़ जाए। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ की जनता की देशभक्ति की भावना जागृत करके प्रतिरोध संगठित करने के लक्ष्य को कला–साहित्य के मोर्चे पर भी केन्द्रीय कार्यभार बना दिया गया था। आइज़ेंस्ताइन की यह नई फ़िल्म तेरहवीं शताब्दी के प्रिंस अलेक्सान्द्र नेव्स्की की शौर्यपूर्ण गाथा पर केन्द्रित थी जिसने बर्बर ट्यूटोनिक आक्रान्ताओं का मुक़ाबला करने के लिए रूसी किसानों की एक सेना खड़ी की थी। कला की दृष्टि से यह फ़िल्म अत्यन्त भव्य और प्रभावशाली थी। फ़िल्म के क्लाइमेक्स में जमी हुई झील की सतह पर युद्ध का वह ऐतिहासिक दृश्य था जिसमें बर्फ़ की सतह के टूटने और अपने ही शस्त्रास्त्रों के बोझ से दुश्मन के सैनिकों के डूबते जाने का वह प्रसिद्ध लाक्षणिक दृश्य फ़िल्माया गया था जो जनता के प्रतिरोध के अथाह जल में हथियारों के जखीरों सहित तमाम हमलावरों के डूबते जाने का रूपक प्रस्तुत करता था।
लेकिन इस महाकाव्यात्मक गाथा को फ़िल्माते हुए आइज़ेंस्ताइन “संघात” या “टकराव” (Collision) की अपनी पूर्ववर्ती अवस्थिति को छोड़कर लगभग पूरी तरह सहलग्नता (Linkage) की पुदोवकिन वाली अवस्थिति पर जा खड़े हुए थे और उद्भावनामूलक मोन्ताज को यहाँ कथा–सूत्र की विवरणात्मकता ने पूरी तरह से विस्थापित कर दिया था। पर देशभक्ति की सामान्य अन्तर्वस्तु के इस सिनेमाई भव्यता वाले रूपाकार में भी आइज़ेंस्ताइन ने द्वन्द्वात्मक पद्धति विषयक कुछ नये–नये प्रयोग करने का रास्ता निकाल ही लिया। यहाँ, मोन्ताज की पूर्ववर्ती सोच से अलग हटकर आइज़ेंस्ताइन ने विरुद्धों की एकता और संघर्ष के ज़रिए कथा को आगे बढ़ाने और सन्देश को सम्प्रेषित करने की तकनीक को लेकर कुछ नये प्रयोग किए। इस फ़िल्म में प्राय: ध्वनि और चित्र को एक–दूसरे के सामने विरोधी रूप में प्रस्तुत करते हुए विचार सम्प्रेषित किया गया है। प्रत्येक फ्रेम और सीक्वेंस की संरचना को विखण्डित करके उनके आन्तरिक अन्तरविरोध की पड़ताल की गई है।
लेकिन इन पद्धतिगत प्रयोगों की नवीनता के बावजूद इस फ़िल्म की विचारधारात्मक–राजनीतिक अवस्थिति कई प्रश्नचिह्न खड़े करती है। फ़ासिस्टों के प्रतिरोध के आसन्न दबाव के तहत रूसी जनता की देशभक्ति की जिस भावना पर बल दिया गया है, वह सर्वहारा राज्य, समाज और संस्कृति के लिए कितना उपयुक्त है, यह सोचने की बात है। दरअसल यह सवाल आइज़ेंस्ताइन की सोच का नहीं बल्कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की तद्विषयक कार्यदिशा का है। ध्यान दें कि नवजात सोवियत संघ पर अठारह साम्राज्यवादी–पूँजीवादी देशों के हमले, घेरेबन्दी और तोड़फोड़ के प्रतिरोध के लिए जनता को गोलबन्द करते समय लेनिन का ज़ोर हमेशा ही “रूसी पितृभूमि” या “समाजवादी पितृभूमि” के बजाय “विश्व सर्वहारा के एक आधार” की हिफ़ाज़त पर होता था और साम्राज्यवादी आक्रमण को भी जनता के सामने वर्ग–संघर्ष के एक रूप के तौर पर ही प्रस्तुत किया जाता था। स्तालिन काल में फ़ासिस्टों के प्रतिरोध के लिए हर तरह से रूसी जनता की देशभक्ति पर, और अतीत के ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रेरणा पर, विशेष ज़ोर दिया गया। “वर्गों” की जगह यहाँ “रूसी जनता” पर पूरा ज़ोर था। जनता की देशभक्ति की पुरानी भावना का कार्यनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस पर मुख्य ज़ोर सर्वहारा अन्तरराष्ट्रीयतावाद से एक वैचारिक विचलन था। ‘अलेक्सान्द्र नेव्स्की’ एक भव्य, जनपक्षधर फ़िल्म होते हुए भी इस विचलन की गवाही देने वाला एक चाक्षुष दस्तावेज़ है, हालाँकि इसके लिए आइज़ेंस्ताइन की मुख्य ज़िम्मेदारी नहीं मानी जा सकती है।
कमोबेश यही बात आइज़ेंस्ताइन की अन्तिम फ़िल्म ‘इवान दि टेरिबल’ के बारे में भी कही जा सकती है। एक महान राष्ट्रीय नायक के बारे में यह एक भव्य, महाकाव्यात्मक फ़िल्म, लेकिन “राष्ट्रवाद” की फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के पहले भाग में इवान को एक त्रासद चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो एक ओर अपनी मानवीय संवेदना और दूसरी ओर उन निर्मम कामों, जिनको उसे अंजाम देना पड़ता है, के तनाव के बीच लगातार खिंचा रहता है। इस तरह आइज़ेंस्ताइन ने इस फ़िल्म में भी, मूल कथ्य के साथ–साथ एक ऐसा शाश्वत मानवीय प्रश्न उपस्थित करने की कोशिश की, जो इसे क्लासिकी कृतियों का कालजयी महत्त्व प्रदान करता है। सोचा जाए तो क्या यही प्रश्न एक उन्नत धरातल पर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं रहते, जिन्हें उदात्त मानवीय लक्ष्यों की ख़ातिर, वर्ग–संघर्ष के दौरान कई बार बेहद निर्मम फ़ैसले भी लेने पड़ते हैं?
इस फ़िल्म का पहला भाग जब रिलीज़ हुआ तो विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था। दूसरा भाग 1946 में पूरा हुआ। अब किसी विदेशी आक्रान्ता के विरुद्ध देशभक्ति की भावनाएँ के उभाड़ने की वैसी फ़ौरी ज़रूरत नहीं थी, हालाँकि यह भी सच है कि शीतयुद्ध का दौर शुरू हो चुका था। इन स्थितियों में आइज़ेंस्ताइन ने इतिहास का कलात्मक पुनसृजन करते हुए, राजनीतिक संघर्ष की वर्गीय संरचनाजन्य जटिलताओं–समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक कोशिश थी। उन्होंने, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, इवान के चरित्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि बोयारों के विरुद्ध संघर्ष में इवान द्वारा उठाए गए क़दम आगे चलकर उसके नियंत्रण से बाहर हो गए, वह मतिभ्रम का शिकार हो गया और ‘ओप्रिच्निकी’ नाम से प्रसिद्ध जिन युवा सैनिकों के दस्तों ने बोयारों को निर्ममता से कुचलने का काम किया, अब वे स्वयं समस्या बन चुके थे। देखा जाए तो प्रगतिशील से प्रगतिशील शासक की वेतनभोगी सेना की यह नियति–परिणति नितान्त स्वाभाविक है। लेकिन आइज़ेंस्ताइन की इस बात के लिए पार्टी द्वारा कठोर आलोचना हुई कि उन्होंने इतिहास को ग़लत ढंग से प्रस्तुत किया तथा प्रगतिशील भूमिका निभाने वाले इवान और उसके सैनिकों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इस आलोचना में भी “राष्ट्रवादी देशभक्ति” का राजनीतिक विचलन मौजूद है। पर इसकी विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव नहीं है।
आइज़ेंस्ताइन के रचनात्मक प्रयोगों की जो आलोचनाएँ हुर्इं और उन पर जो बहसें हुर्इं, वह तो स्वाभाविक थीं। इनके बिना कोई रचनात्मक प्रयोग हो ही नहीं सकता। लेकिन यह प्रश्न ज़रूर है कि समाजवादी समाज में कला–साहित्य के क्षेत्र में आलोचना–प्रतिबन्ध आदि का एकतरफ़ा अधिकार तंत्र के पास होना चाहिए या पार्टी के विचारधारात्मक मार्गदर्शन में लम्बी और खुली बहस के बाद किसी नतीजे तक पहुँचा जाना चाहिए और फिर अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए और बुरी चीज़ों का भण्डाफोड़ करके जनता के सचेत हिस्से को साथ लेकर प्रतिबन्ध आदि जैसे क़दम उठाए जाने चाहिए? यह कला के क्षेत्र में सर्वहारा जनवाद की आम नीति का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हमने आइज़ेंस्ताइन के सिद्धान्त और प्रयोगों की चर्चा करते हुए इस प्रश्न पर भी थोड़ी चर्चा कर ली है। इस सन्दर्भ में चीन की पार्टी की “सौ फूलों को खिलने दो और हजारों चिन्तन–धाराओं को परस्पर टकराने दो” की नीति का और सांस्कृतिक क्रान्ति के प्रयोगों और शिक्षाओं का अध्ययन भी उपयोगी होगा।
फ़िल्म–निर्माण की ठोस और विशिष्ट समस्याओं के अतिरिक्त सामान्य सौन्दर्यशास्त्रीय अवधारणाओं और कलात्मक सृजन की आधारभूत समस्याओं से जुड़ी हुई एक अति समृद्ध सैद्धान्तिक विरासत सेर्गेई आइज़ेंस्ताइन अपने बाद की पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं। यहाँ हमने ख़ास तौर पर फ़िल्म–विषयक चिन्तन के उन अंशों पर चर्चा की है जो अब तक सामने आ चुके हैं। अभी इस विषय पर भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो सामने ही नहीं आया है। इसके अतिरिक्त साहित्य, कला, दर्शन और सौन्दर्यशास्त्र के प्रश्नों पर भी उन्होंने विपुल मात्रा में मौलिक लेखन किया है जिसे सामने लाया जाना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सर्वहारा संस्कृति के सर्जक इतिहास के पुनरान्वेषण–सम्बन्धी अपने कामों में इस काम को भी ज़रूरी समझकर शामिल करेंगे।
- सृजन परिप्रेक्ष्य, जनवरी-अप्रैल 2002