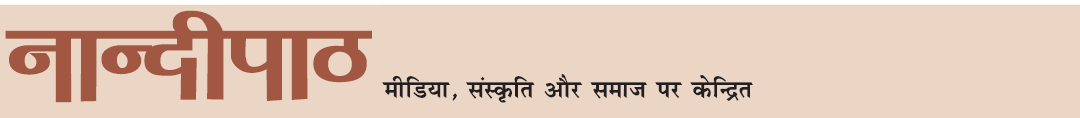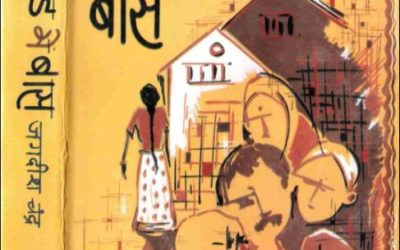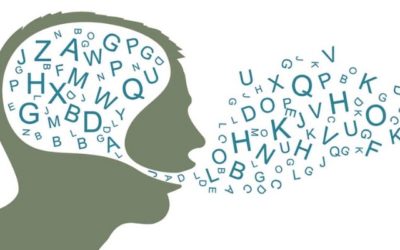गुजरात नरसंहार और “महान भारतीय मध्यवर्ग” का फ़ासीवादी चेहरा
महताब
गुजरात में अल्पसंख्यकों के सफ़ाए की फ़ासीवादी मुहिम के पहले दौर में, जब मुस्लिम व्यापारियों की दूकानों पर पुलिस के संरक्षण पर विहिप और बजरंग दल के गुण्डा गिरोहों ने धावा बोला तो लूटपाट में अभिजात मध्यवर्ग के लोगों ने जमकर हिस्सा लिया।
सिएलो, ज़ेन और मित्सुबिशी लांसर में भरकर समृद्ध परिवारों के स्त्री–पुरुष भागते हुए बाज़ारों में पहुँचे और जलाए जाने से पहले, दूकानों से जितना सामान उठा सकते थे, उठाकर भागे। पुरुष टी–वी–, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि लाद रहे थे। “कुलीन” स्त्रियाँ ओवन, जूतियाँ, सौन्दर्य प्रसाधनों और कपड़ों के बण्डलों से लदी–फदी एक–दूसरे पर गिरती–पड़ती भाग रही थीं।
यह गुजरात के ही नहीं, पूरे भारत के उस कुलीन मध्यवर्ग की अन्तरात्मा का असली चेहरा था जो जलती हुई लाशों की चिरायन्ध के बीच, बाज़ार से उपभोग, फ़ैशन, विलासिता और रौनक के सामानों की लूट का जश्न मना रहा था। यह दिन में दफ्तरों में अफ़सरी करने और बहुप्रचारित सामाजिक कार्यों में लगा रहने वाला और रात में पार्टियों तथा फ़ार्महाउसों में रंगरेलियाँ मनाने वाला वह कुलीन उपभोक्ता समुदाय था, जो इस बुर्जुआ व्यवस्था का मेरुदण्ड है, जो बहुसंख्यक उत्पादक जनता को ग़ुलाम और पशु से अधिक कुछ नहीं समझता। यह परजीवी–परभक्षी वर्ग, समाज में पर्दे के पीछे जारी लूट का भागीदार तो हमेशा से रहा हे। फिर जब खुली लूट का एक सुनहरा अवसर हाथ आया तो बहती गंगा में हाथ धोने से भला यह क्यों चूकता। मौक़ा आते ही, सोसाइटी का यह फ़ैशनेबल, ‘सभ्य–सुसंस्कृत तबका” लालची लुटेरों की अराजक भीड़ में तब्दील हो गया।
गुजरात–काण्ड का यह पहलू दरअसल खुले बाज़ार के सांस्कृतिक महोत्सव का एक प्रतिनिधि दृश्य था। यह ऐसा दृश्य था जो भारतीय मध्यवर्ग के ऊपरी हिस्से की सामान्य सामाजिक भूमिका को, उसके आचार–विचार और संस्कृति को सान्द्र, ‘कण्डेन्स्ड’ फॉर्म में प्रस्तुत करता था। यह “महान भारतीय मध्यवर्ग” की महागाथा का एक नया अध्याय था। यह रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक–नैतिक पतनशीलता को मात देने वाली इक्कीसवीं सदी के बुर्जुआ भारतीय समाज के सत्ताधारियों के दरबारियों की पतनशीलता का एक प्रतिनिधि दृश्य था। इस दृश्य के निहितार्थ को समझकर हम ऊपर की उस बीस करोड़ आबादी के जीवन–दर्शन को समझ सकते हैं जो आँसू और रक्त के सागर में निर्मित ऐश्वर्य और विलासिता के द्वीपों पर निवास करती है। सोचने का अहम मुद्दा यह भी है कि प्रगतिशील होने का दम भरने वाले जो बुद्धिजीवी, सत्ता से नाभिनालबद्ध इन रक्तपायी लोगों के साथ ही उठते–बैठते हैं, वे कहाँ खड़े हैं और उनकी ‘पॉलिटिक्स’ क्या है?
इसी प्रसंग में, एक राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र में प्रकाशित वह रिपोर्ट भी ग़ौरतलब है जिसमें इस तथ्य की विस्तार से चर्चा की गई है कि गुजरात को हिन्दुत्व की प्रयोगशाला बनाने की लम्बे समय से जारी मुहिम में आप्रवासी गुजराती धनिकों-व्यवसाइयों और नौकरीपेशा लोगों की आर्थिक सहायता की कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ये वे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और आराम की ज़िन्दगी के लिए पश्चिम के नन्दन–कानन में जा बसे, लेकिन वहाँ की ज़िन्दगी से कटे–छँटे अपने पुरातनपन्थी विचारों और संस्कृति से चिपके रहे। पश्चिमी जीवन की पतनशीलता का कचरा और सिक्के तो इन्होंने ख़ूब बटोरे, पर वहाँ के आम सामाजिक जीवन में जिस हद तक भी इतिहास–प्रसूत तर्कणा और जनवाद के मूल्य बचे हुए हैं, उनसे अपने को पूरी तरह बचाए रखा। पश्चिम की सड़कों पर जब मज़दूरों, आप्रवासी ग़रीबों, अश्वेतों और स्त्रियों के हुजूम अपने अधिकारों के लिए आन्दोलित होकर उमड़ते हैं, उस समय ये वहाँ बनाए गए मन्दिरों में भजन–कीर्तन करते होते हैं या फिर अपने अपार्टमेण्ट्स में बैठे आसाराम बापू और मुरारी बापू के प्रवचनों के वीडियो कैसेट्स सुनते होते हैं। मलाल इन्हें इस बात का ज़रूर रहता है कि तमाम सुख–सम्पदा के बावजूद, पश्चिमी देशों के नागरिक इन्हें हिक़ारत की निगाह से देखते हैं। ऐसे में, जड़ों से कटे हुए इन स्वार्थी भगोड़ों के लिए हिन्दुत्व श्रेष्ठता–बोध और अस्मिता की पहचान की एक मिथ्याभासी चेतना का काम करता है, लेकिन वास्तव में वह इनकी हीनता–ग्रंन्थि होती है। यही वे लोग हैं जो अयोध्या में राममन्दिर निर्माण के लिए और हिन्दुत्व के प्रचार–प्रसार के लिए विहिप को पिछले दस–बारह वर्षों से लगातार करोड़ों रुपये का सालाना चन्दा भेजते रहते हैं। इनकी निश्चिन्तता का एक कारण यह भी है कि हिन्दू राष्ट्र बनाने के नाम पर संघ परिवार यदि पूरे देश को गृहयुद्ध की आग में भी झोंक दे तो उसकी आँच इन तक नहीं पहुँचने वाली है। यूरोप में जो दक्षिणपन्थी ताकतें तीसरी दुनिया के आप्रवासियों के ख़िलाफ़ नस्लवादी–रंगभेदवादी मुहिम चलाती रहती हैं, उनके शिकार भी मुख्यत: मज़दूर, निम्नमध्यवित्त तबके के नौकरीपेशा लोग और छात्र ही होते हैं। लेकिन उससे धनी आप्रवासियों में भी भय का संचार होता है। इस मनोविज्ञान के चलते भी उनमें “शक्तिशाली हिन्दू राष्ट्र” के निर्माण के नारे के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। भारतीय आप्रवासियों का जो हिस्सा अकादमिक क्षेत्र में काम करता है, वह अपने हमपेशा लोगों के साथ काफ़ी हद तक घुला–मिला जीवन बिताता है और उसी का एक हिस्सा ऐसा भी है जो स्थानीय जनवादी आन्दोलनों में हिस्सा लेता है तथा भारत में साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। पर ऐसे बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत कम है।
मध्यवर्ग के बड़े हिस्से के ऐसे घोर प्रतिक्रियावादी हो जाने के पीछे गुजराती समाज की विशिष्ट संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी भूमिका है। सूरत और अहमदाबाद जैसे औद्योगिक केन्द्रों के बावजूद गुजरात में वाणिज्यिक पूँजी का तथा व्यापारी और मध्य तबके का बोलबाला है। गुजराती व्यवसायी काफ़ी लम्बे समय से विदेशों तक जाकर कारोबार करते रहे हैं और अमेरिका तथा कई अफ्रीकी देशों में इनकी ख़ासी तादाद है। वाणिज्यिक पूँजी से जुड़े व्यापारी तथा मध्य तबके के बीच ग़ैरजनतांत्रिक मूल्यों के हावी होने के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, हम बस इस बात को रेखांकित कर रहे हैं।
सामान्यत: लोग गुजराती मध्यवर्ग की जिस व्यावसायिक उद्यमशीलता की तारीफ़ करते नहीं अघाते, मूल्यों–विचारों के धरातल पर वही उसके नकारात्मक पक्ष का आधार है। व्यावसायिक हित के तकाज़े से वे आम जीवन में विनम्र और धर्मभीरु प्रतीत होते हैं। लेकिन इन धर्मप्राण व्यवसाइयों की अन्तरात्मा में गहराई में घोर मानवद्रोही मूल्य बैठे होते हैं। वे ग़रीब जो इनके सामान ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते वे इनके लिए मानो इन्सान ही नहीं होते। मेरे दफ्तर के जो चन्द–एक लोग गुजरात के क़त्लेआम को सही ठहराने की संघी दलीलों के समर्थक हैं, उनमें से एक महिला सहकर्मी ने आन्ध्र प्रदेश में गर्मी से लोगों के मरने की ख़बरों पर मुँह बिचकाकर कहा कि जाने क्यों अख़बारवाले ये सब ख़बरें देते हैं। गर्मी से तो ज़्यादातर भिखारी या सड़कछाप लोग मरते हैं; उनके जीने–मरने से क्या फ़र्क़ पड़ता है? ये मध्यवर्ग के एक अच्छे–ख़ासे हिस्से के प्रतिनिधि विचार हैं। व्यापारिक पूँजी की बहुलता–प्रचुरता वाले गुजराती समाज में ही मुरारी बापू, आसाराम बापू और तमाम अन्य स्वामी सम्प्रदाय क्यों पनपे, इसे भी समझना कठिन नहीं है।
गुजरात के दंगों की एक नई बात यह भी है कि इनकी लपटें गाँवों तक पहुँच गर्इं। राज्य के 1200 गाँव इससे प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात, इन दंगों में पिछड़ी जातियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। यह चिन्ताजनक है पर आश्चर्यजनक नहीं। जिन भी देशों में धीमी गति से भूमि सुधार लागू हुए वहाँ कुलक सबसे कम जनतांत्रिक वर्ग रहा है। भारत जैसे पिछड़े देशों में तो कुलकों की भूमिका बहुत प्रतिक्रियावादी रही है। दलितों–स्त्रियों का ये बर्बर उत्पीड़न करते रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मध्य जातियों से उभरे कुलकों ने दलितों–स्त्रियों–खेतिहर मज़दूरों के दमन–उत्पीड़न के मामले में सवर्णों को भी पीछे छोड़ दिया है।
गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य जातियों के कुलकों का बोलबाला है। पाटीदार (पटेल) आज़ादी के पहले से ही सम्पन्न थे और कोली, भील तथा अन्य निम्नक्षत्रिय जातियों में ’47 के बाद समृद्धि आई और इनका राजनीतिक–सामाजिक प्रभाव भी बढ़ा। दुग्ध उत्पादन सहकारियों से जुड़े तथा मूंगफली, कपास, गन्ना, तम्बाकू आदि नक़दी फसलों का बाज़ार के लिए उत्पादन करने वाले गुजरात के सम्पन्न किसान आज महज़ किसान नहीं रह गए हैं। इनके ऊपरी तबके का सहकारी व सरकारी ऋणदाता समितियों पर कब्जा है, कृषि उपकरणों, खाद–बीज आदि का व्यापार इनके पास है-ये बड़ी उद्यमी बन चुके हैं। शहर के व्यापारियों–उद्योगपतियों से इनके सम्पर्क–सूत्र जुड़े हैं। मध्यम किसानों की प्रकृति भी देश के अन्य इलाक़ों के मुक़ाबले शहरी मध्यवर्ग के ज़्यादा क़रीब है। (गुजरात में शहरीकरण की रफ्तार भी बाक़ी देश से कहीं तेज़ रही है। वहाँ शहरों–क़स्बों की संख्या 1947 में 100 से बढ़कर आज 260 हो चुकी है।) इनकी फ़ासीवाद से निकटता और संघ परिवार की ग्रामीण इलाक़ों में पैठ का यही आधार है।
दूसरे, पिछड़ी जातियों का उभार तो गुजरात में हुआ पर उसमें ब्राह्मणवाद–विरोध का कोई तत्त्व नहीं था। कुछ धार्मिक सम्प्रदायों के नेतृत्व में संगठित पिछड़ी जातियों ने ऊपर उठने के लिए संस्कृतीकरण का रास्ता अपनाया। ख़ुद को ज़्यादा कट्टर हिन्दू दिखाने की जो प्रवृत्ति देश के कई इलाक़ों में मध्य जातियों में बढ़ी है, उसका असर गुजरात में कुछ ज़्यादा ही है।
मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगों में पिछड़ों और दलितों के इस्तेमाल की बात एक साथ करना ठीक नहीं है। पिछड़ी जातियों में हिन्दुत्ववादी शक्तियों की गहरी पैठ हो चुकी है जिसका एक स्पष्ट वर्गीय और सांस्कृतिक आधार है। गाँवों से मुसलमानों को बेदखल कर उनकी सम्पत्ति और कारोबार पर कब्जा भी एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय कारण है। लेकिन दलितों–आदिवासियों की स्थिति इससे भिन्न है। इनके आर्थिक रूप से सम्पन्न और मध्यवर्गीय तबकों में संस्कृतीकरण की प्रक्रिया ने ज़ोर मारा है। सामाजिक समरसता की बातें करते हुए इस प्रक्रिया को निचले तबकों में ले जाने की कोशिश में आर.एस–एस– जुटा है। चिकित्सा शिविर, स्वरोज़गार जैसे अनेक सुधार कार्यक्रमों की आड़ में संघी कार्यकर्ता दलितों–आदिवासियों के बीच हिन्दुत्व के विचारों का प्रचार करने और उनकी पिछड़ी चेतना का लाभ उठाकर तमाम क़िस्म की अफ़वाहें फैलाने और ख़तरनाक मिथकों को उनके दिमाग़ में बैठाने में लगे हैं। इसके बावजूद दलितों–आदिवासियों के एक अत्यन्त छोटे हिस्से ने ही लूटमार में हिस्सा लिया। ये वह लोग थे जिनके हित किसी न किसी प्रकार से संघ परिवार से जुड़ चुके हैं। उनके बीच पैसे और शराब बाँटने की भी ख़बरें आई हैं।
गुजरात में पूँजीवादी विकास और विदेशी पूँजी–निवेश के पीछे की सच्चाई यह है कि यह रोज़गारविहीन विकास है। वैसे 1980 के दशक के बाद से उद्योग और खेती दोनों की विकास दर में गिरावट आई है। इसने बड़ी तादाद में बेरोज़गारों और लम्पट सर्वहाराओं को जन्म दिया है जिनका इस्तेमाल फ़ासीवाद हमेशा ही करता है। गोर्की के शब्दों में, फ़ासिस्टों की भीड़ में सचेत हत्यारों के चन्द स्वस्थ–चमकते चेहरों के पीछे पीले–बीमार चेहरे और रुग्ण–मन वाले युवाओं की उन्मत्त भीड़ का बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। आर्थिक मन्दी से पैदा हुए सामाजिक विक्षोभ को सही दिशा देने वाले रैडिकल आन्दोलनों की अनुपस्थिति ने इसे जातिगत और साम्प्रदायिक घृणा के रास्तों पर मोड़ने का संघ परिवार का काम आसान किया है।
गुजरात की स्थितियाँ कई मायनों में विशिष्ट हैं, पर यह भी सच है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इन स्थितियों के पैदा होने की ज़मीन पक रही है। गुजरात में भारतीय मध्यवर्ग की महागाथा का ही एक नया अध्याय जुड़ा है। याद करें कि काफ़ी पहले, तीस के दशक में, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रवादी मध्यवर्ग, विशेषकर उच्च मध्यवर्ग में फ़ासीवाद के प्रसार की उर्वर ज़मीन की मौजूदगी को रेखांकित किया था। भारतीय मध्यवर्ग का राष्ट्रवाद अपने प्रारम्भ से ही पुनर्जागरण–प्रबोधन प्रसूत जुझारू भौतिकवादी तर्कणा के बजाय औपनिवेशिक संरचना–प्रसूत पुनरुत्थानवाद से अभिप्रेरित था। आगे चलकर, इसका एक रैडिकल हिस्सा मध्यवर्गीय क्रान्तिकारी आन्दोलन और सर्वहारा आन्दोलन से जुड़ा, पर एक बड़ा हिस्सा “नेहरूवादी–समाजवादी” नारों के व्यामोह में जकड़ा रहा या पुनरुत्थानवादी दुराग्रहों के साथ बुर्जुआ राष्ट्रवाद की अनुदारवादी धारा के साथ जुड़ा रहा। स्वातंत्र्योत्तर काल में “नेहरूवादी समाजवादी” रास्ते ने राजकीय पूँजीवाद के जिस विराट तंत्र का निर्माण किया उसमें हद दर्ज़े की भ्रष्ट नौकरशाही और सत्ता से नाभिनालबद्ध बुद्धिजीवियों का एक व्यापक संस्तर अस्तित्व में आया, जो प्रवृत्ति से श्रम–विरोधी, जन–विरोधी और निरंकुश स्वेच्छाचारी था। इस मध्यवर्ग के ऊपरी हिस्से को आपातकाल की निरंकुश तानाशाही अपने हितों के लिए अत्यधिक अनुकूल प्रतीत हुई थी और इसके निचले हिस्से के बहुलांश ने भी या तो बिना किसी आपत्ति के, या क्षीण असन्तोष के साथ उसे स्वीकार ही किया था। उदारीकरण के दौर में मध्यवर्ग के खाते–पीते हिस्से की भी जनवादी प्रक्रिया और संस्थाओं के प्रति रही–सही प्रतिबद्धता का तेज़ी से ह्रास हुआ है और निम्न मध्यवर्ग के निराश युवाओं का एक बड़ा हिस्सा पूँजीवादी संकट के फ़ासीवादी समाधान की ओर तेज़ी से आकृष्ट हुआ है। इस सन्दर्भ में पॉल आर. ब्रास का यह निष्कर्ष ग़ौरतलब है कि मध्यवर्गों को राजनीतिक लोकतंत्र का मुख्य समर्थक मानने की समझ आज बदलने की ज़रूरत है क्योंकि पिछड़े देशों में इन वर्गों की बढ़ती हुई उपभोग–सम्बन्धी माँगों को बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा करके या दमन करके ही पूरा किया जा सकता है।
औसत दर्ज़े के मध्यवर्ग का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ़ बचत करके ही नहीं, तमाम तरह का भ्रष्टाचरण करके सुख–सुविधा और ऐशो–आराम के उन साधनों को लपक लेना चाहता है, जिनसे बाज़ार उसे ललचा रहा है। ख़ास तौर से भारत जैसे देशों का मध्यवर्ग उत्पादक वर्गों से इस क़दर कट चुका है कि उनके बारे में सोचना तो दूर, उनसे घृणा करता है। आम मेहनतकशों की असहनीय होती जा रही जीवन–स्थितियों, उनसे अतिलाभ निचोड़ने की प्रक्रिया और उनके बढ़ते दमन से वह न सिर्फ़ असम्पृक्त हुआ है, बल्कि वह ख़ुद जनान्दोलनों के मुखर विरोधी और उनके दमन के पैरोकार की भूमिका में आता चला गया है। बेशक इसका एक ख़ासा–बड़ा हिस्सा बेहतर ज़िन्दगी हासिल कर पाने में लगातार पिछड़ते हुए जैसे–तैसे जी रहा है और बदलाव का समर्थक है, पर हम यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करना चाहते हैं कि पूँजीवादी विकास की अर्द्धशती के दौरान फलते–फूलते हुए भारतीय मध्यवर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा उदारीकरण के दौर तक आकर पूरी तरह प्रतिक्रियावादी बन चुका है और फ़ासीवाद के सामाजिक आधार का काम कर रहा है। उदारीकरण के दौर की लोभ–लालच की लुटेरी संस्कृति ने मध्यवर्ग को ज़्यादा रुग्ण बनाया है। उसके बीच व्याप्त अतर्कपरकता, दकियानूसी और घोर कूपमण्डूकता भी फ़ासीवाद की स्वीकार्यता के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। अन्तरराष्ट्रीय ब्राण्डों से लकदक उसके तन के भीतर उसके दिलो–दिमाग़ में सदियों पुराने अलगज़–मलगज़ के साथ ही उपभोग की हिंस्र लालसा घुल–मिल गई है।
विडम्बना यह है कि शिक्षित मध्यवर्ग का जो हिस्सा साम्प्रदायिकता और फ़ासीवाद का विरोध करता है, वह महानगरों के अकादमिक परिसरों, अख़बारी दुनिया और सांस्कृतिक जगत तक सीमित है और वहाँ भी वह अल्पमत में है। मध्यवर्ग के इस हिस्से की धर्मनिरपेक्षता उसकी बुर्जुआ जीवन–शैली और अभिजात बौद्धिक विमर्श की चौहद्दी में क़ैद है। अपने आसपास मौजूद उजरती ग़ुलामी के महासागर में अपनी सुख–सुविधाओं के सुरक्षित टापू पर रहता हुआ यह वर्ग कभी “नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता” के दिनों की वापसी के लिए आहें भरता है तो कभी पश्चिमी देशों के “बुर्जुआ जनवादी” विभ्रमों को देख–देखकर हुलसता–ललकता है तो कभी “बाज़ार समाजवाद” या सामाजिक जनवाद के नये–नये नुस्खे–फ़ार्मूले परसने का काम करता है। मध्यवर्ग के इस हिस्से की कायर–सुविधाभोगी–नपुंसक धर्मनिरपेक्षता के एजेण्डे से आम मेहनतकश जनता का कोई जुड़ाव नहीं है और इस स्थिति का भरपूर लाभ अन्ततोगत्वा फ़ासिस्ट ताकतों को ही मिलता है।
गुजरात के क़त्लेआम में मध्यवर्ग की भूमिका एक प्रातिनिधिक घटना है। कमोबेश उसमें पूरे भारतीय मध्यवर्ग की भूमिका की शिनाख्त की जा सकती है। यह सांस्कृतिक आन्दोलन के समक्ष उपस्थित गम्भीर चुनौतियों का अहसास कराती है और साम्प्रदायिकता–विरोध की पूरी रणनीति पर नये सिरे से सोचने के लिए बाध्य भी करती है।
- सृजन परिप्रेक्ष्य, जनवरी-अप्रैल 2002