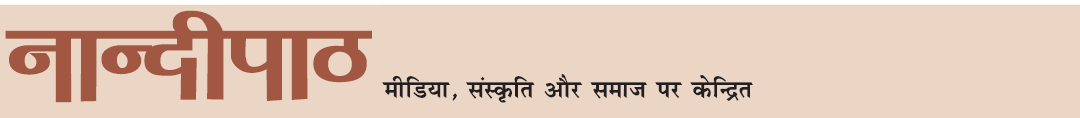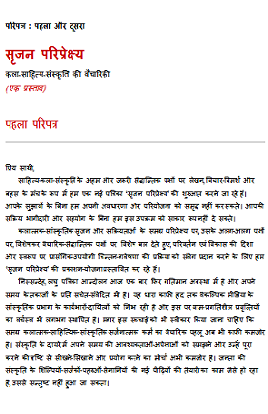सृजन परिप्रेक्ष्य, कला-साहित्य-संस्कृति की वैचारिकी
(एक प्रस्ताव)
पहला परिपत्र
प्रिय साथी,
साहित्य-कला-संस्कृति के अहम और जरूरी सैद्धान्तिक पक्षों पर लेखन, विचार-विमर्श और बहस के मंच के रूप में हम एक नई पत्रिका ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके सुझावों के बिना हम अपनी अवधारणा और परियोजना को समृद्ध नहीं कर सकते। आपकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग के बिना हम इस उपक्रम को साकार रूप नहीं दे सकते।
कलात्मक-सांस्कृतिक सृजन और सक्रियताओं के समग्र परिप्रेक्ष्य पर, उसके अलग-अलग पक्षों पर, विशेषकर वैचारिक-सैद्धान्तिक पक्षों पर विशेष बल देते हुए, परिवर्तन एवं विकास की दिशा और स्वरूप पर प्रासंगिक-उपयोगी चिन्तन-गवेषणा की प्रक्रिया को संवेग प्रदान करने के लिए हम ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ की प्रकाशन-योजना प्रस्तावित कर रहे हैं।
निस्सन्देह, लघु पत्रिका आन्दोलन आज एक बार फिर गतिमान अवस्था में है और अपने समय के तकाजों के प्रति सचेत-संवेदित भी है। यह धारा काफी हद तक वैकल्पिक मीडिया के सांस्कृतिक प्रभाग के कार्यभारों-दायित्वों को निभा रही है और इस पर वाम-प्रगतिशील प्रवृत्तियों का वर्चस्व भी लगभग स्थापित है। मगर इस सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि समग्र कलात्मक-साहित्यिक-सांस्कृतिक सर्जनात्मक कर्म का वैचारिक पहलू अब भी काफी कमजोर है। संस्कृति के दायरे में अपने समय की आवश्यकताओं-अपेक्षाओं को समझने और उन्हें पूरा करने की दृष्टि से सीखने-सिखाने और प्रयोग करने का मोर्चा अभी कमजोर है। जनता की संस्कृति के शिल्पियों-सर्जकों-पहरुओं-सेनानियों की नई पीढ़ियों की तैयारी का काम जैसे हो रहा है, उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ जा सकता।
हाल के वर्षों में सर्वहारा कला-संस्कृति पर, उसके वैचारिक आधारों पर, प्रतिक्रिया के केन्द्रों से निरन्तर घुसपैठ और आक्रमण होते रहे हैं, परवर्ती पूंजीवाद की नई-नई विचारसरणियां नये रंग-रोगन के साथ प्रतिक्रिया की पुरानी विचारधाराओं को पुनर्प्रस्तुत करती रही हैं, लेकिन हमारे पक्ष से उनके समुचित विश्लेषण और जवाबी कार्रवाई का काफी हद तक अभाव रहा है। यही नहीं, इस या उस कोने से पराजय, ‘‘पाप-स्वीकार’’ और समन्वय-समायोजन की आवाज़ें भी सुनाई देती रही हैं। पिछले लगभग दो दशकों के दौरान, प्रगति और प्रतिगामिता के बीच की विभाजक रेखाओं को धूमिल करने और मिटाने के सुनियोजित प्रयास होते रहे हैं। सामाजिक जनवाद और सुधारवाद की प्रवृत्तियां क्रान्तिकारी दायरों के भीतर दिग्भ्रम, प्रदूषण और विघटन को लगातार बढ़ावा देती रही हैं। लेकिन इनके सुसंगठित प्रतिरोध का अभाव रहा है और साथ ही आत्ममन्थन-आत्मालोचना का भी। एक ओर आत्मालोचन की जगह आत्मभर्त्सना और सर्वनिषेधवाद की प्रवृत्तियों और धुरीविहीन ‘‘मुक्त चिन्तन’’ का बोलबाला रहा है, तो दूसरी ओर आत्मतोषी कठमुल्लेपन का। परम्पराओं के पुनर्मूल्यांकन के नाम पर परम्परा-पूजन की, पुराने उपकरणों और विधि-विधानों से नई सच्चाइयों की पड़ताल करने और ‘‘भविष्य की कविता’’ का अन्वेषण करने की जगह ‘‘अतीत की कविता’’ का शरणागत होने की प्रवृत्तियां भी मौजूद रही हैं। ये विसंगतिपूर्ण स्थितियां आज हमें कला-साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में सैद्धान्तिक कार्यों पर जोर देने के लिए प्रेरित ही नहीं, बल्कि बाध्य कर रही हैं।
* * *
विश्व-ऐतिहासिक और भारतीयकृत दोनों ही सन्दर्भों में आज का दौर जटिल-संश्लिष्ट संक्रमण का दौर है और साथ ही, सर्वहारा क्रान्तियों के प्रथम संस्करणों की पराजय के बाद विपर्यय और प्रतिगामी शक्तियों के पुनरुत्थान का भी दौर है।
विगत आधी शताब्दी का प्रदीर्घ काल अर्द्धसामन्ती-अर्द्धऔपनिवेशिक भारत के अर्थतंत्र, राजनीति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के दुस्सह यंत्रणादायी क्रमिक पूंजीवादी रूपान्तरण का समय रहा है, लेकिन भूमण्डलीकरण की विगत एक दशाब्दी के दौरान, हर स्तर पर परिवर्तन की गति काफी तेज हो गई है। साम्राज्यवादी पूंजी के वर्चस्व और देशी पूंजी के साथ उसके सहबन्ध ने पूंजी और श्रम के अन्तरविरोध को अत्यधिक तीखा करते जाने और उजरती गुलामी के मरुस्थली पाट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने के साथ ही समूची सामाजिक संरचना में उथल-पुथल मचा दी है। ध्रुवीकरण अभूतपूर्व रूप से तेज हो गया है। वित्तीय पूंजी के निर्णायक वर्चस्व के इस विश्व-ऐतिहासिक दौर में बुर्जुआ जनवाद के (अलग-अलग स्तरों पर) क्षरण-विघटन की प्रक्रिया के साथ ही भारत जैसे देशों में एक ओर राज्यसत्ता की निरंकुश सर्वसत्तावाद की दिशा में यात्रा तेज हो गई है और पुनरुत्थानवादी, कट्टरपन्थी और फासीवादी बर्बरता की शक्तियों का सामाजिक आधार विस्तारित हुआ है, दूसरी ओर सांस्कृतिक पटल पर उन्नत पूंजीवाद की रुग्ण-बर्बर मानवद्रोही-जनवादनिषेधी संस्कृति और हमारे समाज में पहले से चले आ रहे मध्ययुगीन मूल्यों-संस्थाओं–धार्मिक अन्धविश्वास, रूढ़िवाद, जातिप्रथा, स्त्री-उत्पीड़न आदि के बीच एक ‘‘विचित्र किन्तु सत्य’’ सहबन्ध निर्मित हुआ है। यह प्रतिक्रियावादी ‘‘सम्मिश्र’’ संस्कृति समाज विकास की दशा-दिशा की अपनी स्वतंत्र गति की उपज है और साम्राज्यवाद और देशी पूंजीवाद की सत्ता ने इसके विकास एवं प्रसार को अपने हित में, सचेतन तौर पर अनुकूलित, नियोजित और त्वरित भी किया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिण्ट मीडिया के नये अवतारों के साथ ही, आज कम्प्यूटर भी इस नई सत्ता-संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके और भी अनेक आयाम और पहलू हैं, जिनकी चर्चा यहां सम्भव नहीं। हमारा उद्देश्य यहां अपने देश के स्तर पर संक्रमण की दिशा और दशा को लक्षित करना मात्र ही है।
और जाहिर है कि इस राष्ट्रीय संक्रमण का एक नया वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। या यूं कहें कि यह विश्वव्यापी संक्रमण की प्रक्रिया के अंग के रूप में ही घटित हो रहा है। विश्व-पूंजीवादी तंत्र–यह पूर्वप्रयुक्त शब्दावली भूमण्डलीकरण के नये दौर में काफी हद तक नये निहितार्थ ग्रहण कर चुकी है। यह शायद ही कोई अस्वीकार करेगा कि विश्व पूंजीवाद की कार्यप्रणाली और संरचना में विगत लगभग चैथाई सदी के दौरान कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने अर्थ और राजनीति के साथ ही समाज और संस्कृति के दायरे में भी हमारे समक्ष अध्ययन के नये कार्यभार प्रस्तुत किये हैं, हल करने के लिए नये सवाल खड़े किये हैं और उत्तर देने के लिए नई वैचारिक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन ‘‘नववाम’’ के अनेक घोषित-अघोषित स्वयंभू चिन्तकों को मार्क्सवाद-लेनिनवाद को ‘‘नई ऊंचाइयों’’ तक पहुंचाने, साम्राज्यवाद की नई, अनदेखी ‘‘ऊर्जस्विता’’ का पैरोकार बन बैठने, सामाजिक व्यवहार को स्थगित करके वर्तमान और आगामी ‘‘युगसत्यों के सन्धान’’ में रणतत्पर होकर सन्नद्ध हो जाने और भांति-भांति के कर्मविरत सिद्धान्त गढ़ते हुए नये-नये विभ्रम पैदा करने और ‘ट्रोजन हॉर्स’ की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन घोषित-अघोषित ‘‘नववामपन्थियों’’ की सांस्कृतिक जगत में भी पैठ है जो बढ़ती जा रही है। इनके सैद्धान्तिक विचलनों, अकर्मक विमर्शों और पराजय-बोध के प्रचार के विरुद्ध संघर्ष भी एक जरूरी दायित्व है लेकिन यह तभी हो सकता है जब आर्थिक-राजनीतिक क्षेत्रों के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे में भी नये परिवर्तनों और उनके प्रभावों को सही ढंग से लक्षित किया जाये और समझा जाये। निश्चय ही इन बदलावों की ओर पीठ करके नहीं खड़ा हुआ जा सकता।
भूमण्डलीय और देशीय–इन दोनों ही स्तरों पर संक्रमण की चर्चा के बाद थोड़ी चर्चा विश्व-ऐतिहासिक विपर्यय की भी। सर्वहारा क्रान्तियों के प्रथम संस्करणों की पराजय के साथ ही श्रम और पूंजी के बीच के ऐतिहासिक महासमर के पहले चक्र का समापन हो चुका है और दूसरा चक्र शुरू भी हो चुका है। क्रान्ति के विज्ञान और इतिहास के किसी अध्येता के लिए सर्वहारा क्रान्तियों की विगत पराजय दुखद तो हो सकती है, लेकिन अप्रत्याशित कतई नहीं। इतिहास के पूर्ववर्ती युगों की क्रान्तियां भी प्रायः अन्तिम विजय से पूर्व पराजित होती रही हैं और निर्णायक विजय से पूर्व प्रगतिशील वर्ग प्रतिगामी वर्गों से बार-बार पराजित होते रहे हैं। यह भी याद रखना होगा कि बुर्जुआ व्यवस्था के साथ ही समूचे वर्ग-समाज के विरुद्ध सन्नद्ध सर्वहारा क्रान्ति सर्वाधिक आमूल-चूल क्रान्ति है जो मानव-ऊर्जा के व्यापकतम, कुशलतम और सूक्ष्मतम इस्तेमाल की मांग करती है। इस सर्वोच्च युगान्तरकारी परिवर्तन की राह में लगभग एक शताब्दी बाद आया विपर्यय और प्रतिगामी पुनरुत्थान अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन क्रान्तियों की पराजय विचारधारा की पराजय या अन्त नहीं होती। सर्वहारा क्रान्ति के नये संस्करणों की रचना के लिए समाजवादी प्रयोगों के अनुभवों का समाहार बेहद जरूरी है। समाजवादी अर्थतंत्र, सामाजिक ढांचे, सांस्कृतिक अधिरचना और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण और संघटन के दौरान, अलग-अलग दौरों में समाजवाद की समस्याओं पर बहसें हुई हैं और समाहार हुए हैं। वह विपुल सामग्री मौजूद है। पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के आधारों, सम्भावनाओं पर भी काफी कुछ सोचा और लिखा गया है और इस समस्या को हल करने की दिशा में सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान महत्वपूर्ण प्रयोग भी हो चुके हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व इस बात से कम नहीं हो जाता कि इन सबके बाद भी समाजवाद की पराजय हो गई। कोई इतिहासान्ध व्यक्ति ही देश-दुनिया के स्तर के वर्ग-शक्ति सन्तुलन और समाजवाद की आम दिशा सम्बन्धी बुनियादी ठोस सूत्रों तक पहुंचने तक के लम्बे समय जैसे वस्तुगत कारकों की उपेक्षा कर सकता है।
बेशक समाजवाद की समस्याओं पर सोचने का कार्यभार हमारे सामने है, लेकिन यह शुरुआत शून्य से या नये सिरे से नहीं होनी है। पहली बात यह याद रखनी होगी कि आज जो समीक्षा-समाहार होगा, वह अतीत के प्रयोगों की रोशनी में ही होगा। वह कामकाजू, सामान्य, आरजी (प्रॉविज़नल) और एक जारी प्रक्रिया के रूप में ही होगा। निर्णायक समाहार की मंजिल वह होगी जब हमारे पैरों के नीचे उन्नत सामाजिक प्रयोग की ज़मीन होगी और वह तब होगी जब समाजवादी संक्रमण की ठोस समस्याएं हमारे सामने होंगी। समाजवाद की समस्या पर आज हमारा चिन्तन मुख्यतः विचारधारा की हिफाजत के लक्ष्य से ही निर्देशित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी यह है कि समाजवादी संक्रमण के सर्वतोमुखी, सर्वसमावेशी प्रयोगों और उपलब्धियों पर आज धूल और राख की जो मोटी परत डाल दी गई है, उसे हटाकर हम इतिहास के उन विस्मृत किये जा रहे पन्नों को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। विगत क्रान्तियों की उपलब्धियों को पूंजीवादी चिन्तक-विचारक तो ओझल कर ही रहे हैं, अपने पराजयवाद के चलते और अपने चिन्तन की ‘‘मौलिकता’’ की पालिश चमकाने के चक्कर में नौबढ़ वामपन्थी ‘‘चिन्तकगण’’ भी ऐसा कर रहे हैं और कुछ तो लगातार विक्षिप्त प्रलाप की तरह अपने क्रान्तिकारी पूर्वजों-परम्पराओं को सिर्फ कोसने-धिक्कारने का ही काम कर रहे हैं। सर्वहारा पुनर्जागरण का यह सर्वोपरि कार्यभार है कि दर्शन, राजनीति, समाज विज्ञान, अर्थ-विज्ञान से लेकर कला-संस्कृति तक के क्षेत्र में सिद्धान्त और प्रयोगों की जो एक शानदार विरासत रही है, उसे विस्मृति के अंधेरे तलघरों से बाहर निकालकर रोशनी में लाया जाये। संस्कृति के क्षेत्र में, उपन्यास और कविता को लेकर, संगीत, नाटक और सिनेमा को लेकर, भाषाशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र के प्रश्नों पर तथा आलोचना की सैद्धान्तिकी और पद्धति-विज्ञान के सीमान्तों में लगभग सौ वर्षों के दौर में चली लम्बी बहसों, शानदार प्रयोगों और गम्भीर चिन्तन को लगभग भुला दिया गया है। यदि कुछ सामने आ भी रहा है तो वह मुख्यतः पश्चिमी ‘‘नववाममार्गी मुक्त चिन्तकों’’ का बौद्धिक कचड़ा ही है। बेशक उनसे भी सीखा जाना चाहिए, लेकिन महान सामाजिक प्रयोगों के साथ-साथ कला-साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में जो नई चीजें और नई समस्याएं और नये समाहार सामने आये थे, उनका बुनियादी महत्व अनुपेक्षणीय है। अपने समय की सांस्कृतिक समस्याओं से यदि वास्तव में जूझना है तो परम्पराओं के छूटे हुए सिरों को पकड़कर आलोचनात्मक विवेक के साथ उनका अध्ययन करना होगा और फिर आगे विस्तार देना होगा–अन्तरराष्ट्रीय सन्दर्भों में भी और राष्ट्रीय सन्दर्भों में भी।
उपरोक्त चर्चा का सार-संक्षेप हम इस रूप में रखना चाहेंगे :
संक्रमण और विपर्यय के द्वन्द्वात्मक संघातों के बीच गतिमान हमारे समय में इतिहास और परम्पराओं का पर्यवलोकन-पुनर्विवेचन-पुनर्मूल्यांकन, अतीत के प्रयोगों और उनके वैचारिक आधारों-अवदानों का पुनःस्मरण और आलोचनात्मक अध्ययन जरूरी हो जाता है। साथ ही, विश्व-ऐतिहासिक विपर्यय के ऐसे दौर में वैज्ञानिक तर्कणा और समाज-विकास की नियमसंगति की अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के लिए जुझारू वैचारिक संघर्ष भी जरूरी है।
विगत दशाब्दियों के दौरान, विशेषकर भूमण्डलीकरण के दौर में देश और दुनिया के आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में जो आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, उन्हें देखते हुए, नये यथार्थ के संज्ञान के उपक्रम की–उनके विकास के वस्तुगत नियमों के संज्ञान के उद्यम की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। नई सामाजिक-सांस्कृतिक परिघटनाओं और उनकी अन्तर्वस्तु को समझने के लिए सघन विचार-विमर्श और वाद-विवाद-संवाद की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी प्रक्रिया में, विचार और व्यवहार की परस्पर अन्तर्क्रिया से गुजरकर समाज के विज्ञान और कला की वैचारिकी आगे विकसित होती है।
प्रतिक्रिया के बुर्जों से नये सांस्कृतिक सिद्धान्तों और विमर्शों के रूप में और अन्य अनेकशः रूपों में जो गोलन्दाजी हो रही है, प्रगतिकामी पक्ष के बंकरों-बैरिकेडों से उनका प्रत्युत्तर देना होगा और प्रत्याक्रमण करना होगा। तथाकथित ‘पापुलर कल्चर’ और ‘मास कल्चर’ की नई तकनोलाजी-आधारित विधाओं-उपकरणों के जरिए ‘‘संचार क्रान्ति’’ के दौर में व्यापक जनमानस को प्रभावित करने की जो नई क्षमता पूंजीवादी तंत्र ने अर्जित की है, उनकी सही-सटीक समझ कायम करने की जरूरत है, ताकि जनता के सांस्कृतिक आन्दोलन का आधार और प्रभाव व्यापक बनाया जा सके, और व्यापक लोकप्रिय प्रचार एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध के नये उपकरण गढ़े जा सकें और पुराने उपकरणों का परिष्कार किया जा सके।
मूलतः पराजयवाद और सुविधाभोगी अकर्मण्यता के प्रति समर्पित प्रत्यक्ष-प्रच्छन्न सामाजिक जनवादी ‘‘नववाममार्गियों’’ के चिन्तन-विमर्शों की सच्चाई को उजागर करना भी आज का एक जरूरी कार्यभार है ताकि सांस्कृतिक मोर्चे की क्रान्तिकारी कतारों में दिग्भ्रम, मतिभ्रम और सुधारवाद के कीड़ों-दीमकों का प्रवेश रोका जा सके। सैद्धान्तिक कार्यभारों की अहमियत के ऐसे दौरों में, यह याद रखना बुनियादी तौर पर जरूरी है कि इन्हें वास्तव में वही पूरा कर सकते हैं जो महज किताबी कीड़े न होकर व्यवहार के सिपाही हों। जीवित विश्व के जीवित प्रश्नों पर प्रयोजनमुखी चिन्तन वही कर सकते हैं, यह बात सांस्कृतिक मोर्चे के लिए भी उतनी ही लागू होती है जितनी राजनीतिक मोर्चे के लिए।
यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि जब तक व्यवस्था का चरित्र जन विरोधी है, तब तक बदलाव के हर मोर्चे के लिए बुनियादी प्रश्न राज्यसत्ता का ही बना रहेगा। निस्सन्देह व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन और प्रचार की एक लम्बी प्रक्रिया के दौरान जनता की वैकल्पिक संस्कृति की संस्थाओं-सम्बन्धों की आधारशिला बनती रहती है, ढांचे की रूपरेखा और प्रारूप, प्रकल्प और नमूने भी बनते रहते हैं, लेकिन जनता की वैकल्पिक क्रान्तिकारी संस्कृति व्यवस्था परिवर्तन के बाद ही समाज में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। तब तक वह लगातार सत्ताधारी संस्कृति से संघर्षरत रहती है और व्यवस्था परिवर्तन के निर्णायक संघर्ष में (जिसकी केन्द्रीय रणभूमि राजनीति होती है) सन्नद्ध होने के लिए जनमानस को तैयार करती रहती है। इस बोध से विचलन सुधारवादी राह का राही बनना होगा। कुछ लोग वर्तमान समाज की जटिल संरचना की दुहाई देते हुए यह शिक्षा दे रहे हैं कि वर्ग-संघर्ष आज आर्थिक मांगों या उनकी केन्द्रीभूत अभिव्यक्ति के तौर पर राजनीतिक मांगों के इर्दगिर्द नहीं होगा, वह जातिप्रथा विरोधी, नारी-उत्पीड़न विरोधी, पर्यावरण-विनाश विरोधी तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों के रूप में ही सामने आयेगा। ‘‘क्रान्तिकारी समाज-सुधारकों’’ की यह प्रजाति भी आज सांस्कृतिक मोर्चे और विशेषकर इस मोर्चे के सैद्धान्तिक कार्यों पर जोर दे रही है। पर यह राजनीतिक-आर्थिक वर्ग-संघर्ष से मुंह मोड़े अकादमिक सामाजिक जनवादियों का झुण्ड है जो ‘‘विखण्डित वर्ग-संघर्ष’’ और सामाजिक-सांस्कृतिक ‘‘सुधारकार्य’’ रूपी वर्ग-संघर्ष का पैरोकार है। ऐसी खतरनाक विजातीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष आज के दौर का जरूरी कार्यभार है।
कुल मिलाकर, इन्हीं कार्यभारों के संश्लिष्ट-संग्रन्थित समुच्चय को हम आज के सर्वहारा नवजागरण (रिनेसां) और सर्वहारा प्रबोधन (एनलाइटेनमेण्ट) के आधारभूत और केन्द्रीय कार्यभारों के रूप में निरूपित और प्रस्तुत कर रहे हैं। यूरोप के बुर्जुआ नवजागरण और प्रबोधन के कालखण्डों अथवा उन्नीसवीं शताब्दी के संक्रमणकालीन रूसी समाज से भी कहीं गहरे और व्यापक अर्थों में, हमारे समय में, संस्कृति का क्षेत्र विचारधारात्मक वर्ग-संघर्ष की केन्द्रीय भूमि बना हुआ है, और यह स्वाभाविक भी है।
* * *
हमारे सामने सोचने-विचारने के लिए जो मुद्दे हैं, अब उन्हें समेटते हुए हम सिलसिलेवार रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ की विषयवस्तु का स्वरूप और दायरा और अधिक साफ हो सके।
॰ ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ साहित्य, चित्रकला, संगीत, नाटक, सिनेमा सहित समस्त दृश्य-श्रव्य कला माध्यमों के वैचारिक पक्षों के साथ ही, व्यापक और सामान्य रूप से संस्कृति और समाज के, तथा सांस्कृतिक आन्दोलन के वैचारिक-सैद्धान्तिक प्रश्नों पर केन्द्रित पत्रिका होगी। इन पर मार्क्सवादी दृष्टि से, या उसके भी पहले के समय में जुझारू भौतिकवादी या क्रान्तिकारी यथार्थवादी दृष्टि से, जो काम हुए हैं, जो बहसें चली हैं और जो प्रयोग हुए हैं, उनकी पुनर्प्रस्तुति और पुनर्मूल्यांकन को हम आज का जरूरी कार्यभार समझते हैं।
॰ पहले से मौजूद सैद्धान्तिक प्रश्नों-समस्याओं पर समकालीन सन्दर्भों में जो पुनर्विचार हो रहे हैं और नये समय की नई सच्चाइयों और नई समस्याओं पर जो चिन्तन और बहसें चल रही हैं तथा अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इतिहास के पुनर्मूल्यांकन-विषयक प्रश्नों पर, संस्कृति के क्षेत्र में, सोचने-विचारने का जो काम चल रहा है, ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ उनका मंच बनेगा, इन प्रक्रियाओं को त्वरान्वित करेगा और इनमें सार्थक हस्तक्षेप करेगा।
॰ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पूंजीवादी विचारकों का जोर आज सांस्कृतिक विमर्श पर सर्वाधिक है और परवर्ती पूंजीवाद की नई-नई विचार-सरणियां–तमाम किस्म के ‘‘उत्तर’’वाद और ‘‘अन्त’’वाद–आज मुख्यतः संस्कृति सिद्धान्तों के रूप में ही सामने आ रही हैं। ‘‘नववाम’’ और छद्म वाम के सिद्धान्तकार-भाष्यकार भी आज मुख्यतः संस्कृति के दायरे में ही नये-नये शास्त्र, संहिताएं और सूक्त रच रहे हैं। इन तमाम नई विचार-सरणियों के उत्स क्या हैं, इनकी अन्तर्वस्तु क्या है, इनकी पद्धति और इनका साध्य क्या है? क्या ये सर्वथा नई विचारधाराएं हैं, क्या ये सर्वथा नये संस्कृति-सिद्धान्त और कला दृष्टि प्रस्तुत कर रही हैं, क्या इनकी सौन्दर्यशास्त्रीय और भाषाशास्त्रीय मीमांसाएं सर्वथा नई हैं? अथवा ये उन्नीसवीं शताब्दी और प्रारम्भिक बीसवीं शताब्दी की बुर्जुआ दार्शनिक अवस्थितियों के ही विस्तार और नये संशोधित संस्करण मात्र हैं? वर्तमान ‘‘नववाम’’ वास्तव में नव है या पुराने सामाजिक जनवाद का ही एक नवरूप है जो आज संस्कृति के दायरे में बहुत अधिक सक्रिय है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका केन्द्रीय महत्व है और इसी दृष्टि से इन प्रश्नों पर केन्द्रित विश्लेषण, सकारात्मक लेखन और ‘पॉलेमिकल’ सामग्री को ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ में महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा।
॰ ‘‘नववाम’’ से प्रभावित या पुराने सामाजिक जनवाद से अब भी प्रभावित बुद्धिजीवियों- संस्कृतिकर्मियों के प्रति अलगाव-असम्पृक्तता-बहिष्कार का रुख अपनाने की जगह उनके विचारों को हम पत्रिका में निश्चय ही स्थान देंगे और उनके साथ ‘पॉलिमिक्स’ चलायेंगे। पश्चिम के बहुतेरे मार्क्सवादी अकादमीशियनों-विद्वानों ने अपने वैचारिक विचलनों और गलत प्रस्थापनाओं के बावजूद समाज-संस्कृति, दर्शन, भाषाशास्त्र-सौन्दर्यशास्त्र जैसे विषयों पर कई जरूरी, अनसुलझे और विचारोत्तेजक मुद्दे उठाये हैं और चिन्तन और बहस को नया संवेग प्रदान करने का काम किया है। हम बहस और विचार की दृष्टि से ऐसी सामग्री को भी पत्रिका में स्थान देंगे और उनकी आलोचना और उन पर चलने वाले वाद-विवाद को भी।
॰ समाजवादी प्रयोगों के दौरान, संस्कृति के क्षेत्र में जो वैचारिक-सैद्धान्तिक काम हुए थे और बहसें चली थीं, उनकी पुनर्प्रस्तुति के साथ ही हम उस कालखण्ड में विकासमान नई संस्कृति, नये सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों-संस्थाओं-आन्दोलनों और तत्कालीन कलात्मक-साहित्यिक सर्जना और प्रयोगों के प्रतिनिधि उदाहरणों-प्रकल्पों-प्रारूपों-परियोजनाओं से पाठकों को परिचित कराते रहने का नियमित कार्यभार अपने सामने रखेंगे।
॰ समकालीन पूंजीवाद की अर्थनीति और राजनीति के साथ ही उसकी संस्कृति में जो बदलाव आये हैं, नई तकनोलॉजी और अति उन्नत संचार तंत्र ने बुर्जुआ मीडिया को जो नयी क्षमता, नई प्रभाविता और नया विस्तार दिया है और सांस्कृतिक आक्रमण एवं वर्चस्व के रूपों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके विश्लेषण की सख्त ज़रूरत है ताकि उनकी शक्ति के साथ उनकी कमजोरियों की भी पहचान की जा सके, उनके रहस्यावरण को भेदा जा सके, जनता के सांस्कृतिक मोर्चे को नई नीतियों-रणनीतियों-उपकरणों से लैस किया जा सके और कलात्मक-सृजन और सम्प्रेषण के नये आयाम उद्घाटित किये जा सकें। अपने सांस्कृतिक उपकरणों को गढ़ने में उन्नत तकनोलॉजी का सत्ताधारी अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कालान्तर में यही चीज उनके लिए सिरदर्द भी साबित होती है। जनता के सांस्कृतिक मोर्चे के सेनानी भी उन्नत तकनोलॉजी का लाजिमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही, भारत जैसे तीसरी दुनिया के घोर असमान विकास वाले देशों में परम्परागत कला-रूपों और सांस्कृतिक आयोजनों के पुनर्परिष्कृत-पुनराविष्कृत संस्करणों की महत्ता बनी रहेगी। इन बिन्दुओं पर हमें तफसील से सोचना-विचारना होगा।
॰ एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि हमारे समय में विश्व स्तर पर और देश स्तर पर पूंजी की सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी शक्ति–फासीवाद की शक्तियों के विविध रूपों में फिर से उभार के कारण क्या हैं? इनके उत्स क्या हैं? क्या इसका कारण मात्र समाजवाद की वर्तमान विश्व-ऐतिहासिक पराजय है और क्या (जैसाकि रोजा लक्जेमबर्ग ने कहा था) समाजवाद के विकल्प के फौरी पश्चरायण की स्थिति में दूसरा विकल्प–फासीवादी बर्बरता, एक बार फिर प्रभावी स्थिति में आ गया है? क्या इसका कारण साम्राज्यवाद के दीर्घ विलम्बित जीवन में और बुर्जुआ जनवाद के निश्शेष होने की ऐतिहासिक प्रक्रिया में निहित है? या बुनियादी तौर पर, वित्तीय पूंजी के निर्णायक वर्चस्व, पूंजी के संचय व निस्तारण के लिए अनुत्पादक गतिविधियों जुए और सट्टेबाजी पर प्रमुखतः निर्भरता और कागजी अर्थव्यवस्था का आधार–इसके मुख्य उत्स हैं? भारत के स्तर पर यदि देखें तो फासीवादी प्रवृत्तियों के मौजूदा उभार के कारणों की पड़ताल के लिए हमें राष्ट्रीय जनवादी आन्दोलन के कमजोर वैचारिक आधार, उसमें एक ओर तर्कणा, जुझारू भौतिकवादी दर्शन एवं वैज्ञानिक इतिहासदृष्टि के बजाय जुझारू अतीतोन्मुख पुनरुत्थानवादी धारा और दूसरी ओर समझौतापरस्त सुधारवादी धाराओं की मौजूदगी, तथा सम्पूर्ण बुर्जुआ नेतृत्व के दोहरे चरित्र में समझौतापरस्ती के पहलू की प्रधानता की सम्पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर पश्चदृष्टिपात, औपनिवेशीकरण से लेकर खण्डित अधूरी आजादी तक की पूरी यात्रा का सिंहावलोकन, जरूरी लगेगा। साथ ही, उत्तरवर्ती आधी सदी में समाज के पूंजीवादीकरण की यात्रा जिस यंत्रणादायी, मंथर क्रमिक प्रक्रिया से, पुराने मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं के साथ समझौता करते हुए, उन्हें अपनाते हुए या उनके साथ नये प्रतिक्रियावादी मूल्यों का सहकार सम्बन्ध स्थापित करते हुए, पूरी की गई है; उसकी पड़ताल भी हमें जरूरी लगेगी। राष्ट्रीय आन्दोलन के नायकों की इतिहास कथा का उत्तर भाग खण्डित नायकत्व और पराभूत गौरव की त्रासद गाथा के रूप में आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के अधिकांश साम्राज्यवाद-निर्भर पूंजीवादी देशों में साफ-साफ लिखा जा चुका है और चरम प्रतिक्रिया की वाहक मूलगामी शक्तियां अलग-अलग रूपों में इन सभी देशों में सिर उठा रही हैं। भारत में अल्पसंख्यक-विरोधी धार्मिक मूलतत्ववाद इनकी मुख्य अभिव्यक्ति है, लेकिन सामाजिक स्तर पर दलित-उत्पीड़न और स्त्री-उत्पीड़न जैसी पुरातन निरंकुश स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों के फासीवादी परिष्कार की परिघटना की, भाषाई-इलाकाई शॉवनिज़्म की और राष्ट्रीयताओं-उपराष्ट्रीयताओं के बर्बर राजनीतिक उत्पीड़न के साथ ही उनकी संस्कृतियों के दमन-विलोपन के सत्ता प्रयासों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती।
॰ सोचने का एक अहम प्रश्न यह भी है कि क्या प्रतिक्रिया और पुनरुत्थान की इन बर्बरतम शक्तियों का प्रतिकार हम महज अपनी राष्ट्रीय परम्परा से अर्जित उपकरणों के सहारे कर सकते हैं? यहीं हमें राष्ट्रीय परम्पराओं के पुनर्मूल्यांकन और नई श्रम-संस्कृति के अन्तरराष्ट्रीयतावादी चरित्र पर विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। सोचने का एक अहम प्रश्न यह भी है कि जिस विश्व में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ राष्ट्रीय पूंजी का सहबन्ध अर्थ-राजनीति के साथ ही संस्कृति के धरातल पर भी सुस्थिर हो चुका है और सुचारु रूप से संचालित हो रहा है, उसमें साम्राज्यवाद के राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक आक्रमणों का प्रतिकार क्या राष्ट्रवाद की पुरानी जमीन पर खड़े होकर किया जा सकता है? क्या भूमण्डलीकरण में पूंजी की अभूतपूर्व अन्तरराष्ट्रीय एकता विश्व स्तर पर श्रम की अन्तरराष्ट्रीय एकजुटता का एक वस्तुगत आधार नहीं तैयार कर रही है? तीसरी दुनिया के देशों में इस नये दौर की सामाजिक क्रान्तियां, राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं में ही सम्पन्न होने के बावजूद, यदि विदेशी पूंजी के साथ ही देशी पूंजी के विरुद्ध भी केन्द्रित होंगी, तो उनका चरित्र पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनवादी क्रान्तियों से भिन्न होगा तथा एक अर्थ में उनसे अधिक ‘‘स्पष्ट और मुखर’’ अन्तरराष्ट्रीयतावादी होगा। ऐसी सामाजिक क्रान्तियों की धारा की संस्कृति श्रम की अन्तरराष्ट्रीयतावादी संस्कृति ही हो सकती है–सच्ची सर्वहारा संस्कृति ही हो सकती है। तब क्या यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय परम्पराओं के सकारात्मक तत्वों की विरासत को अपनाते हुए भी और देश की सीमाओं में संघटित होते हुए भी, आज के नये पुनर्जागरण और प्रबोधन का चरित्र मूलतः राष्ट्रीय नहीं बल्कि अन्तरराष्ट्रीयतावादी होगा और यह श्रम की संस्कृति के सार्वभौमिक समतामूलक मूल्यों और मानवीय गरिमा का संवाहक होगा?
॰ उपरोक्त आधारभूत प्रश्नों के विभिन्न सिरों को विस्तार देते हुए हम स्त्री-उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न के प्रश्न, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रश्न तथा साम्प्रदायिक फासीवाद के विश्लेषण और कारगर प्रतिरोध के प्रश्न को भी विश्लेषण का मुद्दा बनायेंगे और साथ ही पर्यावरण से लेकर विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों पर हो रहे आन्दोलनों की भी आलोचना प्रस्तुत करते हुए सही दिशा निर्धारण के व्यावहारिक प्रश्न को केन्द्र में लाने की कोशिश करेंगे।
जाति-प्रथा और दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर वामपंथी राजनीतिक-सांस्कृतिक आन्दोलन की अतीत की गलतियों को ठीक करने के नाम पर वर्ग-विश्लेषण को ही तिलांजलि दे देने की प्रवृत्ति और ‘क्लास-रिडक्शनिज्म’ के परित्याग की आड़ में वर्ग-अवस्थिति से ही विचलन आज एक प्रमुख ‘‘नववाममार्गी’’ भटकाव के रूप में क्रान्तिकारी वामपंथी धारा के भीतर संक्रमित हो रहा है। नवोदित दलित मध्यवर्गीय सुविधाजीवी नेतृत्व के प्रति लल्लो-चप्पो का रवैया अपनाकर और विचारधारा के प्रश्न की अनदेखी करके दलित-मुक्ति का व्यावहारिक कार्यक्रम नहीं बन सकता और उसके बिना व्यापक जन मुक्ति का व्यावहारिक कार्यक्रम भी न तो बन सकता है न ही उसका सफल क्रियान्वयन हो सकता है। जाति प्रथा और जातिगत संस्कारों के विरुद्ध व्यापक सांस्कृतिक-सामाजिक आन्दोलन के साथ ही दलित मेहनतकश जनता को ‘‘जनतांत्रीकरण’’ और ‘‘सुधार’’ के बुर्जुआ विभ्रमों से मुक्त करना, उनके मध्यवर्गीय एवं बुर्जुआ सजातीय नेतृत्व के असली चरित्र का पर्दाफाश करना, दलित प्रश्न का सही ऐतिहासिक सामाजिकार्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करना और यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि दलित मुक्ति जन मुक्ति के सम्पूर्ण प्रोजेक्ट का एक अनिवार्य अंग है, यह सुधार का नहीं बल्कि सामाजिक क्रान्ति का एजेण्डा है और यह कि केवल श्रम और मानव की गरिमा को सम्पूर्ण सच्चे अर्थों में बहाल करने वाली संस्कृति को गढ़ने वाला सामाजिक ढांचा ही सहस्राब्दियों पुरानी इस बर्बरता को सदा-सदा के लिए समाप्त कर सकता है।
इसी तरह नारी-मुक्ति के प्रश्न पर भी न सिर्फ नई-नई नारीवादी, उत्तर मार्क्सवादी नारीवादी, ‘सबआल्टर्न’ नारीवादी वगैरह, बल्कि क्रान्तिकारी वामपंथ की दुहाई देने वाले कतिपय समूह भी आज वर्ग अवस्थितियों को त्याग रहे हैं। पर्यावरण के प्रश्न को लेकर भी ऐसे विचार आज चलन में हैं।
वर्ग-संघर्ष को अलग-अलग इलाकों, समुदायों या मुद्दों और मोर्चों के आधार पर खण्ड-खण्ड विखण्डित करने और उनकी शक्ति विसर्जित करके राज्यसत्ता और व्यवस्था के सीमान्तों को आम जन की नजरों से ओझल करने का काम भी आज खूब हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साम्राज्यवादी देशों की वित्तदाता एजेंसियों के पैसों से ‘‘समाज-सुधार’’ और ‘‘सामाजिक आन्दोलनों’’ में लगे गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के साथ प्रायः दलितवाद, नारीवाद, ‘सबआल्टर्नवाद’ और ‘‘विखण्डित वर्ग-संघर्ष’’ के पुरोधा-प्रस्तोता ‘‘वामपंथियों’’ का प्रगाढ़ सहकार-सम्बन्ध कायम है। इस ‘‘पवित्र गठबंधन’’ के वास्तविक चरित्र और संस्कृति को व्यावहारिक धरातल पर उजागर तो करना ही होगा, लेकिन सबसे जरूरी है ‘‘वामपंथ’’ की इस धारा के उपरोक्त सैद्धान्तिक विचलनों के विरुद्ध घनीभूत वैचारिक संघर्ष। सांस्कृतिक मोर्चे पर भी यह कार्यभार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक मोर्चे पर।
॰ इन कार्यभारों के निर्वहन के प्रयासों के साथ हमारा प्रयास यह भी होगा कि आज जो लिखा जा रहा है या जो कलात्मक सृजन (संगीत, नाटक, सिनेमा, चित्रकला–किसी भी रूप में) हो रहा है उनमें से कुछ प्रतिनिधि कृतित्वों की समालोचना के माध्यम से सोचने-विचारने के जरूरी मुद्दे उठायें। साथ ही, समकालीन आलोचना की आलोचना को भी हम एक जरूरी कार्यभार के रूप में रेखांकित करना चाहते हैं। कला की अन्य विधाओं की वैज्ञानिक आलोचना तो हिन्दी में अभी ढंग से विकसित ही नहीं हुई है। जहां तक साहित्यिक आलोचना की प्रगतिशील-वाम धारा का सवाल है, वहां पद्धति-सम्बन्धी समस्या गम्भीर है। सही द्वन्द्ववादी भौतिकवादी पद्धति की जगह सारसंग्रहवाद, लक्षणवाद और अनेकशः रूपों में आधिभौतिक यांत्रिकता का बोलबाला है। यह एक गम्भीर प्रश्न है, और इसपर गम्भीर विचार-विमर्श की जरूरत है।
॰ ‘सृजन-परिप्रेक्ष्य’ संस्कृति और विचार के मोर्चे पर संघर्ष के ठोस मुद्दों को रेखांकित करने और उस संघर्ष की नीति-रणनीति के निर्धारण तथा वैचारिक-सांस्कृतिक संघर्ष में भागीदारी करने के साथ ही, जनता के सांस्कृतिक मोर्चे के सेनानियों की नई कतारें तैयार करने और प्रशिक्षित करने पर विशेष बल देगा। उनके प्रति हमारा रुख ‘खुद सीखते जाने और फिर सिखाते जाने’ का होगा और वैचारिक बहसों से इस काम में हमें विशेष सहायता मिलेगी।
॰ कविताएं, कहानियां और अन्य रचनात्मक कृतित्व के प्रकाशन के लिए आज हिन्दी की बहुतेरी सम्मानित और महत्वपूर्ण साहित्यिक लघु पत्रिकाओं के मंच उपलब्ध हैं। इसलिए इनके प्रकाशन को हमने प्राथमिकता-क्रम में नीचे रखा है। फिर भी, अतीत की समृद्ध धरोहर से दुनिया की अन्य भाषाओं, अन्य भारतीय भाषाओं और हिन्दी की प्रतिनिधि रचनाओं का चयन हम प्रस्तुत करते रहेंगे। आज जो लिखा जा रहा है, उसमें से भी कुछ प्रतिनिधि रचनाओं को हम समय-समय पर पत्रिका में स्थान देंगे।
* * *
हमारी यह परियोजना निश्चित ही महत्वाकांक्षी है। दायित्वों और कार्यभारों का दायरा बहुत विस्तीर्ण है। जाहिरा तौर पर इन सबको हम एक साथ नहीं पूरा कर सकते। इस परिपत्र में हमने आपके समक्ष अपना बोध और अपनी परियोजना की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक ऐसी पत्रिका की सोच विगत सात-आठ वर्षों से सीझती-पकती रही है, लेकिन संसाधनों और बौद्धिक कार्यों के बोझ की दृष्टि से हम साहस नहीं जुटा पाते थे। हमारी क्षमता अपर्याप्त थी और प्राथमिकताओं का सवाल भी आड़े आता था। दूसरे, इस मसले पर हम स्वयं एक हद तक स्पष्ट हो लेना चाहते थे। अब हम समझते हैं कि पहले ही काफी देर हो चुकी है। जैसे-जैसे हम ताकत, क्षमता और सहयोग जुटाते जायेंगे, जैसे-जैसे सहयात्रियों की संख्या बढ़ती जायेगी, हम अपने घोषित दायित्वों-कार्यभारों के ज्यादा से ज्यादा बड़े हिस्से को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो सम्भव है, वहीं से हमें शुरुआत कर देनी होगी।
हम खुले दिल से आपकी आलोचना और सुझाव-परामर्श आमंत्रित करते हैं। हम आग्रहपूर्वक आपसे हर तरह के सहयोग का अनुरोध करते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आइये, बातचीत की जाये और जिस हद तक बोध और धारणा में सहमति हो, उस हद तक एक साथ मिलकर काम किया जाये और आगे व्यापक एकजुटता की दिशा में लगातार सचेष्ट रहा जाये।
पत्रिका की विषयवस्तु की और अधिक ठोस रूपरेखा हम अगले परिपत्र में आपको भेजेंगे। तब तक कोशिश यही रहे कि आपके सुझाव हमें ज़रूर मिल जायें।
कात्यायनी, सत्यम
9 अप्रैल 2001