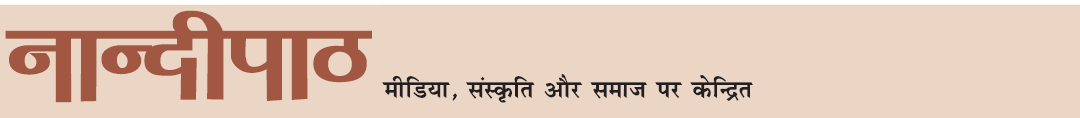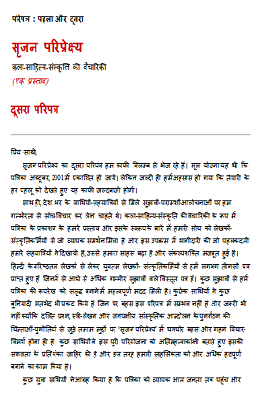सृजन परिप्रेक्ष्य, कला-साहित्य-संस्कृति की वैचारिकी
(एक प्रस्ताव)
दूसरा परिपत्र
प्रिय साथी,
सृजन परिप्रेक्ष्य का दूसरा परिपत्र हम काफी विलम्ब से भेज रहे हैं। मूल योजना यह थी कि पत्रिका अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित हो जाये। लेकिन जल्दी ही हमें अहसास हो गया कि तैयारी के हर पहलू को देखते हुए यह काफी जल्दबाजी होगी।
साथ ही, देश भर के साथियों-सहयात्रियों से मिले सुझावों-परामर्शों-आलोचनाओं पर हम गम्भीरता से सोच-विचार कर लेना चाहते थे। कला-साहित्य-संस्कृति की वैचारिकी के रूप में पत्रिका के प्रकाशन के हमारे प्रस्ताव और इसके स्वरूप के बारे में हमारी सोच को लेखकों-संस्कृतिकर्मियों से जो व्यापक समर्थन मिला है और इस उपक्रम में भागीदारी की जो पहलकदमी हमारे सहयात्रियों ने दिखायी है, उससे हमारा साहस बढ़ा है और संकल्पशक्ति मजबूत हुई है। हिन्दी के वरिष्ठतम लेखकों से लेकर युवतम लेखकों- संस्कृतिकर्मियों से हमें लगभग तीन सौ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से आधे से अधिक गम्भीर सुझावों वाले विस्तृत पत्र हैं। कुछ सुझावों से हमें पत्रिका की रूपरेखा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। कुछेक साथियों ने कुछ बुनियादी मतभेद भी प्रकट किये हैं जिन पर बहस इस परिपत्र में सम्भव नहीं है और जरूरी भी नहीं क्योंकि दलित प्रश्न, स्त्री-लेखन और जनपक्षीय सांस्कृतिक आन्दोलन के पुनर्गठन की चिन्ताओं-चुनौतियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ में घनघोर बहस और गहन विचार-विमर्श होना ही है। कुछ साथियों ने इस पूरी परियोजना को अतिमहत्वाकांक्षी बताते हुए इसकी सफलता के प्रति शंका जाहिर की है और इस तरह हमारी साहसिकता को और अधिक हठपूर्ण बनाने का काम किया है।
कुछ युवा साथियों ने आग्रह किया है कि पत्रिका को व्यापक आम जनता तक पहुंच और युवा प्रतिभाओं को सामने लाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। प्रगतिशील, क्रान्तिकारी साहित्य जनता के बड़े से बड़े हिस्से तक पहुंचे, हम इस चिन्ता के बराबर के साझीदार हैं और अपनी क्षमतानुसार इस दिशा में कई उद्यमों में निरन्तर लगे हुए हैं। जनता तक लोकप्रिय साहित्यिक सामग्री पहुंचाने वाली पत्रिकाओं की जरूरत से भी हम इंकार नहीं करते। कविताओं-कहानियों-गीतों-नाटकों-संस्मरणों-रिपोर्टों से भरी बहुतेरी वामपंथी लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं। लेकिन उनकी पहुंच अतिसीमित क्यों है? उससे भी अहम बात यह है कि जनवादी और प्रगतिशील साहित्य के नाम पर वहां क्या परोसा जा रहा है? जनता के साहित्य का विचार-पक्ष क्या आज बहुत कमजोर नहीं है? क्या परम्परा, विरासत, वर्तमान सामाजिक जीवन की संरचना आदि की जानकारी की स्थिति चिन्तनीय नहीं है? क्या छद्म वाम का घटाटोप और नकली चिन्तक-मुद्राओं का बाहुल्य नहीं है? और ये तो महज कुछ लक्षण हैं। हमें जनता के सांस्कृतिक आन्दोलन की सभी समकालीन समस्याओं-चुनौतियों की जड़ों तक पहुंचना होगा। हमारा आग्रह है कि पहले परिपत्र के रूप में प्रेषित हमारे प्रस्ताव पर एक बार फिर गौर करें। साथ ही, उस पर्चे को भी देखें जो ‘साझा सांस्कृतिक अभियान’ की इलाहाबाद संगोष्ठी (9-11 अप्रैल 1999) में हमारी ओर से प्रस्तुत किया गया था (‘जनता के सांस्कृतिक आन्दोलन की चुनौतियां’, ‘दायित्वबोध’, अक्टूबर-दिसम्बर 1999 अंक में प्रकाशित)। साझा सांस्कृतिक अभियान की विफलता ने यही सिद्ध किया कि अकर्मक, बुद्धिविलासी, अकादमिक नववामपंथी ‘‘चिन्तकों’’ के साथ कोई साझेदारी सम्भव नहीं। लेकिन हम अपनी उस बुनियादी सोच और प्रस्ताव पर कायम हैं और उसी के एक पक्ष को पूरा करने के लिए ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ की शुरुआत करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक मोर्चे के आज के जो भी जरूरी कार्यभार हैं, उनमें से केवल वैचारिक पक्ष से जुड़े कार्यभारों का निर्वहन ही ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ कर सकेगा। आप एक ही औजार से कई काम नहीं कर सकते।
* * *
हम एक बार फिर अपनी यह सोच साफ कर देना चाहते हैं कि आज का समय एक विश्व-ऐतिहासिक विपर्यय और प्रतिगामी पुनरुत्थान का समय है, जबकि क्रान्ति की धारा पर प्रतिक्रान्ति की धारा हावी है। साथ ही, यह, पूरी दुनिया और हमारे देश के स्तर पर महत्वपूर्ण संक्रमण का भी दौर है। पुनरुत्थान और संक्रमण के ऐसे दौरों में, परिवर्तनकामी शक्तियों के लिए इतिहास का पुनरीक्षण, वर्तमान का विश्लेषण और भविष्य की दिशा तय करने का काम केन्द्रीय बन जाता है, यानी विचार-पक्ष पर जोर बढ़ जाता है। संक्रमणकालीन समाजों में प्रायः कुछ समय के लिए संस्कृति का क्षेत्र विचारधारात्मक संघर्ष का अहम मोर्चा बन जाता है। यह अनायास नहीं कि पिछले दो दशकों के दौरान मार्क्सवाद पर जो भी हमले हुए हैं, प्रायः वे सभी, किसिम-किसिम के ‘‘सांस्कृतिक सिद्धान्तों’’ के रूप में ही हुए हैं। आर्थिक-राजनीतिक दायरे में, कुत्सा-प्रचार और विकृतिकरण के अतिरिक्त, मार्क्सवाद के विरुद्ध कोई भी नया तर्क सामने नहीं आया है। हमारी समझ यह है कि सांस्कृतिक मोर्चे पर अपनी समस्त सर्जनात्मक शक्ति की नई लामबन्दी के लिए हमें इन कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी :
(1) पूरी दुनिया और अपने देश के स्तर पर सामाजिक-आर्थिक संरचना में आये परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन आये हैं तथा सांस्कृतिक आक्रमण और वर्चस्व के जो नये रूप विकसित हुए हैं, उन्हें सांगोपांग समझना होगा ताकि प्रतिकार की कारगर रणनीति विकसित की जा सके।
(2) परवर्ती पूंजीवाद की नई-नई विचार-सरणियों–तमाम संस्कृति-सिद्धान्तों की सुसंगत मार्क्सवादी समझ बनानी होगी।
(3) विरोध का स्वांग रचने वाले तथा चिन्ता और चिन्तन की नकली मुद्राएं धारे हुए भांति-भांति के निठल्ले नववामपंथियों, ‘‘अध्ययन-कक्ष के योद्धाओं’’ और ‘‘मुक्त चिन्तकों’’ के चिन्तन का पोस्टमार्टम करना होगा जो मात्र शंका और संशय प्रकट कर रहे हैं, अतीत के प्रति पूर्ण निषेधवादी रवैया अपना रहे हैं, मुक्त चिन्तन के आकाश में उड़ानें भर रहे हैं और सत्ता-प्रतिष्ठानों द्वारा निशा-निमंत्रण की बेकल प्रतीक्षा कर रहे हैं।
(4) साथ ही, संस्कृति के क्षेत्र में उन जड़सूत्रवादियों से भी टकराना होगा, जिनके लिए भविष्य की हर समस्या का समाधान अतीत के प्रयोगों में मौजूद है और जो लकीर की फकीरी से पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।
(5) सांस्कृतिक मोर्चे पर नई पीढ़ी की पूरी तैयारी के लिए, यह अनिवार्य है कि अतीत में, सर्वहारा संस्कृति के हर क्षेत्र में जो भी वैचारिक-सैद्धान्तिक कार्य और प्रयोग हुए हैं तथा बुर्जुआ शिविर पर जो आक्रमण और उनके आक्रमणों के जो प्रतिकार हुए हैं, उनसे युवा रचनाकारों-संस्कृतिकर्मियों को परिचित कराया जाये।
(6) विश्व स्तर पर और देश स्तर पर प्रतिक्रिया और पुनरुत्थान की बर्बरतम शक्ति के रूप में–फासीवाद के नये उभार को समझना होगा, फासीवाद की संस्कृति और आक्रामक सांस्कृतिक उपकरणों को समझना होगा, अतीत के अनुभवों का नये सिरे से समाहार करना होगा तथा प्रतिरोध की कारगर रणनीति तैयार करते हुए सांस्कृतिक कार्यभार तय करने होंगे।
(7) प्रगतिशील, जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलन के इतिहास का पुनर्मूल्यांकन और समाहार करना होगा। इस सन्दर्भ में स्त्री-प्रश्न, दलित-प्रश्न, भाषा-प्रश्न और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रश्न पर सही ऐतिहासिक-भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा तथा इन प्रश्नों की आड़ में जन-एकजुटता को विघटित करने के दुष्प्रयासों को भी समझना होगा।
इन मूल बिन्दुओं और इनसे जुड़े सहायक बिन्दुओं की विस्तृत चर्चा पहले परिपत्र में की जा चुकी है। इन्हीं दायित्वों को हम आज के नये सर्वहारा पुनर्जागरण और नये सर्वहारा प्रबोधन के सांस्कृतिक कार्यभार के रूप में रेखांकित करते हैं।
कुछ साथियों ने पहले परिपत्र की भाषा का प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें। पहली बात यह कि हमने सचेतन तौर पर कोई शब्दाडम्बर नहीं रचा है। नई स्थितियों और कार्यभारों को सही-सटीक सूत्रबद्ध करने की कुछ कठिनाइयां होती हैं और जोखिम भी होते हैं क्योंकि प्रायः गलत समझ लिये जाने का खतरा रहता है। हमने भरपूर सावधानी बरती है। फिर भी, एक हद तक यह हमारी क्षमता-योग्यता की कमी है, जिस पर हम ध्यान देंगे। दूसरे, यह हमारी भाषा (हिन्दी) की एक कमी है जिसके कारण इतिहास में मौजूद हैं कि जब भी अभिव्यक्ति की वैज्ञानिक शुद्धता-सटीकता की जरूरत होती है तो तत्सम शब्दों की बहुलता हो जाती है और वाक्य-संरचना जटिल हो जाती है। तीसरी बात, इस सच्चाई की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाषा वैसी ही बन जाती है जैसा कि विचारों का बोझ उठाने के लिए जरूरी होता है (बेशक इसमें व्यक्तिगत क्षमता का प्रश्न भी है)। आज हिन्दी साहित्य में दो अतियों के छोर मौजूद हैं–एक ओर तो उत्तर-आधुनिकतावादियों और उनसे प्रभावित अकादमिक मार्क्सवादियों की ऐसी बुझौवल वाली भाषा है जो देवभाषा में वर्णित रहस्यमय दैवी सूक्तियों-मंत्रों का अनुवाद लगती है और दूसरी ओर लोकप्रियता और सरलता का एक बालसुलभ हठ। चौथी बात, किसी बात की भाषा इससे तय होती है कि वह बात किससे की जा रही है, यानी ‘टारगेट रीडर’ कौन है! परिपत्र हिन्दी के जनपक्षधर लेखकों-संस्कृतिकर्मियों को सम्बोधित है। राजेन्द्र यादव जी ने हमें पत्र लिखा है कि हम इस परिपत्र का अनुवाद भी भेज दें। उनसे तो बस यही कहा जा सकता है कि अतीत को मुड़-मुड़कर देखते हुए वे आजकल जिस भाषा में लिखने-पढ़ने-बोलने-सुनने के आदी हो गये हैं, उस भाषा में अनुवाद हमारे बूते की बात नहीं है। यह सिद्धपुरुषों का काम है।
एक और साथी का पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे साथ मतभेद रखते हुए अपना यह मत प्रकट किया है कि ‘‘आज संस्कृति का क्षेत्र विचारधारात्मक वर्ग-संघर्ष की केन्द्रीय भूमि नहीं बना हुआ है बल्कि खुद विचारधारात्मक (रेखांकन साथी का) क्षेत्र ही यह केन्द्रीय भूमि बना हुआ है।’’ स्थापनाओं के इस मतभेद और इनके पीछे की सोचों पर बहस हो सकती थी, अगर हमारे विद्वान साथी की बात इतनी ही होती तो! लेकिन नहीं, इन साथी को तो शंका यह है कि हम राजनीतिक दायित्वों को तिलांजलि दे देना चाहते हैं, वर्ग-संघर्ष के मैदान से भाग जाना चाहते हैं और इसीलिए साहित्य-संस्कृति को अपना ‘‘प्रधान कार्य’’ (??) बना रहे हैं। साथी के ख़याल से राजनीतिक क्षेत्र शायद खेत है जबकि सांस्कृतिक क्षेत्र वर्ग-संघर्ष के ताप से रहित फूलों की क्यारी। तभी तो वे हमें फटकार लगाते हैं : ‘‘क्या हम फूल की क्यारियों की चिन्ता करेंगे जब खेत के खेत जल रहे हैं?’’ इस परले दर्जे की कठमुल्लावादी मूर्खता से बहस चलाना तो ‘‘आदिकालीन वर्ग-संघर्ष की ओर वापसी’’ का ही एक रूप होगा या फिर दीवार से सिर टकराने जैसा अहमकपन। नववामपंथी ‘‘मुक्त चिन्तक’’ और अगिया बैतालों की यह नई ब्राण्ड, वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहरहाल, ‘‘वामपंथी’’ लफाजी की खुजली खुजलाने का अपना मजा है। और कुछ की खुजली तो एक्ज़िमा बन चुकी है। उन्हें खुजलाने का आनन्द लूटने दें और हम अपना काम करें।
* * *
सृजन परिप्रेक्ष्य का प्रवेशांक (शिशिर-बसन्त अंक 2002) अप्रैल महीने के प्रथमार्द्ध में आपके हाथों में होगा। इस अंक को हम अपनी सोच के हिसाब से बहुत सही और सन्तुलित ढंग से संगठित तो नहीं कर पाये हैं, फिर भी हम समझते हैं कि पत्रिका की दिशा और फ्रेमवर्क को यह काफी हद तक स्पष्ट कर देगा।
सहकर्मियों से हमारा आग्रह है कि सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक आन्दोलन और कलात्मक सृजन के विविध वैचारिक प्रश्नों पर लेख भेजकर, मतभेद दर्ज कराकर, बहस में हिस्सा लेकर वे इस महत्वाकांक्षी अभियान में शामिल हों। लेखों में प्रस्तुत अवस्थितियों के विरोधी विचारों को स्थान देने और बहस चलाने के लिए हम वाद-विवाद-संवाद स्तम्भ नियमित चलायेंगे। कविता, कहानी, नाटक आदि हम नियमित रूप से नहीं प्रकाशित करेंगे। केवल वही समकालीन रचनात्मक लेखन प्रकाशित होगा जिसे हम अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रयोगधर्मी या प्रवृत्ति-निरूपक की कोटि का समझेंगे।
पत्रिका की सामान्य रूपरेखा और मूल्य आदि की चर्चा पहले परिपत्र में की जा चुकी है। याददिहानी के लिए इस बार भी इनका विवरण प्रकाशित किया जा रहा है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पत्रिका किसी भी प्रकार का संस्थागत अनुदान नहीं लेगी। व्यक्तिगत सहयोग, सदस्यता और विक्रय इसके मुख्य वित्तीय आधार होंगे। विज्ञापन की भी एक स्पष्ट नीति है। सिर्फ साहित्यिक प्रकाशकों और कुछ चुनिन्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन ही हम देंगे, बशर्ते कि उनके साथ कोई शर्त न हो और प्रकाश्य विज्ञापन सामग्री हमें आपत्तिजनक न लगे। हमारा आग्रह है कि वार्षिक सदस्यता लौटती डाक से ही भेज दें, नीचे दिये गये किसी भी पते पर। जो साथी औसत मध्यवर्गीय स्तर का भी जीवन बिताते हैं, वे थोड़ी तकलीफ उठाकर भी आजीवन सदस्यता और विशेष सहयोगी सदस्यता की धनराशि भेजें, ताकि पत्रिका का एक स्थायी कोष हम जल्दी से जल्दी स्थापित कर सकें।
एक और अनुरोध। पहला परिपत्र यदि आपको न मिला हो तो इसे डाक विभाग की कृपा समझकर हमें तत्काल सूचित करें। हो सकता है कि हमारे पतों के रजिस्टर में आपका पुराना या गलत पता दर्ज हो।
शुभकामनाओं और बिरादराना अभिवादन सहित,
कात्यायनी, सत्यम
18 फरवरी, 2002