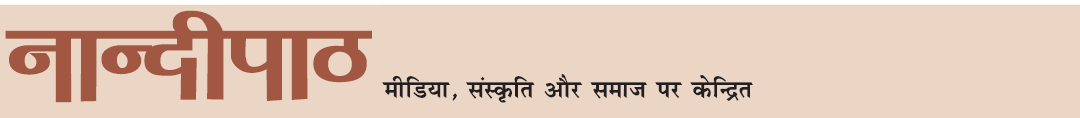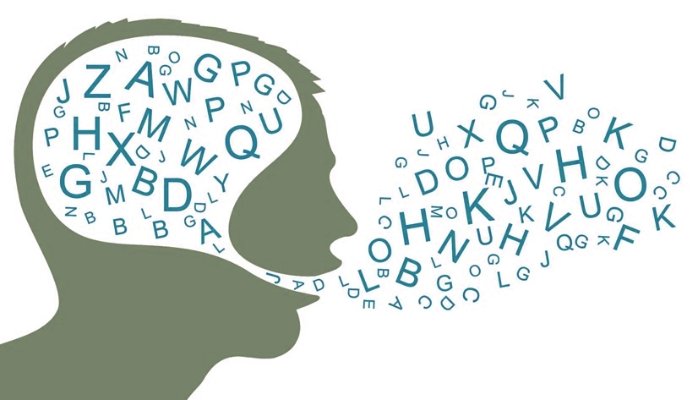भाषा–विज्ञान के इतिहास में मार्क्सवाद और वोलोशिनोव
कात्यायनी / सत्यम
मानव–चिन्तन और संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों की खोज में आगे बढ़ते हुए, भाषा के प्रश्न से दर्शन की मुठभेड़ प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। मानव–समाज की समस्त भौतिक और आत्मिक गतिविधियों के दौरान संज्ञानात्मक और संसर्गात्मक प्रकार्यों (Function) की पूर्ति करनेवाली आधारभूत संकेत–प्रणाली के रूप में भाषा के विकास, उसकी प्रकृति और संरचना के अध्ययन के साथ–साथ, अव्यवस्थित ढंग से ही सही, पर शताब्दियों तक, दार्शनिक इन प्रश्नों से भी जूझते रहे कि भाषा किस हद तक मनुष्य की अन्य प्राणियों से इतर, प्राकृतिक–जैविक विशिष्टता की उपज है और किस हद तक यह एक सामाजिक परिघटना है।
यह धारणा मार्क्सवाद के जन्म से पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुकी थी कि भाषा एक सामाजिक परिघटना है जो मानव कार्य–कलाप के समन्वय का साधन है। ऐतिहासिक भौतिकवाद ने भाषा–वैज्ञानिक चिन्तन को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त धारणा में यह बात जोड़ी कि भाषा सामाजिक उत्पादन के विकास के दौरान जन्म लेती है तथा उत्पादन–सम्बन्धों के कुल योग के आधार पर जीवन की जो आम सामाजिक–बौद्धिक–राजनीतिक प्रक्रिया गतिमान होती है, उसका माध्यम बनने के साथ ही, उसके दौरान, उसके साथ–साथ, सतत् विकसित भी होती रहती है।
समाज–विज्ञान या मानविकी की एक पृथक् प्रशाखा के रूप में, भाषा–विज्ञान का उन्नीसवीं शताब्दी से पहले अस्तित्व नहीं था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक यह तर्कशास्त्र से अलग नहीं माना जाता था। उस समय तक दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र के एक अंग के तौर पर, चिन्तन की अभिव्यक्ति के एकीकृत, सार्वभौमिक साधनों का अध्ययन भाषा–विज्ञान का विषय था।
तर्कशास्त्रीय भाषा चिन्तन की दो सहस्राब्दियाँ
भाषा के अध्ययन की प्राचीनतम अवस्थाएँ हमें प्राचीन यूनान और भारत में देखने को मिलती हैं। अफलातून (पाँचवी–चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) के प्रसिद्ध दार्शनिक संवादों में, पहली बार, विचारों के पाठ (text) में रूपान्तरण की परिकल्पनाओं (“प्रकल्पों” या “model”) की एक पूरी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। अफलातून का कहना था कि वस्तुओं का सारतत्त्व (“वस्तुगत विचार”) आत्मगत मानव–संज्ञान में विविध पक्षों से परावर्तित होता है और तदनुरूप, विभिन्न नामों द्वारा द्योतित–निरूपित होता है। अरस्तू (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) ने तर्कशास्त्र का पूरक अंग मानते हुए भी भाषा को अफलातून से अधिक महत्त्व दिया। अरस्तू की तर्कशास्त्रीय–भाषावैज्ञानिक अवधारणा का प्रस्थान–बिन्दु है-शब्द–अवधारणाओं (logoi) की व्यवस्था जो प्रवर्गों में बँट जाती है और अन्त में वह उद्गारों और निर्णयों और उनके पूर्वापर सम्बन्धों के विभिन्न प्ररूपों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अरस्तू ने अपनी दार्शनिक प्रणाली में वस्तुगत अस्तित्वों की उच्चतम व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले दस प्रवर्गों की अवधारणा प्रस्तुत की। इन प्रवर्गों में सारतत्त्व, परिमाण, गुण और सम्बन्ध सहित कठोर पद–सोपानिक क्रम में विधेय के वे सभी रूप (संज्ञा–रूपों से लेकर क्रिया–रूपों तक तथा स्वतंत्र रूपों से लेकर सापेक्षत: निर्भर रूपों तक) शामिल थे जो प्राचीन यूनानी भाषा के एक सरल वाक्य में पाए जा सकते थे। अरस्तू पहला क्लासिकी चिन्तक था जिसने व्याकरणिक रूपों की समस्या को छुआ और शब्दों की विभिन्न व्याकरणीय कोटियों के लिए एक शब्दभेद–सिद्धान्त विकसित किया।
भारत में ऐन्द्र, शाक्तायन, यास्क आदि वैयाकरणों की पाणिनी पूर्व काल में लम्बी परम्परा थी, लेकिन इनमें से यास्क का ‘निरुक्त’ ही विस्मृत होने से बच सका। अपने पहले की परम्पराओं को आगे विकसित करते हुए पाणिनी (पाँचवी–चौथी शताब्दी ईसा–पूर्व) ने अफलातून और अरस्तू द्वारा आम दार्शनिक चिन्तन के तन्तुबद्धीकरण की प्रक्रिया में भाषा पर चिन्तन की प्रवृत्ति से अलग हटकर भाषा–प्रश्न को एक स्वतंत्र–स्वायत्त प्रश्न के रूप में उठाया। व्याकरण की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘अष्टाध्यायी’ में पाणिनी ने, अर्थ–विज्ञान (semantics) की किसी प्रणाली के बग़ैर ही, संस्कृत के स्वर–विज्ञान (phonetics), आकृति–विज्ञान (morphology), शब्द–संरचना और वाक्य–विन्यासगत तत्त्वों पर विस्तार से विचार किया। पाणिनी शब्द के मूल, प्रत्यय और धातु की अवधारणाएँ तथा शब्द–रूपों के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत करनेवाले पहले व्यक्ति थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यादृच्छिक प्रतीकात्मक वर्णनात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। कई मायने में पाणिनी का व्याकरण बीसवीं शताब्दी के भाषाशास्त्रीय अध्ययनों के स्तर का है। पाणिनी की चिन्तन–परम्परा को उत्तरवर्ती काल में नागेश भट्ट, कुन्द भट्ट, कात्यायन, पतंजलि और भर्तृहरि ने आगे विकसित किया। इसी भारतीय व्याकरण–परम्परा में स्फोट सिद्धान्त का प्रवर्तन हुआ जिसमें ठोस भाषिक–रूपों के आदि–प्ररूप (प्रोटो–टाइप) देखने को मिलते हैं।
यूरोपीय संस्कृति के बाहर सर्वाधिक सांगोपांग विकसित तर्कशास्त्रीय–भाषावैज्ञानिक अवधारणाएँ यदि कहीं दीखती हैं तो वह है नव्य–न्याय का भारतीय दर्शन जिसका सूत्रपात तेरहवीं शताब्दी में हुआ। नव्य–न्याय की चिन्तनधारा प्रवर्गों पर आधारित ‘अप्रोच’ की अरस्तू की अवधारणा से मिलती–जुलती थी, लेकिन नव्य–न्यायवादी ‘जेण्डर’ और विधेय के रूपों के बजाय प्रारम्भिक प्रवर्गों को ही गुण मानते थे। वे भाषा के सारतत्त्व और नामों के अर्थों का वास्तविक, वस्तुपरक अस्तित्व स्वीकार करते थे। वे मानते थे कि ज्ञान यदि सत्य है तो वह एक वस्तुगत तथ्य है। अरस्तू की ही तरह नव्य–न्याय का दर्शन भी सीधे भाषा पर निर्भर था।
यहीं पर प्रारम्भिक स्टोआ काल (तीसरी–दूसरी शताब्दी ईसा–पूर्व) के जेनो और क्रिसिप्पस आदि स्टोइक पन्थ के दार्शनिकों की भी चर्चा ज़रूरी है जिन्होंने उद्गार (utterance) पर आधारित एक तर्कसंगत ‘अप्रोच’ विकसित किया। पहली बार उन्होंने यह खोज की कि उद्गार के दो विषय होते हैं : पहला, टेलोस (telog), यानी यथार्थ जगत की कोई वस्तु [बीसवीं शताब्दी की तर्कशास्त्रीय और भाषा–वैज्ञानिक शब्दावली में “संकेत या व्याप्ति की वस्तु”( object of denotation), “संकेतित” (denotete), “अभिप्राय या आशय” (meaning) या, “विस्तारात्मक़ (extensional),] और दूसरा, लेक्टोन (lecton), कोई विशिष्ट, अमूर्त सारतत्त्व ख्बीसवीं शताब्दी की अर्थ–वैज्ञानिक (semantic) शब्दावली में “अभिप्रेत” (intentional), द्योतक अथवा अर्थ–संकेतक (signifier),। अफलातून या अरस्तू के विपरीत, स्टोइकों ने उद्गार की अन्तर्वस्तु का तर्कपूर्ण–परीक्षण, अमूर्त अवधारणाओं या किसी एक विशिष्ट टाइप या क़िस्म के सार–तत्त्वों के समुच्चय के रूप में नहीं, बल्कि एक इकाई के रूप में, अवधारणाओं, अवबोधों और मानवीय भावनाओं के एक सम्मिलन के रूप में किया। ‘लेक्टोन’ स्वीकरण या अस्वीकरण से अधिक व्यापक, ज्ञान का एक विशिष्ट रूप था, जिसकी सादृश्यता काफ़ी हद तक ज्ञान की प्राचीन भारतीय अवधारणा के साथ स्थापित की जा सकती है।
यूनानी और भारतीय भाषा–वैज्ञानिक चिन्तन की परम्पराओं के ही प्रभाव में प्राचीन अरबी भाषा–विज्ञान का भी विकास हुआ जिसका स्वर्ण युग सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच माना जा सकता है जब शब्दकोश–कला (lexicography) का विकास हुआ, अरबी व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक ‘अल–क़िताब’ और फिरुज़ाबादी का शब्दकोश प्रकाशित हुए। इस दौरान अरबी और अन्य सामी भाषाओं की अभिलाक्षणिकताओं के अध्ययन हुए, इनके त्रिपक्षीय मूलों को, जो इनकी एक विशिष्टता थी, परिभाषित किया गया और ध्वनियों के उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया गया। अरबी भाषा–विज्ञान में पहली बार शब्दों और ध्वनियों के बीच फ़र्क़ किया गया। अरब विद्वानों द्वारा प्रस्तावित धातुओं और प्रत्ययों की परिभाषाओं ने उन्नीसवीं शताब्दी के, ख़ास तौर पर, फ्रांत्स बॉप के, भाषा–वैज्ञानिक अध्ययनों को काफ़ी प्रभावित किया।
भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में तर्कशास्त्रीय प्रवृत्ति का वर्चस्व कमोबेश अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक बना रहा, हालाँकि तब तक अरस्तू के और स्टोइकों के बहुतेरे विचार भुलाए जा चुके थे। फ्रांस के पोर्ट–रोयाल भाषा–वैज्ञानिकों द्वारा विकसित व्याकरण और तर्कशास्त्र के सिद्धान्त इस प्रवृत्ति के विकास के चरम–बिन्दु थे। पोर्ट–रोयाल के भाषा–वैज्ञानिकों ने अवधारणा, निर्णय और नौ शब्द–भेदों (parts of speech) जैसे भाषा के तर्कशास्त्रीय रूपों को सभी भाषाओं के लिए सामान्य, सार्वभौमिक रूप माना। तर्कशास्त्रीय प्रवृत्ति के इस सामान्य फ्रेमवर्क का सकारात्मक पहलू यह था कि इसने मनुष्य के एक सार्वभौमिक गुण के रूप में भाषा का अध्ययन करने की दिशा में, एक सार्वभौमिक व्याकरण की रचना की दिशा में और ऐसे अध्ययनों की एक सामान्य पद्धति के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण क़दम उठाए। लेकिन इनका नकारात्मक पहलू यह था कि विश्व की अलग–अलग भाषाओं की विशिष्ट ऐतिहासिक भिन्नताओं की उपेक्षा की गई। भाषा–विज्ञान की यह प्रवृत्ति उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक विभिन्न भाषाओं के विद्वत्तापूर्ण व्याकरणों के आधार के रूप में इस्तेमाल होती रही और बीसवीं शताब्दी में भी व्याकरण की शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है।
भाषा–विज्ञान की परिपक्व अवस्था : ऐतिहासिक–तुलनात्मक भाषा–विज्ञान का उद्भव और विकास
भाषा–विज्ञान के विकास की अगली मंज़िल की शुरुआत अठारहवीं शताब्दी के अन्त से मानी जा सकती है जब ऐतिहासिक–तुलनात्मक अध्ययन–पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। ऐतिहासिक–तुलनात्मक भाषा–विज्ञान शुरू में एक पूर्णत: स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखा गया जिसके अभिलाक्षणिक बुनियादी सिद्धान्त निम्नलिखित थे :
(i) प्रत्येक भाषा के अपने विशिष्ट गुण–धर्म होते हैं जो उसे अन्य भाषाओं से अलग पहचान देते हैं। ये विशिष्ट गुण–धर्म तुलना के द्वारा पहचाने जाते हैं।
(ii) भाषाओं की तुलना उनके बीच के उन सम्बन्धों को उद्घाटित करती है जो एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए रहते हैं। वह स्रोत मूल भाषा (parent language) होती है। वह एक जीवित भाषा हो सकती है या मृत हो सकती है। भाषाओं का वंश–विषयक प्रवर्गीकरण सम्बन्धित भाषाओं को अलग–अलग समूहों में ऐक्यबद्ध करता है, जैसे कि जर्मेनिक या स्लाविक भाषाएँ। और फिर ये समूह वृहत्तर भाषा–परिवारों में संगठित होते हैं, जैसे कि इण्डो–यूरोपियन, फिनो–उग्रिक या सामी भाषा–परिवार।
(iii) सम्बन्धित भाषाओं के बीच के विभेदों की व्याख्या सिर्फ़ भाषाओं के सतत ऐतिहासिक परिवर्तन के आधार पर ही की जा सकती है। यह परिवर्तन हर भाषा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गुण होता है।
(iv) भाषाओं के ऐतिहासिक परिवर्तन में, दूसरे तत्त्वों के मुक़ाबले ध्वनियाँ अधिक तेज़ी से बदलती हैं। किसी एक भाषा के भीतर ध्वनि–रूपान्तरण पूरी तरह से नियमबद्ध ढंग से होते हैं और उन्हें स्वर विज्ञान के नियमों के अनुसार स्पष्टत: सूत्रबद्ध किया जा सकता है। किसी भाषा के मूल तत्त्व-शब्द मूल, प्रत्यय, और विभक्तियाँ-हजारों वर्षों तक स्थिर–अपरिवर्तित बनी रहती हैं।
(v) ऐतिहासिक परिवर्तनों के आधार पर, पहले मौजूद रही किसी सर्वनिष्ठ भाषा की सामान्य अभिलाक्षणिकताओं का पुन:कल्पन या पुनर्गठन (reconstruction) किया जा सकता है (इसके पूर्व यह माना जाता था कि किसी मूल भाषा का पूरी तरह से पुन:कल्पन किया जा सकता है)।
मूल भाषा और पुन:कल्पन की अवधारणाओं ने भाषा के सामान्य अध्ययन और अलग–अलग विशिष्ट भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्प्रेरक और उपकरण की भूमिका निभाई। भाषा के मुख्य तत्त्वों के स्थायित्व की धारणा ने विद्वानों को उसे (यानी भाषा को) एक विशेष क़िस्म की स्वतंत्र प्रणाली (system) या व्यवस्था मानने के विचार तक पहुँचाया। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में, अधिकांश भाषा–वैज्ञानिक भाषा को एक अंगभूत या समाकलित (integral) प्रणाली मानने के बजाय यह मानते थे कि यह परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील-दो प्रकार के तत्त्वों से संघटित होती है। ये तत्त्व ही तुलनात्मक–ऐतिहासिक व्याकरण के विषय होते हैं, जो तुलनात्मक–ऐतिहासिक पद्धति के साधनों से निर्मित होता है।
इन विचारों को सूत्रबद्ध करने का काम पहली बार फ्रांत्स बॉप और रास्मस क्रिश्चियन रास्क ने किया। फिर फ्रेडरिक फ़ॉन श्लेगेल, जैकब ग्रिम और वोस्तोकोव आदि ने इन्हें आगे विकसित किया। पहली बार बॉप के तुलनात्मक व्याकरण (1833) ने इन विचारों को ठोस रूप दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विभिन्न इण्डो–यूरोपियन भाषा–समुदायों के ऐतिहासिक–तुलनात्मक व्याकरण तैयार किए गए जिनमें ग्रिम (जर्मेनिक भाषा–समूह), दिएज़़ (रोमान्स भाषा–समूह) और मिक्लोसिक (स्लाविक भाषा–समूह) के व्याकरण उल्लेखनीय हैं। फिर इनके आधार पर, रेनान ने सामी भाषा–समूह के भी तुलनात्मक–ऐतिहासिक व्याकरण की पुस्तक तैयार की। एक नया समाहारमूलक अध्ययन ऑग्यूस्त श्लीखर की व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक (1861-62) में सामने आया जो एक सामान्य इण्डो–यूरोपियन मूल भाषा की अवधारणा पर आधारित था। डार्विनवाद के जीवशास्त्रीय सिद्धान्तों को लागू करते हुए श्लीखर ने यह विचार प्रतिपादित किया कि भाषा एक विकासमान ‘आर्गेनिज़्म’ के समान होती है। इन विचारों के आधार पर भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में जीवशास्त्रीय प्रकृतवाद का विचार भी उभरा, लेकिन वह अल्पप्रचलित और अल्पजीवी ही सिद्ध हुआ।
तुलनात्मक–ऐतिहासिक भाषा–विज्ञान के दृष्टिकोण के समान्तर और साथ ही, काफ़ी हद तक उसी के फ्रेमवर्क के भीतर, कार्ल विल्हेल्म फ़ॉन हम्बोल्ट ने अपना भाषा–वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसका न सिर्फ़ उन्नीसवीं शताब्दी में, बल्कि बीसवीं शताब्दी में उससे भी अधिक प्रभाव रहा। हम्बोल्ट जर्मन दार्शनिक काण्ट के प्रागनुभविक प्रत्ययवाद और अज्ञेयवाद से प्रभावित थे और “वस्तु–निजरूप” (thing in itself) की दार्शनिक अवधारणा की ही तरह भाषा को एक स्वत:स्फूर्त (self contained) प्रणाली के रूप में देखते थे, एक ऐसी व्यवस्था के रूप में, जो अन्तिम नहीं है बल्कि “जन समुदाय की गूढ़–गहन स्पिरिट” को अभिव्यक्त करनेवाली “सक्रियता” के रूप में निरन्तर सृजित हो रही है। आगे चलकर बीसवीं शताब्दी की नवहम्बोल्टवादी और संरचनावादी भाषा–वैज्ञानिक विचार–सरणियों पर हम्बोल्ट के चिन्तन का गहरा प्रभाव मौजूद रहा।
तुलनात्मक–ऐतिहासिक भाषा–विज्ञान के ही फ्रेमवर्क से एक और शाखा जो फूटी वह जर्मन विद्वान स्टाइन्थाल और कुछ अन्य भाषा–वैज्ञानिकों द्वारा प्रवर्तित मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति थी जो भाषा–विज्ञान के तर्कशास्त्र से किसी भी क़िस्म के बुनियादी सम्बन्ध को अस्वीकार करती थी और मनोवैज्ञानिक नियमों की एकता के आधार पर मानवीय भाषा की एकता की व्याख्या करती थी जबकि भाषाओं की विविधता की व्याख्या वह अलग–अलग जन–समुदायों की मनोवृत्तियों की विशिष्ट अभिलाक्षणिकताओं के आधार पर करती थी। प्रसिद्ध उक्रइनी–रूसी भाषाविद् पोतेब्निया भी इसी धारा के विचारों को मानता था। उसने इन विचारों को आगे विकसित किया। पोतेब्निया की अवधारणा के अनुसार, भाषा का अध्ययन मनुष्य द्वारा चिन्तन में, मानस में, भाषा में और कलात्मक सृजन में, वस्तुगत जगत के अभिज्ञान को प्रकट करता है। पोतेब्निया–स्कूल के अनुसार, चिन्तन सुनिश्चित अर्थ–वैज्ञानिक (semantic) नियमों के अनुसार भाषा के घनिष्ठ सहयोजन में विकसित होता है। इन नियमों में संकेत–प्रतिस्थापन (sign substitution) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जो शब्दों में (शब्द के अतिरिक्त रूप के स्तर पर) भी होता है और वाक्यों के अर्थगत और विन्यासगत रूपान्तरण (शब्द–भेदों यानी parts of speech के प्रतिस्थापन) में भी होता है। तुलनात्मक–ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक भाषा–विज्ञान के विकास के आधार पर जो शोध–पद्धतियाँ विकसित हुर्इं, उनसे विशेष तौर पर, भाषा के रूपों के अध्ययन और पुनर्रचना से जुड़े उपक्रमों को विशेष लाभ मिला।
रूसी विद्वान फोर्तुनातोव ने भाषा के संरचनागत पक्षों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। मनोवैज्ञानिक भाषा–अध्ययन के आधार पर परवर्ती उन्नीसवीं शताब्दी में, तुलनात्मक–ऐतिहासिक भाषा–विज्ञान की एक और प्रशाखा नवव्याकरणवाद (neogrammerianism) सामने आई जिसका आधारभूत सिद्धान्त जर्मन भाषा–वैज्ञानिक ओस्थोफ और ब्रुगमान ने अपनी पुस्तक ‘मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ इन दि इण्डो–यूरोपियन लैंग्वेजेज़’ (भाग 1-6, 1878–1910) में तथा एच– पॉल ने ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ दि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज’ (1880) में प्रस्तुत किया। इन पुस्तकों को नवव्याकरणवाद का घोषणापत्र माना गया। किसी भी भाषा के अध्ययन का, विशेष तौर पर आकृति–विज्ञान (morphology) की दृष्टि से इसकी संरचना या रूप की पुनर्रचना का, आधार तैयार करने के साथ ही इन नववैयाकरणों ने मनोवृत्तिगत नियमों की एकता और वक्तृत्व के स्वर–विज्ञानगत या ध्वन्यात्मक (phonetic) नियमों की अपरिवर्तनीयता के विचारों को बढ़ावा दिया।
उन्नीसवीं शताब्दी में तुलनात्मक–ऐतिहासिक भाषा–विज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका यह रही कि उसने भाषाओं की तुलना तथा उनके लुप्त रूपों और नियमों की पुनर्रचना की श्रमसाध्य पद्धति विकसित की। वृहद भाषा–परिवारों के, विशेष तौर पर इण्डो–यूरोपियन परिवार के, इतिहास के अध्ययन में तथा जीवित भाषाओं में होनेवाले परिवर्तनों के प्रमुख स्वर–विज्ञान विषयक तथा अर्थ–विज्ञान विषयक नियमों को स्थापित करने में इसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। लेकिन इस प्रवृत्ति के समक्ष एक संकट यह पैदा हुआ कि भाषा–वैज्ञानिक अध्ययन के विषय के-भाषा और मानसिक स्थिति–संरचना के रूप में जारी विभाजन की प्रवृत्ति की परिणति अनेक द्वैतवादी सादृश्यों के रूप में सामने आई, जैसे, ध्वनि और ध्वनि की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति, तथा अर्थ (meaning) और अर्थ की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति। उत्तरवर्ती दौर में, मनोवैज्ञानिक और नवव्याकरणीय प्रवृत्तियों सहित, तुलनात्मक–ऐतिहासिक भाषा–वैज्ञानिक अध्ययन की धारा की एक नकारात्मक प्रवृत्ति यह विकसित हुई कि भाषा के तंत्र के सामग्रिक अध्ययन का स्थान अनेकश: छोटे–बड़े, अविच्छिन्न उपादानों (जैसे ध्वनियाँ, शब्द–रूप आदि–आदि) के विश्लेषण ने ले लिया। व्यक्तिगत मनोविज्ञान और व्यक्तिगत वक्तृत्व (speech) की भूमिका बढ़ा–चढ़ाकर देखी जाने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति के वक्तृत्व को “एकमात्र भाषा–वैज्ञानिक यथार्थ” की मान्यता दी जाने लगी।
संरचनावादी भाषा–विज्ञान की विकास–यात्रा
नवव्याकरणवाद के उपरोक्त संकट ने एक नई धारा-संरचनावादी भाषा–विज्ञान या भाषा–वैज्ञानिक संरचनावाद के उद्भव और विकास का आधार निर्मित करने में अहम भूमिका निभाई। संरचनावादी भाषा–विज्ञान संरचनावादी दार्शनिक–सौन्दर्यशास्त्रीय विचारसरणि के ‘फ्रेमवर्क’ के भीतर ही विकसित हुआ था, या यूँ कहें कि उसी की एक प्रशाखा या उपधारा था। दरअसल, बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में, मानविकी के क्षेत्रों में विषयों और वस्तुओं की आन्तरिक संरचना को प्रकट करनेवाली एक ठोस वैज्ञानिक पद्धति के रूप में संरचनावाद का जन्म प्रत्यक्षवादी विकासक्रमवाद (positivist evolutionism) की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ था और इसी के समान्तर संरचनावादी भाषा–विज्ञान का विकास नवव्याकरणवाद के प्रतिक्रियास्वरूप हुआ था।
संरचनावाद ने साहित्य–कला की आलोचना, मनोविज्ञान, नृजातिविज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रकृति–विज्ञानों द्वारा विकसित संरचनात्मक अन्वेषण–विधियों का इस्तेमाल किया। यह अनुसन्धान के विषयों या वस्तुओं की वर्तमान अवस्था के वर्णन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनके अन्तर्निहित कालेतर गुणों को उद्घाटित करता है तथा अनुसन्धान का विषय बनी प्रणाली के तथ्यों या तत्त्वों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। विषय का अनुसन्धान करने में संरचनावाद पर्यावलोकित तथ्यों के प्रारम्भिक संगठन से विषय की आन्तरिक संरचना (उसके सोपान, प्रत्येक स्तर पर तत्त्वों के बीच अन्तर्सम्बन्ध) को उजागर करने तथा उनका वर्णन करने की ओर, और उसके बाद विषय का सैद्धान्तिक प्रतिरूप निर्मित करने की ओर आगे बढ़ता है। संरचनावाद के विचारों ने सांस्कृतिक परिघटनाओं के अन्तर्विषयगत अध्ययनों का एकीकरण करने तथा मानविकी और प्रकृति–विज्ञान के क्षेत्रों में गति के नियमों और विश्लेषण–पद्धतियों के बीच की समरूपता को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन संरचनात्मक विधियों के व्यापक प्रयोग ने इसे दार्शनिक प्रणाली के स्तर तक ऊपर उठाने की कोशिशों को जन्म दिया, जो सर्वथा ग़लत थीं। कारण कि एक वैज्ञानिक विधि के रूप में संरचनावाद की संज्ञानात्मक सीमाएँ स्पष्ट हैं। संरचना की अवधारणा के प्रति इसका दृष्टिकोण इतिहास–विरोधी है। साथ ही, वस्तुओं या विचारों की संरचनाओं के विकास तथा परिवर्तन के स्रोत के रूप में संरचनावाद आन्तरिक व्याघातों का या आन्तरिक द्वन्द्वात्मक गति का निषेध करता है।
संरचनावादी भाषा–विज्ञान भी इन्हीं दार्शनिक असंगतियों और संज्ञानात्मक सीमाओं से ग्रस्त था, लेकिन संरचनात्मक विधियाँ जिस हद तक विज्ञान–सम्मत थीं, उसके चलते भाषा–विज्ञान में भी इनके इस्तेमाल के सकारात्मक परिणाम निकले। इनके चलते लिपि रहित भाषाओं के वर्णन तथा अज्ञात भाषाओं की लिपियों की ‘डिकोडिंग’ जैसे काम सम्भव हो सके। संरचनावादी भाषा–विज्ञान के मुख्य सिद्धान्तों को इस रूप में सूत्रबद्ध किया जा सकता है :
(i) मूल और मुख्य यथार्थ किसी भाषा–विशेष का अलग–थलग तथ्य नहीं होता, बल्कि एक प्रणाली (system) के रूप में भाषा का अंग होता है। किसी भाषा का प्रत्येक तत्त्व उक्त प्रणाली के अन्य तत्त्वों के साथ अन्तर्सम्बन्धित रूप में ही मौजूद होता है। प्रणाली अपने तत्त्वों का कुल योग नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत, उन्हें परिभाषित करती है।
(ii) उक्त प्रणाली का संरचनागत ‘फ्रेमवर्क’ कालेतर सम्बन्धों (extratemporal relationships) से निर्धारित होता है तथा व्यवस्था के भीतर के सम्बन्ध व्यवस्था के तत्त्वों को परिचालित करते हैं।
(iii) इसलिए, तत्त्वों की अलग–अलग विशिष्टता या उनकी भौतिकता के बजाय सम्बन्धों के आधार पर भाषा–प्रणाली का कालेतर “बीजगणितीय” अध्ययन सम्भव है और भाषा–विज्ञान में परिशुद्ध गणितीय पद्धतियाँ भी प्रयुक्त हो सकती हैं।
(iv) भाषा एक विशिष्ट प्रकार की प्रणाली अथवा व्यवस्था या तंत्र (system) होती है-एक संकेत–प्रणाली (sign system) होती है जो एक ओर, वस्तुगत तौर पर, मानव–मनोजगत के बाहर, अन्तर्वैयक्तिक अन्तर्सम्बन्धों में, मौजूद रहती है, और दूसरी ओर, मानव–मनोजगत के भीतर मौजूद रहती है।
(v) मानव–समाजों में काम करनेवाली, लोकगीत, रीति–रिवाज़–आचार, अनुष्ठान–कर्मकाण्ड और सगोत्रीय सम्बन्ध आदि अन्य प्रणालियाँ (व्यवस्थाएँ) भी भाषा के ही सदृश संगठित हुई हैं। भाषा की ही तरह इन सभी संरचनाओं का भी भाषा–वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, ख़ास तौर पर, “बीजगणितीय ढंग से” या अन्य साधनों से उन्हें औपचारिक रूप दिया जा सकता है। संकेत–विज्ञान (semiotics) की विधा ख़ास तौर पर संकेतों और संकेत–प्रणालियों का, संकेत–चिह्नित सम्बन्धों की अभिलाक्षणिक विशिष्टताओं का अध्ययन करती है।
संरचनावादी भाषा–विज्ञान का विधिवत प्रारम्भ स्विस भाषा–वैज्ञानिक फर्दिनान्द द सॉस्युर की पुस्तक ‘कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स’ (1916, मरणोपरान्त प्रकाशित) से माना जाता है। सॉस्युर के साथ ही कजान स्कूल के रूसी भाषाविदों-विशेषकर क्रुशेव्स्की और बोदिन द कर्टने ने भाषा–विज्ञान में संरचनागत की ज़मीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।
भाषा सहित सभी संकेत–प्रणालियों के अध्ययन के लिए बीसवीं शताब्दी में एक विशेष विज्ञान-संकेत–विज्ञान (semiotics या semiology) का जन्म हुआ जिसमें सॉस्युर की अहम भूमिका मानी जाती है। सूचनाओं के प्रेषण या अर्थ की अभिव्यक्ति के साथ ही संसर्ग, यानी सम्प्रेषित सूचना का श्रोता/पाठक द्वारा बोध सुनिश्चित करना और संक्रिया की उत्प्रेरणा तथा भावनात्मक प्रभाव किसी भी संकेत–प्रणाली के मुख्य प्रकार्य होते हैं। इन प्रकार्यों की पूर्ति संकेत–प्रणाली के एक सुनिश्चित आन्तरिक संगठन की, यानी भिन्न–भिन्न संकेतों तथा उनके संयोजन के नियमों की उपस्थिति की पूर्वकल्पना करती है। नानाविध प्रकार के प्रकार्यों को निष्पादित करनेवाली संकेत–प्रणालियों की आन्तरिक संरचना के अध्ययन की प्रशाखा संकेत–सम्बन्ध विज्ञान (syntactics) के रूप में विकसित हुई। अर्थ–विज्ञान (semantics) अर्थ व्यक्त करने के साधन के रूप में संकेत–प्रणालियों का अध्ययन करता है। संकेत–प्रयोग विज्ञान (pragmatics) संकेत–प्रणालियों के उनके साथ सम्बन्ध का अध्ययन करता है, जो उनका प्रयोग करते हैं।
संरचनावादी भाषा–विज्ञान की, अलग–अलग देशों में अलग–अलग चिन्तन–सरणियाँ विकसित हुर्इं और कुछ समय के लिए भाषा–विज्ञान की एकता खो–सी गई। लेकिन दूसरी ओर, अपनी सैद्धान्तिक कमज़ोरियों के बावजूद संरचनावादी भाषा–चिन्तन की विविध सरणियाँ काफ़ी हद तक एक–दूसरे के पूरक की भूमिका भी निभाती रहीं।
स्विस स्कूल और फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय स्कूल ने, सॉस्युर के संकेत–सिद्धान्त को तथा एक हद तक, संरचनावाद की बीजगणितीय दिशा को भी आगे विकसित किया। संरचनावाद की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय सॉस्युर के शिष्य आंत्वाँ मेये, सी– बैली, कार्त्सेवस्की तथा स्विस विद्वान गोदेल और फ्रांसीसी विद्वान बेन्वेनिस्ते को दिया जा सकता है। इन भाषा–वैज्ञानिकों ने भाषाई संकेतों की प्रकृति का विशद अध्ययन किया, इस अध्ययन के आधार पर फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी भाषाओं के अर्थ–विज्ञान और संकेत–प्रयोग विज्ञान के अन्तर्भूत नियमों को उद्घाटित किया, इण्डो–यूरोपियन भाषाओं के व्याकरण और निघण्टु (lexicon) या शब्दकोश के व्यापक संस्तर को व्यवस्थित और पुनर्गठित किया; तथा इन भाषाओं के व्युत्पत्तीय (etymological) शब्दकोशों के लिए आधार तैयार किया।
आगे चलकर संरचनावादी भाषा–विज्ञान के तीन स्कूल विकसित हुए : अमेरिकी संरचनावादी भाषा–विज्ञान या चित्रणवाद (descriptivism), प्राग भाषा–वैज्ञानिक स्कूल या पूर्वी यूरोपीय संरचनावाद, और कोपेनहेगन स्कूल।
अमेरिका में 1920 के दशक में फ्रांत्स बोआज़ और एडवर्ड सपेर आदि ने अलिखित अमेरिकी इण्डियन भाषाओं का अध्ययन करते हुए उनके ध्वनिग्रामों (phoneme), रूपग्रामों (morpheme) और बुनियादी संकेत–प्रयोग संरचनाओं या विन्यासगत ढाँचों को समझकर व्यवस्थित करते हुए, उनके आधार पर किसी भाषा के अधिकतम सम्भव वस्तुपरक प्रारम्भिक निरूपण के लिए पद्धतियाँ विकसित कीं। अमेरिकी इण्डियन भाषाओं के अध्ययन से वितरण की अवधारणा पर आधारित एक विशेष पद्धति विकसित करने में भी मदद मिली जिसका इस्तेमाल ब्लूमफील्ड, हैरिस, पाइक और ट्रेगर अदि भाषा–वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में किया। लेकिन 1960 के दशक तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सिद्धान्त व्याख्यापरक क्षमता की दृष्टि से कमज़ोर है और अर्थ–विज्ञान तथा संकेत–प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की दृष्टि से अपर्याप्त है। इन कमियों को दूर करने की कोशिशों ने एक नई धारा-प्रजनक भाषा–विज्ञान (generative linguistics) को जन्म दिया।
प्राग भाषा–वैज्ञानिक स्कूल भी 1920 के दशक में ही अस्तित्व में आया। इसका केन्द्र प्राग भाषा–विज्ञान सर्किल था जो दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक मौजूद रहा। इस सर्किल में कई रूसी और चेक भाषा–वैज्ञानिक शामिल थे जिनमें त्रुबेत्स्कोई, मैथेसियस, जेकबसन, ट्रिन्का, हैव्रानेक, मकारोव्स्की, वाचेक, स्कालिका आदि प्रमुख थे। पोलिश विद्वान कुरिलोविज़ के कार्य प्राग स्कूल और कोपेनहेगन स्कूल-दोनों से सम्बद्ध माने जाते हैं। प्राग स्कूल के विचारों को आगे विकसित करने में श्चेर्बा, बोगातिरेव और पोलिवानोव जैसे सोवियत विद्वानों की भी अहम भूमिका रही।
चित्रणवादियों से अलग, प्राग स्कूल ने यूरोपीय भाषाशास्त्र (philology) की परम्परा का अनुसरण करते हुए समृद्ध सांस्कृतिक इतिहासवाली यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन किया और उस आधार पर उन्होंने “प्रणालियों की प्रणाली” (system of systems) के रूप में भाषा की अवधारणा विकसित की, ऐसी प्रणालियों के विकास की गतिकी को परिभाषित किया, तथा वाक्य के प्रकार्यात्मक (functional) विभाजन सहित उद्गार की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। सैद्धान्तिक स्वर–विज्ञान की रचना प्राग स्कूल का मुख्य अवदान था जिसका केन्द्रीय उपादान था-वैपरीत्य की अवधारणा। इस अवधारणा ने भाषा के अन्य क्षेत्रों के निरूपणों को सूत्रबद्ध करने में उदाहरण का काम किया। प्राग स्कूल की अहम कमज़ोरी यह थी कि इसने सिद्धान्त और पद्धति के तर्कशास्त्रीय पहलुओं पर यथोचित ध्यान नहीं दिया।
1930 के दशक के मध्य में कोपेनहेगन स्कूल संरचनावाद के केन्द्र के रूप में उभरा। वहाँ एक सार्वभौमिक व्याकरण की समस्या को हल करने के लिए ह्येल्मस्लेव, ब्रोण्डल और उल्दाल ने भाषा–विज्ञान की पद्धतियों में आमूल सुधार की आवश्यकता महसूस की और एक नई प्रशाखा ‘ग्लॉसमैटिक्स’ (glossematics) का विकास किया। उन्होंने भाषा के नये सिद्धान्त और भाषा के वर्णन–चित्रण की पद्धति को तत्त्वों के ऊपर सम्बन्धों की निरपेक्ष प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया। भाषा की व्याख्या उन्होंने “शुद्ध सम्बन्धों की प्रणाली” के रूप में की। कोपेनहेगन भाषा–वैज्ञानिक सिद्धान्त ने, अन्तर्वस्तु और रूप में विविध अन्तरविरोधों से ग्रस्त होने के बावजूद भाषा के अमूर्त सिद्धान्त को गणित के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया।
1960 के दशक के मध्य में भाषा–विज्ञान में एक नई प्रवृत्ति निर्मितिवाद (constructivism) के रूप में सामने आई जो सैद्धान्तिक वस्तुओं की निर्मितिशीलता की आवश्यकता के सिद्धान्त पर आधारित थी। शुरू–शुरू में इस सिद्धान्त का सूत्रीकरण गणितीय तर्कशास्त्र के फ्रेमवर्क के भीतर हुआ, जिसे बाद में भाषा–विज्ञान के प्रदेश में विस्तारित किया गया। इस सिद्धान्त के दो मुख्य भाग हैं : पहला, किसी वस्तु को सिद्धान्त की वस्तु तभी माना जा सकता है जबकि उसकी निर्मिति सम्भव हो; और दूसरा, वस्तुओं के अस्तित्व या उनके संज्ञान की सम्भावना की बात तभी की जा सकती है जबकि उनकी सैद्धान्तिक निर्मिति या अनुरूपण (simulation) सम्भव हो। निर्मितिवादी पद्धति की एक बुनियादी अवधारणा कलन–गणित (algorithm) पर आधारित है जिस पर सबसे पहले अफलातून और पाणिनी तथा आगे चलकर अरस्तू, स्पिनोजा और पोतेब्निया आदि दार्शनिक विचार कर चुके थे। कलन–गणित से निगमित अवधारणाओं ने निर्मितिवाद की एक विशेष क़िस्म को जन्म दिया जो प्रजनक व्याकरणों और गणितीय भाषा–विज्ञान के सिद्धान्त का आधार बना। प्रजनक व्याकरणों ने अमेरिकी संरचनावादी भाषा–विज्ञान की कई कमियों को दूर करने का दावा किया, लेकिन विशिष्ट भाषा–वैज्ञानिक आँकड़ों पर लागू करने के बाद पाया गया कि ये सिद्धान्त अति सीमित दायरे में ही प्रभावी और उपयोगी हैं। प्रजनक व्याकरण के सिद्धान्त और गणितीय तर्कशास्त्र की एक शाखा के रूप में औपचारिक भाषा के सिद्धान्त की आधारशिला नोम चोम्स्की ने रखी थी। चोम्स्की का एक विवादास्पद विचार यह था कि किसी प्राकृतिक भाषा के वाक्य–विन्यास तथा अर्थ–विज्ञान के विविध पहलुओं के निरूपण के लिए प्रजनक व्याकरण का औपचारिक उपकरण पर्याप्त है। इस विश्वास के आधार पर कि दुनिया की सभी भाषाओं की बुनियादी, अन्तर्भूत संरचनाएँ समान होती हैं, चोम्स्की ने मस्तिष्क के अध्ययन के एक साधन के रूप में भाषा–विज्ञान के इस्तेमाल की सम्भावनाओं की ओर भी इंगित किया। कुछ सीमित तकनीकी इस्तेमाल के बावजूद चोम्स्की के भाषा–वैज्ञानिक सिद्धान्तों की नवप्रत्यक्षवादी और औपचारिक तर्कवादी प्रवृत्ति की सीमाएँ आज स्पष्ट हो चुकी हैं।
संरचनावाद और नव व्याकरणवाद की विविधरूपा आलोचनाओं ने भाषा–वैज्ञानिक भूगोल, नवभाषा–विज्ञान और क्षेत्रीय भाषा–विज्ञान जैसी कई नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया, लेकिन ये आम भाषा–वैज्ञानिक सैद्धान्तिक ‘फ्रेमवर्क’ के रूप में किसी पूर्ववर्ती व्यापक सिद्धान्त को प्रतिस्थापित करने योग्य कदापि नहीं थीं। इनका दायरा संकुचित था, प्रयोग सीमित थे और दार्शनिक आधार कमज़ोर था।
भाषा–विज्ञान के इतिहास का एक संक्षिप्त (और काफ़ी हद तक असन्तोषजनक भी), परिचयात्मक सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हुए अब हम उस मुक़ाम पर आ गए हैं कि मार्क्सवाद के भाषा–दर्शन की या मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान की संघटन–प्रक्रिया की चर्चा कर सकें।
भाषा प्रश्न : सामान्य, आधारभूत मार्क्सवादी प्रस्थापनाएँ
मार्क्सवाद और समकालीन भाषा–विज्ञान के सम्बन्धों के मद्देनज़र, यह सवाल किया जा सकता है कि क्या ‘मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान’ जैसी कोई चीज़ मौजूद है। और इसका उत्तर देने में कोई हिचक या कठिनाई नहीं महसूस होती क्योंकि मार्क्सवाद मानव–सभ्यता के भौतिक–आत्मिक विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हुए मानव–भाषाओं की व्याख्या के प्रति एक सुनिश्चित ‘अप्रोच’ प्रस्तुत करता है और एक सुनिश्चित पद्धति लागू करते हुए कुछ सुनिश्चित स्थापनाएँ प्रस्तुत करता है।
भाषा–दर्शन के मार्क्सवादी सिद्धान्त की आधारशिला यह स्थापना है कि भाषा का चरित्र सामाजिक है, और यह आदि मानव की सामाजिक श्रम–प्रक्रियाओं और समाजीकरण की प्रक्रियाओं के सतत विकास के क्रम में उन्नत से उन्नततर अवस्थाओं में विकसित होती गई है (फ्रेडरिक एंगेल्स)। भाषा संज्ञान का प्रत्यक्ष यथार्थ है, जो सामाजिक संसर्ग के दौरान अस्तित्वमान हुई है (मार्क्स–एंगेल्स)। वस्तुगत यथार्थ का परावर्तन मानव चेतना के साथ ही, भाषा–रूपों की अन्तर्वस्तु के धरातल पर भी होता है (लेनिन का परावर्तन–सिद्धान्त)। भाषा के सामाजिक मूल, सामाजिक प्रकृति तथा सामाजिक संसर्ग और सम्प्रेषण में इसकी भूमिका की मार्क्सवादी अवधारणा इसके (यानी भाषा के) संरचनात्मक पक्ष के व्याख्या–विश्लेषण तक सफलतापूर्वक विस्तारित होती है। मार्क्सवादी भाषा–दर्शन संरचनावादियों की इस एक बुनियादी स्थापना को स्वीकार करता है कि भाषा संकेतों की एक निश्चित प्रणाली, अपने आन्तरिक संगठन समेत एक ‘संरचना” होती है, जिसके बाहर भाषा के संकेत और अर्थ को नहीं समझा जा सकता। लेकिन तुलनात्मक–ऐतिहासिक भाषा–विज्ञान और संरचनावादी भाषा–विज्ञान के पूरे काल के दौरान, प्रत्यक्षवाद, रूपवाद और नवप्रत्यक्षवाद द्वारा विभिन्न रूपों में भाषा के संकेत–वैज्ञानिक और अर्थ–वैज्ञानिक अध्ययनों का जो निरपेक्षीकरण किया जाता रहा और दार्शनिक अध्ययन या ज्ञान–मीमांसा की सारी समस्याओं को भाषा के तार्किक विश्लेषण तक सीमित कर देने के जो प्रयास होते रहे, मार्क्सवाद ने उनका विरोध किया। नवप्रत्यक्षवाद ने दर्शन की समस्याओं को मिथ्या समस्याएँ घोषित करते हुए समकालीन ज्ञान और व्यवहार के दार्शनिक विश्लेषण के आधार पर “चिन्तन के बाह्य रूपों”-यानी भाषा और विचार व्यक्त करने की अन्य सभी संकेत–प्रणालियों के भाषाई-अर्थवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में, विशेषकर सोवियत संघ के मार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिकों ने विज्ञान के रूप में दर्शन को सारत: विघटित कर देने की इन कोशिशों का तर्कपूर्ण विरोध प्रस्तुत किया।
मार्क्सवाद के अनुसार चिन्तन के अस्तित्व और अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होने के साथ ही भाषा चेतना के गठन में अहम भूमिका निभाती है। भाषा का संकेत अपनी वास्तविक प्रकृति के अनुसार, उसके प्रसंग में, जिसके अर्थ का वह द्योतक है, सोपानिक होते हुए भी अन्तत: यथार्थ के संज्ञान की प्रक्रिया से अनुकूलित होता है। भाषा अमूर्त चिन्तन के अस्तित्व और विकास को सम्भव बनाती है और चिन्तन के सामान्यीकरण का आवश्यक साधन होती है, लेकिन भाषा और चिन्तन को एक ही चीज़ नहीं कहा जा सकता। एक बार उत्पन्न हो चुकने के बाद भाषा सापेक्षत: स्वतंत्र होती है और अपने ही विशिष्ट नियमों का पालन करती है, जो चिन्तन के नियमों से भिन्न होते हैं। इसलिए, संकल्पना तथा शब्द, निर्णय तथा वाक्य आदि के बीच पूर्ण तादात्म्य का अभाव होता है।
भाषा के उद्भव, समाज में इसके स्थान और चिन्तन और यथार्थ की सामान्य मार्क्सवादी प्रस्थापनाओं की सामान्य चर्चा के बाद यह उल्लेख कर देना ज़रूरी है कि मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान के उद्भव और विकास की पूरी यात्रा के दौरान एक ओर इसे रूपवाद, आत्मगत प्रत्ययवाद और नवप्रत्यक्षवाद से संघर्ष करना पड़ा, तो दूसरी ओर इसके सीमान्तों के भीतर भी प्रकृतवादी, विभिन्न कोटि के वर्ग–अपचयनवादी (class-reductionist), नवकाण्टवादी और नवहेगेलवादी विचलन पैदा होते रहे। भाषा–विज्ञान के विस्तार और सूक्ष्मता के कई ऐसे प्रश्न आज भी खड़े हैं जिनसे मार्क्सवाद जूझ रहा है और भौतिक–आत्मिक जीवन का विकास ऐसे बहुतेरे नये–नये प्रश्न भी उपस्थित करता जा रहा है, जिनका उत्तर ढूँढ़ते हुए मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान को आगे विकसित होना है। आधुनिक सैद्धान्तिक भाषा–विज्ञान व्याकरणिक संरचनाओं के निरूपण के जिस प्रश्न से जूझ रहा है, वह मार्क्सवाद के सामने भी मौजूद है। इससे सम्बन्धित किसी सिद्धान्त का चरित्र मार्क्सवादी है या नहीं, यह फ़ैसला मात्र व्याकरणिक वर्णन–निरूपण के धरातल पर नहीं हो सकता। इस धरातल पर हम केवल पद्धति की द्वन्द्वात्मकता की जाँच–पड़ताल कर सकते हैं। व्याकरणिक संरचनाओं, जैसे किसी सूक्ष्म, तकनीकी प्रश्न पर प्रस्तुत किसी सिद्धान्त के मार्क्सवादी चरित्र का फ़ैसला समग्रता में इस बात से ही हो सकता है कि उस संस्तर पर मौजूद हमारा ज्ञान, हमारे व्यापक, सामान्यीकृत ज्ञान के अनुरूप है या नहीं, अथवा यूँ कहें कि हमारे ज्ञान की सम्पूर्णता के साथ समाकलित है अथवा नहीं।
भाषा–प्रश्न पर मार्क्स–एंगेल्स का चिन्तन
मार्क्स और एंगेल्स ने भाषा–विज्ञान पर कोई स्वतंत्र–सांगोपांग थीसिस नहीं लिखी। भौतिक जीवन और चिन्तन के अन्तर्सम्बन्धों, सामाजिक जीवन और चेतना के अन्तर्सम्बन्धों तथा सामाजिक वर्गों और विचारधारा के बारे में सोचते हुए उन्होंने भाषा–वैज्ञानिक प्रश्नों को यहाँ–वहाँ अपने एजेण्डे पर उठाया। लेकिन भाषा के प्रश्न पर उनकी दृष्टि सुसंगत और चिन्तन व्यवस्थित था-इसके स्पष्ट साक्ष्य हमें अवश्य देखने को मिल जाते हैं।
भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक भौतिकवाद को लागू करने का पहला स्पष्ट उदाहरण शायद फ्रेडरिक एंगेल्स का लेख ‘फ्रैंकिश डायलेक्ट’ (Frankish Dialect) है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
भाषा–विज्ञान विषयक मार्क्स की कुछ स्थापनाएँ हमें उनकी एक प्रारम्भिक कृति जर्मन विचारधारा में ही देखने को मिलती हैं जहाँ अपना सामाजिक सिद्धान्त निरूपित करते हुए वे भाषा की सारवस्तु और प्रकृति के बारे में कुछ पर्यवेक्षण रखते हैं तथा भौतिक–सामाजिक क्रिया–कलाप और भाषा की एकता का विचार प्रस्तुत करते हैं। साथ ही, वे स्पष्ट करते हैं कि सम्प्रेषण भाषा का एकमात्र प्रकार्य नहीं है, बल्कि तर्कश: और तथ्यत:, लोगों के बीच पारस्परिक सम्पर्क–संसर्ग और अन्तर्क्रिया के लिए भी भाषा का अस्तित्व अनिवार्य है। या यूँ कहें कि भाषा इसी प्रक्रिया में विकसित होती है और फिर इसमें सहायक होती है। “भाषा, चेतना की ही भाँति, केवल अन्य लोगों से संसर्ग की आवश्यकता और अनिवार्यता से ही उत्पन्न होती है” (जर्मन विचारधारा) चेतना और भाषा के चरित्र के सामाजिक निर्धारण का यह विचार मार्क्सवाद को उन सहजातवादी (innatism) विचारों से एकदम अलग कर देता है जो मानते हैं कि भाषा मनुष्य की एक सहजात नैसर्गिक जैविक योग्यता है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नोम चोम्स्की के भाषा–सिद्धान्त ने जब इसी स्थापना को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया तो मार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिकों ने भाषा के सामाजिक उद्गम और सामाजिक प्रकृति–विषयक मार्क्स के बुनियादी तर्कों को आधार बनाकर ही उसकी आलोचना की। एक सामाजिक परिघटना के रूप में भाषा की अवधारणा, ज़ाहिरा तौर पर व्यक्तिगत भाषा की तार्किक सम्भावना सम्बन्धी अटकलों का भी विरोध करती है। आगे चलकर, इसी आधार पर एक नवमार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिक फेरूसियो रोस्सीलान्दी ने विटगेंस्टाइन के भाषाई दर्शन के ‘मार्क्सवादी उपयोग’ के बारे में अपने विवादास्पद विचार प्रस्तुत किए (Per un uso Marxiano de Wittgenstein, 1968)। लेकिन रोस्सीलान्दी भी भाषा से, चेतना से स्वतंत्र रूप में विद्यमान वस्तुगत यथार्थ–विषयक विचार को अस्वीकार करते हुए अहंमात्रवाद (solipsism) के आत्मगत प्रत्ययवादी भटकाव के शिकार हो जाते हैं जिसका ज्ञानमीमांसीय सिद्धान्त यह है कि संवेदन संज्ञान का निरपेक्ष स्रोत है।
भाषा की सामाजिक प्रकृति–विषयक थीसिस को एंगेल्स ने ऐतिहासिक प्रेक्षण पर आधारित इस आनुभविक परिकल्पना से बल प्रदान किया कि भाषा की उत्पत्ति श्रम से या कार्य (work) से हुई है। तब से लेकर आजतक मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान की लगभग सभी विचार–सरणियाँ किसी न किसी रूप में भाषा का उद्गम श्रम में, सामाजिक उत्पादन–प्रक्रिया में या सामाजिक श्रम–प्रक्रिया में देखती रही हैं।
आगे चलकर जार्ज लूकाच ने एंगेल्स की इस उत्पत्तिमूलक परिकल्पना को व्याख्यायित–विस्तारित करते हुए यह स्थापना दी कि श्रम या कार्य भाषा के जन्म के साथ ही इसके संरचनागत गुणों की भी व्याख्या करता है। लूकाच के विचार से श्रम या कार्य सभी मानवीय क्रिया–कलापों का आधारभूत प्रकल्प (basic model) है और इनमें भाषाई क्रिया–कलाप भी शामिल हैं।
भाषा, चिन्तन और यथार्थ के अन्तर्सम्बन्धों के प्रश्न पर मार्क्स की स्थापना यह थी कि भाषा विचारों के अस्तित्वमान होने की विधि या सत्व–प्रणाली (mode of being) होती है और प्रकार्यात्मकता या क्रियाशीलता के सन्दर्भ में भाषा और चिन्तन–रूप (thought form) की एकता अपृथक्करणीय होती है। उल्लेखनीय है कि मार्क्स की यह अवधारणा काण्ट के बाद के समय के जर्मन भाषा–दर्शन तथा जर्मन भाषाशास्त्र (philology), और ख़ासकर हेर्डर, श्लेगेल, बॉप, ग्रिम और विल्हेल्म फ़ॉन हम्बोल्ट आदि की तुलनात्मक–ऐतिहासिक पद्धति की परम्परा की निरन्तरता में नज़र आती है। चिन्तन और भाषा की एकता के बारे में मार्क्स और एंगेल्स की इसी थीसिस का एक अतिवादी छोर तक विस्तार हमें बीसवीं शताब्दी में एडवर्ड सपेर और बेंजामिन ली व्होर्फ जैसे भाषा–वैज्ञानिकों की परिकल्पना (Sapir-Whorf hypothesis) में तथा नवहम्बोल्टवादियों के भाषाई सापेक्षवाद (linguistic relativism) में दिखाई पड़ता है जिनका यह मानना है कि भाषाई संरचनाएँ सोचने के तरीक़ों और विश्व–दृष्टिकोणों का निर्धारण करती हैं।
मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान, मुख्यत: परावर्तन के सिद्धान्त (theory of reflection) के आधार पर, भाषाई सापेक्षवाद को अस्वीकार करता है। परावर्तन के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त पर आधारित मार्क्सवादी ज्ञान–मीमांसा के अनुसार, विचार और भाषा सहित संज्ञान के परिणाम अपने मूल स्रोत के सापेक्षत: अनुरूप होते हैं। वस्तुगत जगत और उसमें जारी प्रक्रियाओं का चिन्तन या भाषा के धरातल पर निर्जीव “छाया–चित्रण” नहीं होता, अपितु यह परावर्तन, संवेदी तथा बौद्धिक–संज्ञान, मानसिक तथा व्यावहारिक क्रिया–कलाप की संजटिल तथा व्याघातपूर्ण क्रिया होता है, जिसमें मनुष्य अपने को निष्क्रिय ढंग से बाह्य जगत के अनुकूल नहीं ढालता, बल्कि उस पर अपना प्रभाव डालता है, उसे बदलता है और उसे अपने उद्देश्यों के अधीन करता है। अधिकांश मार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिकों ने इस परावर्तन सिद्धान्त को भाषा और चिन्तन के अन्तर्सम्बन्धों पर भी लागू किया। उनके अनुसार, भाषा और चिन्तन दोनों ही सामाजिक श्रम–प्रक्रिया के दौरान अन्य लोगों से संसर्ग की आवश्यकता से तथा लगातार उन्नततर धरातल पर श्रम–प्रक्रिया के पुनर्गठन की आवश्यकता से उत्पन्न हुए। भाषा चिन्तन के अस्तित्वमान होने की विधि है जो मूलत: और व्यापकत: चिन्तन के सत्व से अनुकूलित होती है और अन्योन्यक्रिया के तौर पर, अपनी पारी में उसे प्रभावित भी करती है। भाषा में चिन्तन का निर्जीव–निष्क्रिय प्रतिबिम्बन नहीं, बल्कि सजीव–सक्रिय परावर्तन होता है। इस द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध का मुख्य पहलू, सामान्य और व्यापक सन्दर्भों में, चिन्तन द्वारा भाषा का अनुकूलन होता है, न कि भाषा द्वारा चिन्तन का अनुकूलन।
मार्क्सवाद मानव–चिन्तन के रूपों की सार्वभौमिकता पर ज़ोर देता है। इस सार्वभौमिकता की एक अभिव्यक्ति भाषा की ‘टाइपोलॉजी’ (typology) द्वारा निरूपित सार्वभौमिक भाषाई संरचनाओं में देखी जा सकती है।
मार्क्स के भाषा–वैज्ञानिक चिन्तन का जो एक और दायरा है वह सामाजिक वर्गों और विचारधाराओं के सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने जर्मन विचारधारा में “बुर्जुआ भाषा” शब्द का इस्तेमाल किया है। अपने एक अन्य लेख सन्त मैक्स में भी वे बताते हैं कि बुर्जुआ वर्ग की “अपनी भाषा” होती है। ग्रुंड्रिशे में वे कहते हैं कि “विचार भाषा से अलग मौजूद नहीं होते” (पेंग्विन क्लासिक्स संस्करण, पृ. 163) और जर्मन विचारधारा में वे बताते हैं कि “हर युग में सत्ताधारी वर्ग के विचार ही सत्ताधारी विचार होते हैं।” मार्क्स की इन उक्तियों को सन्दर्भ से काटकर यांत्रिक ढंग से देखने से बीसवीं शताब्दी में एक वर्ग–अपचयनवादी भाषा–सिद्धान्त भी विकसित हुआ जो मानता था कि भाषा का एक वर्ग–चरित्र होता है। इस सोच के एक मुख्य प्रवर्तक सोवियत मार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिक एन.वाई. मार्र थे। मार्र के विचारों और वोलोशिनोव तथा स्तालिन द्वारा प्रस्तुत उनकी आलोचना का उल्लेख हम आगे करेंगे।
मार्क्स के विचारों को व्यापकता और समग्रता में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भाषाई व्यवहार पर वर्ग–सम्बन्धों और विचारधाराओं की छाप और प्रभाव–छायाओं की बात करते हैं, न कि वर्ग–भाषा की। वे सिर्फ़ यह उल्लेख करते हैं कि शासक वर्ग की सत्ता भाषा के प्रयोग के दायरे तक विस्तारित–प्रभावी होती है। विचारधारा से भाषा की अवियोज्यता का यह अर्थ वे कदापि नहीं लेते कि दोनों समानार्थक हैं और कहीं भी वे विचारधारा की तरह भाषा को अधिरचना की कोटि में नहीं रखते। मार्क्स का तात्पर्य बुर्जुआ समाज में एक राष्ट्रीय भाषा के दायरे के भीतर बुर्जुआ वर्ग की अपनी वर्ग–उपभाषा (class-dialect) या जमाती भाषा (huckster’s lingo) या कामकाजी वर्ग–बोली (huckster’s jargon) से था। फ्रेडरिक एंगेल्स भी अपनी पुस्तक इंग्लैण्ड में मज़दूर वर्ग की दशा में ब्रिटिश बुर्जुआ समाज में मज़दूर वर्ग द्वारा अपनी भिन्न वर्ग–उपभाषा बोले जाने की चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पर मार्क्स के समस्त चिन्तन और विमर्श के सारतत्त्व को आत्मसात करते हुए कहा जा सकता है कि भाषा सामान्यत: पूरे समाज की और समस्त मानवीय क्रिया–व्यापार की सामूहिक प्रकृति की अपरिहार्य आवश्यकता होती है, जबकि ठोस सामाजिक–विचारधारात्मक संरचनाओं के साथ इसके अन्तर्सम्बन्ध भाषाई व्यवहार या बरताव (linguistic usage) की विशिष्ट अनुसंकेत–पद्धतियों (subcodes) के धरातल पर अभिव्यक्त होते हैं। इस अन्तर्सम्बन्ध के आनुभविक पहलुओं का अध्ययन आज सामाजिक भाषा–विज्ञान के दायरे में किया जा रहा है।
बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक के सोवियत मार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिक एन.वाई. मार्र के विपरीत, (मार्र ने ऐतिहासिक–तुलनात्मक भाषा–विज्ञान को प्रत्ययवादी बताते हुए खारिज कर दिया था और बाद में स्तालिन ने उनकी स्थापना का खण्डन किया था) मार्क्स और एंगेल्स ने ऐतिहासिक–तुलनात्मक भाषा–विज्ञान के प्रेक्षणों–निष्कर्षों को काफ़ी महत्ता दी तथा बॉप, ग्रिम और दिएज़ की स्थापनाओं का, प्राय: वैज्ञानिक मानकों के तौर पर उल्लेख किया। एंगेल्स ने स्वयं भी तुलनात्मक भाषा–वैज्ञानिक इतिहास के क्षेत्र में कुछ काम किया। प्राचीन जर्मेनिक भाषाओं-विशेषकर फ्रैंकों और फ्रैंकिश भाषा के युग के इतिहास से सम्बन्धित अपनी दो पाण्डुलिपियों में (जिनमें The Frankish Dialect प्रमुख है) एंगेल्स ने अपनी स्थापनाओं को सूत्रवत प्रस्तुत किया है। उदाहरण के तौर पर, कबीलाई उपभाषाओं (dialects) के श्लिष्टयोगात्मक रूपों और ध्वन्यात्मक अभिलाक्षणिकताओं के अध्ययन के बाद उन्होंने तथाकथित द्वितीय जर्मन स्वरान्तन्रण (second German vowel shift) के आधार पर जर्मन उपभाषाओं के वर्गीकरण की आलोचना की और प्रत्येक उपभाषा को उच्च या निम्न जर्मन के रूप में मान्यता देने का विचार प्रस्तुत किया। एंगेल्स की इन पाण्डुलिपियों में भाषा–विशेष बोलनेवाले समुदाय के इतिहास के अनुसार भाषाई विकास पर विचार किया गया है तथा तर्कशास्त्रीय और ऐतिहासिक पद्धतियों को परस्पर सम्बद्ध किया गया है। इस दृष्टि से इन्हें मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान की आधारशिला मानना अत्युक्ति नहीं होगी।
बीसवीं शताब्दी : भाषा–वैज्ञानिक विमर्श में मार्क्सवादी हस्तक्षेप और वोलोशिनोव
बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान की दो प्रवृत्तियाँ विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। पहली प्रवृत्ति का सम्बन्ध भाषा और विचारधारा के अन्तर्सम्बन्धों के बारे में मार्क्स की प्रारम्भिक स्थापनाओं से जाकर जुड़ता है। दूसरी प्रवृत्ति पाव्लोव के प्रतिवर्तों के सिद्धान्त (theory of reflexes) से जुड़ी है जो शरीरक्रिया–विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हुए भाषा को द्वितीय संकेत–प्रणाली (secondary signalling system) मानती है।
1920 और 1930 के दशक मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान के विकास की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण थे। जार्ज लूकाच की व्याख्या के अनुसार, मार्क्स का भाषा–चिन्तन, भाषा के ऊपर ‘रीइफ़िकेशन’ (reification) के प्रभावों को उजागर करता है। इस आधार पर अपनी पुस्तक इतिहास और वर्ग चेतना (1923) में, लूकाच ने ऐतिहासिक भौतिकवादी अवस्थिति से भाषाशास्त्रीय (philological) अध्ययन की सम्भावनाओं की ओर इंगित किया। आगे चलकर, 1960 के दशक में मार्क्सवादी संकेत–विज्ञान ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण काम किये। इसने ‘भाषाई परकीयकरण’ (linguistic alienation) जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर काम किया और भाषा–वैज्ञानिक सिद्धान्त ‘भाषाई कार्य’, ‘भाषाई उपकरण’ और ‘भाषाई पूँजी’ आदि नये प्रवर्गों से समृद्ध हुआ (विशेष तौर पर देखी जा सकती है, रोस्सीलान्दी की पुस्तक : (Linguistics and Economics, 1975)।
एक सामाजिक और विचारधारात्मक परिघटना के रूप में, भाषा की प्रकृति और प्रकार्यों पर मार्क्सवादी चिन्तन को 1920 और 1930 के दशक में सोवियत भाषा–वैज्ञानिकों ने बहुपक्षीय रूप में आगे बढ़ाया। 19वीं शताब्दी के रूसी भाषा–विज्ञान और विशेषकर कजान स्कूल के प्रारम्भिक संरचनावादियों के चिन्तन में मौजूद भौतिकवादी प्रवृत्तियों को भी उन्होंने अपना सैद्धान्तिक आधार तैयार करते हुए अपनाया और आगे विकसित किया। इस दौरान सोवियत संघ में आर.ओ. शोर, ई.डी. पोलिवानोव, एल.पी. याकुबिंस्की और वी.एम. झिरमुंस्की आदि ने भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में जो काम किया, वह मुख्यत: भाषा और समाज के अन्तर्सम्बन्धों से जुड़ा हुआ था। एन.वाई. मार्र और वोलोशिनोव के परस्पर–विरोधी भाषा–चिन्तन भी मुख्यत: इसी दायरे से जुड़े हुए थे पर उन्होंने एक हद तक भाषा और चिन्तन के अन्तर्सम्बन्धों पर भी अपनी प्रस्थापनाएँ रखीं। भाषा और चिन्तन के प्रश्न पर मुख्यत: मेश्चानिकोव और विगोत्स्की ने महत्त्वपूर्ण काम किया।
1929 में प्रकाशित वी.एन. वोलोशिनोव की पुस्तक मार्क्सवाद और भाषा का दर्शन पहली ऐसी पुस्तक थी जिसमें भाषा–विज्ञान के कुछ प्रमुख आधारभूत प्रश्नों पर मार्क्सवादी विश्व–दृष्टिकोण और पद्धति से विचार करने का प्रयास दिखाई देता है। आगे चलकर, 1930 और ’40 के दशक में सोवियत भाषा–विज्ञान में हावी एन.वाई.मार्र की वर्ग–अपचयनवादी अवस्थिति के कारण वोलोशिनोव की यह पुस्तक ही नहीं, बल्कि वोलोशिनोव भी भुला–से दिए गये। पश्चिमी दुनिया के बुद्धिजीवी वोलोशिनोव की गुमनामी के लिए प्राय: स्तालिन के “सर्वसत्तावादी शासन” को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा मानने का कोई भी तथ्यगत आधार नहीं है। इसके विपरीत, यह तथ्य उल्लेखनीय है कि एन.वाई. मार्र और उनके शिष्यों द्वारा मार्क्सवाद के सरलीकरण और विकृतिकरण का विरोध करनेवाले भाषा–वैज्ञानिकों के उपेक्षा–उत्पीड़न का हवाला स्वयं स्तालिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका मार्क्सवाद और भाषा–विज्ञान की समस्याएँ में दिया है। अलबत्ता, यह सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है कि प्रावदा में भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में हावी मार्र के वर्ग–अपचयनवादी विचार के विरुद्ध चली बहस और 1950 में स्तालिन द्वारा उसके समाहार के बाद भी वोलोशिनोव का भाषा–विषयक चिन्तन चर्चा और विमर्श के केन्द्र में क्यों नहीं आ सका! इसका कारण सम्भवत: यह रहा हो कि साहित्यिक–सांस्कृतिक हल्कों में, ज़्दानोव (सांस्कृतिक मामलों के पार्टी–प्रभारी) के कार्यकाल में, लुनाचार्स्की और गोर्की के समय के विपरीत, यांत्रिक भौतिकवादी और जड़सूत्रवादी विचलन मौजूद थे तथा विरोधी वैचारिक अवस्थितियों के साथ बहस का उतना खुला माहौल नहीं था। वोलोशिनोव चूँकि मार्बुर्ग पन्थ के नवकाण्टवादियों से प्रभावित बख्तीन स्कूल से जुड़े रहे थे और उनके चिन्तन और लेखन पर कास्सिरेर के चिन्तन का विचलनकारी प्रभाव अन्त तक मौजूद रहा, इसलिए ऐसा सम्भव है कि इसी कारण से बाद के दौर में भी उनकी उपेक्षा हुई हो। हालाँकि यह भी सच है कि विनोग्रादोव जैसे कुछ अग्रणी सोवियत भाषा–वैज्ञानिकों ने वोलोशिनोव के अवदानों की खुलकर चर्चा की।
वोलोशिनोव (1895–1936) प्रसिद्ध बख्तीन सर्किल के एक सदस्य थे जिसके सैद्धान्तिक नेता मिखाइल मिखाइलोविच बख्तीन माने जाते रहे हैं। कागान (1889–1937), मद्वेदेव (1891-1938), पम्पियांस्की (1891-1940), सोलेरतिंस्की (1902-1944) सर्किल के अन्य सदस्य थे। यद्यपि बख्तीन 1950 के दशक तक रचनात्मक रूप से सक्रिय रहे तथा उपन्यास के सौन्दर्यशास्त्रीय सिद्धान्त तथा वक्तृत्व–शैली और संकेत–सिद्धान्त सहित साहित्यिक–कलात्मक भाषा के सिद्धान्त पर काम करते रहे, लेकिन बख्तीन सर्किल की सघन सक्रियता का काल 1920 का दशक ही था। बख्तीन सर्किल समाजशास्त्रीय काव्यशास्त्र और विमर्श–सिद्धान्त (discourse theory) की नई प्रणालियाँ विकसित करने की दिशा में सक्रिय था। आम तौर पर सामाजिक जीवन में, और विशेष तौर पर, कलात्मक सृजन के क्षेत्र में संकेतीकरण से जुड़े हुए प्रश्न इस ग्रुप के विचारकों के कृतित्व के केन्द्र में थे। सामाजिक समुदायों के बीच के टकरावों की भाषा में इन्दराज़ी, और अभिव्यक्ति के रूपों–रास्तों पर बख्तीन और उनके साथियों ने विशेष तौर पर विचार किया। बख्तीन सर्किल का केन्द्रीय विचार यह था कि भाषाई उत्पादन सारत: संवादात्मक (dialogic) होता है जो सामाजिक अन्तर्क्रिया के दौरान अस्तित्व में आता है। यह विभिन्न सामाजिक मूल्यों की अन्तर्क्रिया के रूप में सामने आता है जो दूसरों के वक्तृत्व के पुनर्बलाघात (reaccentuation) के रूप में दर्ज़ होता है। शासक तबका एकल (अथवा इकहरे) विमर्श को निदर्शनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, जबकि ‘सबाल्टर्न’ वर्गों का झुकाव इस एकालापी या स्वगत (monologic) समापन को छिन्न–भिन्न करने की दिशा में होता है। साहित्य के क्षेत्र में, कविता और महाकाव्य, संस्कृति के दायरे के अन्तर्गत केन्द्राभिसारी (centripetal) शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि उपन्यास लोकप्रिय विचारधारात्मक आलोचना की, संरचनात्मक दृष्टि से जटिल–सुपरिष्कृत अभिव्यक्ति होता है।
बख्तीन सर्किल पर मार्बुर्ग पन्थ के नवकाण्टवाद का स्पष्ट प्रभाव था जिसका मुख्य माध्यम कागान था जो लीपजिग, बर्लिन और मार्बुर्ग में दर्शन का अध्ययन करते हुए मार्बुर्ग पन्थ के संस्थापक हरमन कोहेन का शिष्य रहा था। इसी दौरान उसे अर्न्स्ट कास्सिरेर के भाषण सुनने के भी अवसर मिले थे। मार्बुर्ग पन्थ के नवकाण्टवादियों (कोहेन, कास्सिरेर, नाटोर्प और श्टामलेर) ने काण्ट के विचारों की भौतिकवादी प्रवृत्ति को तिलांजलि देकर सुसंगत आत्मगत प्रत्ययवाद की अवस्थिति अपना ली थी। इनका मानना था कि दर्शन विज्ञानों की विधि और तर्क मात्र ही बना रहता है और वह जगत का ज्ञान नहीं बन सकता। समाज–विकास के वस्तुगत नियमों को अस्वीकार करते हुए मार्बुर्गपन्थी समाजवाद को केवल नैतिक परिघटना या वर्गोपरि “नैतिक आदर्श” मानते थे। मार्क्सवाद की काण्टवाद से “अनुपूर्ति” करने का आह्वान करते हुए उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की आधारभूत आर्थिक और राजनीतिक अन्तर्वस्तु को ख़त्म कर दिया। कास्सिरेर ने इस बात का प्रतिवाद किया कि विज्ञानसम्मत अमूर्तीकरण यथार्थ का परावर्तन है। उसने भौतिक जगत को विशुद्ध चिन्तन के प्रवर्गों में घुला–मिला दिया, उसके नियमों के स्थान पर प्रत्ययवादी ढंग से परिभाषित प्रकार्यात्मक अधीनता को रखा; और आगे चलकर, वैज्ञानिक संज्ञान को “प्रतीकात्मक़ चिन्तन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यह तथ्य ग़ौरतलब है कि साहित्यिक–भाषावैज्ञानिक दायरे में बख्तीन सर्किल को प्रभावित करनेवाले मार्बुर्ग पन्थ के समाजशास्त्रीय विचारों ने रूस के “क़ानूनी मार्क्सवादियों” और दूसरे इण्टरनेशनल के बर्नस्टीन, काउत्स्की, एडलर आदि अवसरवादियों को विशेष तौर पर प्रभावित किया था और दक्षिणपन्थी समाजवादी धाराएँ मार्क्सवाद के विरुद्ध इन विचारों को आज भी इस्तेमाल करती हैं। इस तथ्य की रोशनी में एक और तथ्य को समझने की कोशिश की जा सकती है। गत शताब्दी के सातवें–आठवें दशक में न केवल बख्तीन सर्किल के, और विशेषकर बख्तीन के विचारों का पश्चिमी साहित्यालोचना और भाषा–विज्ञान की दुनिया में अचानक महत्त्व बढ़ गया, बल्कि ख्रुश्चेव–ब्रेझनेव के संशोधनवाद के समय में सोवितय संघ में बख्तीन की ज़ोर–शोर से पुनर्स्थापना हुई। और पश्चिमी अकादमिक नववामपन्थी दायरों के एक आराध्य–पुरुष तो बख्तीन विगत लगभग तीन दशकों से बने ही हुए हैं।
हम इस बात पर यहाँ विशेष तौर पर ज़ोर देना चाहते हैं कि बख्तीन सर्किल का विचार–जगत एकाश्मी और सुबद्ध क़तई नहीं रहा है। वैज्ञानिक संज्ञान और प्रतीकात्मक रूपों के बारे में कास्सिरेर के विचारों के गहन प्रभाव के बावजूद वोलोशिनोव के लेखन की, और एक अन्य धरातल पर मद्वेदेव के लेखन की, सर्किल के अन्य पुरोधाओं से कुछ महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं जो उन्हें मार्क्सवादी विचारों के दायरे में ज़्यादा विश्वासपूर्वक रखने का आधार देती हैं। कागान और बख्तीन की स्थिति उनसे भिन्न थी। बख्तीन अपनी सर्जनात्मकता के अन्तिम दौर तक नवकाण्टवादी, आत्मगत प्रत्ययवादी प्रभाव–छायाओं से मुक्त नहीं हो सके थे और भाषा, उपन्यास, महाकाव्य, तथा कार्निवाल से लेकर वक्तृत्व–शैली तक की विवेचना करते हुए वे वैचारिक–कलात्मक परिघटनाओं के सामाजिक चरित्र और सामाजिक श्रम–प्रक्रिया तथा वर्गीय संरचना से उनके अन्तर्सम्बन्धों की अनदेखी–सी करते हुए दिखाई देते हैं। वोलोशिनोव और मद्वेदेव की स्थिति बख्तीन और सर्किल के अन्य सदस्यों से इस मायने में भिन्न है। उनके लेखन का मार्क्सवादी चरित्र अधिक मुखर था। बख्तीन ने विमर्श (discourse), संवादात्मकता (dialogism), कार्निवाल आदि कई विषयवस्तुओं पर पर्याप्त अमूर्त और अति पाण्डित्यपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रतिपादित किए थे जिनका पश्चिम की अकादमिक साहित्यालोचना के हलकों में बाज़ार भाव काफ़ी ऊँचा रहा और समकालीन उत्तरसंरचनावादी– उत्तरआधुनिकतावादी आदि–आदि भी बख्तीन के विचारों को काफ़ी अहमियत देते हैं। बख्तीन सर्किल के लेखन में बख्तीन के अवदानों को लेकर भी काफ़ी विवाद रहे। विशेष तौर पर, 1970 के बाद पश्चिम में इस बात को लगभग पूरी तरह स्थापित करने की कोशिश की गई कि वोलोशिनोव और मद्वेदेव के नाम से प्रकाशित लेखन वस्तुत: बख्तीन का लेखन है और स्थापित विद्वान भी बिना किसी तथ्यगत–तार्किक आधार के, अपनी पुस्तकों और लेखों में यह लिखते रहे कि बख्तीन ही वोलोशिनोव के छद्मनाम से लिखते थे। दिलचस्प बात यह है कि बख्तीन ने अपने जीवनकाल में (1975 तक) न तो इससे सहमति ज़ाहिर की, न ही इसका खण्डन किया। पश्चिमी साहित्यिक दायरों में तो यह भी कहा जाता रहा कि वोलोशिनोव की मार्क्सवादी शब्दावली महज़ एक आवरण है और वस्तुत: उनके विचार बख्तीन, कागान आदि के ही विचार थे।
बहरहाल, बख्तीन सर्किल के सभी लोगों की रचनाओं को-उनकी स्थापनाओं, शैलियों और दार्शनिक–वैचारिक अवस्थितियों के फ़र्क़ को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त बातें महज़ बेपर की उड़ानें हैं और पश्चिम की शीतयुद्धकालीन सांस्कृतिक रणनीति का ही एक हिस्सा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यह माना जा सकता था कि सभी साहित्यिक–समाजशास्त्रीय–मनोवैज्ञानिक–भाषावैज्ञानिक विषयों पर पूरे ग्रुप में जीवन्त बहसें होती थीं और उसके बाद अलग–अलग विषय–वस्तु पर अपने–अपने परिप्रेक्ष्य से अलग–अलग व्यक्ति लेखन करते थे। यह स्पष्ट है कि मार्बुर्गपन्थी नवकाण्टवादी प्रभावों से शुरू करने के बाद, कालान्तर में ग्रुप के अलग–अलग व्यक्तियों की अवस्थितियों में फ़र्क़ आते चले गये। 1928 में बख्तीन सर्किल के टूटने के बाद यह प्रक्रिया और स्पष्ट हो गई। तथ्यत: और तर्कश: यह मानने का कोई आधार नहीं है कि वोलोशिनोव का लेखन वस्तुत: बख्तीन का लेखन था और न ही इस कथन का कोई आधार है कि वोलोशिनोव की मार्क्सवादी शब्दावली महज़ दिखावे के लिए थी। बल्कि इसके विपरीत, यह मानने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि भाषाई धरातल पर सक्रिय अन्तरविरोधों में वर्ग–संघर्ष की अन्तर्वस्तु पर लगातार ज़ोर देने के कारण, वोलोशिनोव के प्रति पश्चिमी साहित्यालोचना के बुर्जुआ और नववामपन्थी दायरों में उतनी ललक या उतना आग्रह नहीं दिखाई देता। वर्ग–अन्तरविरोधों की, भाषा के धरातल पर अभिव्यक्ति और प्रतिफलन पर यह ज़ोर वोलोशिनोव की दोनों ही प्रमुख कृतियों-फ्रायडवाद : एक मार्क्सवादी आलोचना (1927, 1976 में अंग्रेज़ी में अनूदित) तथा मार्क्सवाद और भाषा का दर्शन (1929, 1973 में अंग्रेज़ी में अनूदित) में स्पष्ट नज़र आता है। भाषा के धरातल पर वर्ग–संघर्ष पर वोलोशिनोव का ज़ोर भोण्ड़े भौतिकवादी ढंग का, या एन.वाई. मार्र जैसे वर्ग–अपचयनवादी ढंग का नहीं था। वोलोशिनोव भाषा को स्पष्टत: एक सामाजिक– विचारधारात्मक परिघटना मानते थे, पर भाषाई समुदायों के बीच के भेद को वे वर्ग–विभेद का सम्पाती नहीं मानते थे क्योंकि विभिन्न वर्ग एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। वोलोशिनोव की मान्यता थी कि स्वयं भाषा के भीतर, वर्ग–संघर्ष जारी रहता है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, “संकेत वर्ग–संघर्ष का एक क्षेत्र बन जाता है।”
उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, वोलोशिनोव के लेखन की शुरुआत 1918 के आसपास वितेब्स्क में हुई, जहाँ बख्तीन ग्रुप के लोग गृहयुद्ध की कठिनाइयों से बचने के लिए रह रहे थे। उसी समय वहाँ मालेविच और शागाल जैसे अवाँगार्द कलाकार भी रह रहे थे। वहाँ बख्तीन सर्किल के सदस्यगण सिर्फ़ अकादिमक दार्शनिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर उस दौर की रैडिकल सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी भी करते थे। पावेल मद्वेदेव वितेब्स्क सर्वहारा विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्त हो गए थे और नगर की सांस्कृतिक पत्रिका ‘इस्कुस्त्वो’ (‘कला’) का सम्पादन भी करते थे। इसी पत्रिका में उनके और युवा वोलोशिनोव के लेख नियमित प्रकाशित हुआ करते थे। 1924 में लेनिनग्राद आने के बाद का समय, बख्तीन सर्किल के सदस्यों की महत्त्वपूर्ण कृतियों का रचनाकाल था। यह सिलसिला 1928 में सर्किल के बिखरने तक चलता रहा जब ‘सेण्ट पीटर्सबर्ग धार्मिक–दार्शनिक समाज’ नामक संगठन से सम्बन्ध के कारण बख्तीन को दस वर्ष के लिए सोलोवेत्स्की द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। बाद में गोर्की और लूनाचार्स्की के हस्तक्षेप के कारण, सज़ा घटाकर उन्हें छह वर्ष के लिए कजाकिस्तान भेज दिया गया। वोलोशिनोव 1934 तक लेनिनग्राद में ‘हर्जेन शिक्षाशास्त्रीय संस्थान’ में काम करते रहे। 1934 में ही उन्हें तपेदिक हुआ और दो वर्ष बाद एक सेनेटोरियम में उनका देहान्त हो गया। मृत्यु के समय वे अर्न्स्ट कास्सिरेर की तीन खण्डोंवाली पुस्तक प्रतीकात्मक रूपों का दर्शन के पहले खण्ड का अनुवाद कर रहे थे, जो अधूरा ही रह गया।
लेनिनग्राद में रहते हुए सॉस्युर और उनके शिष्यों द्वारा प्रवर्तित–विकसित संरचनावादी भाषा–विज्ञान और तत्कालीन रूपवादियों के कृतित्व में उसके निरूपण द्वारा उपस्थित चुनौतियों को वोलोशिनोव ने, और पूरी बख्तीन सर्किल ने, गहराई के साथ महसूस किया। मार्क्सवाद और भाषा का दर्शन पुस्तक के अतिरिक्त, 1926 से 1930 के बीच वोलोशिनोव ने भाषा–विज्ञान विषयक लेखों की एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित की।
1926 में वोलोशिनोव का लेख जीवन में विमर्श और कविता में विमर्श : समाजशास्त्रीय काव्यशास्त्र के प्रश्न प्रकाशित हुआ। यह शोध–निबन्ध उन्होंने लेनिनग्राद में ‘भौतिक, कलात्मक और वाचिक संस्कृति संस्थान’ में स्नातकोत्तर अध्ययन के दौरान तैयार किया था। उनके शोध–सलाहकारों में याकुबिंस्की भी एक थे जो संवादात्मक वक्तृत्व के अध्ययन के प्रवर्तक थे। यह निबन्ध न सिर्फ़ संकेत–प्रयोग विज्ञान (pragmatics) का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है बल्कि बख्तीन सर्किल के बीच से आई पहली मार्क्सवादी कृति भी मानी जाती है। इस निबन्ध में वोलोशिनोव ने ‘सौन्दर्यपरक’ की परिभाषा सामाजिक अन्तर्क्रिया के एक विशिष्ट रूप के तौर पर करने की कोशिश की है। “कलात्मक कृति की सर्जना द्वारा (इसके) समापन और सह–सर्जनात्मक अवबोध (cocreative perception) में इसके सतत पुनर्सृजन” को वोलोशिनोव ने इसकी (यानी ‘सौन्दर्यपरक’ की) अभिलाक्षणिकता बताया और यह भी कि, “इसे दूसरे किसी वास्तवीकरण (objectification) की आवश्यकता नहीं होती।” वोलोशिनोव ने यह विचार रखा कि किसी भी कलाकृति में अनकहे सामाजिक मूल्यांकन ‘संघनित’ (condensed) होते हैं जो कला–रूप का निर्धारण करते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक अन्तर्क्रिया की गहनतर संरचनागत अभिलाक्षणिकताएँ एक सफल कलाकृति में अभिव्यक्त होती हैं। वोलोशिनोव के ही शब्दों में, “रूप को अन्तर्वस्तु का स्वीकरणीय मूल्यांकन होना चाहिए।” इस तरह वोलोशिनोव ने प्रारम्भिक बख्तीनियन परिघटनाशास्त्र को एक विशिष्ट समाजशास्त्रीय ‘फ्रेम ऑफ रेफ़रेन्स’ के साथ विमर्शात्मक अन्तर्क्रिया (discursive interaction) के एक नये साँचे में ढालने की शुरुआत की।
वोलोशिनोव की दूसरी परियोजना थी, नई-नई उभर रही मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति तथा मार्क्सवाद और फ्रायडवाद के समागम के समकालीन प्रयासों की एक समालोचना प्रस्तुत करना। 1927 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई : फ्रायडवाद : एक मार्क्सवादी आलोचना। यह पुस्तक दरअसल 1925 में लिखे गए एक लेख, सामाजिक से परे की विषयवस्तु का ही अग्रवर्ती विस्तार थी जिसमें फ्रायड पर मार्क्सवाद की स्पिरिट से सर्वथा विजातीय, जैविक अपचयनवाद और मनोगतवाद का आरोप लगाया गया था। वोलोशिनोव के अनुसार, हर प्रकार के अर्थ (meaning) का उत्पादन, और अर्थों का दमन भी, व्यक्तिगत या जैविक नहीं होता जैसाकि फ्रायड का मानना था, बल्कि सामाजिक–विचारधारात्मक होता है। उत्तरवर्ती लूकाच की ही स्पिरिट में वोलोशिनोव ने भी फ्रायडवाद को ‘बुर्जुआ पतनशीलता’ के रूप में देखा। साथ ही, इस कृति में वोलोशिनोव नवकाण्टवादी प्रभाव–छायाओं से मुक्त होकर, सांस्कृतिक–दार्शनिक प्रश्नों पर हेगेलवादी पहुँच–पद्धति की ओर संक्रमण करते दीखते हैं।
1920 के दशक के परवर्ती दौर में विमर्श–विषयक वोलोशिनोव के निबन्ध से उनके विचारों में महत्त्वपूर्ण समाजशास्त्रीय–भाषावैज्ञानिक मोड़ का संकेत मिलता है। वोलोशिनोव यहाँ पहुंचकर, पहली बार भाषा को सामाजिक सम्बन्धों के अभिसूचक (index) और विचारधारात्मक विश्व–दृष्टिकोणों के द्वन्द्व के मूर्त रूप के तौर पर परिभाषित करते हैं। वोलोशिनोव की चिन्तन–प्रक्रिया के इस विकास पर अर्न्स्ट कास्सिरेर की उस विचार–यात्रा का भी काफ़ी प्रभाव था जो उनकी पुस्तक प्रतीकात्मक रूपों का दर्शन में अभिव्यक्त हुई थी। कास्सिरेर का मार्बुर्गपन्थी नवकाण्टवाद से, काण्ट के हेगेलियन दोष–निवारण में संक्रमण इस पुस्तक में एकदम स्पष्ट था।
वोलोशिनोव ने विचारधारा और भाषा के प्रति सॉस्युर के संरचनावाद और विटगेंस्टाइन के भाषाई दर्शन से सम्बद्ध परम्पराओं से सर्वथा अलग ‘अप्रोच’ अपनाया तथा संकेत–विज्ञान और विमर्श–सिद्धान्त की ऐसी प्रणालियाँ प्रस्तावित कीं जो मार्क्सवादी साहित्यिक आलोचना को कई धरातलों पर समृद्ध बनाने की सम्भावना से युक्त थीं। मार्क्सवाद और भाषा का दर्शन का पहला संस्करण 1929 में और दूसरा संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ। इसमें वोलोशिनोव ने भाषा और विचारधारा के बीच के सम्बन्धों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, वह अपने कई विवादास्पद उपप्रमेयों और उपांगों के बावजूद, भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में मार्क्सवाद को लागू करने का अभूतपूर्व उदाहरण था। न केवल दशकों बाद तक, मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान इसे एक सन्दर्भ–बिन्दु के रूप में देखता रहा और इसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्थापनाओं तथा उठाए गए अनसुलझे प्रश्नों से जूझता रहा, बल्कि आज भी यह प्रक्रिया जारी है।
पुस्तक में वोलोशिनोव ने अपने समय में स्थापित दो प्रमुख भाषा–वैज्ञानिक चिन्तन–सरणियों को विश्लेषण का विषय बनाया है-पहली, सॉस्युर से जुड़ी धारा जिसे वे ‘अमूर्त वस्तुपरकतावाद’ (abstract objectivism) की संज्ञा देते हैं, और दूसरी, स्वच्छन्दतावादी प्रत्ययवादी (नवहेगेलपन्थी) इतालवी दार्शनिक बेनेडेट्टो क्रोचे (1866–1952) और कार्ल वोस्लर (1872-1942) द्वारा विल्हेल्म फ़ॉन हम्बोल्ट के कृतित्व से विकसित धारा, जिसे वे ‘व्यक्तिवादी आत्मपरकतावाद’ (individualistic subjectivism) की संज्ञा देते हैं। वोलोशिनोव की स्थापना है कि ये दोनों धाराएँ क्रमश: तर्कणावाद और स्वच्छन्दतावाद से निकली हैं और इन आन्दोलनों की मजबूतियाँ और कमज़ोरियाँ-दोनों ही इनमें से मौजूद हैं। पहली धारा, सही ढंग से, भाषा के प्रणालीगत और सामाजिक चरित्र को रेखांकित करती है, लेकिन यह ‘स्वत:–समरूपी फॉर्मों की प्रणाली’ को समाज में भाषाई व्यवहार का स्रोत समझ बैठने की भूल करती है, उपयोग के ठोस ऐतिहासिक सन्दर्भ में पृथक करके भाषा का अमूर्तीकरण कर देती है; सम्पूर्ण की क़ीमत पर अंश की जाँच–पड़ताल करती है; वक्तृत्व की गतिमानता की उपेक्षा करके अलग–अलग भाषाई तत्त्व को स्वतंत्र–स्वायत्त मानते हुए उन्हें ‘वस्तु’ के रूप में देखती है; अर्थ और बलाघात की बहुलता की उपेक्षा करके शब्दार्थ की एकता की कल्पना करती है; तथा भाषा को एक बनी–बनाई प्रणाली के रूप में देखती है और उसमें होनेवाले परिवर्तनों को मात्र विच्युति मानती है। दूसरी धारा, सर्वथा सही ढंग से भाषा को एक सतत् प्रजननशील प्रक्रिया के रूप में देखती है और इस बात पर बल देती है कि यह प्रक्रिया अर्थयुक्त है, लेकिन यह इसकी रचना के नियमों का व्यक्तिगत मनोविज्ञान के नियमों के रूप में देखने की ग़लती करती है; भाषाई प्रजनन–प्रक्रिया और कलात्मक सृजन के बीच सादृश्यता स्थापित करने की भूल करती है; तथा संकेतों की प्रणाली को सर्जनात्मक प्रक्रिया के निष्क्रिय भूपृष्ठ (पपड़ी) के रूप में देखती है। इन आंशिक अन्तर्दृष्टिगत पर्यवेक्षणों के बाद, वोलोशिनोव ये आधारभूत तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भाषाई संकेतों की स्थायित्वपूर्ण प्रणाली महज़ एक वैज्ञानिक अमूर्तन है; भाषा की प्रजनक प्रक्रिया वक्ताओं की सामाजिक–वाचिक अन्तर्क्रिया में क्रियान्वित होती है; भाषा–प्रजनन के नियम समाजशास्त्रीय नियम होते हैं; तथा, हालाँकि भाषाई और कलात्मक सर्जनात्मकता एक–दूसरे के अनुरूप अथवा परस्पर सम्पाती नहीं हुआ करतीं, लेकिन इस सर्जनात्मकता को भाषा में सम्पूरित विचारधारात्मक अर्थों और मूल्यों से सम्बन्धित–सन्दर्भित करके ही समझा जा सकता है।
वोलोशिनोव का कहना है कि प्रत्येक ठोस उद्गार की संरचना एक समाजशास्त्रीय संरचना होती है। ग़ौरतलब है कि हमारे समय के उत्तर–संरचनावादी, संरचनावादी और अन्य पूर्ववर्ती भाषा–वैज्ञानिक विचार–सरणियों की जो आलोचनाएँ प्रस्तुत करते हैं, उनमें से बहुतेरी वोलोशिनोव की विवेचना में पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वोलोशिनोव न तो उत्तर संरचनावादियों के भाषाई सापेक्षवाद का शिकार होते हैं, न ही देरिदा के ‘hors text’ या पाठ से बाहर की शून्यता ही उन्हें व्यापती है। वोलोशिनोव चेतना की संकेतबद्व प्रकृति और भाषा–प्रणाली की अन्तरणशील प्रकृति (shifting nature) पर विशेष बल देते हैं, लेकिन वे विषय को भिन्नता के यथार्थ द्वारा विखण्डित रूप में नहीं देखते और प्रत्येक उद्गार को सामाजिक संघर्ष या घात–प्रतिघात के सूक्ष्म प्रतिरूप (microcosm) के रूप में देखते हैं। यह स्थापना विमर्श की समाजशास्त्रीय संरचना और बहुलता को ऐतिहासिक विकास की एकात्मकता के अनुसार सहसम्बन्धित करने में मदद करती है। इन अर्थ–सन्दर्भों में, वोलोशिनोव की विवेचना और अन्तोनियो ग्राम्शी द्वारा ‘प्रिज़न नोटबुक्स’ में प्रस्तुत वर्चस्व की व्याख्या में साम्य के बहुतेरे सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। वोलोशिनोव की ही तरह, ग्राम्शी ने भी क्रोचे, वोस्लर और मात्तियो बर्तोली के सॉस्युरियन ‘स्थानिक भाषा–विज्ञान’ के कृतित्व की विवेचना प्रस्तुत की है और फिर मार्क्सवाद के “हेगेलियन पाठ” के साथ इसे जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन, जैसाकि हमने देखा है, वोलोशिनोव कास्सिरेर से काफ़ी प्रभावित थे जो प्रजनक भाषा–विज्ञान के प्रवर्तक विल्हेल्म फ़ॉन हम्बोल्ट के प्रशंसक थे। अत: तर्कणावाद और स्वच्छन्दतावाद की दोनों धाराओं से समान दूरी के दावे के बावजूद वोलोशिनोव का झुकाव दूसरे ध्रुव की ओर कुछ ज़्यादा दीखता है। जैसे कि सामाजिक समूहों को वे सामाजिक–आर्थिक आधारों पर गठित वर्गों या समुदायों के रूप में स्पष्टत: परिभाषित नहीं करते। उनका यह कथन भी उनके इसी विचलन को इंगित करता है कि किसी शब्द का अर्थ “पूरी तरह से” उसके सन्दर्भ से “निर्धारित होता है।” वोलोशिनोव ने एक महत्त्वपूर्ण काम यह किया कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भाषाई परिवर्तनशीलता की हम्बोल्ट की धारणा के साथ एक समाजशास्त्रीय आयाम जोड़ दिया। उन्होंने हम्बोल्ट के भाषा के ‘अन्तस्थ रूप’ (inner form) की अवधारणा को विमर्श की सम्बन्धात्मकता (relationality) या संवादात्मकता के साँचे में ढालकर उसे नया रूप दे दिया। वोलोशिनोव ने भाषा के धरातल पर सामाजिक वर्गों के टकरावों को मान्यता देते हुए भी इसे मूलाधार अथवा अधिरचना में से किसी प्रवर्ग से जोड़ने की सोच को सर्वथा ग़लत बताया तथा विविध भाषाई रूपों को एक एकल सारवस्तु की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में निरूपित करते हुए कास्सिरेर और हेगेल का अनुसरण किया। उल्लेखनीय है कि ग्राम्शी ने भी सुसंगत अर्थक्रियावादी ज्ञानमीमांसीय पद्धति अपनाकर इसी मार्ग का अनुसरण किया तथा उनके और वोलोशिनोव के सूत्रीकरणों में भी आश्चर्यजनक समानता देखने को मिलती है।
मार्र का भोंड़ा भौतिकवादी भाषा–विज्ञान
वोलोशिनोव की ही तरह सोवियत भाषा–वैज्ञानिक एन.वाई. मार्र ने भी भाषा को एक सामाजिक–विचारधारात्मक परिघटना बताया, लेकिन इस तर्क को नितान्त यांत्रिक भौतिकवादी ढंग से आगे बढ़ाते हुए और घोर वर्ग–अपचयनवादी अवस्थिति अपनाते हुए उन्होंने यह स्थापना दी कि भाषा का एक सुनिश्चित वर्ग–चरित्र होता है और यह अधिरचना का अंग होती है। मार्र के अनुसार, भाषा वर्ग–शासन के एक उपकरण के रूप में अस्तित्व में आई और विकास के प्रत्येक चरण में, कार्य–कारण सम्बन्धानुसार, इसका निर्धारण वर्ग–संघर्ष के द्वारा ही होता है। भाषा–सृजन की प्रक्रिया (glottogony) की इसी एकता के चलते, सभी ज्ञात भाषाओं के मूल तत्त्व एक समान होते हैं। अपने चार–तत्त्वीय विश्लेषण में मार्र ने यह दावा किया कि मनुष्य की आदिम भाषा का उच्चारण चार मूल ध्वनि–इकाइयों से विकसित हुआ था। भाषाओं के बीच की भिन्नताओं का विश्लेषण मार्र इस तथ्य के आधार पर करते थे कि विकास की प्रक्रिया की अलग–अलग मंज़िलों में वे अस्तित्व में आर्इं। भाषाओं के वर्ग–चरित्र का निर्धारण करते हुए, मार्र मानते थे कि अलग–अलग भाषाएँ अलग–अलग कबीलाई, नृजातीय या राष्ट्रीय समुदायों की नहीं, बल्कि अलग–अलग वर्गों की उपज हैं।
मार्र और उनके अनुयाइयों का यह वर्ग–अपचयनवादी सिद्धान्त 1930 के दशक में सोवियत भाषा–विज्ञान के परिदृश्य पर पूरी तरह से छाया रहा और स्वस्थ बहस–मुबाहसे के ज़रिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र की आधिकारिक नौकरशाही के ज़रिए सभी विरोधी विचारों को पूरी तरह से दबा दिया गया। वोलोशिनोव का भाषा–चिन्तन लगभग पूरी तरह से विस्मृति के अँधेरे में खो गया। बख्तीन सर्किल से जुड़े होने के कारण वोलोशिनोव पर भी नवकाण्टवादी आत्मगत प्रत्ययवाद से ग्रस्त और अध्यात्मवादी होने का आरोप लगाया जाना सुगम था। उनके चिन्तन में मौजूद विचलनों पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया और उनके द्वारा निगमित सही निष्पत्तियों, भाषा–विज्ञान में ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्धति को लागू करने के प्रयासों, उनके लेखन में काण्ट, हेगेल, कास्सिरेर की प्रभाव–छायाओं और मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण के बीच सतत मौजूद एक ‘जेनुइन’ तनाव तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अनसुलझे प्रश्नों और नई सम्भावनाओं की उपेक्षा कर दी गई।
सोवियत संघ से बाहर, जेकबसन आदि के प्राग भाषा–वैज्ञानिक स्कूल के चिन्तन पर वोलोशिनोव का स्पष्ट प्रभाव दीखता है। इस स्कूल के विचारों के विकास में श्चेरबा, बोगातिरेव, पोलिवानोव आदि जिन सोवियत विद्वानों का योगदान था, उन पर भी वोलोशिनोव के भाषा–विज्ञान का पर्याप्त प्रभाव था। आगे चलकर श्चेरबा के स्वर–विज्ञान, व्याकरण और कोश–रचना विषयक प्रसिद्ध सिद्धान्तों पर वोलोशिनोव की संकेत प्रणाली विषयक अवधारणा का विशेष प्रभाव दीखता है। रूसी भाषा, साहित्यिक भाषा, शैली विज्ञान और काव्यशास्त्र से सम्बन्धित विनोग्रादोव का सिद्धान्त भी वोलोशिनोव की धारणाओं और तर्क–पद्धति से प्रभावित दीखता है। बाद के समय में, विनोग्रादोव एक ऐसे भाषा–वैज्ञानिक थे जो वोलोशिनोव के अवदानों को मुखर रूप में स्वीकार करते थे।
मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान और स्तालिन
1940 के दशक के अन्त में, प्रावदा में भाषा–विज्ञान की समस्याओं पर एक खुली बहस चली, जिसका समाहार करते हुए 1950 में स्तालिन की प्रसिद्ध पुस्तिका मार्क्सवाद और भाषा–विज्ञान की समस्याएँ प्रकाशित हुई। इस पुस्तिका ने न केवल सोवियत भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में मार्रवादी प्रभुत्व का अन्त कर दिया, बल्कि पहली बार इसमें भाषा के प्रश्न पर मार्क्स–एंगेल्स, पाल लफार्ग और लेनिन की छिटफुट स्थापनाओं को समेटते हुए, ऐतिहासिक–तुलनात्मक और संरचनावादी स्कूलों के सकारात्मक अवदानों को समाहित करते हुए तथा भाषा–विषयक स्थापित तथ्यों का ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण–समाहार करते हुए, सांगोपांग, सारगर्भित और सुगम ढंग से मार्क्सवादी भाषा–वैज्ञानिक अवस्थितियों को प्रस्तुत किया गया। ग़ौरतलब है कि द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में जब स्तालिन अतीत के प्रयोगों के अनुभव के आधार पर, समाजवादी संक्रमण की वैचारिक और अर्थशास्त्रीय विच्युतियों को ठीक कर रहे थे तथा पार्टी और राज्य के स्तर पर नौकरशाही की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक क़दम उठाने की सोच रहे थे; ठीक उसी समय भाषा–विज्ञान के क्षेत्र में भी मार्र के भोंड़े भौतिकवाद और वर्ग–अपचयनवाद के विरुद्ध उन्होंने वैचारिक संघर्ष छेड़ा। फिर भी यह प्रश्न अनसुलझा रह जाता है कि क्यों वोलोशिनोव के सकारात्मक–नकारात्मक पक्षों की विवेचना तो दूर, स्तालिन ने भाषा–विज्ञान सम्बन्धी अपने निबन्ध और साक्षात्कारों में उनकी चर्चा तक नहीं की है! बहरहाल, इस पर अटकलें लगाने के बजाय इस तथ्य को तथ्य के रूप में स्वीकारते हुए आगे बढ़ना होगा। इस सन्दर्भ में समाजवाद के दौर में सांस्कृतिक क्षेत्र में वैचारिक संघर्ष चलाने के तौर–तरीक़ों और अतीत के (सोवियत संघ और चीन के) अनुभवों पर कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन यहाँ यह प्रसंगातर होगा।
स्तालिन की भाषा–विज्ञान विषयक आधारभूत प्रस्थापनाओं को इस रूप में सूत्रबद्ध किया जा सकता है :
(i) भाषा और अधिरचना को परस्पर उलझाना, और भाषा को आर्थिक मूलाधार पर आधारित अधिरचना मानना एक गम्भीर ग़लती है। मूलाधार-यानी उत्पादन–सम्बन्ध वर्ग–विशेष के हितों के अनुरूप होते हैं और उससे प्रादुर्भूत और उस पर आधारित अधिरचना का एक स्पष्ट वर्ग–चरित्र होता है। लेकिन भाषा समाज के किसी एक मूलाधार का प्रतिफलन नहीं, बल्कि समाज के शताब्दियों के इतिहास और मूलाधारों के इतिहास की उपज होती है। यह किसी एक वर्ग द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज द्वारा, और सैकड़ों पीढ़ियों के प्रयासों से निर्मित हुई है। यह किसी वर्ग–विशेष की आवश्यकताओं की नहीं, बल्कि पूरे समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अत: भाषा के वर्ग–चरित्र की धारणा अवैज्ञानिक है।
(ii) भाषा की, उत्पादन के उपकरणों-यानी मशीनों की प्रकृति से कुछ बुनियादी समानताएँ हैं। मशीनें सभी वर्गों के लिए वैसे ही समान हैं, जैसे कि भाषा। जैसे, पूँजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था क़ायम हो जाने पर भाषा और मशीनें पूर्ववत समाज का हितसाधन करती रहती हैं। लेकिन इनके बीच की एक बुनियादी भिन्नता यह है कि उत्पादन के उपकरण भौतिक सम्पदा का उत्पादन करते हैं जबकि भाषा ऐसा नहीं करती। अत: भाषा को मूलाधार, अधिरचना के आम प्रवर्गों और उत्पादन के साधनों से पृथक, एक सर्वथा भिन्न सामाजिक परिघटना के रूप में देखा जाना चाहिए जो चिन्तन, संसर्ग और सम्प्रेषण के प्रकार्य सम्पन्न करती है।
(iii) अधिरचना मनुष्य की उत्पादक कार्रवाई से सीधे नहीं, बल्कि परोक्षत:, आर्थिक मूलाधार के माध्यम से-उत्पादन–सम्बन्ध के माध्यम से जुड़ी होती है। भाषा व्यक्ति की उत्पादक गतिविधियों से सीधे जुड़ी होती है। साथ ही वह व्यक्ति के सभी कार्यक्षेत्रों की गतिविधियों से सीधे जुड़ी होती है। अत: वह उत्पादन में हुए परिवर्तनों को तत्काल और प्रत्यक्षत: परावर्तित करती है, मूलाधार में परिवर्तनों के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करती।
(iv) भाषा का विकास गोत्र भाषाओं, जातीय भाषाओं, राष्ट्रीयताओं की भाषाओं और फिर राष्ट्रीय भाषाओं के अनुवर्ती विकास–क्रम में हुआ है। पूँजीवाद के उदय के साथ और राष्ट्रीय बाज़ारों के निर्माण के साथ राष्ट्रीयताओं का विकास राष्ट्रों में तथा राष्ट्रीयताओं की भाषाओं का विकास राष्ट्रीय भाषाओं में हुआ।
(v) भाषा समाज के सभी वर्गों के प्रति तटस्थ होती है, लेकिन विभिन्न सामाजिक वर्ग भाषा के प्रति तटस्थता का रुख नहीं अपनाते। वे भाषा का अपने हक़ में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से उस पर अपनी विशेष शब्दावली और अभिव्यक्तियाँ आरोपित करते हैं। आम लोगों की बोलचाल की शब्दावली व शैली से अलग, शासक वर्ग प्राय: अपनी विशेष ‘जमाती भाषा’ (lingo), वर्ग–उपभाषा (dialect) और वर्ग–बोली (jargon) इस्तेमाल करते हैं। पर ये पृथक स्वतंत्र भाषाएँ न होकर, प्राय: एक राष्ट्रीय भाषा के परिक्षेत्र में ही बरती जाती हैं, तथा उसी का अंग होती हैं। इनका अपना अलग से मूल शब्द–भण्डार या व्याकरण–प्रणाली नहीं होती।
(vi) मूल शब्द भण्डार और व्याकरण–प्रणाली-ये किसी भी भाषा की दो बुनियादी अभिलाक्षणिकताएँ होती हैं। मूल शब्द भण्डार, शताब्दियों तक बना रहता है, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यन्त मद्धम होती है, वह भाषा को नये शब्दों के निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है। शब्दों में परिवर्तन और वाक्यों में उनके संयोजन को नियंत्रित करती हुई व्याकरण–प्रणाली, शब्दों और वाक्यों-दोनों के सन्दर्भ में, विशिष्ट और सुनिश्चित प्रकारों से अपने को अमूर्त या निरपेक्ष बनाते हुए उन चीज़ों को अपनाती है जो शब्दों के परिवर्तन और वाक्यों की रचना में आधारभूत और सामान्य होती हैं, और उन्हें व्याकरणीय नियमों की शक्ल देती है। व्याकरण मस्तिष्क द्वारा काफ़ी लम्बे समय से जारी अमूर्तीकरण की प्रक्रिया का प्रतिफलन है। यह चिन्तन की व्यापक उपलब्धियों का एक संकेत है। व्याकरण इस सन्दर्भ में कुछ हद तक ज्यामिति जैसा होता है जो अपने नियमों को प्रस्तुत करते हुए स्वयं को ठोस वस्तुओं से अमूर्त कर लेता है और उन वस्तुओं को ठोसपन से रहित पिण्डों की तरह लेती है तथा उनके बीच के सम्बन्धों को ठोस वस्तुओं के निश्चित सम्बन्धों के रूप में परिभाषित करने के बजाय सभी प्रकार के ठोसपन से रहित पिण्डों के सम्बन्धों के रूप में परिभाषित करती है।
(vii) भाषाओं के विकास में आकस्मिक विस्फोटों (गुणात्मक छलाँग) और आकस्मिक भाषाई क्रान्ति के माध्यम से नई भाषा के जन्म की अवधारणा अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है। भाषा–सम्पर्क (linguistic crossing) किसी निर्णायक आघात (blow) का अकेला संघात नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक चलनेवाली एक लम्बी प्रक्रिया है।
(viii) “भाषा विचारों की प्रत्यक्ष वस्तुवत्ता है”(मार्क्स)। सामान्य आदमी के दिमाग़ में विचार केवल भाषा–तत्त्व के आधार पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। भाषा तत्त्व से रहित “नग्न” विचारों की मार्र की अवधारणा एकदम ग़लत है।
स्तालिन भाषा–विज्ञान के संकेत–प्रायोगिक, अर्थ–वैज्ञानिक, स्वर–वैज्ञानिक, और शैली–विज्ञान आदि से सम्बन्धित अमली तकनीकी विस्तार में तो नहीं गए, लेकिन इतना तय है कि भाषा–विज्ञान के लगभग सभी दार्शनिक और अवधारणागत पहलुओं को अपनी पुस्तिका में समेटते हुए उन्होंने एक सांगोपांग मार्क्सवादी फ्रेमवर्क पहली बार प्रस्तुत किया। उनके इस हस्तक्षेप ने मार्र के भांेड़े भौतिकवादी भाषा–विज्ञान को हमेशा के लिए दफ्न कर दिया।
पाव्लोव, लूकाच, डेला वोल्पे का चिन्तन और नववाम के भाषाई खेल : नया मार्क्सवादी हस्तक्षेप ज़रूरी है!
भाषा और सामाजिक संरचना तथा भाषा और विचारधारा के अन्तर्सम्बन्धों की इस मीमांसा से अलग एक और प्रश्न था जिसका उल्लेख मार्क्स से होकर स्तालिन तक के विमर्श में नहीं आया था। वह प्रश्न कुछ इस रूप में रखा जा सकता है : मनुष्य की अन्य प्राणियों से अलग वह कौन–सी विशिष्टता है, जिसके चलते सामाजिक जीवन में संज्ञानात्मक और संसर्गात्मक प्रकार्यों की पूर्ति के लिए आधारभूत संकेत–प्रणाली के रूप में वह भाषा का विकास कर सका? यह प्रश्न शरीरक्रिया–विज्ञान से जाकर जुड़ता था और इस दृष्टि से पाव्लोव ने इस पर विचार किया। पाव्लोव के प्रतिवर्तों (reflexes) के सिद्धान्त के अनुसार, भाषा द्वितीय संकेत प्रणाली (secondary signalling system) है। भाषा–विज्ञान के सामाजिक पहलू से जुड़े होने के बजाय, पाव्लोव का सिद्धान्त भाषा और संज्ञान के अन्तर्सम्बन्धों की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है।
आगे चलकर पाव्लोव के सिद्धान्त को लूकाच ने भी अपनी एक भाषा–वैज्ञानिक अवधारणा के आधार के तौर पर, किंचित संशोधित रूप में लागू करने की कोशिश की। दैनन्दिन जीवन की भाषा सहित, दैनन्दिन जीवन के अपने सिद्धान्त के फ्रेमवर्क में लूकाच ने तथाकथित ‘संकेत–प्रणाली–I’ से सम्बन्धित प्राक्कल्पना प्रस्तावित की। लेकिन साथ ही उन्होंने प्रकृतवादी रुझान के लिए पाव्लोव की आलोचना भी की। परवर्ती दौर की अपनी रचनाओं में लूकाच ने मुख्यत: सामाजिक पुनरुत्पादन के एक तत्त्व के रूप में तथा सामाजिक जीवन की निरन्तरता के एक साधन के रूप में भाषा की भूमिका पर विचार किया है।
भाषा–विज्ञान जैसे सापेक्षत: अमूर्त, वैज्ञानिक विषय के साथ प्राय: एक समस्या यह देखने में आती है कि व्यवहार के क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्य से कटकर अकादिमक सीमान्तों में घुसते ही आवश्यक अमूर्तन का स्थान अनावश्यक अमूर्तन ले लेता है, गौण मुद्दों पर सिराविहीन बहसों का अनन्त सिलसिला जारी हो जाता है, चरम अमूर्त प्रस्थापनाओं का अम्बार लग जाता है और मूल लक्ष्य जटिल भाषा के भँवरों में खो जाते है। नववामपन्थ के विभिन्न यूरोपीय दायरों में भी आज यह ख़ूब हो रहा है। एक हद तक, वोलोशिनोव में भी यह अकादमिक अमूर्तन मौजूद है, लेकिन बख्तीन के लेखन में तो यह अति की सीमा तक जा पहुँचता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि न केवल पश्चिम के अकादमिक नववाममार्गी, बल्कि उत्तर–संरचनावादी और उत्तर–आधुनिकतावादी भी बख्तीन को हाथों हाथ लेते रहे हैं। पश्चिमी नववाम की वर्तमान लहर से पहले, जिन कुछ पश्चिमी वामपन्थी विचारकों ने साहित्यालोचन के विविध प्रश्नों से जूझते हुए भाषा–विज्ञान सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्थापनाएँ दीं, उनमें इतालवी मार्क्सवादी दार्शनिक गाल्वानो डेला वोल्पे (1895–1968) का प्रमुख स्थान है। डेला वोल्पे ने वोलोशिनोव की ही भाँति भाषा के भौतिकवादी सौन्दर्यशास्त्र से जुड़ी कई एक महत्त्वपूर्ण अनुसलझी समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की है और उन पर विचार करने का एक सुनिश्चित कोण भी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘क्रिटीक ऑफ टेस्ट’ (Critique of Taste, 1960) में डेला वोल्पे ने प्लेखानोव, ग्राम्शी और लूकाच के साथ विमर्श में उलझते हुए ऐतिहासिक भौतिकवादी सौन्दर्यशास्त्र की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है तथा यथार्थवाद की समाजवादी अवधारणा की हिफ़ाज़त की है। इस दौरान डेला वोल्पे ने एक नई बात यह कही है कि मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्र ने साहित्य के भाषागत आयामों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया है। संरचनावादी भाषा–विज्ञान के कोपेनहेगन स्कूल के प्रवर्तक ह्येल्मस्लेव के ‘ग्लॉसमेटिक्स’ (glossematics) के सिद्धान्त के आधार पर डेला वोल्पे ने सौन्दर्यशास्त्रीय संकेत–विज्ञान की एक नई प्रशाखा विकसित की। एकार्थक वैज्ञानिक भाषा, अनेकार्थक कविता और सामान्य भाषा के बीच के द्वन्द्वात्मक सम्बन्धों का वर्णन करते हुए डेला वोल्पे ने कविता की बहुअर्थी तर्कपरकता के रहस्यीकरण की आलोचना की। इस विश्लेषण ने काव्यालोचना के क्षेत्र में मौजूद प्रत्ययवाद और रूपवाद की आलोचना को एक नया आयाम दिया। डेला वोल्पे के सिद्धान्त के आधार पर इतालवी आलोचक फ्रांको मोरेत्ती ने मार्क्सवादी संकेत–विज्ञान में नया और महत्त्वपूर्ण काम किया है (Signs Taken For Wonders, 1983)।
हेबरमास और फ्रैंकफर्ट स्कूल के कुछ अन्य नव मार्क्सवादियों के अनुसार, भाष्यशास्त्र (hermeneutics) का काम यह है कि वह भाषा के विश्लेषण से “शासन तथा सामाजिक सत्ता के साधन” को उजागर करे जो “संगठित ज़ोर–दबाव के सम्बन्धों का औचित्य” ठहराने का काम करता है। यह वस्तुत: एक तरह का नवप्रत्यक्षवादी “भाषा विश्लेषण” है जो अस्तित्ववादी हाइडेगर की ही भाँति दर्शन को भाषा की चौहद्दी में क़ैद कर देता है और भाषा के विश्लेषण को राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषण का स्थानापन्न बनाने की कोशिश करता है।
आज तमाम “उत्तर” सिद्धान्तों के प्रस्तोताओं–प्रवक्ताओं ने जीवन के यथार्थ और उसकी गतिकी से मुँह मोड़कर भाषा–वैज्ञानिक विमर्श के नाम पर भाषा का जो खेल खेलना शुरू किया है, उसका एक मूल उद्देश्य सामाजिक संघर्ष की उस सार्वभौमिक सच्चाई की अनदेखी करना है, जो भाषा के धरातल पर भी लगातार जारी रहता है। सत्य की सार्वभौमिकता, नियमनिष्ठता और वस्तुगत चरित्र को अस्वीकार करनेवाले ये सभी सिद्धान्त सत्य के पीछे तथ्य के आग्रह और संकेतों में अर्थ की उपस्थिति के आग्रह को खारिज करते हैं तथा सत्य के दावे को मानसिक उपनिवेशन बताते हैं। देरिदा कला–साहित्य में निश्चित अर्थ की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। इतिहास, दर्शन, साहित्य ही नहीं, विचार, विश्वास, व्यवहार, घटनाओं आदि को भी ये पाठ मानते हैं और पाठ का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यह पाठक और उसकी व्याख्या पर निर्भर करता है। उत्तर–आधुनिकतावादी संकेतक (signifier) और संकेतित (signified) के मान्य सम्बन्ध को अस्वीकार करते हुए उनके बीच एक क़िस्म का ‘आर्बिट्रेरी’ सम्बन्ध स्थापित करते हैं।
देखा जाए तो उत्तर–आधुनिकतावादियों के सांस्कृतिक तर्कों की ही भाँति उनके भाषा–वैज्ञानिक तर्क भी पहले के प्रत्ययवादी और रूपवादी तर्कों के ही नये संस्करण मात्र हैं। मार्क्सवादी भाषा–विज्ञान काफ़ी पहले इन प्रश्नों पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार कर चुका है। मार्क्सवादी भाषा–चिन्तन की उस परम्परा को आज पुनर्जीवित करने की और आगे विस्तार देने की ज़रूरत है। साथ ही, भाषा–प्रश्न पर ऐतिहासिक भौतिकवादी चिन्तन के सामने आज भी कई ज़रूरी, अनुसलझे प्रश्न खड़े हैं जिन्हें हल करना साहित्य की मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी के अग्रवर्ती विकास की एक आवश्यक पूर्वशर्त है।
(वी.एन. वोलोशिनोव की पुस्तक ‘मार्क्सवाद और भाषा का दर्शन’ के राजकमल प्रकाशन से छपे हिन्दी अनुवाद की सम्पादकीय प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित)
- सृजन परिप्रेक्ष्य, जनवरी-अप्रैल 2002