हमारी बात
‘नान्दीपाठ’ का दूसरा अंक लेकर हम आपके बीच ऐसे समय में उपस्थित हुए हैं जब फ़ासीवाद का ख़तरा क्षितिज पर मँडराने लगा है। आम चुनाव में हिन्दुत्ववादी फ़ासिस्ट इस बार जीतें या नहीं, मगर समाज के तृणमूल स्तर तक इनकी ख़तरनाक ढंग से पैठ हो चुकी है और पूँजीवाद का दिन-ब-दिन गम्भीर होता संकट व्यवस्था को एक फ़ासीवादी समाधान की ओर धकेल रहा है। विशेषकर, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्र में फ़ासीवादी प्रवृत्तियाँ कितने व्यापक और गहरे तौर पर फ़ैली हुई हैं इसे बताने की ज़रूरत नहीं। मगर चिन्ता और क्षोभ का विषय यह है कि कला-साहित्य-संस्कृति के मोर्चे पर समकालीन धार्मिक कट्टरपन्थी फ़ासीवादी उभार का प्रतिरोध प्रायः रस्मी, प्रतीकात्मक और कुलीनतावादी सीमान्तों में क़ैद है। इसकी एक वजह यह भी है कि बहुतेरे प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और संस्कृतिकर्मियों के बीच भी इस उभार की वैचारिक-ऐतिहासिक समझ में गम्भीर दृष्टिदोष मौजूद हैं।
रचनात्मक साहित्य में आम तौर पर हिन्दुत्ववादी कट्टरपन्थियों का विरोध प्रायः ‘सर्वधर्म सम्भाव’ की ज़मीन से या बुर्जुआ मानवतावाद या बुर्जुआ जनवाद की ज़मीन से करने की प्रवृत्तियाँ दिखायी देती हैं। यह निरर्थक और घातक है। हमें “उदार हिन्दू” या “रैडिकल हिन्दू” का रुख अपनाने के बजाय धर्म के जन्म और इतिहास की भौतिकवादी समझ का प्रचार करना होगा, धर्म के प्रति सही सर्वहारा नज़रिये को स्पष्ट करना होगा, धर्म और साम्प्रदायिकता के बीच के फ़र्क को स्पष्ट करते हुए एक आधुनिक परिघटना के रूप में साम्प्रदायिकता की समझ बनानी होगी तथा संकटग्रस्त पूँजीवाद की विचारधारा और राजनीति के रूप में साम्प्रदायिक फ़ासीवादी उभार का विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा। यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि इस फ़ासीवादी उभार का सम्बन्ध मूलगामी तौर पर, विश्व पूँजीवाद के ढाँचागत संकट से है, आर्थिक कट्टरपन्थ की वापसी के दौर से है और बुर्जुआ जनवाद के निर्णायक विश्व-ऐतिहासिक पराभव के दौर से है। आज का धार्मिक कट्टरपन्थ मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी अधिरचना के बहुतेरे तत्त्वों को अपनाये हुए है, लेकिन यह एक आधुनिक परिघटना है, इसकी जड़ें वित्तीय पूँजी के वैश्विक तंत्र और भारतीय पूँजीवादी राज, समाज, उत्पादन और संस्कृति की रुग्णता में हैं।
मगर फ़ासीवाद की वैचारिक समझ के लिए गम्भीर विमर्श और जनता के जनवादी अधिकारों पर फ़ासिस्ट डकैती के विरोध के साथ ही हमें इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि फ़ासिज़्म के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष करने वाले मज़दूर वर्ग और बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी को जागृत, शिक्षित और गोलबन्द करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? धार्मिक कट्टरपन्थ के हर पहलू पर सीधी-सादी भाषा में पर्चे, पुस्तिकाएँ लिखकर उनका व्यापक वितरण, औद्योगिक क्षेत्रों में और गाँव के ग़रीबों के बीच गीतों-नाटकों-फ़िल्मों-डॅक्युमेंट्री आदि के ज़रिए व्यापक शिक्षा और प्रचार के काम क्यों नहीं संगठित हो पा रहे हैं? क्या इसके लिए वामपन्थी लेखकों-संस्कृतिकर्मियों के भीतर व्याप्त मध्यवर्गीय कुलीनता-कायरता और सुविधाभोगी स्वार्थपरता जि़म्मेदार नहीं है? सेक्युलर, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की विशाल आबादी केवल सीमित प्रसार वाली पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखकर, गोष्ठियाँ और अध्ययन चक्र करके, शहरों में कुछ रैलियाँ निकालकर और सोशल मीडिया पर मोदी और संघ परिवार पर, उनके चाल-चेहरा-चरित्र पर, उनकी मूर्खताओं और झूठ पर टिप्पणियाँ करके इस जनद्रोही राजनीति का प्रभावी प्रतिकार नहीं कर सकती। हर बार जब ख़तरा सिर पर मँडराने लगता है तब बुद्धिजीवी कहते हैं कि जनता के बीच प्रचार और सांस्कृतिक कार्रवाइयाँ तो लम्बे दौर की बात है, फ़ासीवाद का दानव तो सामने खड़ा है। उससे बचने के लिए कुछ लोग अपनी शुतुरमुर्गी गर्दन रेत में छिपा लेते हैं तो कुछ एक बार फ़िर चुनावी पार्टियों की जोड़तोड़ से फ़ासिस्टों को सत्ता में आने से रोकने की उम्मीद लगाने लगते हैं।
धार्मिक कट्टरपन्थ के विरुद्ध सांस्कृतिक मोर्चे पर जो व्यावहारिक-आन्दोलनात्मक कार्रवाइयाँ होती भी हैं उनका स्वरूप अत्यन्त संकुचित, अनुष्ठानिक और कुलीनतावादी रहता है और अन्तर्वस्तु मुख्यतः सामाजिक जनवादी या एनजीओ-वादी होती है। वामपन्थी संस्कृतिकर्मियों की अधिकांश कार्रवाइयाँ शहरी मध्यवर्ग तक सीमित रहती हैं। साम्प्रदायिक फ़ासिस्टों की आक्रामक कार्रवाइयों के विरुद्ध महानगरों में रस्मी विरोध-प्रदर्शन, दंगाग्रस्त क्षेत्रों में टीमें भेजना और रिपोर्टें जारी करना, उन्नत चेतना वाले शिक्षित मध्यवर्ग तक सीमित साहित्यिक पत्रिकाओं में कविताएँ-कहानी-निबन्ध आदि लिखना, कुछ गोष्ठी-सेमिनार व अन्य आयोजन तथा कभी-कभार कुछ नुक्कड़ नाटक या संगीत कन्सर्ट जैसे कार्यक्रम – हमारी सांस्कृतिक जन-कार्रवाइयों की कुल मिलाकर यही स्थिति है। विगत ढाई दशकों के साम्प्रदायिक उभार और समाज की पोर-पोर में फ़ासिस्टों की विचारधारा और संस्कृति की बढ़ती पैठ ने भी साबित किया है कि यह किस क़दर नाकाफ़ी है।
_
काफ़ी लम्बे अन्तराल के बाद ‘नान्दीपाठ’ का यह दूसरा अंक आपके बीच प्रस्तुत है। पहले अंक का पाठकों ने जिस उत्साह से स्वागत किया है उससे ऐसी एक पत्रिका की ज़रूरत के प्रति हमारा विश्वास और पुख़्ता हुआ है। इसे निरन्तर और बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमें भरोसा है कि आपका हर प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहेगा।
(4 मार्च 2014)
- नान्दीपाठ-2, जुलाई-सितम्बर 2013
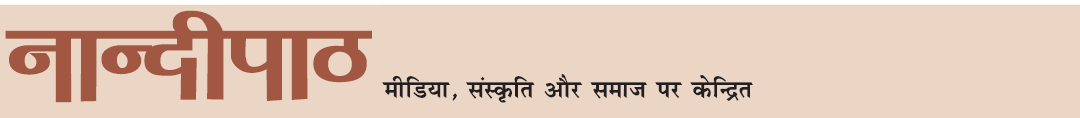
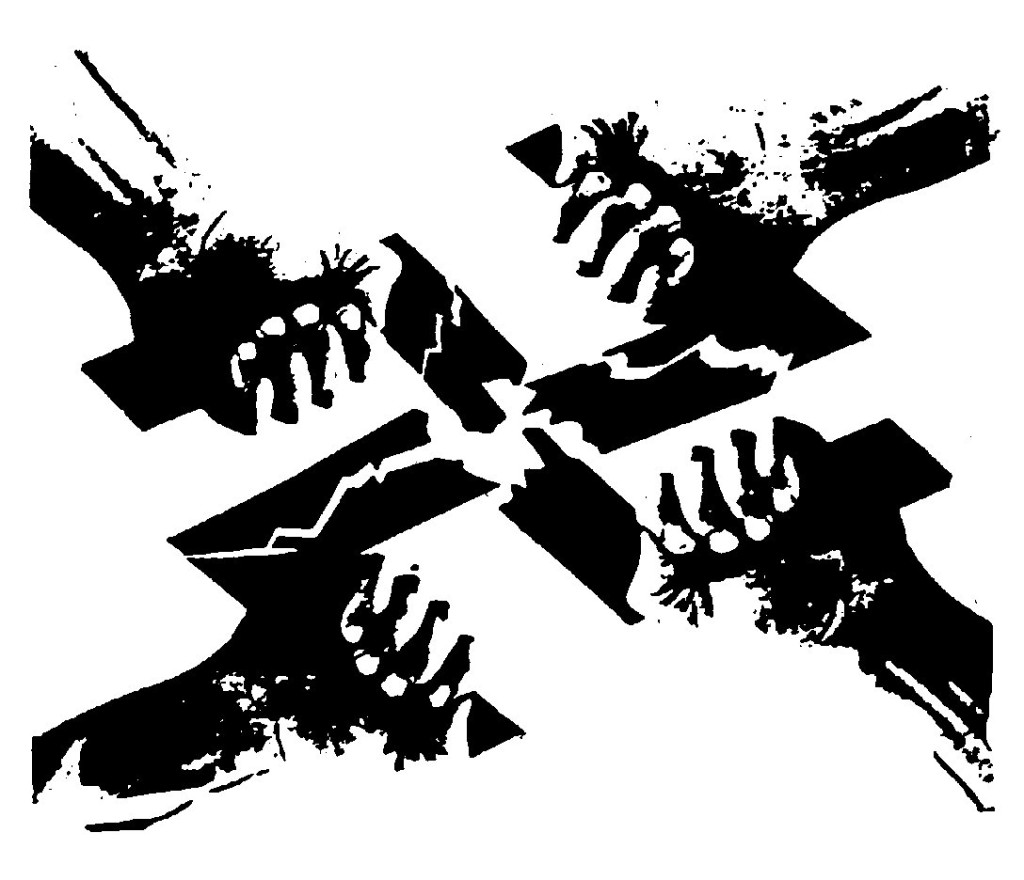
I am eagerly reading your magazine….