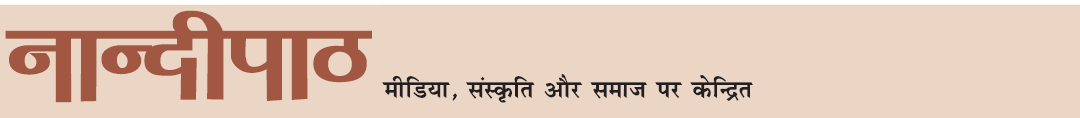पूँजीवाद का संकट और ‘सुपर हीरो’ व ‘एंग्री यंग मैन’ की वापसी (पहली किश्त)
अभिनव सिन्हा
पिछले लगभग एक दशक की भारतीय फ़िल्मों पर निगाह दौड़ाएँ तो एक बात विशेष तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है: ‘एंग्री यंग मैन’ और ‘सुपर हीरो’ की वापसी! 2006-7 के बाद से जो फ़िल्में सबसे बड़ी हिट साबित हुर्इ हैं उनमें ‘गजनी’, ‘दबंग’, ‘वाण्टेड’, ‘रेडी’, ‘राउडी राठौड़’, ‘सिंघम’, ‘दबंग-2’ आदि ने सबसे ज़्यादा कमार्इ की है। इन फ़िल्मों में जो बात ख़ास है वह है एक अपवादस्वरूप शक्तिशाली नायक की मौजूदगी जो कि अकेले अपने दम पर कर्इ ख़तरनाक खलनायकों से टकराता है और उन्हें पराजित कर देता है। अब आम अख़बारी फ़िल्म आलोचकों का भी इस बात पर ध्यान जा चुका है कि ये फ़िल्में कोर्इ अलग-थलग उदाहरण नहीं हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा जगत में एक प्रवृत्ति या रुझान का अंग हैं। हम भारतीय सिनेमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बालीवुड के अतिरिक्त, तेलुगू, तमिल, मलयाली, कन्नड़, बंगला, मराठी और यहाँ तक कि भोजपुरी फ़िल्म जगत में भी ऐसी फ़िल्में लगातार बन रही हैं। वास्तव में, कर्इ ऐसी हिन्दी फ़िल्में तमिल, तेलुगू व कन्नड़ फ़िल्मों की ‘रीमेक’ हैं। यह प्रवृत्ति दरअसल सिर्फ़ भारतीय नहीं है बल्कि हालीवुड में भी देखी जा सकती है। 2005-6 के बाद से हालीवुड में भी लगातार ‘सुपर हीरो’ वाली फ़िल्में बन रही हैं। ऐसे में, यह सोचने का विषय है कि यह दुनिया भर में फ़िल्मों (साथ ही, पाप कल्चर के अन्य माध्यमों जैसे कि कामिक्स, ग्राफ़िक उपन्यास आदि) में यह रुझान क्यों पैदा हुआ है? इसके लिए फ़िल्म जगत के एक ऐतिहासिक विश्लेषण की ज़रूरत है। जैसा कि ज्याँ लुक-कोमोली व ज्याँ नारबोनी ने लिखा है, “चूँकि हर फ़िल्म पूरे आर्थिक तन्त्र का अंग होती है, इसलिए वह उस विचारधारात्मक तन्त्र का भी अंग होती है – क्योंकि ‘सिनेमा’ व ‘कला’ भी विचारधारा की ही शाखाएँ होती हैं।” (ज्याँ लुक कोमोली, ज्याँ नारबोनी, “सिनेमा/आइडियालाजी/ क्रिटिसिज़्म” स्क्रीन, सिप्रंग 71, खण्ड-12, अंक-1, पृ. 27)
भारतीय सिनेमा के आज के ‘एंग्री यंग मैन’ और सुपरहीरो और पहले आ चुके ‘एंग्री यंग मैन’ व सुपरहीरो में काफ़ी अन्तर है। वैसे भी इतिहास कला के क्षेत्र में भी अपने आपको ज्यों का त्यों नहीं दुहराता, बल्कि कुण्डलाकार विकास करते हुए एक नये स्तर पर “दुहराता” है, जिसे मार्क्स ने दूसरे शब्दों में कहा था, “इतिहास में हर घटना अपने आपको दुहराती है, पहली बार त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में।” लेकिन फ़िर भी चूँकि तुलनात्मक अध्ययन से कर्इ बातें साफ़ होती है, इसलिए हम भारतीय सिनेमा में ‘एंग्री यंग मैन’ के अवतारों के प्रकट होने के अलग-अलग क्षणों का विश्लेषण करेंगे। इससे आज के ‘एंग्री यंग मैन’ और सुपरहीरो का चरित्र भी काफ़ी हद तक उजागर होगा। साथ ही, महानायक या ‘एंग्री यंग मैन’ की पूरी अवधारणा के दार्शनिक मूलों का भी विवेचन करना ज़रूरी है ताकि इस परिघटना की बारीकियों और इसके बार-बार प्रकट होने के सन्दर्भों को भी समझा जा सके।
1973 में ‘ज़ंजीर’ के साथ भारतीय सिनेमा में पहले ‘एंग्री यंग मैन’ अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। खुद अमिताभ बच्चन के मुताबिक सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के पहले ‘एंग्री यंग मैन’ थे। यह बात कुछ मायनों में सच भी है। लेकिन सुनील दत्त का ‘एंग्री यंग मैन’ का संस्करण अभी प्राक-पूँजीवादी दुनिया या फ़िर एक ऐसी दुनिया का ‘एंग्री यंग मैन’ था जो अभी संक्रमण में थी। ‘मेरी माँ के कंगन वापस कर दे लाला’ वास्तव में सामन्तवाद से पूँजीवाद के संक्रमण के दौर में पैदा हुए ‘एंग्री यंग मैन’ का एक रूप था। अमिताभ बच्चन का ‘एंग्री यंग मैन’ शहर में आ चुका है – ‘दीवार’, ‘ज़ंजीर’, आदि – और वह आज़ादी के बाद पूँजीवादी व्यवस्था की सबसे नग्न अभिव्यक्तियों के समक्ष एक ‘पैथोलाजिकल’ आक्रोश की सहज अभिव्यक्ति है। सुनील दत्त का ‘एंग्री यंग मैन’ बहुत दिन तक जि़न्दा नहीं रह सकता था। 1960 के दशक के अन्त तक ऐसे महानायक का अन्त होना ही था; क्योंकि 1960 के दशक के अन्त के साथ पुराना भारत भी निर्णायक तौर पर नेपथ्य में जा रहा था। इस रूप में सुनील दत्त के ‘एंग्री यंग मैन’ का संस्करण एक लघुजीवी परिघटना थी और ऐसा ही हो भी सकता था।
अमिताभ बच्चन जिस ‘एंग्री यंग मैन’ का संस्करण पेश कर रहे थे, वह उभरते हुए पूँजीवादी भारत का ‘एंग्री यंग मैन’ था, जो आज़ादी के बाद दिखलाये गये सपनों के खणिडत होने पर जनता के असन्तोष की अभिव्यक्ति था। 1973 में ‘ज़जीर’ के आने के बाद अमिताभ बच्चन की कर्इ फ़िल्में आयीं जिसमें उन्होंने ‘एंग्री यंग मैन’ का किरदार निभाया। इनमें से अधिकांश फ़िल्में बड़ी हिट साबित हुर्इं। इन फ़िल्मों के हिट होने के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसी फ़िल्मों का एक ‘ट्रेण्ड’ पैदा हुआ। दक्षिण में रजनीकान्त और बंगाली फ़िल्मों में रंजीत मलिक इस रुझान के प्रमुख नुमाइन्दे थे। पूरे देश में ऐसी फ़िल्में उस समय काफ़ी सफ़ल हुर्इं। किसी भी विशिष्ट समय में यदि कुछ ख़ास किस्म की फ़िल्में सफ़ल होती हैं, तो इसके कारणों को सिर्फ़ कुछ कलाकारों की प्रतिभा और उनके सुदर्शन होने के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। बहुत से सुदर्शन और अभिनय की प्रतिभा से परिपूर्ण कलाकार कभी सफ़ल नहीं हो पाये। जबकि उनसे उन्नीस पड़ने वाले तमाम कलाकार सफ़ल हुए। उनकी सफ़लता और असफ़लता के कारणों की तलाश सबसे पहले उस युग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सन्दर्भ में की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी सफ़ल कलाकार की सफ़लता को महज़ सामाजिक सन्दर्भ पर अपचयित कर रहे हैं। इसका अर्थ सिर्फ़ यह है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृति व आर्थिक सन्दर्भों के अनुकूल होने पर ही व्यक्तिगत प्रतिभाओं का प्रस्फ़ुटन होने की सम्भावना ज़्यादा होती है और इस रूप में किसी कलाकार की प्रतिभा में अपने युग की नब्ज़ पर पकड़ होने को भी शामिल किया जाना चाहिए।
1970 के दशक में फ़िल्मों में एक आधुनिक और शहरी ‘एंग्री यंग मैन’ के पैदा होने और फ़िर ज़बर्दस्त रूप से सफ़ल होने के कारणों की पड़ताल भी 1970 के दशक के पूरे सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सन्दर्भों में की जानी चाहिए। 1970 का दशक भारतीय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए एक अभूतपूर्व संकट का दौर था। आज़ादी के ठीक पहले और तुरन्त बाद तेलंगाना, तेभागा और पुनप्रा-वायलार की ज़बर्दस्त किसान बग़ावतों को बर्बरता से कुचलने के बाद भारतीय पूँजीवादी व्यवस्था के स्थिरीकरण का एक दौर चला था जिसमें नेहरू के नेतृत्व में भारतीय पूँजीपति वर्ग ने पूँजीवादी विकास का एक विशिष्ट रास्ता चुना। इस रास्ते में क्रमिक प्रक्रिया में लगभग युंकर शैली के भूमि सुधार, राष्ट्रीय बचत को संकेनिद्रत कर पूँजीपति वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करना, अवसंरचनागत उधोगों का विकास और आयात प्रतिस्थापन की नीतियाँ शामिल थीं। इस स्थिरीकरण में हुए परिवर्तनों ने भारतीय पूँजीवाद के भावी विकास की दिशा निर्धारित की। लेकिन इसी दौर में भारतीय जनता के आज़ादी के बाद के खुशहाली के, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के, सामाजिक न्याय के और उत्पीड़न से मुक्ति के सपने धीमी मौत मर रहे थे। आज़ादी के समय का बेहद तनु और कमज़ोर पूँजीपति वर्ग जनता की मेहनत की कमार्इ पर खड़ा हो रहा था, मेहनतकश जनता की लूट को तेज़ी के साथ शुरू करने के लिए पूँजी संचय और कर्इ जगहों पर ‘आदिम पूँजी संचय की प्रक्रिया चला रहा था; भारतीय पूँजीवादी राजनीतिज्ञ आज़ादी के कुछ समय बाद से ही अपनी सेवाओं का अनौपचारिक लाभांश पूँजीपति वर्ग से वसूलने के लिए घपलों-घोटालों के भारतीय महाकाव्य की प्रस्तावना लिखना शुरू कर चुके थे। पब्लिक सेक्टर का जो विशालकाय और भारी-भरकम ढाँचा खड़ा किया गया था, उसके भीतर का टटपुँजिया और साथ ही ऊपरी स्तरों का भ्रष्टाचार जनता के सामने आने लगा था। पुलिस और सेना आम जनता पर दमन के मामले में अंग्रे़जों द्वारा स्थापित कीर्तिमानों से प्रतिस्पर्धा में लगी हुर्इ थी। देश के तमाम इलाकों में मज़दूरों और ग़रीब किसानों के संघर्ष का नग्न दमन किया जा रहा था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से यह प्रक्रिया सहज दिखलायी पड़ने वाली प्रक्रिया बन चुकी थी। कर्इ जगहों पर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों, विशेष तौर पर, रेलवे कर्मचारियों के बीच भी असन्तोष बढ़ रहा था। इसके अलावा, देश का आम मध्यवर्ग बेरोज़गारी और महँगार्इ के बोझ तले कराह रहा था और सरकारी भ्रष्टाचार और पुलिस आदि के दमनकारी रवैये के विरुद्ध उनमें भी आक्रोश था। ग़रीब दलित आबादी पर जातिगत उत्पीड़न के आर्थिक-राजनीतिक ढाँचे में परिवर्तन आ गया था, लेकिन अगर सिर्फ़ परिमाण की बात करें तो दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुर्इ थी। इन सभी कारकों ने मिलकर जो प्रभाव पैदा किया था वह था जनता में सत्ता के विरुद्ध सघन आक्रोश और असन्तोष।
1960 के दशक के उत्तरार्ध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के संसदवादी और संशोधनवादी चरित्र के सामने आने के साथ कम्युनिस्ट आन्दोलन के भीतर भी नयी सुगबुगाहट पैदा हो चुकी थी, जो कि 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह और उसके बाद शुरू हुए मार्क्सवादी-लेनिनवादी आन्दोलन के साथ ठोस आकार ग्रहण करने लगी थी। नक्सलबाड़ी विद्रोह और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के गठन ने कुछ समय के लिए देश के ग़रीब किसानों, दलितों के बीच उम्मीद जगाने के साथ ही मध्यवर्ग के एक हिस्से में भी कुछ आशा का संचार किया था, जिसमें विशेष तौर पर विश्वविधालयों के छात्र और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी प्रमुख थे। लेकिन भारतीय क्रान्ति की किसी उपयुक्त समझदारी और जनदिशा के अभाव के कारण जल्द ही यह आन्दोलन वामपंथी-दुस्साहसवाद के गड्ढे में जा गिरा और आन्दोलन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1974-75 आते-आते यह आन्दोलन निर्णायक रूप से कुचला जा चुका था और बिखराव का दौर अपने चरम पर था। सच है कि 1975 से ही कुछ पुनर्संगठन के प्रयास भी शुरू हुए थे, लेकिन इस दौर में भी विभिन्न धड़े आम तौर पर कार्यक्रम के प्रश्न पर पुराने खाँचे से बाहर नहीं जा रहे थे, और कुछ राजनीतिक पैबन्दसाज़ी से काम चलाना चाह रहे थे। आगे क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन का क्या हुआ, इस पर बहुत विस्तार में जाना यहाँ सम्भव नहीं है। लेकिन 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में इसकी वजह से जो उम्मीद जगी थी, वह ख़त्म होने लगी थी। इसी दौर में, मज़दूरों का हड़ताल आन्दोलन भी पूरे देश में ज़ोरों पर था। रेलवे की आम हड़ताल ने पूरी पूँजीवादी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद 1975 में आपातकाल लागू हुआ और इन सभी संघर्षों का इन्दिरा गाँधी की सरकार ने जमकर दमन किया। आपातकाल के विरुद्ध जनता का गुस्सा आपातकाल के ख़त्म होने के बाद इन्दिरा गाँधी की चुनावी हार और जनता पार्टी के विजय के रूप में निकला। जनता पार्टी ने एक छद्म विकल्प पेश कर जनता के असन्तोष की लहर को व्यवस्था में सहयोजित किया और उसे व्यवस्था की चौहिद्दियों से बाहर जाने से रोका। लेकिन ऐसे सभी प्रयास जल्द ही अपनी असलियत के साथ सामने आने लगते हैं और जनता पार्टी की सरकार के साथ भी यही हुआ।
1973 में डालर-स्वर्ण मानक के टूटने के साथ जो वैश्विक पूँजीवादी संकट शुरू हुआ (जो कि थोड़े उतार-चढ़ावों, बुलबुलों के बनने और फ़ूटने और हर बार संकट के और गहराते जाने के साथ आज तक जारी है) उसका प्रभाव साल भर के भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता था। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में बढ़ोत्तरी के साथ महँगार्इ आज़ादी के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर जा रही थी। अति-उत्पादन के संकट के कारण भी बाज़ार में मन्दी रफ्तार पकड़ रही थी। इस समूचे सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक संकट और साथ ही कारगर विकल्पों की अनुपस्थिति में समाज में जो असन्तोष और गुस्सा कुलबुला रहा था, उसे अन्तत: कला के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिलनी ही थी।
यह कहना कोर्इ नयी बात नहीं होगी कि कला का एक सामाजिक प्रकार्य होता है। लेकिन यह सामाजिक प्रकार्य क्या होता है, इस पर शुरू से ही बहसें मौजूद रही हैं। कुछ का कहना था कि कला की रचना का ‘आब्जेक्ट कला की रचना ही है’ कला व्यक्ति के आन्तरिक भावोद्वेगों की अभिव्यक्ति है और कला की रचना स्वयं कला की रचना का उददेश्य है। ज़ाहिर है कि ‘कला के लिए कला में यक़ीन करने वाला पक्ष तार्किक तौर पर बहुत मज़बूत स्थिति में नहीं था और इसका अवसान होना ही था। कुछ अन्य के मुताबिक कला का प्रकार्य होता है समाज का ज्यों का त्यों चित्रण करना। हालाँकि, कला के क्षेत्र का हर गम्भीर अध्येयता जानता है कि ‘ज्यों का त्यों’ चित्रण एक मिथक है। प्रेक्षक जिस यथार्थ का अवलोकन कर रहा होता है, एक तो वह स्वयं उस यथार्थ का एक जैविक अंग भी होता है और दूसरी बात यह कि उस यथार्थ को छेड़े और प्रभावित किये बग़ैर वह उसका प्रेक्षण भी नहीं कर सकता है। वास्तव में, प्रेक्षण की प्रक्रिया वस्तुत: एक अन्तःक्रिया की प्रक्रिया के रूप में ही सम्पन्न हो सकती है। यह बात विज्ञान के क्षेत्र में जितनी सत्य ठहरती है, उतनी कला के क्षेत्र में भी। इस प्रक्रिया में न तो प्रेक्षक वह रह जाता है और न ही प्रेक्षित, लेकिन इन दोनों की गतियों और परिवर्तनों के द्वन्द्व के रूप में जो चीज़ अस्तित्व में आती है, वही तो यथार्थ है और इस यथार्थ को ही अभिव्यक्ति देना कला का प्रकार्य होता है। इस द्वन्द्व को सही ढंग से नहीं समझने के कारण कुछ लोगों के ने विज्ञान के क्षेत्र में और साथ ही कुछ लोगों ने कला के भी क्षेत्र में यथार्थ के अपने आपमें मौजूद होने पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया और काण्टवाद और नवकाण्टवाद के नये संस्करण रचने शुरू कर दिये। लेकिन इन धाराओं का चलन अब ख़त्म हो रहा है। अब यदि कला का प्रकार्य यथार्थ की इस द्वन्द्वात्मकता को कलात्मक व सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति देना है, तो यह कार्य कैसे सम्पन्न हो सकता है?
कला के इस प्रकार्य को सम्पन्न करना तभी सम्भव है जब कला यथार्थ में मौजूद अनुपस्थित मूल्यों/तत्वों की आपूर्ति करे। कला सिर्फ़ यथार्थ का चित्रण नहीं है, बल्कि यह यथार्थ में मौजूद ‘अभाव’/अनुपस्थिति (Lack) को सम्बोधित करती है; यह अभाव/अनुपस्थिति यथार्थ में मौजूद द्वन्द्वों के कारण पैदा होती है। और ठोस शब्दों में कहें तो किसी भी ऐतिहासिक युग में मनुष्यों की चाहतों या आकांक्षाओं, जो कि सम्पूर्ण ऐतिहासिक-राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती हैं (जिनका कोर्इ आद्यरूपीकरण करना ‘मानव स्वभाव’ के अनैतिहासिक सिद्धान्त की ओर ले जायेगा), और यथार्थ के बीच के अन्तर से यह अभाव/अनुपस्थिति पैदा होती है। मनोविश्लेषकों की भाषा में कहें तो ‘वास्तविक’ और ‘आदर्श’ के बीच का अन्तर ‘आकांक्षाओं/इच्छाओं को जन्म देता है, बस मनोविश्लेषण की ज्ञान शाखा के पास न तो ‘वास्तविक’ की ऐतिहासिकता को समझने की क्षमता होती है और न ही ‘आदर्श’ की ऐतिहासिकता को समझने की। कला का प्रकार्य यह होता है कि इन आकांक्षाओं/इच्छाओं को कलात्मक अभिव्यक्ति दे और उनकी एक प्रकार की ‘फ़ैण्टास्टिक’ पूर्ति भी करे। कला यदि अभाव/अनुपस्थिति को भरने के लिए मूल्यों की आपूर्ति नहीं करती, तो वह कला नहीं है बल्कि एक सांख्यिकी रपट है (हालाँकि कर्इ उत्तरऔपनिवेशिक सिद्धान्तकार सांख्यिकीय रपटों को भी कलात्मक रचना मानते हैं!)।
अब कला का यह प्रकार्य किस रूप में पूरा हो रहा है, यह उस कला व कलाकार की भौतिक वर्गीय अवस्थिति और चुनी गयी वर्गीय अवस्थिति के द्वन्द्व और तत्कालीन ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक कारकों के कुल प्रभाव से निर्धारित व (अल्थूसर की भाषा) में अति-निर्धारित होता है। मिसाल के तौर पर, एक ही सामाजिक-आर्थिक सन्धि-बिन्दु (Conjuncture) कर्इ प्रकार की कलात्मक रचनाओं को जन्म दे सकते हैं। बुर्जुआ कलाकार जनता की अपूर्ण आकांक्षाओं को सम्बोधित करने के लिए जो कलात्मक रचना सृजित करेगा, वह उस ‘अभाव/अनुपस्थिति की एक पश्चगामी (यथास्थितिवादी) पूर्ति करेगी। किसी भी कलात्मक रचना की तरह यह बुर्जुआ कलात्मक रचना भी आनन्द का सृजन करेगी; लेकिन यह आनन्द उन्मादपूर्ण और कार्निवालीय (carnivalesque) होगा। यह चिन्तन और आलोचनात्मकता की ओर ले जाने की बजाय एक ऐसा आनन्द प्रदान करेगी जिसकी तुलना नशे या अर्द्धबेहोशी से की जा सकती है। यह पूरा कार्य बुर्जुआ कला कर्इ प्रकार से करती है। कर्इ बार यह सीधे तौर पर आलोचनात्मकता और चिन्तन का दमन करके करती है (मिसाल के तौर पर, तमाम किस्म की मसाला फ़िल्में) और कर्इ बार यह कार्य आलोचनात्मकता और चिन्तन को प्रोत्साहित करने के छद्म आवरण में किया जाता है (जैसे गोविन्द निहलानी, श्याम बेनेगल, सुधीर मिश्रा आदि की फ़िल्में)। जिन मामलों में आलोचनात्मकता और चिन्तन को प्रोत्साहित करने के छद्म आवरण को अपनाया जाता है उनमें व्यवस्था की एक प्रतीतिगत आलोचना भी होती है; लेकिन यह आलोचना दो स्तरों पर वास्तव में आलोचना का निषेध होती है, या अन-आलोचना होती है। मिसाल के तौर पर, ‘अंकुर’ (प्रतीकात्मक नपुंसक विद्रोह), ‘आक्रोश’ (गुस्से और असन्तोष के अन्त:स्फोट का कलात्मक महिमा-मण्डन), ‘अर्द्धसत्य’ (मध्यवर्गीय प्रतिक्रियावादी ‘आत्मिक’ उभार का फ़ासीवादी विस्फोट और इसका महिमा-मण्डन), आदि जैसी फ़िल्मों में व्यवस्था की आन्तरिक सड़न, मानवीय दु:ख, विद्रोह की भावना आदि का एक चित्रण है। लेकिन अन्त में, यह ‘आलोचनाएँ व्यवस्था को अपराजेय बनाती हैं, एक वर्ग के असन्तोष और गुस्से का वैयक्तिक संघनन (individualistic condensation) करके उसे एक व्यक्ति पर आरोपित करती हैं और उसे एक वैयक्तिक/व्यक्तिवादी विद्रोह के रूप में चित्रित करती हैं और इसके साथ ही इन विद्रोहों की असफ़लता को तार्किक अन्त के रूप में पेश करना सहज बन जाता है। कुल मिलाकर यह परिवर्तन से अभिकरण छीनने का प्रयास करती हैं।
ख़ास तौर पर, गोविन्द निहलानी की फ़िल्मों में व्यवस्था की घृणास्पद और जुगुप्सा पैदा करने वाली सड़न को दिखलाया जाता है, लेकिन साथ ही व्यवस्था को एक सर्वशक्तिशाली और सर्वत्रा उपस्थित वस्तु के रूप में पेश किया जाता है और साथ ही उसको लेकर एक भय का वातावरण तैयार किया जाता है (जैसे कि ‘द्रोहकाल’ और ‘देव’) जिससे कि देखने वाला एक पराजयबोध का शिकार हो जाये। दूसरे शब्दों में निहलानी की फ़िल्में व्यक्ति को राज्यपूजा (statolatry) के लिए प्रेरित करती हैं। यह सबवर्सिव आलोचना के आवरण में आलोचना का ही सबवर्ज़न है। यह एक व्यक्ति को परवर्ट बन जाने को प्रेरित करती हैं; इनका सन्देश होता है, “तुम सत्ता से जीत नहीं सकते, इसलिए सत्ता के साथ आ जाओ।” दूसरी चीज़ जो कि निहलानी की फ़िल्मों में ख़ास तौर पर पहचानी जा सकती है वह है विद्रोह का चित्रण। निहलानी की फ़िल्मों में विद्रोह का चित्रण या तो वैयक्तिक होता है और हमेशा विस्फोट (explosion) की बजाय अन्त:स्फोट (implosion) के रूप में होता है, या फ़िर उसका विस्फोट होता भी है तो हमेशा प्रतिक्रियावादी-अस्तित्ववादी और निरंकुश व्यक्तिवादी रूप में होता है; या फ़िर अगर इस विद्रोह को किसी भी रूप की सामूहिकता प्रदान की जाती है तो यह दिखलाया जाता है कि सामूहिक या संगठित विद्रोह हमेशा स्वयं सत्ता के रूपों को जन्म देता है, उसमें भी पतन और भ्रष्टाचार का अंकुरण होने लगता है। जैसे कि ‘द्रोहकाल’ में क्रान्तिकारियों का चित्रण। यानी, निहलानी के फ़िल्मों की ‘बाटमलाइन’ यह होती है: सत्ता सर्वशक्तिमान और सर्वस्व है और उसका प्रतिरोध व्यर्थ है क्योंकि स्वस्थ प्रतिरोध वैयक्तिक होगा और उसका या तो अन्त:स्फोट होगा या फ़िर उसका विस्फोट प्रतिक्रियावादी रूप में होगा, और यदि प्रतिरोध संगठित या सामूहिक होगा तो वह भ्रूण रूप में स्वयं पतित और निरंकुश किस्म की सत्ता को जन्म देगा। दूसरे शब्दों में, दमन का प्रतिरोध व्यर्थ है और सत्ता से बचने का कोर्इ रास्ता नहीं है। यहाँ पर हम अचरज करते हैं क्या गोविन्द निहलानी मिशेल फूको को पढ़ चुके थे? निश्चित तौर पर, 1968 के बाद फांसीसी “वाम” में जो कुछ चल रहा था वह दुनिया भर के बौद्धिक दायरों में चर्चा का विषय था और निश्चित तौर पर श्याम बेनेगल और गोविन्द निहलानी जैसे फ़िल्मकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके सम्पर्क में आये होंगे (हमारा यहाँ यह मन्तव्य बिल्कुल नहीं है कि हम गोविन्द निहलानी और श्याम बेनेगल के बीच कोर्इ सादृश्य-निरूपण करें; बेनेगल ने बुर्जुआ मानवतावादी दृष्टिकोण से कुछ अच्छी कलात्मक रचनाओं का सृजन किया है, जिन्हें उनकी सीमाओं के बावजूद देखा और आपत्तियों के साथ सराहा जा सकता है)। लेकिन यह महज़ एक अटकलबाज़ी है और हम किसी फ़िल्मकार की कलात्मक रचना का मूल्यांकन बाहय प्रभावों के आधार पर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, फूको में एक छद्म आमूलगामिता थी (जहाँ फूको प्रतिरोध की सम्भाव्यता का अपना सिद्धान्त देते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सभी मानकों के विरुद्ध विद्रोह करके सत्ता के वर्चस्व को चुनौती देगा), लेकिन निहलानी में (अगर उन पर फूको का प्रभाव है तो भी!) कोर्इ छद्म आमूलगामिता भी नहीं है। यहाँ मैं उन फ़िल्म देखने वालों की समझदारी की बात नहीं कर रहा जिनकी प्रतिक्रियाएँ सिनेमा हाल में आह-कराह के रूप में निकल पड़ती हैं। स्लावोय जि़ज़ेक ने एक जगह लिखा है कि फ़िल्म को किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ देखना सबसे प्रबोधनकारी होता है, क्योंकि इससे फ़िल्म के सामाजिक प्रभाव के कर्इ ऐसे पहलू उजागर होते हैं, जो कि आलोचकों के साथ फ़िल्म देखने में नहीं हो सकते; फ़िर जि़ज़ेक ‘मैट्रिक्स’ फ़िल्म को एक सिनेमा हाल में देखने का अनुभव बताते हैं, जिसमें एक मूर्ख व्यक्ति उनकी बगल में बैठा हुआ था और वह बीच-बीच में विस्मय में कुछ बोल उठता था, जैसे कि “ओह, तो कोर्इ यथार्थ नहीं होता!!” निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के साथ फ़िल्म देखना फ़िल्म के सामाजिक प्रभाव के न्यूनतम साझा हर (lowest common denominator) को समझने में मददगार हो सकता है, लेकिन आलोचनात्मक तौर पर फ़िल्म को समझना एक अलग मसला है।
बहरहाल, इस प्रकार की सभी बुर्जुआ कला फ़िल्में वास्तव में ‘अभाव/अनुपस्थिति’ को भरने के लिए कुछ मूल्य देतीं हैं। इन मूल्यों का निर्धारण बुर्जुआ वर्ग के विश्व-दृष्टिकोण के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पर, पूँजीवादी समाज और संस्कृति की जुगुप्सित दरिद्रता को “यथार्थवादी” (प्रकृतवादी पढ़ें!) रूप से दिखलाने के बावजूद ये फ़िल्में दर्शक के भीतर तथ्यों के अपने विशिष्ट चयन, चित्रण और दृष्टिकोण से पराजयबोध, यथास्थितिवाद, ‘विकल्प का भय’ (मतलब यह कहना, “माना व्यवस्था ख़राब है बन्धु, लेकिन कोर्इ विकल्प नहीं है! अगर विकल्प बनाने की तरफ़ जाओगे तो अन्त में कुछ ऐसा पैदा कर बैठोगे जो आज की व्यवस्था से भी ज़्यादा निरंकुश, सर्वसत्तावादी और फ़ासीवादी होगा!), और निराशावाद पैदा करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को विद्रोह की पराजय या कभी विजय हासिल न कर पाने वाले दिशाहीन, व्यक्तिवादी और कीर्केगार्दियन अस्तित्ववादी विद्रोह का आनन्द लेने की आज्ञा होती है। ‘अर्द्धसत्य’ जैसी फ़िल्में भी एक विशेष प्रकार के ‘एंग्री यंग मैन’ को ही पेश करती हैं; बस फर्क यह होता है कि ‘ज़जीर’ के ‘एंग्री यंग मैन’ के मुकाबले यह कम ‘फ़ैण्टास्टिकट चित्रण है और दूरगामी तौर पर यह ज़्यादा असरदार होता है। वैसे यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि ‘अर्द्धसत्य’ में ओमपुरी की भूमिका के लिए निहलानी की पहली पसन्द क्लासिकीय ‘एंग्री यंग मैन’ अमिताभ बच्चन ही थे। बहरहाल, इस गासिप को छोड़कर मूल मुददे पर आते हैं। कला फ़िल्मों में भी यह दौर ‘एंग्री यंग मैन’ को पेश कर रहा था और साथ ही एकदम ठेठ कामर्शियल सिनेमा में भी यही स्थिति थी।
‘ज़ंजीर’ में जब अमिताभ बच्चन प्राण की कुर्सी को ठोकर मारकर बोलते हैं, “यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं!” तो यह उस दौर का एक प्रातिनिधिक कथन बन जाता है जो बहुत सी जनभावनाओं को अमूर्त रूप में अभिव्यक्ति देता था। यह कथन भारतीय सिने जगत में एक आधुनिक, शहरी, मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय और पेशेवर सामाजिक वर्ग से आने वाले ‘एंग्री यंग मैन’ का पदार्पण था। इसके बाद जो तमाम फ़िल्में आयीं उनमें भी किसी न किसी रूप में इसी ‘एंग्री यंग मैन’ का कोर्इ संस्करण पेश किया गया। इस दौर का ‘एंग्री यंग मैन’ बुनियादी तौर पर एक अच्छा, नैतिक, संवेदनशील, न्यायप्रिय, और आम तौर पर स्त्रियों का सम्मान करने वाला नायक था, चाहे वह पेशे से अपराधी या माफ़िया ही क्यों न हो। वास्तव में, सभी अपराधी ‘एंग्री यंग मैन’ चरित्र चयन करके अपराधी नहीं बने थे, बल्कि स्थितियों के हाथों मजबूर होकर अपराधी बने थे। अक्सर उनका अपराधी होना भी विद्रोह की एक सर्वखण्डनवादी अभिव्यक्ति हुआ करता था। 1970 के दशक का ‘एंग्री यंग मैन’ आदर्शवादी था और व्यवस्था के ख़िलाफ़ खड़ा था, चाहे उसकी ज़मीन कानून के दायरों का अतिक्रमण ही क्यों न करती हो। लेकिन अपने विद्रोह में वह अकेला था; वह अकेले ही खलनायकों (जो कि सम्पूर्ण पूँजीवादी सत्ता के अलग-अलग स्तम्भों की नुमाइन्दगी करते थे!) से निपट लेता था और अक्सर ऐसा करते हुए खुद भी मारा जाता था। उसके विद्रोह के साथ दर्शक ‘फ़ैण्टास्टिक’ तदनुभूति महसूस करता है, जो कि कल्पना में उसके अहं की मालिश करता है। मिसाल के तौर पर, मैं ‘गंगाजल’ फ़िल्म का उदाहरण पेश करना चाहूँगा, जो कि ‘एंग्री यंग मैन’ के उत्तर-क्लासिकीय दौर में क्लासिकीय ‘एंग्री यंग मैन’ को पेश करती है। अजय देवगन का सवर्ण चरित्र जिस तरीके से मध्य कुलक जातियों की जातिगत दबंगर्इ के खि़ालाफ़ अकेले मुकाबला करता है और अन्त में खलनायकों को पराजित भी करता है, जिस तरीके से सवर्ण पुलिस वाले मध्य जातियों के अपराधियों को बर्बर तरीके से यातना देते हैं, उसे देखकर एक कायर मध्यवर्गीय व्यक्ति को भी आनन्द मिलता है; जो सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति सड़क पर अपराधियों और गुण्डों के जुल्म को सहता है और उसका कोर्इ सामूहिक प्रतिरोध न कर पाने के कारण चुप रह जाता है, जिसके दिल में इन चीज़ों के विरुद्ध जमा हो रहा गुस्सा संघनित होता रहता है, वह अन्तत: एक प्रतिक्रियावादी रुख़ ले लेता है; वह वास्तविकता में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब वह सिनेमा के पर्दे पर किसी र्इमानदार पुलिस अधिकारी को इन गुण्डों से बर्बरतापूर्वक निपटते हुए देखता है, तो सिनेमा हाल में चवन्नियाँ उछालता है और सीटियाँ बजाता है; उसे लगता है कि यह सब वह कर रहा है, और इस भावना को ही मैं ‘फ़ैण्टास्टिक’ तदनुभूति कह रहा हूँ। अभी हम ‘गंगाजल’ में जातिगत तौर पर जो गतिकी सतह के नीचे काम कर रही है, उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ़ एक ‘एंग्री यंग मैन’ चरित्र के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपोत्पादों का ज़िक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, ‘गंगाजल’ कर्इ स्तरों पर साथ काम करने वाली एक फ़िल्म है और अलग से एक आलोचनात्मक लेख की माँग करती है। ‘गंगाजल’ में ‘एंग्री यंग मैन’ का उपकरण अपना काम बेहद संवेदनहीन और बर्बर तरीके से करता है और उसके सौन्दर्यात्मक मूल्य में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि यह पूँजीवाद के कहीं ज़्यादा पतनशील दौर का ‘एंग्री यंग मैन’ है; इस विषय पर हम आगे आयेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि 1970 के दशक का ‘एंग्री यंग मैन’ गुणात्मक तौर पर इसी प्रकार्य को पूरा करता था, यानी कि एक ‘फ़ैण्टास्टिक’ और अहंपोषण करने वाली तदनुभूति को पैदा करना; दर्शक जो वास्तविक जीवन में नहीं कर सकता, वह इस चरित्र के साथ तदनुभूति के ज़रिये फ़िल्म के पर्दे पर वही चीज़ें करता है। चाहे वह ‘ज़जीर’ के अमिताभ बच्चन हों, या फ़िर ‘दीवार’ के, दोनों के ही चरित्रों के साथ एक ‘फ़ैण्टास्टिक’ तदनुभूति का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन 1970 के दशक के ‘एंग्री यंग मैन’ के क्रिया-कलाप अभी उस पतनशीलता का प्रतिबिम्बन नहीं करते थे, जिस पतनशीलता का प्रतिबिम्बन आज का नया ‘एंग्री यंग मैन’ कर रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे।
1970 के दशक में पैदा हुए ‘एंग्री यंग मैन’ का दौर राजनीति में जनता पार्टी के दौर के बाद उतार पर था। जनता पार्टी ने जहाँ बिना कोर्इ विकल्प दिये आम जनता की आशाओं और उसकी नाराज़गी को हस्तगत किया और व्यवस्था के दायरे में सहयोजित किया। इसके बाद के दौर में कुछ ‘एंग्री यंग मैन’ वाली शैली की फ़िल्में बनती रहीं, लेकिन दो अन्य प्रकार की फ़िल्मों का रुझान भी पैदा हुआ। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में एक ओर तो एकदम सड़कछाप फ़िल्मों का दौर आया जिसका नायक न तो खुद गम्भीर था और न ही यह उम्मीद करता था कि उसे गम्भीरता से लिया जाय, जैसे कि सफ़ेद जूतों, चुस्त सफ़ेद पैण्ट, रंग-बिरंगे फूलों की छाप वाली कमीज़ और पेंसिल जैसी मूछों वाले जितेन्द्र, जो कि तमाम ऐसी फ़िल्मों में आये, जैसे कि ‘हिम्मतवाला’। इस तरह की फ़िल्में हिट भी हुर्इं क्योंकि आशाओं के ज्वार के चढ़ने और फ़िर नपुंसक तरीके से झड़ जाने के बाद लोग इस मिजाज़ में होते हैं कि कुछ बेतुका या अर्थहीन करें; तो इस दौर में ऐसी कर्इ अर्थहीन और बेतुकी फ़िल्में बनीं जिसमें नायक, नायिका से लेकर खलनायिका तक हर चरित्र प्रहसनात्मक होता है। हास्य कलाकारों के बेकार होते जाने का जो रुझान आज चरम पर है, इसकी शुरुआत इसी दौर में हुर्इ थी। क्योंकि जब हरेक चरित्र प्रहसनात्मक हो जायेगा तो फ़िर हास्य कलाकार क्या करेगा?
एक दूसरे प्रकार का मध्यवर्गीय सिनेमा भी इस दौर में काफ़ी फला-फूला। मध्यवर्ग भव्यता और दिव्यता की सारी फन्तासियों से उफब चुका था। मोहभंग का वह दौर जारी था, जब भव्य (ग्रैण्ड) चीज़ों पर इंसान को हँसी आने लगती है, उन्हें लेकर वह शंकालु हो जाता है और उनसे ऊबकर अपनी छोटी दुनिया में जीने और सोचने का मसाला ढूँढता है। यह दौर ‘छोटे और तुच्छ के जश्न’ का दौर था जिसमें ऐसी फ़िल्में बनीं जो कि आम पेशेवर मध्यवर्ग के जीवन की छोटी-छोटी सांसारिक खुशियों और दुखों पर आधारित थीं। निश्चित तौर पर, इनमें से तमाम फ़िल्मों में इस जीवन का चित्रण काफ़ी हद तक यथार्थवादी ढंग से किया गया था और इस वर्ग के मनोविज्ञान से जुड़े कर्इ मानवीय प्रश्न उठाये गये थे। लेकिन साफ़ तौर पर, किसी भी तरह का भव्य नायकत्व इन फ़िल्मों में अनुपस्थित था। ऐसी फ़िल्में जल्द ही बनना कम भी हो गयीं क्योंकि ये फ़िल्में बहुत समय तक वांछित प्रकार्य को पूरा नहीं कर सकती हैं। ये अभाव/अनुपस्थिति को सम्बोधित करने वाले मूल्यों की आपूर्ति की बजाय अभाव/अनुपस्थिति को ही ‘नार्म’ बनाती हैं। ऐसे में, ऐसी फ़िल्मों के बेहद छोटे दौर बीच-बीच में आते हैं।
क्लासिकीय ‘एंग्री यंग मैन’ के दौर के ख़त्म होने और 1990 के दशक की शुरुआत का दौर विशेष तौर पर हिन्दी सिनेमा के लिए एक संक्रमण का दौर था। इस दौर का भ्रम इस दौर की फ़िल्मों में नज़र आ रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत में नयी आर्थिक नीतियों का श्रीगणेश औपचारिक तौर पर होता है (हालाँकि नवउदारवादी नीतियाँ छोटे और बिखरे रूपों में 1985-86 से ही जारी थीं)। इसके साथ ही हिन्दी सिनेमा का परिदृश्य भी कुछ ही वर्षों में तेज़ी से बदलता है। नये प्रकार के नायकों का उदय होता है, जैसे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, और अक्षय कुमार। 1980 के दशक में आये कुछ नायक भी अपने रंग-रूप को बदलकर मैदान में मौजूद रहते हैं, जैसे कि अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्राफ़ और सनी देओल। इस दौर की कुछ फ़िल्मों में तो अभी अस्सी के भ्रमित दशक की छाया नज़र आती है, लेकिन कुछ फ़िल्में कुछ प्रतीकात्मक चरित्र खड़े करती हैं, जो कि नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद समाज में निरंकुशता, असंवेदनशीलता, और फ़ासीवादी प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि नकारात्मक शेड वाले नायकों के चरित्र जिनका सबसे प्रातिनिधिक संस्करण हमें ‘डर’, ‘बाज़ीगर’, ‘अंजाम’, ‘फरेब’ आदि जैसी फ़िल्मों में देखने का मिलता है। साथ ही, इसी दौर में उच्च मध्यवर्ग के जीवन पर आधारित कुछ रोमाण्टिक फ़िल्में भी काफ़ी सफ़ल हुर्इं। यह उच्च मध्यवर्ग अक्सर अप्रवासी भारतीय होता था और विदेशों में रहने के बावजूद वह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर बिल्कुल रूढि़वादी और परम्परावादी होता था। यह दौर 1990 के दशक के अन्त तक जारी रहा, जिसके बाद हिन्दी सिनेमा में कुछ बुनियादी परिवर्तन होते हैं।
2000 के दशक का सिनेमा कर्इ नये प्रकार की फ़िल्मों को लेकर आता है। यह दौर भाजपा-नीत राजग सरकार का दौर था जबकि नवउदारवादी नीतियों के फलस्वरूप पैदा हुआ नवधनाढ्य वर्ग भारतीय सामाजिक ढाँचे में सुस्थापित हो चुका था। इस दौर में इस शहरी नवधनाढ्य वर्ग के जीवन की चिन्ताओं, आनन्दों और उसकी आशाओं-आकांक्षाओं पर आधारित कर्इ फ़िल्में आयीं। इनमें सबसे प्रातिनिधिक फ़िल्म थी ‘दिल चाहता है’। यह इस वर्ग के विजयवाद का दौर था। यह वर्ग खुश था, मगन था, जीवन का लुत्फ़ उठा रहा था। इसी दौर में राजनीतिक तौर पर भी ‘इण्डिया शाइनिंग’ और ‘भारत उदय’ के नारे उछाले गये थे और नवउदारवादी उन्मादी विजयवाद अपने चरम पर था। एक मायने में यह दौर अभी भी जारी है जिसके प्रतिबिम्बन के तौर पर ‘जि़न्दगी न मिलेगी दोबारा’, आदि जैसी फ़िल्मों को देखा जा सकता है। साथ ही, कुछ प्रयोगात्मक फ़िल्में भी बनीं जो कि पुरानी फ़िल्मों या क्लासिकीय रचनाओं का तथाकथित उत्तरआधुनिकतावादी या स्थानीयतावादी-उत्तरआधुनिकतावादी पाठ था, जैसे कि ‘देव डी’, ‘ओंकारा’, ‘मकबूल’, ‘इश्किया’ आदि जैसी फ़िल्में। इन फ़िल्मों के बारे में अलग से लिखा जाना चाहिए, लेकिन अभी इतना कहना पर्याप्त है कि ये फ़िल्में अपने विषयवस्तु और प्रस्तुति के ज़रिये पतनशीलता का आनन्द लेने का सांस्कृतिक प्रशिक्षण देती हैं। मिसाल के तौर पर, ‘गैंग्स आफ वासेपुर’ ऐसी ही एक ख़तरनाक फ़िल्म है। एक छद्म-यथार्थवादी प्रस्तुति के ज़रिये यह अपराध, हिंसा, पतन, अश्लीलता का एक ऐसा ‘सबआल्टर्न’ संस्करण पेश करती है जो कि वास्तव में अपराध, हिंसा, पतन और अश्लीलता का इस हद तक गुणगान और महिमा-मण्डन करती हैं कि दर्शक को आनन्दपूर्ण सनसनी का अनुभव होता है; परवर्ज़न का आनन्द कैसे उठाया जाय, यह सिखलाने में नये निर्देशकों की एक टोली एकदम महारत हासिल कर चुकी है, जिनमें तिगमांशु धूलिया, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी जैसे निर्देशक शामिल हैं। इन फ़िल्मकारों की शैली की अलग से आलोचना लिखी जानी चाहिए। साथ ही, 2000 के दशक में कुछ अन्य फ़िल्में भी बनीं जिन्होंने पूँजीवादी सामाजिक जीवन के अलग-अलग अन्धकारमय कोनों पर प्रकाश डाला और पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था की सड़ाँध को भी पेश किया लेकिन साथ ही उसे व्यवस्था की नैसर्गिक पैदावार बताने की बजाय व्यवस्था की विकृति या विचलन के तौर पर पेश किया जैसे कि ‘चाँदनी बार’, ‘पेज 3’ आदि जैसी फ़िल्में। इन फ़िल्मों में कोर्इ महानायक जैसा चरित्र नहीं होता था, बल्कि आम मध्यवर्गीय नायक या नायिका ही मुख्य चरित्र की भूमिका निभाते हैं और व्यवस्था के भीतर ही रहकर उसे दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन यह इस तरह की फ़िल्मों का रुझान दीर्घजीवी नहीं था और जल्द ही हिन्दी सिनेमा पर ‘एंग्री यंग मैन’ का नया संस्करण अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला था।
2006-7 से ‘गजनी’, ‘दबंग’, ‘सिंघम’ आदि जैसी ‘सुपरहीरो’ जैसे ‘एंग्री यंग मैन’ की फ़िल्में बनने लगीं। यह नया ‘एंग्री यंग मैन’ पुराने क्लासिकीय ‘एंग्री यंग मैन’ का दुहराव नहीं था। हम देख चुके हैं कि क्लासिकीय ‘एंग्री यंग मैन’ का उदय पूँजीवादी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के संकट के तौर पर पैदा हुआ था और वह जनता के बीच पल रहे गुस्से और असन्तोष के संचित हो रहे दबाव को मुक्त करने का काम करता था। यह बुर्जुआ कला की एक अहम भूमिका को अदा करता था: समस्याओं के कारणों और उसके समाधान के बारे में कोर्इ आलोचनात्मक दृष्टि दिये बग़ैर उनके समाधानों का एक सरलीकृत और ‘फ़ैण्टास्टिक’ संस्करण पेश करना, जिसमें कि एक बहादुर और ताक़तवर नायक सभी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देता है, दर्शक को अपने साथ एक किस्म की तदनुभूति महसूस कराता है और दर्शक के मसितष्क में ‘यथार्थ’ और ‘आदर्श’ के बीच के टकराव का एक काल्पनिक आनन्ददायी हल पेश कर उसके असन्तोष और गुस्से के दबाव को एक हद तक मुक्त करता है, और इस रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पूँजीपति वर्ग के ही वर्चस्व को पुनस्र्थापित करता है। इन फ़िल्मों में भ्रष्टाचार का चित्रण वास्तव में व्यवस्था की कलात्मक अधिरचना में पेश की जाने वाली व्यवस्था की एक ‘आत्मालोचना’ भी था, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार या अपराधीकरण व्यवस्था का नैसर्गिक गुण या बुनियादी समस्याओं का लक्षण नहीं था, बल्कि वह व्यवस्था का एक विचलन (aberration) था और इस रूप में यह भ्रष्टाचार या अपराधीकरण किसी और गम्भीर आधारभूत समस्या की अभिव्यक्ति नहीं था बल्कि, स्वयं ही समस्या था। और इस समस्या का समाधान क्या था? एक महानायक, एक विजिलाण्टे, एक ‘एंग्री यंग मैन’ जो कि एक व्यवस्थागत विसंगति (systemic anomaly) है; वह व्यवस्था का अभिन्न अंग है, लेकिन एक विसंगति भी है जो व्यवस्था के विचलनों को कानून और नियम के दायरे से उफपर उठकर दुरुस्त करता है।
‘एंग्री यंग मैन’ का नया संस्करण कर्इ मायनों में पुराने ‘एंग्री यंग मैन’ से भिन्न है। एक तो उसकी शक्ति अयथार्थवादी तरीके से बढ़ गयी है; दूसरी बात, उसका आदर्शवादी, न्यायप्रिय, संवेदनशील होना अब अनिवार्य नहीं है। वह भ्रष्टाचारी और अपराधी हो सकता है, और इस सूरत में उसने भ्रष्टाचार या अपराध के रास्ते को मजबूर होकर नहीं चुना है। यह उस व्यक्ति का तार्किक चयन है! मिसाल के तौर पर, ‘दबंग’ का चुलबुल पाण्डेय एक भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी है जो घूस लेता है, लूट का माल पकड़ने पर उसे खुद ही हड़प जाता है, किसी अगवा किये गये बच्चे को छुड़ाने पर फ़िरौती की रकम गड़प जाता है, और इसका कुछ हिस्सा वह ‘सामाजिक कल्याण’ पर ख़र्च करने के बाद, बाकी रकम का पूँजी संचय कर लेता है! यह ‘एंग्री यंग मैन’ संजीदा नहीं है, वह लुच्चा या लफंगा हो सकता है; वह लड़कियों पर सीटी मार सकता है, अश्लील गाने गा सकता है और अश्लील नृत्य कर सकता है! या फ़िर वह अर्द्ध पागल है या ‘शार्ट टर्म मेमोरी लॉस’ का शिकार है जो कि बदले को सबसे बर्बर रूप में अंजाम दे सकता है, डरावना हो सकता है, एक ऐसा उपकरण हो सकता है जो कि नियन्त्रित न किये जाने पर किसी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, जैसे कि ‘गजनी’ का नायक। और हाँ, यह ‘एंग्री यंग मैन’ ज़रूरत पड़ने पर तनाव से मुक्ति भी दे सकता है और कामेडी भी कर सकता है! चूँकि समस्या को पेश करने का पूरा अन्दाज़ ही ग़ैर-संजीदा और प्रहसनात्मक हो गया है इसलिए थोड़ी प्रहसनात्मकता इस ‘एंग्री यंग मैन’ के चरित्र में भी आ गयी है। लेकिन ‘एंग्री यंग मैन’ के इस नये उत्तर-क्लासिकीय संस्करण में जो फर्क आया है उसे किस तरह से व्याख्यायित किया जाय?
वास्तव में, 1970 के दशक के संकट और 2000 के दशक के संकट के चरित्र में ही फर्क। उस समय का सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संकट एक आदर्शवादी धोखाधड़ी (नेहरूवियार्इ समाजवाद) से पैदा हुए मोहभंग से जन्मा था। नेहरूवादी ‘समाजवादी’ पबिलक सेक्टर पूँजीवाद का संकट पहली बार अपने आपको पूरी सघनता के साथ अभिव्यक्त कर रहा था। आज़ादी के समय जनता को दिखलाये गये सपने चूर-चूर हो चुके थे और स्वातंत्र्योत्तर भारतीय पूँजीवादी व्यवस्था का असली चरित्र लोगों के सामने उजागर हो रहा था। यह मोहभंग जिस प्रकार के गुस्से और असन्तोष को जन्म दे रहा था उसे सहयोजित करने के लिए सांस्कृतिक जगत में जिस प्रकार के महानायक की ज़रूरत थी वह ‘एंग्री यंग मैन’ का अमिताभ बच्चन वाला क्लासिकीय संस्करण ही हो सकता था, जो कि आदर्शवादी, न्यायप्रिय, संजीदा, गुस्सैल, और संवेदनशील हो। आज का संकट भारतीय पूँजीवाद में नवउदारवाद और भूमण्डलीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद पैदा हुआ संकट है, जबकि एक नवधनाढ्य वर्ग अपनी पतनशीलता और अश्लीलता से पूरे समाज को हैरान कर रहा है, पूँजीवादी राजनीतिक वर्ग का भ्रष्टाचार और अपराधीकरण अभूतपूर्व रूप से प्रकट हो रहा है, धनबल और बाहुबल की राजनीतिक नग्नता के सभी रिकार्ड ध्वस्त कर रही है। यह मंजि़ल किसी आदर्शवादी यूटोपिया से होने वाले ताज़ा मोहभंग की मंज़िल नहीं है। असल में, 1970 के दशक से 1990 के दशक के बीच भारतीय पूँजीपति वर्ग जनता का तमाम मुददों पर इस कदर विसंवेदीकरण कर चुका है, कि अब उस किस्म का मोहभंग होना सम्भव ही नहीं है क्योंकि वैसा कोर्इ मोह बचा ही नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया कि पुराना ‘एंग्री यंग मैन’ व्यवस्था के विचलन, यानी कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, को प्रतिसन्तुलित करने या उसका समाधान करने के लिए खड़ी एक व्यवस्थागत विसंगति था; लेकिन आज का ‘एंग्री यंग मैन’ इस विचलन का ही अंग बन गया है! व्यवस्था के ‘विचलन’ का द्वन्द्वात्मक अन्य (dialectical other) समाप्त हो गया है और इस रूप में विचलन अब विचलन रहा ही नहीं! व्यवस्था अब यह बोलने की बेशर्मी नहीं कर पा रही है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण उसका विचलन है; उल्टे उसने इस विचलन का ही नैसर्गिकीकरण कर दिया है! अब आपसे जिस चीज़ की उम्मीद करने की उम्मीद की जा रही है, वह है एक ऐसे ‘एंग्री यंग मैन’ की उम्मीद करना जो हो सकता है कि स्वयं थोड़ा भ्रष्ट हो लेकिन वह कानूनेतर तरीके से वह थोड़ा न्याय बाँट देता है, थोड़ा सम्पत्ति और समृद्धि का पुनर्वितरण कर देता है, थोड़ा मनोरंजन भी कर देता है और वह न तो ज़्यादा ‘टेंशन’ लेता है और न ही ज़्यादा ‘टेंशन’ देता है और उसका हमें भी यही सन्देश है कि ‘ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो यार?’ और इन सबके बदले में अगर वह अपना लाभांश ले लेता है, तो इसमें क्या बुरा है? आज का ‘एंग्री यंग मैन’ इस रूप में व्यवस्था के उन गुणों को स्वीकार्य बनाना है और उनके प्रति हमारा विसंवेदीकरण करता है, जो इस कदर अनावृत्त हो चुके हैं, कि उन्हें छिपाने का कोर्इ भी प्रयास असफ़ल ही होगा। इसलिए बेहतर है कि उन्हें स्वीकार्य बना दिया जाय। लेकिन साथ ही, ‘एंग्री यंग मैन’ अपने पुराने प्रकार्य को भी पूरा करता है: यानी, बिना कोर्इ समाधान पेश किये इस रूप में एक ‘फ़ैण्टास्टिक समाधान पेश करना जो कि गुस्से और असन्तोष के प्रेशर को ‘रिलीज़ करे। बस फ़र्क यह है कि अब यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक अश्लीलता की सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी है और हर प्रकार के आदर्शवाद, न्यायप्रियता, संवेदनशीलता के झीने पर्दे को फ़ाड़कर फेंक चुकी है, क्योंकि आज का पूँजीवादी राजनीतिक-सामाजिक यथार्थ भी यही है। अब ‘एंग्री यंग मैन’ सांस्कृतिक तौर पर लघुजीवी राहत पहुँचाने का कार्य करता है; आप अपना दिमाग़ घर पर रखकर जाइये और सिनेमा हाल में समस्याओं के समाधान की फन्तासी का आनन्द लीजिये! जैसे कि आपको पता है कि अन्त निकट है, मर्ज असमाधेय है, तो कुछ दर्द-निवारक उपाय (palliative measures) अपना लिये जायें! आप सोच क्यों रहे हैं? ज़्यादा सोचिये मत! आनन्द लीजिये! इसीलिए इन फ़िल्मों की पूरी संरचना, शैली, पटकथा, अभिनय और निर्देशन के बारे में कोर्इ ‘अन्दर से’ पेश की जाने वाली आलोचना नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि उनमें आलोचना करने के लिए कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद कम ही है; लेकिन ऐसी फ़िल्मों की एक ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आलोचना पेश की जा सकती है और की जानी चाहिए।
‘एंग्री यंग मैन’ के पुराने संस्करण से नये संस्करण में आये पतन को तभी समझा जा सकता है जब इसे पूँजीवादी समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था की पतनशीलता के प्रतिबिम्बन के रूप में देखा जाये। भारतीय सिनेमा में प्रकट हुआ नया ‘एंग्री यंग मैन’ पतनशील, मरणोन्मुख और अश्लील पूँजीवाद के अन्तकारी संकट की पैदावार है; यह अपने पर हँस रहा है और हमें भी हँसने को कह रहा है। यह अपने पूरे वजूद के पीछे खड़े संकट के प्रति सचेत है और अपने पूरे वजूद के अवास्तविक होने का पहचानता है।
(अगले अंक में हालीवुड में सुपरहीरो फ़िल्मों के बारे में)
- नान्दीपाठ-2, जुलाई-सितम्बर 2013