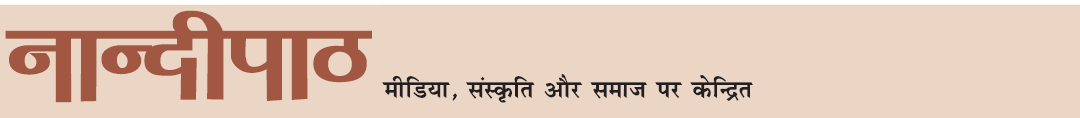क्या हमारे देश के जनपक्षधर संस्कृतिकर्मी आसन्न युद्ध के लिए तैयार हैं?
नान्दीपाठ के तीसरे अंक को एक बार फिर काफ़ी देरी के साथ लेकर प्रस्तुत होने के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। इसके लिए कोई बहाना नहीं बनायेंगे। सिर्फ़ माफ़ी माँगेंगे। पत्रिका के पहले दो अंकों पर जितनी प्रेरणादायी प्रतिक्रिया देश भर से प्राप्त हुई है, उसके मद्देनज़र हम आगे से इसे नियमित करने का पूरा प्रयास करेंगे।
आज पूरे देश में संस्कृति और मीडिया का क्षेत्र एक सघन वर्ग संघर्ष का केन्द्र बन रहा है। मौजूदा फासीवादी उभार किसी भी अन्य फासीवादी आन्दोलन के समान राजनीति के संस्कृतिकरण पर आधारित है। यही कारण है कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थाएँ और मीडिया सबसे पहले फासीवादी विकृतिकरण और ‘टेक ओवर’ का निशाना बन रहे हैं। फासीवादी राजनीति वॉल्टर बेंजामिन के शब्दों में राजनीति का सौन्दर्यीकरण करती है और कम्युनिज़्म सौन्दर्य(शास्त्र) का राजनीतिकीकरण करके फासीवाद को जवाब देता है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीति के सौन्दर्यीकरण की सबसे अहम ज़मीन अक्सर संस्कृति का क्षेत्र बनता है। सांस्कृतिक माध्यमों के ज़रिये ही फासीवादी ताक़तें मिथकों को सामान्य बोध के तौर पर स्थापित करती हैं; एक कल्पित अतीत के गौरव को एक कल्पित समुदाय के लिए ‘फ़ेटिश’ में तब्दील करती हैं; सांस्कृतिक माध्यमों के ज़रिये ही फासीवादी शक्तियाँ अपने राजनीतिक विरोध को अविश्वसनीय बनाती हैं; इन्हीं के ज़रिये फासीवादी शक्तियाँ टुटपुँजिया (पेटी-बुर्जुआ) वर्गों के रूमानी उभार को खड़ा करती हैं। ऐसे में, देश के जनपक्षधर संस्कृतिकर्मियों को आज और अभी यह निर्णय लेना होगा कि वे कहाँ खड़े हैं? क्या वे युद्धस्तर पर जनता के बीच उतर कर ‘संस्कृति के राजनीतिकरण’ के लिए तैयार हैं? यह आज प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन के लिए ही नहीं बल्कि समूचे प्रगतिशील आन्दोलन के लिए ही एक अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हम आज ही इसका जवाब देने के लिए अपने आपको प्रस्तुत नहीं करते तो शायद कल जवाब देने की स्थिति ही न रह जाये।
कई वामपंथी टीकाकारों, चिन्तकों और बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि देश में जो बुर्जुआ-जनवादी संवैधानिक ढाँचा है, देश के सामाजिक ढाँचे की जो विशिष्टताएँ हैं (बहुल पहचानों की मौजूदगी) और मोदी सरकार के सांस्कृतिक व विचारधारात्मक हमलों का जो अतार्किक चरित्र है, जिसे जनता समझ ही जायेगी (!), वह जर्मनी या इटली जैसे फासीवादी उभार को असम्भाव्य बनाता है। पहली बात तो यह है कि वैसे फासीवादी उभार की आज कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास अपने आपको हूबहू दुहराता नहीं है। प्रतिक्रियावादी विचारधाराएँ और आन्दोलन भी अपने अतीत से सीखते हैं। यह सोचना कि जब तक जर्मनी की तरह कोई ‘फ्यूहरर कल्ट’ या इटली की तरह ‘ड्यूस कल्ट’ नहीं पैदा होगा, जब तक नंगे तौर पर नस्ली या जातीय सफ़ाये की बात नहीं की जायेगी, जब तक ऑशवित्स जैसी परिघटनाएँ सामने नहीं आयेंगी तब तक फासीवाद का उभार सम्भव नहीं है, एक अनैतिहासिक दृष्टिकोण से पैदा हुई नादानी होगी। 1920 के दशक और आज के दौर में पूँजीवाद के संकट और फासीवादी उभार दोनों में ही कुछ बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। 1920 के दशक के समान अब कोई संकट और तेज़ी के दौरों के बारी-बारी से आने की प्रक्रिया नहीं चलेगी; लिहाज़ा, अब संकट में अचानकपन और आकस्मिकता का तत्व भी नहीं होगा। संकट आज पूँजीवादी विश्व व्यवस्था की एक स्थायी परिघटना है। यह पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे गहरा संरचनागत संकट है। यह कभी मन्द मन्दी के रूप में मौजूद रहता है तो कभी गहरे संकट का स्वरूप ले लेता है। लेकिन तेज़ी जैसा कोई दौर 1970 के दशक की शुरुआत से ही विश्व पूँजीवाद ने नहीं देखा है। जिस प्रकार संकट अब एक आकस्मिक घटना के रूप में प्रकट नहीं हो रहा है, उसी प्रकार फासीवाद भी अब एक आकस्मिक घटना (रोम पर चढ़ाई या हिटलर के अपवादस्वरूप कानून) के रूप में नहीं घटित होगा। फासीवाद उत्तरकालीन पूँजीवाद (late capilalism) के दौर में पूँजीवादी समाज की एक स्थायी परिघटना के रूप में मौजूद है। यह कभी सत्ता में आ सकता है, तो सत्ता में नहीं भी आ सकता है। दोनों ही सूरतों में यह क्रान्तिकारी आन्दोलन के एक प्रति-भार के रूप में बुर्जुआ वर्ग के हितों की सेवा के लिए एक टुटपुँजिया रूमानी उभार खड़ा करता है। आज फासीवाद इसी रूप में दुनिया के तमाम देशों में मौजूद है। चाहे वह भारत में संघ परिवार हो या यूनान में गोल्डेन डॉन, अलग-अलग ऐतिहासिक सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए भी उनकी इस साझा विशिष्टता को देखने से चूकना राजनीतिक अन्धापन होगा। फासीवादी उभार के चरित्र में आने वाले इस परिवर्तन के मद्देनज़र फासीवाद-विरोधी रणनीति में बदलाव के बारे में सोचने का वक़्त आज ही है।
दूसरी बात यह कि जिन्हें यह लगता था कि भारत का उदार जनवादी बुर्जुआ संविधान और राज्य फासीवादियों को ‘बर्बर से सभ्य बना देगा’ वे सभी लोग अपनी बगलें झाँक रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में एफटीआईआई, जेएनयू, एचसीयू, आईसीएचआर, आईसीसीआर, आईसीएसएसआर आदि में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, उसके लिए उसे संविधान में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। 2019 में अपनी आसन्न चुनावी हार को देखकर फासीवादी गिरोह कौन से अपवादस्वरूप कदम उठायेगा इसके बारे में भी दावे से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि ‘सत्ता में निश्चिन्तता से विद्यमान फासीवाद’ के मुकाबले ‘सत्ता खो देने की असुरक्षा से बौराया हुआ फासीवाद’ जनता के लिए तात्कालिक तौर पर कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ऐसे में, अभी पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद और विशेष तौर पर 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले मोदी सरकार और संघ परिवार जनता के दमन, प्रतिक्रियावादी आन्दोलनों को हवा देने, दंगे करवाने और प्रतिगामी टुटपुँजिया रूमानी उभार को बढ़ाने के लिए किन हदों तक जायेंगे, इसके बारे में कुछ अनुमान ही लगाये जा सकते हैं। यह सोचना भी भयंकर नादानी है कि इतनी सारी जातियों, राष्ट्रीयताओं से भरे देश में फासीवादी उभार सम्भव नहीं है क्योंकि वह देशव्यापी नहीं हो पायेगा। ऐसे लोगों ने इटली और जर्मनी में फासीवादी उभार के विषय में ठीक से जानकारी हासिल नहीं की है। ग़ौरतलब है कि फासीवादी उभार को देश में सत्तासीन होने के लिए पूरे देश में समान सघनता और व्यापकता के साथ उभरना ज़रूरी नहीं है। ऐसा न तो अतीत में हुआ था और न ही आज हो रहा है। निश्चित तौर पर, भारतीय स्थिति भिन्न है ठीक वैसे ही जैसे कि जर्मनी और इटली की स्थितियाँ भी भिन्न थीं। यह भी सच है कि वह समय अलग था और आज का समय अलग है, लेकिन इस परिवर्तन के कारण फासीवादी उभार में क्या बदलाव आये हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं।
आज इस नये फासीवादी उभार का मुकाबला करने के लिए जनता के बीच, नागरिक समाज के भीतर क्रान्तिकारी ताक़तों को अपनी खन्दकें खोदनी होंगी। और इस कार्य में क्रान्तिकारी संस्कृति की एक महती भूमिका है। हिटलर और मुसोलिनी के उभार की व्याख्या करते हुए तमाम समकालीन कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसे ‘हिटलर साइकोसिस’ और ‘ऑब्फ़स्केशन ऑफ कॉन्शसनेस’ आदि की संज्ञाएँ दी थीं। ये कितनी ग़लत थीं, इसे इतिहास साबित कर चुका है। एक फासीवादी नेता ने एक बार कहा था, “हमारा आन्दोलन एक तात्विक आन्दोलन है। चूँकि यह तर्कों से खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए इसे तर्कों से नहीं हराया जा सकता है।” समकालीन कम्युनिस्ट विमर्श में यह प्रश्न ही पूरी महत्ता के साथ नहीं उठाया गया कि जनसमुदायों की और विशेष तौर पर टुटपुँजिया जनसमुदायों की चेतना में ऐसा क्या है जिससे कि वह अपने आर्थिक और भौतिक हितों के विरुद्ध अपने ‘साइकोसिस’ की इजाज़त देता है? किस रूप में टुटपुँजिया वर्गों में अपनी वर्ग अवस्थिति के कारण स्वयं प्रतिक्रियावादी सम्भावना होती है, चाहे वह सुषुप्त ही क्यों न हो? किस प्रकार यह प्रतिक्रियावादी सम्भावना बुर्जुआ परिवार, बुर्जुआ पितृसत्ता, बुर्जुआ यौनिकता (या उसके दमन), बुर्जुआ नैतिकता, बुर्जुआ राष्ट्रवाद और बुर्जुआ धर्म की रहस्यवादी (mystical) मनोवैज्ञानिक संरचनाओं में घुलमिलकर परिघटनात्मक रूप से प्रकट होती है? क्यों केवल आर्थिक प्रचार ही फासीवादी प्रचार को निरस्त और निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्यों राष्ट्रवाद की रहस्यवादी अपीलें (‘भारत माता की जय’) टुटपुँजिया वर्ग के बीच आर्थिक प्रचार के मुकाबले कहीं ज़्यादा अनुगूँज पाती हैं? इसके कारणों की पड़ताल की जाये तो हम पाते हैं कि आर्थिक और भौतिक परिस्थितियाँ जिस रूप में अपने आपको सामाजिक चेतना में अभिव्यक्त करती हैं वह बेहद जटिल होता है; किस तरीके से इनके बीच का सम्बन्ध समानुपातिक नहीं होता; विशेष तौर पर, मध्यवर्ती वर्गों में किस प्रकार आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों का चेतना में प्रतिबिम्बन उल्टा (inverted) या किसी अन्य प्रकार से विकृत रूप में होता है; बुर्जुआ उत्पादन सम्बन्धों की ही एक तात्विक इकाई परिवार की इसमें क्या भूमिका होती है; पितृसत्ता बुर्जुआ उत्पादन सम्बन्धों और वर्ग समाज के एक अहम विचारधारात्मक रूप के तौर पर इसमें क्या भूमिका निभाती है; साथ ही, आरोपित और खोखली बुर्जुआ नैतिकता और आचार की इसमें क्या भूमिका होती है; किस प्रकार ये विचारधारात्मक व सांस्कृतिक कारक एक ऐसे अधीनस्थ वर्ग को पैदा करते हैं जो कि फासीवादी प्रचार के सामने राजनीतिक तौर पर अरक्षित होता है। इन सारी प्रवृत्तियों को हम बस टुटपुँजिया वर्गों का पिछड़ापन कहकर ख़ारिज करेंगे, तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसे समझे बग़ैर हम फासीवादी प्रचार का जवाब देने में कहीं न कहीं असमर्थ होंगे। 1950 के दशक से विशेष तौर पर जर्मनी में शुरू हुए मार्क्सवादी-लेनिनवादी शोध ने फासीवादी उभार के तमाम पहलुओं को परखा और उनका विश्लेषण पेश किया। उस विश्लेषण को समझने की आज शिद्दत से ज़रूरत है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि उससे आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है।
अब अगर हम इन तमाम कारकों को समझकर आज फासीवाद-विरोधी प्रचार की रणनीति तैयार करें तो हमें यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि इसमें संस्कृति और वैकल्पिक मीडिया की क्या भूमिका होगी। आज फासीवाद-विरोधी प्रचार को प्रमुख तौर पर सांस्कृतिक माध्यमों और वैकल्पिक मीडिया पर निर्भर करना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कार्य करने के लिए हज़ारों प्रतिबद्ध प्रगतिशील संस्कृतिकर्मियों की आवश्यकता होगी जो कि युद्धस्तर पर और ज़मीनी तौर पर जनता के बीच फासीवादी राजनीति, संस्कृति, मूल्यों और विचारधारा को नंगा करते हुए उसे निष्प्रभावी बना सकें। यह क्रान्तिकारी आन्दोलन फासीवाद को वहाँ चोट पहुँचा सकता है, जहाँ इसे सबसे ज़्यादा तक़लीफ़ होती है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, देशभक्ति पर इनके दावों को पूरी तरह से ख़ारिज किया जा सकता है। जनता के बीच जनता की भाषा और जनता के सांस्कृतिक माध्यमों के ज़रिये इनकी पूरी जन्मकुण्डली को खोलना और इनके रहस्यवाद की सच्चाई को उजागर करना आज की बुनियादी ज़रूरत है। इस काम को अगर प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन अभी हाथ में नहीं लेता, अगर अभी वह वामपंथी एक्टिविज़्म की टापूनुमा पहाड़ियों से बाहर नहीं निकलता तो कल बहुत देर हो जायेगी। एक भयंकर युद्ध राजनीतिक तौर पर देश में आसन्न है। एक भयंकर युद्ध संस्कृति की रणभूमि में भी लड़ा जाने वाला है। सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे देश के जनपक्षधर प्रगतिशील संस्कृतिकर्मी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं तो भी हम हार सकते हैं और ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन तब हम जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर हम यह चुनौती स्वीकार नहीं करते और किसी किस्म की खुशफहमी पालकर घर बैठे रहते हैं, तो हम पहले ही हार चुके हैं और यह सिर्फ़ वक़्त की बात है कि हम कब ख़त्म हो जायेंगे।
(15 अप्रैल )
- नान्दीपाठ-3, अप्रैल-जून 2016