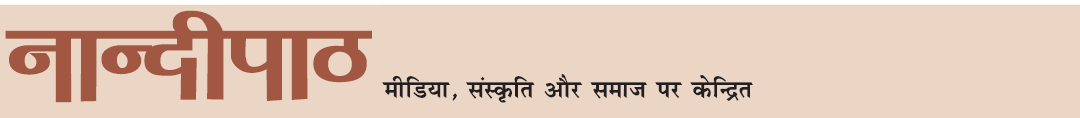सौन्दर्यीकरण के बारे में कुछ नोट्स
सत्यव्रत
- चीज़ों को इतना अधिक सुन्दर बनाने की, सजाने–सँवारने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि वे निर्जीव और पहुँच से बाहर प्रतीत हों।
- निष्कलुषता एक मिथक है। यह मानवेतर ही नहीं, मानवद्रोही भी होती है। यह इहलोकवाद की विरोधी है। क्रान्तियों के महान नेता त्रुटिरहित नहीं थे और महानतम क्रान्तियाँ भी निष्कलुष नहीं थीं। क्रान्तियों का आदर्शीकरण या सौन्दर्यीकरण उन्हें अलौकिक बना देता है और लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्रान्तियाँ मानवीय क्षमता से परे की चीज़ हैं।
- महान क्रान्तिकारी घटनाओं को साहित्य–सृजन का विषय बनाना बेहद जोखिम भरा काम है। हिंसा, रक्तपात, आँसू, विश्वासघातों, गलतियों, मानवीय कमज़ोरियों में लिथड़ी महान मौलिकताएँ धुल–पुँछकर रूमानी और स्वप्निल बन जा सकती हैं। कला में क्रान्ति का ऐन्द्रजालिक मिथ्याभास नहीं रचा जाना चाहिए।
- यूँ भी, कविता या उपन्यास पढ़कर कोई क्रान्तिकारी नहीं बन जाता। वहाँ से मिलता है दुनियादारी की काई छाँटता हुआ भावनात्मक आवेग का एक स्फुरण, और फिर, घटनाओं के तर्क से नि:सृत आलोचनात्मक विवेक, इतिहास–बोध और जीवन–दृष्टि। कलाकृति को चाहिए कि वह हमें जीवन और क्रान्ति के यथार्थ–सौन्दर्य से परिचित कराए और बीहड़ता–विकटता– कुरूपता से भी।
- बारीक़ तराश और महीन कताई-मुर्दाबाद!
- याद नहीं आ रहा, ब्रेष्ट या वाल्टर बेंजामिन ने कहीं इंगित किया है : ‘राजनीति का सौन्दर्यीकरण एक फ़ासीवादी उपक्रम है।’ संस्कृति के सौन्दर्यीकरण की राजनीति भी उतनी ही जनविरोधी होती है जितनी राजनीति के सौन्दर्यीकरण की संस्कृति।
- वह जो हमेशा उड़ने के बारे में सोचा करता था, उसे विश्वास हो चला था कि उसकी आँखों का रंग गहरा नीला है सागर की तरह, या हल्का नीला, आकाश की तरह। लेकिन उसकी फटी–फटी आँखों में एक क़िस्म का धूसर भूरापन था-उन्माद या पागलपन का संकेत देता हुआ।
- वह एक दिन फुदकता हुआ मर जाएगा। मगर सलीके और तहज़ीब के साथ फुदकता हुआ।
- अभिव्यक्ति की शैली के प्रश्न को पूरी तरह से स्वत:स्फूर्तता या नैसर्गिकता के हवाले तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बुनियादी सच्चाई की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हर विषय–वस्तु का अपना रूप होता है जो उसके जन्म के साथ स्वत: प्रकट होता है। कथ्य या विषयवस्तु की बात पहले आती है, उसकी अभिव्यक्ति को माँजने–तराशने, प्रभावी और उन्नत बनाने का काम बाद में शुरू होता है।
- अमौलिक, नक़लची, खोखले व्यक्तित्व प्राय: रूपवादी होते हैं-साहित्य में भी और राजनीति में भी। उनके पास कोई सार्थक उद्देश्य और कथ्य हो तो भी, आदतन, उनका ध्यान पहले इस बात पर जाता है कि वे अपनी बात कितने सुन्दर और प्रभावशाली ढंग से रख रहे हैं। इस उपक्रम में उनका ध्यान लगातार सुन्दर आकर्षक जुमले और ‘स्टाइल’ उधार लेने और गढ़ने में लगा रहता है और वे अपनी रही–सही मौलिकता और प्रयोग की शक्ति भी खो बैठते हैं। खोखला, आडम्बरपूर्ण, अति आलंकारिक, कृत्रिम, अमौलिक व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति उन्हें जनविमुख, नाकारा, निरंकुशता की हद तक व्यक्तिवादी तथा अति आत्मसजग बना देती है। अपनी कमज़ोरियों को ढँकने, आत्मरक्षा के तर्क गढ़ने और भाव–ताव बनाए रखने में उनकी नब्बे प्रतिशत ऊर्जा ख़र्च हो जाती है। वे चौकन्ने, आत्मविश्वासहीन और कायर होते हैं। वे व्यक्तिवादी और “विनम्र” नौकरशाह होते हैं। पर जैसे ही आप उन्हेें कोंचेंगे, वे अपनी विनम्रता तत्क्षण त्यागकर फन काढ़ लेंगे या फिर बालू की भीत की तरह भरभरा जाएँगे। अत: माँजने–तराशने, सुन्दर बनाने के अतिरिक्त आग्रह के पीछे की मानसिकता की भी पड़ताल की जानी चाहिए।
- रचनाकार हो या राजनीतिक कर्मी, सौन्दर्यीकरण के अतिरिक्त आग्रह के पीछे साम्प्रतिक सामाजिक परिवेश में प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य तो काम करते ही हैं, इसमें व्यक्ति–विशेष के व्यक्तिगत इतिहास की भी विशिष्ट भूमिका होती है। बचपन और किशोरावस्था में मित्रों की टोली में नायक–नेता बनने के लिए, माँ–बाप की नज़रों में “अच्छे बालक़ की छवि बनाने या बनाए रखने के लिए या फिर अपने किसी हीनता–बोध के सहज प्रतिकार के लिए हम अपना एक कृत्रिम व्यक्तित्व माँजते–तराशते हैं और फिर नक़ली भाव–मुद्राओं का वही नाट्य–परिधान पहने जीवन–पर्यन्त नाटक करते रह जाते हैं। यह पूरा बौद्धिक–सामाजिक जीवन ही एक मण्डी है जिसमें ऊपरी चमक–दमक, भाव–ताव का ऊँचा बाज़ार–मूल्य है, चाहे उसका उपयोग–मूल्य कुछ भी न हो। यह परिवेश हमारी मानसिकता को भी अनुकूलित करता जाता है और सौन्दर्यीकरण का दुराग्रह हमारी सबसे स्वाभाविक आदत बन जाता है।
- सामूहिक उत्पादक कार्रवाइयों में भागीदारी, उत्पादन–सक्रिय जनता के जीवन और संघर्षों से पूरी तरह जुड़ जाना और सहयात्रियों के समूह के साथ स्वयं को अविभाज्य बना देना ही सौन्दर्यीकरण–कुचक्र के शिकार व्यक्तित्वों को ‘एलियनेशन’ और आत्मनिर्वासन से मुक्त कर सकता है।
- उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, जब पूरा यूरोप विशेषकर फ्रांस, क्रान्तिकारी उथल–पुथल से गुज़र रहा था, तो मार्क्स उद्विग्न होकर सोच रहे थे कि जितनी जल्दी “सुन्दर” क्रान्तियों का स्थान “कुरूप” क्रान्तियाँ ले लें, उतना ही अच्छा! “सुन्दर” क्रान्ति और “कुरूप” क्रान्ति से उनका तात्पर्य क्रमश: बुर्जुआ क्रान्ति और सर्वहारा क्रान्ति से था। बुर्जुआ समाज की वर्चस्वकारी सोच के हिसाब से जो “कुरूप” है, वही भविष्य में सुन्दर कहलाएगा, वही “कुरूपता” मेहनतकशों के लिए उन्मोचक है, अत: वह उनके लिए सुन्दर है। इस “कुरूपता” के सौन्दर्यशास्त्र को समझना होगा।
- चीज़ों को निर्जीवता और अलौकिकता की हद तक सुन्दर बनाने की कोशिश “कुरूप” क्रान्ति के विरुद्ध एक उपक्रम है।
- अपने व्यक्तित्व को भी सुन्दर बनाने का अतिरिक्त आग्रह एक आत्मरति है, जो इन्सान को चीज़ बना देता है। या फिर केंचुआ। या शायद, गम्भीरता–सुन्दरता का स्वाँग रचने वाला एक विदूषक।
टिप्पणी : Aesthetisation के लिए कुछ और न सूझने पर मैंने सौन्दर्यीकरण शब्द का इस्तेमाल किया है।
- सृजन परिप्रेक्ष्य, जनवरी-अप्रैल 2002