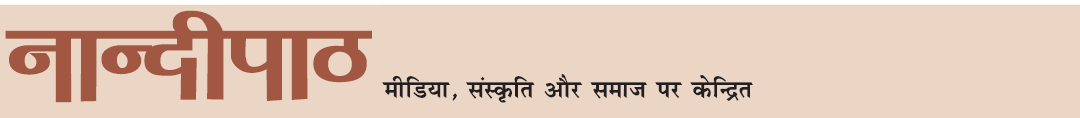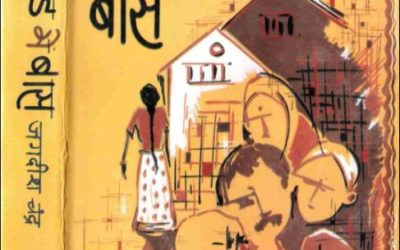साहित्य में अवसरवादी घटाटोप के सामाजिक-आर्थिक कारण
कविता कृष्णपल्लवी
कथित वामपंथी धारा के साहित्यिक परिदृश्य पर अवसरवाद का अद्भुत बेशर्म घटाटोप छाया हुआ है। कुछ दशकों पहले कुछ थोड़े लोग हुआ करते थे जो रात के अँधेरे में छुपकर सत्ता संग सेज सजाते थे और भाण्डा फूट जाने पर दिन के उजाले में कुछ दिनों तक शर्माये-शर्माये घूमते थे। अब माहौल बदल चुका है। डोमाजी उस्ताद के जुलूस में साहित्यिक-बौद्धिक जन पहले रात के अँधेरे में शामिल होते थे। अब ऐसे जुलूस दिन-दहाड़े निकलते हैं। सत्ता और पूँजी के संस्कृति प्रतिष्ठानों के साथ दिन-दहाड़े सौदेबाजियाँ होती हैं। चतुर्दिक पद-पीठ-पुरस्कार की आपाधापी मची रहती है। “वैचारिक-लोकतंत्र” के तर्क को इतना लचीला बना दिया गया है कि बच्चों और मानवता के भविष्य और युद्धों की विभीषिका को लेकर कविता में चिन्तातुर मुद्रा अपनाने वाले लोग हिन्दुत्ववादी फासिस्टों की सरकार के आयोजन में बेशर्मी के साथ शिरकत करते हैं और गिरोहबन्द होकर अपना बचाव करते हैं। हम्माम में नंगों की संख्या इतनी अधिक है कि शर्माने के बजाय एकजुट होकर वे कपड़े पहने लोगों पर हल्ला बोलने लगे हैं। अब कम ही लोग हैं जो खुले गले से मुक्तिबोध की तरह यह प्रश्न पूछते हों- “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?”
अवसरवाद की ढलान पर जारी इस यात्रा में रायपुर में रमनसिंह सरकार के साहित्यिक महोत्सव में कई जाने-माने प्रगतिशील-सेक्युलर- वामपंथी साहित्यकारों की भागीदारी की घटना एक नया मील का पत्थर है। रमन सिंह उसी राजनीति के एक प्रमुख सिपहसालार हैं जिसने आडवाणी की रथयात्रा के बाद लगातार पूरे देश में कई भीषण रक्तपातपूर्ण दंगों के कुचक्र रचे। इसी राजनीति के वाहक गुजरात-2002 के अमानुषिक रक्तपात के सूत्रधार थे। यही सरकार है जो माओवाद के खात्मे के नाम पर बस्तर के सैकड़ों गाँवों के हज़ारों आदिवासी परिवारों को उजाड़ चुकी है और लगातार वहाँ बर्बर अत्याचारों के नये-नये कीर्तिमान रच रही है। उसी सरकार को लोकतांत्रिक और सहिष्णु सिद्ध करते हुए उसके आयोजन में वामपंथ को रोज़ पानी पी-पीकर गाली देने वाले अशोक वाजपेयी और उन जैसों के साथ प्रगतिशीलता की दुशाला ओढ़े रहने वाले जगदीश्वर चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, नरेश सक्सेना, आदिवासियों दलितों के स्वयम्भू साहित्य मसीहा रमणिका गुप्ता, प्रभात रंजन और हाल ही में साहित्याकाश पर खद्योत सम भुकभुकाने वाले दर्जनों गलीज किस्म के नौबढ़ “युवा तुर्क” शोभायमान हुए।
एक जमाना था जब फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा वित्तपोषित भारत भवन में अर्जुन सिंह के प्रिय नौकरशाह साहित्यकार अशोक वाजपेयी एक कुशल बहेलिये की तरह कई वामपंथी साहित्यकारों को तरह-तरह के लालच देकर फँसाने में कामयाब हुए थे। उस समय भी भारत भवन कुचक्र के आलोचकों की संख्या अच्छी-ख़ासी हुआ करती थी। बाद में भारत भवन लाभान्वितों में से बहुतेरे शर्मिन्दा भी हुए, अलगाव के शिकार भी हुए, कुछ ने पश्चाताप भी किया और कुछ ने पाप-प्रक्षालन के कुछ उपक्रम भी किये। अब देश में केन्द्र और राज्य सरकारों के संस्कृति प्रतिष्ठानों और अकादमियों के रूप में कई “भारत भवन” हैं, पूँजीपति घरानों के कई-कई पुरस्कार और सम्मान हैं, एन-जी-ओ- वाले भी साहित्यकारों को भाव दे रहे हैं, विश्वविद्यालयों में उनके लिए नये-नये विशेष पद और पीठ सृजित हो रहे हैं। जिस समय समाज में जनवादी स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा क्षरित और संकुचित होता जा रहा है, उसी समय सत्ता साहित्यकारों-बुद्धिजीवियों-कलाकारों को पूर्वापेक्षा ज़्यादा भाव दे रही है क्योंकि उसे पता है कि विचारों के धरातल पर “सहमति का निर्माण” करने में और व्यवस्था की चौहद्दी के भीतर “असहमति” का लोकतांत्रिक छद्म रचने में व्यवस्था द्वारा सहयोजित प्रगतिशील मुखौटे वाले बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है।
पूँजीवादी सत्ता की नीतियों में आये परिवर्तन से भी अधिक उन सामाजिक-आर्थिक कारणों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जिनके कारण बुद्धिजीवियों का बड़ा हिस्सा आज आसानी से व्यवस्था द्वारा खरीद-फरोख्त, सौदेबाज़ी और सहयोजन का सहर्ष शिकार होने लगा है। यह अनायास नहीं है कि 1990 के दशक में नवउदारवाद की चौतरफा लहर के बाद यह परिघटना ज़्यादा बड़े पैमाने पर, एक आम प्रवृत्ति बनकर उभरी है। नब्बे के दशक की शुरुआत में कवि केदारनाथ सिंह ने तमाम वामपंथी साहित्यकारों और ज.ने.वि. के छात्रों के विरोध के बावजूद उन पूँजीपतियों के प्रतिष्ठान से सम्मान ग्रहण किया, जिन पर शहीद शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड्यंत्र रचने का अभियोग था। फिर जल्दी ही सबकुछ भुला दिया गया और केदारनाथ सिंह वाम दायरे में भी समादरणीय माने जाते रहे। फिर तो जैसे शर्मों-हया के सारे परदे ही हटते चले गये। फासिस्ट योगी आदित्यनाथ से सम्मान ग्रहण करने वाले उदय प्रकाश, पहले भाजपाई मुख्यमंत्री नित्यानन्द स्वामी को अपना पिता बताने वाले और फिर उत्तराखण्ड की कांग्रेसी सरकार की हिमालय में बाँध-निर्माण की विनाशकारी नीति की वकालत करने वाले लीलाधर जगूड़ी, आर-एस-एस- के राममाधव से लेकर बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव तक के पुस्तकों का विमोचन करने वाले और छत्तीसगढ़ के हत्यारे डी.जी.पी. विश्वरंजन को महत्वपूर्ण कवि घोषित करने वाले, राजकमल प्रकाशन के मालिकों के घर के “रामू काका” (विष्णु खरे के शब्दों में) नामवर सिंह, स्त्रियों के प्रति अपने मर्दवादी उद्गारों और लम्पट व्यवहार के लिए कुख्यात और म.गा.हि.वि.वि. में दारोगा की तरह कुलपतिगीरी कर चुके विभूति नारायण राय, उनके हमप्याला-हमनिवाला पुराने अवसरवादी रवीन्द्र कालिया, राय साहब के जमाने में म.गा.हि.वि.वि. में कोई पद या शोधवृत्ति लेकर मस्ती काटने वाले दर्जनों लेखक-कविगण, हत्यारे विश्वरंजन के साहित्यिक आयोजन की शोभा बढ़ाने और विभूति नारायण राय से उपकृत होने के बाद पटना जाकर नीतीश सरकार के सरकारी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से नवाजे जाने वाले किसी जमाने के “महा क्रान्तिकारी” अग्निमुखी कवि आलोकधन्वा, भाजपा सांसद विद्यानिवास मिश्र के जन्मदिन पर स्वामी करपात्री के आश्रम में विद्याश्री न्यास के तत्वावधान में आयोजित लेखक शिविर के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जलेस, प्रलेस और जसम की वाराणसी इकाई के कर्ताधर्तागण, विश्वरंजन के आयोजन में भागीदारी और अपनी पत्नी की पिटाई करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णमोहन, शोध छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी अजय तिवारी, सैफई महोत्सव में जाकर मुलायम सिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा करने वाले केदारनाथ सिंह, अखिलेश सरकार से लखटकिया भारत-भारती पुरस्कार लेने वाले दूधनाथ सिंह,और ऐसे तमाम लोग कुछ दिनों की आलोचना और शिकायतों के बाद वामपंथी साहित्यकारों की बिरादरी में फिर से स्वीकार्य हो जाते हैं। रायपुर में भाजपा सरकार के साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल, नरेश सक्सेना, रमणिका गुप्ता, रणेन्द्र, प्रभात रंजन, बहुतेरे कथित वाममार्गी युवा तुर्कों और जसम-जलेस-प्रलेस से नत्थी छुटभैय्यों के साथ भी ऐसा ही होगा। जब ज़्यादातर एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तो कौन किसपर ऊँगली उठाये! कुछ तो महज़ इसलिए सदाचार की ताबीज बाँट रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें कदाचार का कोई आकर्षक, प्रलोभनकारी मौका मिला ही नहीं। जो असन्तुष्ट है वह विद्रोही है। जब वह सन्तुष्ट हो जाता है तो तरह-तरह के तर्कों से सत्ता और पूँजी-प्रतिष्ठानों के कोठों पर महफिलों में जाने के पक्ष में तर्क देने लगता है।
ज़िन्दगी में गन्द और दन्द-फन्द का सवाल इन कथित वामपंथियों के साहित्य-सृजन में वैचारिकता के अण्ड-बण्ड-भरभण्ड से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इनके एक बड़े हिस्से को आज अज्ञेय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, अशोक वाजपेयी और विनोद कुमार शुक्ल तक में प्रगतिशीलता दीखने लगी है। “वामपंथी” ज्ञान धुरन्धर आलोचक-शिरोमणियों द्वारा संकीर्ण अनुभववादी और प्रकृतवादी दलितवादी लेखन और लम्पट देहमुक्तिवादी कुलीनतावादी नारीवादी लेखन पर अनालोचनात्मक प्रशंसा-पुष्प बरसाते रहने का चलन आम हो चला है। जादुई यथार्थवाद की भोंड़ी प्रहसनात्मक नकलों से कलात्मक चौंक-चमत्कार पैदा करने की कोशिशें जारी हैं। वैचारिक स्तर पर अकड़ी गर्दनों वाले अपढ़-कुपढ़ अधकचरे “चिन्तक” आलोचकों द्वारा मार्क्सवाद को उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर-औपनिवेशिकता, उत्तर-मार्क्सवाद, ‘सबआल्टर्न स्टडीज़’, ‘आइडेंटिटी पॉलिटिक्स’ आदि के साथ फेंट-फाटकर विचित्र खिंचड़ी परोसी जा रही है। जीवन और लेखन दोनों में ही प्रगतिशीलता और प्रतिगामिता की विभाजक रेखायें मिटा-सी दी गयी हैं।
भारतीय बौद्धिक समुदाय की मुख्य धारा के बड़े हिस्से का यह घृणित, निर्लज्ज अवसरवादी विपथगमन और पतन चन्द लोगों के व्यक्तिगत पतन का परिणाम नहीं है। यह एक समकालीन आम प्रवृत्ति है, जिसके कारणों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और सामाजिक आर्थिक संरचना की गतिकी में तलाशना होगा। बौद्धिक समुदाय की मुख्य धारा उस खुशहाल मध्यवर्ग की ही एक परत है, जो मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था का विशेष सुविधाप्राप्त अल्पसंख्यक उपभोक्ता वर्ग है और जो अब जनता का पक्ष त्यागकर सत्ताधारियों के पक्ष में खड़ा हो चुका है तथा इस व्यवस्था में व्यवस्थित हो चुका है। समाज के मुखर तबके के रूप में कभी यह सत्ताधारियों के वर्चस्व (हेजेमनी) के विरुद्ध खड़ा होता था, लेकिन अब यह उस वर्चस्व की स्थापना के लिए वैचारिक-सांस्कृतिक भूमिका निभा रहा है। कहा जा सकता है कि साहित्यिक-सांस्कृतिक परिदृश्य की पतनशीलता भारत के खुशहाल मध्यवर्ग के ऐतिहासिक विश्वासघात और पक्ष-परिवर्तन की ही एक अभिव्यक्ति है, उसीका नतीजा है, या उसी का एक रूप है।
दरअसल, भारतीय बौद्धिक मानस की निर्मिति यूरोप की तरह ‘पुनर्जागरण-प्रबोधन- बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति’ की प्रक्रिया के दौरान नहीं हुई थी, न ही रूस की तरह विलंबित पूँजीवादी विकास के स्वतंत्र मार्ग पर चलते हुए इसने क्रान्तिकारी जनवाद की वैचारिकी तक की (और साहित्य में बुर्जुआ यथार्थवाद तक की) यात्रा तय की थी। भारत में एक औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना के भीतर जो मरियल वैचारिक आधार और खण्डित जनपक्षधरता वाली राष्ट्रीय जनवादी चेतना विकसित हुई, उसमें भी अनैतिहासिक अतीतोन्मुखता और धार्मिक प्रतिच्छायाओं का घटाटोप था और जुझारू भौतिकवादी तर्कणा काफी हद तक अनुपस्थित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन के बुर्जुआ नेतृत्व का नायकत्व खण्डित होने और उसके गौरव के पराभूत होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसी का नतीजा था कि पचास और साठ के दशक में भारतीय बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों का बड़ा हिस्सा पलायनवाद और अस्तित्वाद से लेकर सर्वनिषेधवाद और अन्धविद्रोह तक की यात्रा करता रहा, या फिर अपने मध्यवर्गीय जीवन के सुखों-दु:खों-त्रासदियों-विडम्बनाओं और अलगाव की पीड़ा में शुतुर्मुर्गी ढंग से गर्दन धँसाये रहा। तेलंगाना संघर्ष की पराजय और वाम आन्दोलन के संशोधनवादी विपथगमन के बाद विचार और साहित्य-कला के क्षेत्र में वाम धारा पृष्ठभूमि में चली गयी। वैसे इस वाम धारा की भी इतिहास-प्रदत्त अपनी कमजोरियाँ और सीमाएँ थीं। 1967 के नक्सलबाड़ी जन-उभार के बाद मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की एक नयी पीढ़ी ‘रेडिकलाइज’ होकर वाम प्रभाव में आयी। अपनी विचारधारात्मक कमजोरियों और “वाम” दुस्साहसवादी विचलन के चलते नक्सलबाड़ी उभार से पैदा हुई क्रान्तिकारी वाम धारा भले ही जल्दी ही बिखराव-ठहराव का शिकार हो गयी हो, लेकिन विचार और कला-साहित्य की दुनिया में इसने प्रगतिशील जनवादी धारा को नया संवेग प्रदान किया। हालाँकि सत्तर के दशक में यांत्रिक नारेबाज़ी का घटाटोप अधिक था, लेकिन इस बीच स्तरीय लेखन भी बड़े पैमाने पर हुआ और वाम जनवादी धारा साहित्य की प्रभावी धारा के रूप में स्थापित हो गयी। लेकिन 1980 का दशक साहित्य-कला के क्षेत्र में भी ‘ग्लास्नोस्त-पेरेस्त्रेइका’ का दौर लेकर आया। दशक के अन्त तक वामपंथी साहित्य में नवरूपवादी प्रवृत्ति ने अपना प्रभाव निर्णायक तौर पर स्थापित कर लिया। 1990 के दशक में जब नवउदारवाद के अश्वमेध का घोड़ा पूरे भूमण्डल को रौंद रहा था तथा मार्क्सवाद की पराजय और समाजवाद की पराजय का शोर दिग्-दिगन्त में गूँज रहा था, तब पुनरुत्थान और विपर्यय के उस दौर में बहुप्रचारित उत्तर-आधुनिक विचार-सरणियों के साथ कथित वामपंथी विचारकों और साहित्यकारों ने भी प्रणय-लीला शुरू कर दी, जो लगातार उन्मत्त रूप लेती चली गयी। तात्पर्य यह है कि जिस समय विचार और सृजन की दुनिया में कथित वामपंथ को उत्तर आधुनिकता की महाठगिनी प्रेम पाश में जकड़ रही थी, उसी समय जीवन में वह सत्ता संग अवैध सम्बन्धों के भँवर में ज़्यादा से ज़्यादा उलझता जा रहा था।
दरअसल 1980 के दशक तक, तीसरी दुनिया की अगली कतार के तमाम उत्तर-औपनिवेशिक समाजों की तरह भारतीय समाज में भी पूँजीवादी विकास का राजकीय पूँजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीतियों वाला दौर अपने सन्तृप्ति-बिन्दु तक पहुँच चुका था। इसी की तार्किक परिणति 1990 के दशक में नवउदारवाद के दौर के रूप में सामने आयी। बुर्जुआ दायरे के भीतर राष्ट्रीय जनवाद के कार्यभारों का जिस रूप में और जिस हद तक पूरा होना सम्भव था, वह कम होते जाने के साथ मध्य वर्ग का विभेदीकरण होता चला गया और उसका ऊपरी संस्तर बुर्जुआ ढाँचे में व्यवस्थित होता चला गया। पूँजी के सामाजिक आधार के विस्तार के साथ यह हिस्सा समानुपातिक रूप से बड़ा भी होता चला गया। 1980 के दशक से प्रोफेसर, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह और वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और निजी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की संख्या और खुशहाली में भारी वृद्धि हुई है, जबकि मज़दूरों की ज़िन्दगी की बदहाली ज्यों की त्यों कायम है। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी समुदाय का बहुलांश आज पूँजी के पाले में खड़ा हो चुका है। ऊपर वर्णित राजनीतिक परिदृश्य के आत्मगत प्रभाव के अतिरिक्त इस वस्तुगत यथार्थ के वस्तुगत प्रभाव का ही यह नतीजा है कि आज वामपंथी दायरे में साहित्यिक सर्जना में नवरूपवाद और जीवन के स्तर पर घटिया अवसरवाद का घटाटोप सा छा गया है।
कथित वामपंथी बुद्धिजीवियों-साहित्यकारों का बहुलांश प्रोफेसर, नौकरशाह, मीडियाकर्मी या स्वतंत्र पेशेवर आदि के रूप में खुशहाल मध्यवर्गीय प्राणी बन चुका है जो मेहनतकश जनता के जीवन और संघर्षों से काफी दूर सुरक्षित, सुविधासम्पन्न जीवन बिताता है। अन्दर से सर्वहारा क्रान्ति के भविष्य में न उसकी आस्था है, न ही ऐसी क्रान्ति उसे अपने लिए हितकारी प्रतीत होती है। ऐसे में “वामपंथ” उसके लिए पद-प्रतिष्ठा ख़रीदने वाला बाज़ारू सिक्का या तरक्की की सीढ़ी बन चुका है। क्रान्तियों के “महाख्यानों” के प्रति संशय दिखलाते हुए और विखण्डित सामाजिक आन्दोलनों तथा क्षुद्र विमर्शों का “जश्न” मनाते हुए ऐसे लोग वास्तव में अपनी वर्गीय स्थिति को और बुर्जुआ सत्ता के समाजिक अवलम्ब के रूप में अपनी भूमिका को ‘जस्टिफाई’ कर रहे होते हैं और अपनी ज़िन्दगी की बर्बर खुशहाली को भी। “वामपंथ” का लबादा ओढ़कर सत्ता के कोठों पर व्यभिचार करते हुए और गाहे-बगाहे साम्प्रदायिकता, विस्थापन, पुलिस दमन या दलित-उत्पीड़न जैसे प्रश्नों पर अनुष्ठानिक विरोध-प्रदर्शनों, हस्ताक्षर अभियानों में हिस्सा लेते हुए ये बुद्धिजीवी ठगों और गिरहकटों जैसी भूमिका निभाते हैं। साहित्य की राजनीति ये लोग माफिया गिरोहों की तरह करते हैं, कभी-कभी आपस में कुत्तों की तरह लड़ते भी हैं, लेकिन कोई यदि इनकी असलियत सामने लाने की कोशिश करता है तो ये एकजुट होकर आपके विरुद्ध खुले युद्ध, परोक्ष युद्ध या शीतयुद्ध चलाने लगते हैं या शातिराना साज़िशों का कुचक्र रचने लगते हैं। बहुतेरे लोग अपनी क्षुद्र यशोकामी आकांक्षाओं-महत्वाकांक्षाओं के चलते अनजाने ही इन गिरोहों के षड्यंत्रकारी दुश्चक्रों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कालान्तर में उन जैसे ही बन जाते हैं। घाटों और श्मशानों के पण्डों-पुजारियों जैसे इन छद्मवेषी “वामपंथी” गिरोहों को ठिकाने लगाने के लिए मेहनतकशों के क्रान्तिकारी आन्दोलन को क्रान्तिकारी बुद्धिजीवियों-संस्कृतिकर्मियों-साहित्यकारों की नयी कतारें तैयार करनी होंगी, सर्वहारा के ‘आर्गेनिक इंटेलेक्चुअल’ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयार करने होंगे।
- नान्दीपाठ-3, अप्रैल-जून 2016