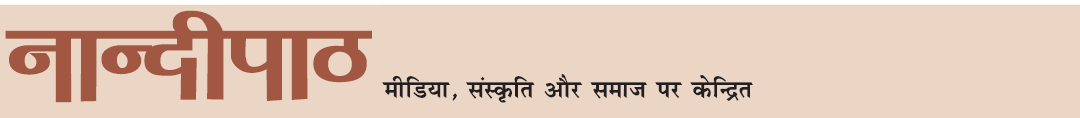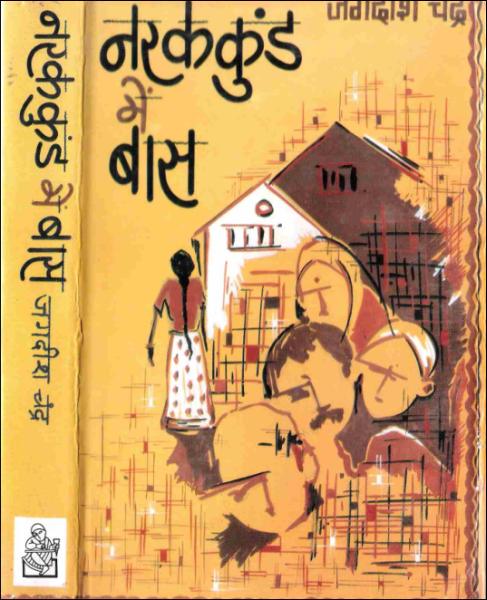हमारे समय का यथार्थ और जगदीशचन्द्र के उपन्यास
मीनाक्षी
हिन्दी आलोचना के फ़तवेबाज़ों से बिना मुँह लगे हुए, जगदीशचन्द्र अपनी रचनात्मकता से जीवनपर्यन्त उन्हें थोथा और खोखला साबित करते रहे। उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपन्यास–त्रयी की दूसरी कड़ी (‘नरककुण्ड में बास’) जब प्रकाशित हुई (1994 में) तो हिन्दी जगत ‘उपन्यास का अन्त’ और ‘उपन्यास की मुक्ति’ जैसे नारों के शोर से सरगर्म था। और अब उसकी तीसरी और अन्तिम कड़ी (‘ज़मीन अपनी तो थी’) 2001 में छपकर आई है जब हिन्दी उपन्यासों की दुनिया में, यथार्थ को जादू में तब्दील कर देने और जादू में यथार्थ की खोज के हैरतअंगेज़, सनसनीख़ेज़ कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है।
जगदीशचन्द्र आज हमारे बीच नहीं हैं। यह दुखद है कि उनका आख़िरी उपन्यास उनकी मृत्यु (अप्रैल, 1996) के पाँच वर्ष बाद प्रकाशित हो सका जबकि वे इसका पहला ड्राफ़्ट 1995 में ही पूरा कर चुके थे। और यह भी हिन्दी आलोचना के समकालीन रीति–रिवाज़ों के मुताबिक ही हो रहा है कि तमाम प्रायोजित चर्चाओं के बीच इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कृति पर जैसे किसी का ध्यान ही नहीं हैं। बहरहाल, जो रचनात्मकता साहित्य के विकास में, वास्तव में मील का पत्थर होती है, वह प्रायोजित चर्चाओं की मोहताज नहीं होती।
वैसे तो जगदीशचन्द्र हिन्दी के एक ऐसे उपन्यासकार हैं, जिनकी तीस वर्ष लम्बी पूरी रचना–यात्रा का सम्यक् विश्लेषण–मूल्यांकन बेहद ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हम अपने को उनकी प्रसिद्धतम उपन्यास–त्रयी के तीन उपन्यासों-‘धरती धन न अपना’, ‘नरककुण्ड में बास’ और ‘ज़मीन अपनी तो थी’ पर ही केन्द्रित करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले एक और महत्त्वपूर्ण उपन्यास ‘कभी न छोड़ें खेत’ पर थोड़ी बातचीत ज़रूरी है।
‘धरती धन न अपना’ के प्रकाशन (1972) के बाद जगदीशचन्द्र ने जिस उपन्यास पर काम किया, वह था ‘कभी न छोड़ें खेत।’ ‘धरती धन न अपना’ की कहानी चमारड़ी में रहने वाले दलित भूमिहीनों के जीवन पर केन्द्रित रहते हुए पंजाब के गाँवों की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जबकि ‘कभी न छोड़ें खेत’ (1976) पंजाब के जट्ट किसानों के जीवन पर केन्द्रित है। दोनों की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद का गाँव है। स्वाधीनता की लहर से अछूते पंजाब के गाँव कूपमण्डूकता, अविश्वास, अज्ञान, अशिक्षा, निरंकुशता, निर्ममता और शोषण के दलदली रसातल में ऊँघ रहे थे। ‘कभी न छोड़ें खेत’ के जट्ट किसान इन अन्धकारमय स्थितियों में शोषण और दारुण यातनाओं के शिकार होते हुए भी जीवन के प्रति चीमड़ लगाव और अदम्य जिजीविषा से भरपूर दीखते हैं। ज़रा सी बात में सिर–फुटौवल और क़त्ल, लम्बी मुकदमेबाज़ियाँ, कोर्ट–कचहरी की भाग दौड़, पुलिस–साहूकारों और बिचैलियों की भूमिका और परम्परा के प्रति विद्रोह की भावना तथा अदम्य आत्मविश्वास से भरी जसवन्त कौर जैसी निम्न मध्यम किसान स्त्री। प्रेमचन्द के ‘गोदान’ के बाद यदि किसी उपन्यास में भारतीय किसानी जीवन इतनी सूक्ष्मता, विस्तार और आधिकारिकता के साथ उपस्थित हुआ है तो निस्सन्देह वह है-‘कभी न छोड़ें खेत।’ फ़र्क़ यह है कि प्रेमचन्द का गाँव ग़ुलाम भारत का पुरबिया गाँव है जहाँ ज़मीन्दारी–प्रथा लागू थी जबकि जगदीशचन्द्र का गाँव आज़ादी के ठीक बाद के पंजाब का गाँव है जहाँ जागीरदारी प्रथा लागू थी और ऊपर के धनी चैधरियों को छोड़कर मध्यम तबके तक के किसानों पर साहूकारों–बिचैलियों की जकड़बन्दी नागपाश के समान कसी हुई थी। ‘कभी न छोड़ें खेत’ पढ़ते हुए बार–बार बाल्जाक के ‘किसान’ उपन्यास की याद आती है। साथ ही, जट्ट किसानों के जीवन की तस्वीर तोल्स्तोय और शोलोख़ोव द्वारा चित्रित कज़्जाकों के जीवन की बहुत अधिक याद दिलाती है।
‘कभी न छोड़ें खेत’ टूटते हुए अर्द्धसामन्ती समाज के किसानी जीवन के बिखरते ताने–बाने की त्रासद गाथा है तो ‘धरती धन न अपना’, ‘नरककुण्ड में बास’ और ‘ज़मीन अपनी तो थी’ की उपन्यास–त्रयी स्वातंत्र्योत्तर भारत के प्रारम्भिक पच्चीस वर्षों की पृष्ठभूमि में दलित जीवन की असह्य घुटन, अपमान और यातना का महाकाव्य प्रस्तुत करती है। भारतीय जीवन के कुरूपतम–बर्बरतम यथार्थ को इस उपन्यास–त्रयी में जगदीशचन्द्र ने बिना किसी अतिरिक्त भावावेश के, बिना नक़ली विद्रोह और काल्पनिक समाधान के, नितान्त वस्तुपरक ढंग से प्रस्तुत किया है। दलित जीवन के निर्मम–कठोर यथार्थ का कलात्मक पुनर्सृजन करते हुए जगदीशचन्द्र ने नायक काली द्वारा यथास्थिति के अस्वीकार को आरोपित ढंग से राजनीतिक विद्रोह का रंग देने, चेतना के तीव्र क्रान्तिकारीकरण की कृत्रिम–यांत्रिक प्रक्रिया प्रस्तुत करने या चटख आशावाद के बनावटी रंग भरने की कोई कोशिश नहीं की है। उपन्यास की जनपरक प्रयोजनमूलकता कथा–विन्यास की आभासी सतह पर मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी संरचना में समाई हुई है। लेखक समाधान प्रस्तुत करने का रास्ता नहीं अपनाता, बल्कि सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक संरचना के स्वरूप, आन्तरिक गति और दिशा को नितान्त रचनात्मक ढंग से उद्घाटित करता चलता है। यह उपन्यास–त्रयी प्रश्नचिह्नों से प्रश्नचिह्नों तक की एक सुदीर्घ यात्रा है-पाठक की आँख में उँगली डालकर भारतीय जीवन की सर्वाधिक अमानवीय और जटिल सच्चाई को देखने के लिए विवश करती हुई। यह जिन सवालों से शुरू होती है, वे आधे–अधूरे ही हल हो पाते हैं। फिर नये सवाल उठते हैं और वे भी या तो आधे–अधूरे हल होते हैं या फिर कोने में धकेल दिए जाते हैं। यही सिलसिला जारी रहता है और तीसरा उपन्यास जब समाप्त होता है तो पाठक के सामने कई सवाल फिर भी खड़े रह जाते हैं। इसी यात्रा की पड़ताल और इन्हीं प्रश्नों के समाधान की प्रक्रिया में दलित–प्रश्न को हल करने की आगे की कोई दिशा फूटती है। साहित्यिक कृतियों की सोद्देश्यता या प्रयोजनमुखता को स्वीकारते हुए फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि “प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति या कार्यकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना, और लेखक अपने द्वारा वर्णित सामाजिक टकरावों का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयारशुदा रूप में प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है।” आशावाद कोई निरपेक्ष–शाश्वत चीज़” नहीं होती। मिथ्या आशावाद को तोड़ने से यदि निराशा और निरुपायता भी पैदा होती है तो वह सकारात्मक है क्योंकि वास्तविकता को स्वीकारना राह निकालने की पहली शर्त होती है। एंगेल्स के शब्दों में, “समाजवादी प्रयोजनमूलक उपन्यास उस समय अपने ध्येय की पूर्णतया पूर्ति करता है जब वह वास्तविक सम्बन्धों का सच्चा चित्रण कर इन सम्बन्धों के स्वरूप के बारे में हावी रहने वाले प्रचलित भ्रमों को मिटा देता है, बुर्जुआ दुनिया के आशावाद को झकझोर देता है तथा अस्तित्वमान के आधार की शाश्वतता के बारे में शंका का समावेश करता है, भले ही उसने कभी–कभी कोई पक्ष तक न लिया हो।” (एंगेल्स : मिन्ना काउत्स्की को पत्र, 26 नवम्बर, 1885)। जगदीशचन्द्र अपने उपन्यासों में प्रयोजनमूलकता को घटनाओं–चरित्रों के ट्रीटमेण्ट के ज़रिए प्रकट करते हैं और समाधानवादी स्थूलता से हर हाल में बचते हैं। मिथ्या आशावाद के मायालोक से अलग यथार्थ की ठोस ज़मीन पर खड़े रहकर वे सामाजिक स्थितियों में अन्तर्व्याप्त मानवद्रोही प्रवृत्तियों को अनावृत्त करते हैं और साथ ही समाज–विकास की गतिकी को घटना–विन्यास के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उनके यथार्थवाद के यही दो बुनियादी संघटक अवयव हैं और इनके संश्लेषण में जो असामान्य दक्षता उन्होंने दिखलाई है उसी के चलते, एक मार्क्सवादी न होते हुए भी, हमारे समय के सारभूत यथार्थ को उसकी वैविध्यपूर्ण प्रतीतियों सहित पकड़ने और प्रस्तुत करने में जगदीशचन्द्र की सफलता निस्सन्देह अद्वितीय है। यदि “यथार्थवाद का अर्थ तफ़सील की सच्चाई का, आम परिस्थितियों में आम चरित्रों का सच्चाई भरा पुनर्सृजन है”, जैसाकि फ्रेडरिक एंगेल्स ने बताया है (मार्गरेट हार्कनेस को पत्र, अप्रैल 1888); तो जगदीशचन्द्र को मात्र उनके चार उपन्यासों (‘धरती धन न अपना’, ‘कभी न छोड़ें खेत’, ‘नरककुण्ड में बास’ और ‘ज़मीन अपनी तो थी’) के आधार पर, विगत आधी सदी के महानतम यथार्थवादी भारतीय उपन्यासकारों में निस्संकोच शामिल किया जा सकता है।
बाल्जाक विचारों से राजतंत्रवादी थे, लेकिन अपनी कृतियों में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत निष्ठाओं से ऊपर उठकर, बुर्जुआ समाज की अमानवीयताओं के साथ–साथ सामन्ती पतनशीलता पर भी मारक चोट की और सामन्तवाद से पूँजीवाद में संक्रमण कर रहे समाज की तमाम तफ़सीलों को नितान्त वस्तुपरक ढंग से प्रस्तुत किया जिसे फ्रेडरिक एंगेल्स ने “यथार्थवाद की विजय” की संज्ञा दी। यथार्थवाद की यही विजय प्रेमचन्द के कृतित्व में, विशेषकर उनकी परवर्ती रचनाओं में मूर्त रूप लेती दीखती है जब अपनी गांधीवादी निष्ठाओं का अतिक्रमण करते हुए वे अपने पात्रों के मंुह से या स्थिति–चित्रण के द्वारा सामन्त वर्ग के प्रति कांग्रेस की समझौतापरस्ती को, उसकी बुर्जुआ पक्षधरता और मज़दूर–विरोध को तथा “हरिजन–उद्धार” की यूटोपिया और निष्फलता को अनावृत्त करने लगते हैं। प्रेमचन्द के सन्दर्भ में “यथार्थवाद की विजय” और आगे, वहाँ तक जाती है कि वे जीवन के अन्तिम वर्षों में, सचेतन तौर पर आमूलगामी से आमूलगामी सुधारवाद की सीमाओं को पहचानने लगते हैं। मध्य जाति के और मध्य किसान वर्ग के काश्तकारों के सामन्ती उत्पीड़न और दलित भूमिहीनों की त्रासद–बर्बर जीवन स्थितियों को वे ‘गोदान’ में प्रस्तुत करते हैं। ‘ठाकुर का कुआँ’ और ‘सद्गति’ जैसी कहानियों में वे सवर्ण सामन्ती समाज की बर्बर अमानवीयता का ऐतिहासिक कलात्मक दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं। “यथार्थ की विजय” की यही परिघटना हमें फिर जगदीशचन्द्र के उपन्यास ‘धरती धन न अपना’ में निरूपित होती दीखती है। जगदीशचन्द्र विचारों से मार्क्सवादी नहीं थे, पर जीवन–यथार्थ की पड़ताल करते हुए वे तथ्यों की वस्तुपरकता, सूक्ष्म ब्योरों और तफ़सीलों के प्रति उत्कट आग्रही और सजग अध्येता के रूप में सामने आते हैं। बचपन और किशोरावस्था में अपने ननिहाल में अछूतों का जो जीवन और परिवेश उन्होंने देखा था, उससे पैदा हुई उद्विग्नता उनके मन–मस्तिष्क में बरसों बनी रही। आगे चलकर, शायद अर्थशास्त्र की औपचारिक शिक्षा और जीवनानुभवों ने उन्हें वह समझ और क्षमता दी कि नितान्त वस्तुपरकता, आधिकारिकता और तफ़सीलों के साथ दलित जीवन के यथार्थ की कलात्मक इन्दराज़ी में उन्होंने अद्वितीय सफलता अर्जित की। बचपन की स्मृतियों के बारे में जगदीशचन्द्र ने स्वयं लिखा है, “…गाँव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएँ भड़क उठीं।… मैं हर साल यही देखता कि गाँव में मर्यादाओं की सीमाएँ टूटनी तो दूर रहीं, उनकी जकड़न दिनों–दिन सख्त होती जा रही है… मैं यह सब देखकर बहुत उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग–युगान्त से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बाँध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया।”
“धरती धन न अपना’ की शुरुआत नायक काली के गाँव लौटने से होती है। गाँव है पंजाब के दोआबे के होशियारपुर ज़िले का घोड़ेवाहा गाँव। पिता और चाचा की मृत्यु के बाद, भुखमरी की स्थिति में काली छह वर्ष पहले गाँव छोड़कर कानपुर चला गया था और एक कारख़ाने में मज़दूरी करने लगा था। इस नाते उसकी चेतना, हालाँकि वह वर्ग–सचेत सर्वहारा की चेतना नहीं है, लेकिन गाँव के दलित भूमिहीन मज़दूरों से उन्नत है। उसकी इसी चेतना को माध्यम बनाकर लेखक ने गाँव के दलितों के जीवन के निर्मम यथार्थ से पाठक का साक्षात्कार कराया है।
काली अपनी चाची प्रतापी की देखभाल के लिए गाँव लौटा है, जिसने उसे पाल–पोसकर बड़ा किया था। गाँव लौटने पर वह वहाँ की पूर्ववत् अत्याचारपूर्ण स्थितियों को देखकर उदास हो जाता है, लेकिन फिर अपनों के बीच धीरे–धीरे मन रमा लेता है। दलित होकर भी वह शहर से लाए “बहुत सारे नोट” (तीन सौ रुपये से कुछ कम) से “पक्का” मकान बनाना चाहता है जो चैधरियों और शाहों के लिए एक अजूबा बात है। छज्जू शाह काली को बताता है कि जिस ज़मीन पर उसका मकान है वह “शामलात” की ज़मीन है जिस पर उनका केवल “मास्सी” अधिकार है (यानी सिर्फ़ रहने का अधिकार है, मालिकाना नहीं)। ज्ञातव्य है कि पंजाब में 1960 तक यही स्थिति थी। इसके बाद कुछ भुगतान लेकर भूमिहीनों को वासभूमि पर मालिकाना दे दिया गया था।
इस बीच वह चमारड़ी में रमने लगता है। एक बहादुर और ईमानदार लड़की ज्ञानों से उसका प्रेम होता है। घर बनाने का सपना और प्रेम-इन दोनों की परिणति अन्तत: दुखान्त में होती है। झाड़–फूंक करने की प्रक्रिया में चाची की मौत और दुख के इन्हीं दिनों में उसकी जमा–पूँजी की चोरी के प्रसंग सदियों के उत्पीड़ित लोगों के जीवन में व्याप्त सांस्कृतिक पिछड़ेपन और अमानुषीकरण की स्थितियों को सामने लाते हैं। इस बीच गाँव में चैधरियों–चमारों के बीच टकराव के रूप में वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। काली चमारों की अगुवाई करता है। चौधरी उसके दुश्मन हो जाते हैं। ज्ञानों का भाई मंगू चैधरियों की दलाली करता है और काली को तंग करता है। संघर्ष के इसी प्रसंग में पाठकों का परिचय डा. बिशनदास और टहलसिंह जैसे क़स्बाई, क़िताबी कम्युनिस्टों से होता है जो चमारों और चैधरियों के बीच संघर्ष भड़क उठने से प्रसन्न हैं क्योंकि स्थितियाँ उन्हें 1905 की रूसी क्रान्ति की शुरुआत से मिलती–जुलती प्रतीत होती हैं। वे काली और कुछ अन्य चमार कार्यकर्ताओं और कम्युनिस्ट हमदर्दों की मीटिंग बुलाते हैं जहाँ हड़ताली खेत मज़दूरों की मदद के ठोस रूपों पर विचार के बजाय बिशनदास और टहलसिंह त्रात्स्कीपन्थ और उसने विरोध के प्रश्न पर बहस करते हैं। खेत मज़दूर अपने संघर्ष के लिए अनाज या आर्थिक मदद की अपेक्षा करने पर “सुधारवादी” करार दे दिए जाते हैं क्योंकि वे भूखे पेट लड़ नहीं सकते। ऐसे क़िताबी, अव्यावहारिक कम्युनिस्टों के अतिरिक्त उदारपन्थियों और धार्मिक उपदेशकों से भी चमारों को कोई मदद नहीं मिलती। काली जिस लालू पहलवान के वहाँ काम करता है, वह चमारों के साथ समझौते का पक्षधर है क्योंकि चैधरियों–चमारों का काम एक–दूसरे के बिना नहीं चलने का, लेकिन संघर्ष के दिनों में वह काली की कोई मदद नहीं करता, कारण कि अपने वर्ग के लोगों से वह कटकर नहीं रह सकता।
उपन्यास में बड़ी कुशलता के साथ जगदीशचन्द्र ने इस नग्न–निर्मम यथार्थ को भी उजागर किया है कि धर्म–परिवर्तन दलित–प्रश्न का वास्तविक समाधान नहीं है और धार्मिक उपदेशकों की भी एक स्पष्ट वर्ग दृष्टि है जो अछूतों को अपमानित करने का ही काम करती है। उपन्यास का एक जूते सिलने वाला पात्र नन्द सिंह रमदासिया जातिगत अपमान से बचने के लिए पहले सिख और ईसाई बनता है लेकिन चैधरियों के उसके प्रति बरताव में कोई फ़र्क नहीं आता। बाढ़ के समय हिन्दू पण्डित और सिख ज़मीन्दार अपने कुओं से चमारों को पानी नहीं लेने देते। ऐसे में चमारों की गन्दगी को देखकर ईसाई धर्मपिता की पत्नी भी अपने हैण्डपम्प पर ताला लगा देती है।
ग्रामीण दलितों की जीवन स्थितियों का प्रामाणिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हुए जगदीशचन्द्र दलितों के सामाजिक जीवन के नितान्त पिछड़े हुए सांस्कृतिक पहलुओं-झाड़–फूंक, अन्धविश्वास, रूढ़ियों आदि की भी उपेक्षा नहीं करते, जो शताब्दियों के दमन–उत्पीड़न से पैदा हुए अमानुषीकरण की अभिव्यक्तियाँ हैं। काली और ज्ञानो का निष्कलुष प्रेम भी गाँव में दुष्प्रचार का माध्यम बन जाता है। अपने ही दलित समाज की संकीर्ण मान्यताओं के कारण दोनों का ब्याह नहीं हो सकता। ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और स्वयं उसकी माँ और भाई मंगू ही उसकी हत्या कर देते हैं। काली को गाँव छोड़कर भागना पड़ता है।
‘नरककुण्ड में बास’ की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ ‘धरती धन न अपना’ का अन्त हुआ था। गाँव के प्रभुत्वशाली लोगों के ज़ुल्म, अपने लोगों की दिमाग़ी ग़ुलामी व सांस्कृतिक पिछड़ेपन और आर्थिक तबाही की चपेट में अवश–निरुपाय काली को भागकर शहर आना पड़ता है। वैसे, एक दलित का उजड़ना भी क्या! एक किसान तो सामन्ती उत्पीड़न या पूँजी की मार से तबाह होकर, अपनी जगह–ज़मीन से उजड़कर उजरती ग़ुलामों की कतार में शामिल होता है। लेकिन एक दलित के लिए तो बस इतना ही फ़र्क पड़ता है कि बेगारी करने वाले और हर तरह का अपमान झेलने वाले अर्द्धदासों की स्थिति से उबरकर वह शहर आकर सबसे नारकीय काम करने वाले और सबसे सस्ती दरों पर श्रम बेचने वाले उजरती ग़ुलामों की कतार में शामिल हो जाता है। शहर में फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि वह अपना श्रम बेचने को मुक्त होता है, जातिगत भेदभाव के बावजूद गाँवों जैसा उत्पीड़न और अपमान नहीं झेलना पड़ता तथा कठिन जीवन–स्थितियाँ अन्य जातियों के उजरती मज़दूरों के साथ भी एकता का एक आधार मुहैया करती हैं।
शहर आकर काली उन तमाम बिना पहचान के लोगों की ‘बेचेहरा’ भीड़ में शामिल है जो अपनी श्रमशक्ति बेचकर उजरत कमाने के लिए चारों ओर दौड़ते–भागते और हर जुगत भिड़ाते रहते हैं। एकदम अकेला और बेसहारा काली के हृदय में ज्ञानो को लेकर एक गहरा पश्चाताप भी है। उसे लगता है कि उसने ज्ञानो को उसके हाल पर छोड़कर धोखा दिया है और अब जीवन शायद उसे सफ़ाई का कोई अवसर भी नहीं देने वाला है। इस मन:स्थिति में वह पिछली हर पहचान की छाया तक से भागता है। पारिवारिक–सामाजिक–भावनात्मक-सभी स्तरों पर जड़ों से उखड़ा हुआ काली अपने अस्तित्व को बचाए रखने की ख़ातिर, अन्ततोगत्वा निकृष्टतम कोटि के उजरती ग़ुलामों के उस पेशे में नियति द्वारा धकेल दिया जाता है जो आज भी, आधी सदी की आज़ादी के बाद और जनतंत्र के तमाम दावों के बावजूद, हमारे देश में सिर्फ़ दलितों के लिए ही आरक्षित माना जाता है। कुलीगीरी करने और रेहड़ा खींचने वाले मज़दूर के तौर पर काम करके पेट पालने में क़िल रहने के बाद काली को अन्ततोगत्वा टैनरीज़ में कच्चा चमड़ा धोने और साफ़ करने वाले मज़दूर के तौर पर काम मिलता है। नारकीय गन्दगी और बदबू के भयानक माहौल में मितली दबाते हुए और जानलेवा ख़ारिश बर्दाश्त करते हुए काली को काम करना पड़ता है। जगदीशचन्द्र ने कुलियों और रेहड़ा खींचने वाले मज़दूरों की ज़िन्दगी से लेकर टैनरीज़ के मज़दूरों तक की ज़िन्दगी और कच्चे चमड़े की सफ़ाई जैसे कामों का जितना आधिकारिक ब्योरा तफ़सीलों के साथ प्रस्तुत किया है, वह स्पष्ट कर देता है कि गहन अर्थशास्त्रीय–समाजशास्त्रीय अध्ययन के कारण ही वह उपन्यास की विषय–वस्तु को जीवन्त रूप में प्रस्तुत कर पाए हैं। यहाँ टैनरीज़ के नर्क में ज़िन्दगी घिसने वाले, समाज के अँधेरे रसातल के निवासियों की मरणान्तक जद्दोजहद का वर्णन है, टैनरीज़ के ग़ैरदलित मालिकों के साथ ही दलित मालिकों के मक्कार शोषक चरित्र और उनकी आपसी वर्गीय एकता की तस्वीर है और दलितों का नेता होने का दम भरने वाले सत्ताधर्मियों का भी चरित्र–चित्रण है, लेकिन यह सब कुछ लेखक ने नितान्त वस्तुपरक “तटस्थता” के साथ प्रस्तुत किया है। अन्त में काली स्वयं अपने साथी मज़दूरों का छोटा–मोटा लीडर हो जाता है और टैनरीज़ में मुंशीगीरी करने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह स्वयं मज़दूरों से ही कट जाता है और उनका विश्वास खो बैठता है। वह ईमानदारी से कोशिश करता है कि मज़दूरों को थोड़ी सुविधाएँ दिलवा सके, लेकिन इस कोशिश में बुरी तरह क़िल होता है। एक बार फिर वह अपने को सड़क पर खड़ा पाता है। इन्हीं हालात में अचानक उसकी मुलाक़ात एक बार फिर अपने गाँव के नन्दसिंह से होती है। नन्दसिंह को भी अपनी ज़िन्दगी और इज़्जत बचाने के लिए अन्तत: गाँव से भागना पड़ा था और अब जालन्धर से छह–सात कोस दूर सड़क किनारे अड्डे पर वह जूते सिलता था और पास के गाँव में रहता था। नन्दसिंह से काली को पता चलता है कि ज्ञानो को गर्भवती हो जाने की वजह से उसके अपने परिवार वालों ने ही ज़हर देकर मार दिया था। यहाँ सामने आने वाली विडम्बना पूरे उपन्यास को और सारगर्भित बना देती है। जिस ज्ञानो का अपराधी होने का पश्चाताप काली को बाहरी नर्क के समान्तर एक भीतर नर्क में भी लगातार धीमी आँच पर झुलसा रहा था, वह उसकी नर्क–यात्रा शुरू होने के पहले ही मर चुकी थी। ज्ञानो की मृत्यु की ख़बर से काली एकदम टूट जाता है। फिर नन्दसिंह उसे दिलासा देकर अपने घर ले जाता है। वह काली से कहता है कि वह उसके साथ ही रहकर काम में उसकी मदद करे।
उपन्यास–त्रयी की अन्तिम कृति ‘ज़मीन अपनी तो थी’ दलित जीवन के त्रासद यथार्थ के सभी आयामों और पक्षों को प्रस्तुत करने के जगदीशचन्द्र के संकल्प की अन्तिम फलश्रुति है। यहाँ जगदीश चन्द्र सामाजिक परिवर्तन की उस संश्लिष्ट प्रतिगामी प्रक्रिया को और अधिक तफ़सील के साथ, और अधिक गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते स्वतंत्रता और जनतंत्र की तमाम उपलब्धियाँ और पूँजीवादी विकास के तमाम फल ऊपर की बीस फ़ीसदी आबादी तक ही सिमट कर रह गये। मध्यम किसानों की एक छोटी आबादी सत्ता और सुविधाओं का भागीदार ज़रूर बन गई लेकिन दलित, जो भूमिहीन किसान और बँधुआ मज़दूर थे, वे अब उजरती मज़दूर बन गये। भूमि.सुधार से मालिक बने काश्तकारों को तो लाभ हुआ, लेकिन भूमि.वितरण भूमिहीनों के साथ मात्र एक छल साबित हुआ तथा सीलिंग को भूस्वामियों ने छल–बल से नाकाम कर दिया। सभी सुधार दलितों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति के लिए मात्र ‘कॉस्मेटिक’ सिद्ध हुए। सारी प्रगति के प्रसाद का मात्र चूरा ही उन्हें नसीब हुआ। आज़ादी के बाद के (अतिसीमित ही सही) बुर्जुआ सुधारों और दलितों की संगठित चेतना के प्रभाव से दलितों के बर्बर दमन की स्थितियों में कुछ फ़र्क़ तो पड़ा (वह भी पूरे देश में नहीं), लेकिन उनके सामाजिक अपमान और पार्थक्य (सेग्रिगेशन) की स्थिति अब भी बनी रही। सबसे अहम बात यह है कि सुधारवादियों की गलदश्रु भावुकता और मध्यवर्गीय दलित कुलीनतावादी लेखकों के खोखले आवेश के बजाय जगदीशचन्द्र ने इस उपन्यास में दलित–प्रश्न की वर्ग–अन्तर्वस्तु को अत्यन्त सटीक ढंग से उजागर किया है। वे यह दिखलाते हैं कि किस तरह दलितों के बीच से ही पिछली आधी सदी के दौरान भितरघाती सत्तासेवियों की राजनीतिक जमातें पैदा होती रही हैं। चौधरी शिंगाराराम जैसे बूढ़ेे खुर्राट दलित नेता से सेठ रामप्रकाश जैसे नई पीढ़ी के दलित नेताओं तक के विकासक्रम में कांग्रेसी हरिजन नेताओं से आज के बसपा ब्राण्ड दलित नेताओं तक के विकास की पथ–रेखा की शिनाख्त की जा सकती है। साथ ही, लेखक ने इस सामाजिक–आर्थिक परिघटना को भी बहुत रचनात्मक ढंग से उपन्यास में प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार दलितों का जो एक अत्यन्त छोटा–सा हिस्सा नौकरशाही में या डॉक्टरों–इंजीनियरों की जमात में शामिल हुआ है, वह शेष दलित आबादी से अपने को पूरी तरह से काटकर अपने टापू पर जीता है और अपने निजी स्वार्थों के लिए आम दलितों के साथ विश्वासघात करने तथा उनके हितों पर डाका डालने से भी बाज़ नहीं आता। यही दलित कुलीन मध्यवर्ग है जिसका वास्तविक प्रतिनिधित्व आज की बुर्जुआ संसदीय दलित राजनीति करती है। अम्बेडकर के नाम पर फ़रेब रचकर ऐसी दलितवादी पार्टियाँ व्यापक दलित आबादी में जनाधार बनाती हैं और फिर निष्ठापूर्वक, सर्वाधिक निकृष्ट अवसरवादी ढंग से सत्ताधर्म निभाती हैं। ‘ज़मीन अपनी तो थी’ अर्द्धसामन्ती भूमि-सम्बन्धों के पूँजीवादी रूपान्तरण के दौरान भूमि.सुधार के नाम पर दलितों के साथ हुए छल, दलित–उत्पीड़न और अपमान की निरन्तरता, बुर्जुआ दलित राजनीति के चैधरियों की कुत्सित चालों और दलितों के बीच से उभरने वाले नये अभिजन समाज की विश्वासघाती स्वार्थान्धता पर केन्द्रित कृति है।
उपन्यास कथा–सूत्र को वहीं से पकड़ता है, जहाँ ‘नरककुण्ड में बास’ का समापन हुआ था। काली नन्दसिंह के परिवार के साथ आकर रहने लगता है और जूते की दूकान में बतौर शागिर्द उसकी मदद करने लगता है। पहले ज्ञानो–प्रकरण को लेकर परिवार में काली के प्रति दुराव का माहौल रहता है, लेकिन उसके निश्छल–नि:स्वार्थ व्यवहार से पूर्वाग्रह दूर हो जाते हैं और वह परिवार का एक सदस्य–सा बन जाता है। काली के अध्यवसाय से नन्दसिंह के कारोबार की प्रगति, उसकी बेटी पाशो से उसकी नज़दीकी और फिर शादी, फिर उन दोनों का अलग गृहस्थी बसाना-इस लाइन पर कहानी आगे बढ़ती है। इसी के साथ गाँव के सरदारों–चैधरियों और अड्डे के बनियों–साहूकारों द्वारा चमारों के साथ बात–बात पर अपमानजनक व्यवहार, चमारों की अवशता आदि का लेखक ने बड़ा ही जीवन्त चित्रण किया है।
उपन्यास का कालखण्ड सातवें दशक के आसपास का है। तब गाँव के ग़रीबों को घर बनाने या हारी–बीमारी जैसी ज़रूरतों के लिए कर्ज़ देने के मक़सद से सहकारी समितियाँ बन रही थीं। जगदीशचन्द्र ने तफ़सील से यह दिखलाया है कि किस तरह ये समितियाँ बड़े किसानों की जेब में घुस गर्इं और इन्होंने गाँव के ग़रीबों को एक नये प्रकार की साहूकारी–महाजनी के पाश में जकड़कर पूरी तरह से उजरती ग़ुलाम बन जाने के लिए बाध्य कर दिया। काली और उसकी पत्नी पाशो भी सोसाइटी के मेम्बर बनते हैं। उन्हें कर्ज़ महज़ इसलिए मिल पाता है कि भूस्वामी सरदार चाहता है कि तमाम फर्जी मामलों पर पर्दा डालने के लिए एकाध जेनुइन केस भी होने चाहिए। इस बीच दलित दम्पति लखबीर और मागो की बेटी बलजीतो की त्रासद उपकथा भी आती है जो पूरे तंत्र के दलित–विरोधी चरित्र और आम दलितों की बेबसी को अनावृत्त करने का काम करती है। पण्डोरी के नम्बरदार गण्डासिंह का बेटा नसीबसिंह बलजीतो के साथ प्यार का नाटक रचाकर उसे भगा ले जाता है। पूरी दलित बस्ती एकजुट होकर बलजीतो की खोज करती है। वे बड़े सरदार (पृतपाल सिंह) की ड्योढ़ी पर भी जाकर फ़रियाद करते हैं। सरदार उन्हें मदद का झूठा आश्वासन देता है, पर अन्दर ही अन्दर गण्डासिंह की मदद करता है। सभी दलित बुजुर्ग मख्खन सिंह के साथ जाकर इलाक़ा मजिस्टेªट कुलतार सिंह से मिलते हैं, जो उन्हीं की बस्ती के दलित बुनकर का बेटा था। काली उसी के मकान में किराएदार था। कुलतार सिंह पद–प्रतिष्ठा और काली कमाई के बाद अब अपने नाम के साथ काहलों पदवी लगाकर जाट बनने की कोशिश करता है, पर उसके पण्डित और सवर्ण अमले भी अन्दर ही अन्दर उस पर हँसते हैं। रिश्वतख़ोरी के चलते उसे अपने बाबू वग़ैरह से दबना और बनाकर रखना भी पड़ता है। कुलतार सिंह के कहने पर पुलिसिया अमला कुछ धर–पकड़ की औपचारिकता भी करता है, लेकिन बलजीतो का पता नहीं चलता। कुछ महीनों बाद हारी–टूटी बलजीतो लौटती है। चाहे भय हो या बेबसी, वह किसी का नाम नहीं बताती और पुलिस केस समाप्त हो जाता है। इस पूरे प्रसंग में जगदीशचन्द्र ने गाँव के चैधरियों से लेकर अड्डे के बनियों तक के नितान्त घृणास्पद दलित–विरोधी, स्त्री–विरोधी रवैये को बख़ूबी उजागर किया है। सभी मानकर चलते हैं कि बलजीतो ही चरित्रहीन है और कि दलित लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाना बड़ी बात नहीं है। उन्हें यह बात अनहोनी और बहुत नागवार लगती है कि दलित इस मामले को लेकर एकजुट होकर पुलिस–प्रशासन तक पहुँच गये। इस मसले पर काली को बाज़ार में अपमानित भी होना पड़ता है। ऐसे कई छोटे–छोटे प्रसंग हैं उपन्यास में, जिनके माध्यम से रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में दलितों द्वारा झेले जाने वाले मारक अपमान की दारुण यंत्रणा को जगदीशचन्द्र ने सूक्ष्मग्राही ढंग से चित्रित किया है।
इसके बाद ही सीलिंग की फ़ाज़िल ज़मीन के भूमिहीनों में वितरण का वह प्रसंग आता है जो पूरे सामाजिक–राजनीतिक ताने–बाने को उजागर करने वाला, उपन्यास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रसंग है। काली और उसकी बस्ती के अन्य दलित भी ज़मीन अलॉटमेण्ट के लिए आवेदन करते हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद उन्हें ज़िला माल अफ़सर के दफ़्तर में अगली कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है। ज़मीन के मालिकाने के लिए सदियों से तरसे दलितों के मन में उम्मीदें जगती हैं। वे अलॉटमेण्ट के काम में मदद के लिए फिर अपने पूर्व परिचित दलित अफ़सर इलाक़ा मजिस्ट्रेट कुलतार सिंह से मिलते हैं। कुलतार मदद के बहाने अपने बाबू की मदद से काग़ज़ पर अंगूठे लगवाकर फरेब रचता है। काग़ज़ पर ज़मीन अलॉट हो जाती है और कुलतार सिंह के नाम बिक जाती है। ऐसी ही जालसाज़ियों से कुलतार सिंह सौ एकड़ के फ़ार्महाउस का मालिक हो चुका है। इस पूरे प्रसंग में जगदीशचन्द्र की अर्थशास्त्र की शिक्षा ख़ूब काम आई है। भूमि सुधार में क्या हुआ और किसे लाभ हुआ तथा दलितों को भूमि.वितरण की असलियत क्या थी-इन सबकी बारीकियों को उन्होंने ख़ूब उजागर किया है। इन कार्रवाइयों में पटवारी की भूमिका, पृतपाल जैसे भूस्वामियों, कुलतार जैसे दलित अधिकारियों और सेठ रामप्रकाश जैसे दलित नेताओं की कुत्सित चालों, सत्ताधर्मी चरित्र और मिली–भगत को घटनाक्रम विकास के ज़रिए नितान्त स्वाभाविक और विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। काली की बस्ती के लोगों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में देर से पता चलता है। चारों ओर भाग–दौड़ के बाद वे अपने को बेबस पाते हैं। कुलतार सिंह अपने क्लर्क केे ज़रिए सात–सात सौ रुपये दिलाकर उन्हें चुप कर देता है। वे बस्ती लौट आते हैं। कुछ शराब पीने चले जाते हैं और कुछ के पैसे साहूकारों की उधारी चुकता करने में लग जाते हैं। काली इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता और लड़ने की ठानता है। इसी प्रक्रिया में वह एक बार फिर टैनरीज़ के मालिक और नई पीढ़ी के दलित नेता सेठ रामप्रकाश से मिलता है तथा पुराने दलित नेता शिंगारा राम के साथ उसकी रस्साकशी और दलित राजनीति के अन्दरूनी दांवघातों और घटिया अवसरवादी चरित्र का साक्षी बनता है। सेठ रामप्रकाश जैसे दलित नेताओं की गाँठ भी कुलतारसिंह जैसे भ्रष्ट दलित अफ़सरों से ही जुड़ी है और आम दलितों को ठगने में वे इसी तंत्र के पुर्ज़े और ‘ट्रोजन हॉर्स’ की भूमिका निभाते हैं-इस तथ्य को जगदीशचन्द्र ने बड़ी कुशलता से उपन्यास की कथा में पिरोया है। अपनी ज़िद में काली को अन्ततोगत्वा गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ता है। उसका लड़का ज्ञानप्रकाश उर्फ लाटू, जो अब बैंक में क्लर्क हो गया है, अपने कालेज के एक दोस्त के वकील पिता की मदद से उसे थाने से जाकर छुड़ाता है।
इन घटनाओं के साथ काली के परिवार की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। उसका बड़ा बेटा ज्ञान प्रकाश बैंक में क्लर्क हो गया है और छोटा बेटा सतप्रकाश मेडिकल का छात्र। अपनी दूकान, मकान, दो भैंसों और बेटों की वजह से सामाजिक सम्मान-बेहतर आर्थिक स्थिति के बावजूद काली–पाशो मेहनत–मशक़्क”त की ज़िन्दगी बिताते हैं। लेकिन उनके जीवन और परिवेश से धीरे–धीरे उनके बेटे इतना कट जाते हैं कि उन्हें घर आना तक नाग़वार लगता है। इसी बीच ज्ञान आई.ए–एस. की परीक्षा पास कर लेता है और ट्रेनिंग पर चला जाता है। दोनों बेटे अब माँ–बाप से सिर्फ़ मिलने घर आते हैं, रुकते हैं वे शहर में दोस्तों के घर पर। शहर में उनके जो कुछ दोस्त हैं वे जाट, ब्राह्मण और अन्य सवर्ण–जातियों के ऐसे युवा हैं जो आम चलन से हटकर, जातिगत भेदभाव नहीं मानते।
ज्ञान की पहली पोस्टिंग होती है। न चाहते हुए भी, बेटों की ख़ातिर, पाशो के आग्रह पर काली पाशो के साथ, गाँव का घर बन्द करके ज्ञान के पास उसकी सरकारी कोठी में रहने चला जाता है। वहाँ के शाही ठाठ–बाट के माहौल को देखकर वह दंग है। उसे लगता है कि पूरे जीवन के अँधेरे को पारकर वह मुक्ति और उजाले की दुनिया में निकल आया है। ज़मीन की मिल्कियत की चाहत अभी भी काली के दिल में है। वह चाहता है कि ऊँचा अफ़सर होने के नाते ज्ञान कुलतार को उचित सज़ा दिलाए। ज्ञान उसे बताता है कि कुलतार क़ानूनन नहीं फँस रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। वह यह भी समझाता है कि यदि कहीं बंजर ज़मीन का एक टुकड़ा मिल भी जाए तो किस काम का। ज्ञान अपने अफ़सर मित्रों के बीच अपनी दलित पहचान को यथासम्भव छिपाकर भरपूर अभिजात ढंग से रहने की कोशिश करता है। एक दिन उसके दोस्तों की मण्डली में बैठा काली निहायत सादगी से उसके एक दोस्त को मशविरा देता है कि वह अपने उधड़ते हुए महँगे बूट की जल्द से जल्द मरम्मत करा ले। इससे ज्ञान बेहद अपमानित महसूस करता है। भीतर जाकर वह पिता को झिड़कता है, “मेरे दोस्तों को क्या यह बताना ज़रूरी था कि तुम चमार हो और मोची का काम करते हो?” वह कहता है, “यह जूतों की दुकान नहीं, आई.ए.एस. अफ़सर की कोठी है?” काली महसूस करता है कि पद और ओहदे ने स्वयं उसके बेटे को उन लोगों की कतारों में शामिल कर दिया है, जिनके द्वारा अपमान की ठोकरें वह जीवन भर खाता रहा। वह कोठी की सुख–सुविधा की जगह स्वतंत्रता और सम्मान का जीवन चुनता है। कोठी का अपमान उसे समाज में झेले जाने वाले अपमान से अधिक बुरा लगता है क्योंकि यहाँ उसे अपने बूते अपने ढंग से जीने की आज़ादी नहीं है। वह पाशो के साथ गाँव लौट जाता है।
‘धरती धन न अपना’ उपन्यास को रमेश कुन्तल मेघ ने ‘धरती के दुखियारों’ की जीवन–कथा कहा था। कमोबेश उनका यह कथन जगदीशचन्द्र के इन तीनों उपन्यासों के बारे में कहा जा सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उपन्यास–त्रयी की तीनों कृतियाँ हिन्दी के पहले ऐसे उपन्यास हैं जिनमें स्वातंत्र्योत्तर भारत के शुरुआती लगभग ढाई दशक के दौरान के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों की आधिकारिक तस्वीर दलितों के जीवन को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत की गई है। दलित–उत्पीड़न के प्रश्न को जगदीशचन्द्र ने दलित लेखकों की तरह सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक वस्तुगत स्थितियों से काटकर नहीं बल्कि उनके एक संघटक अवयव और परिणति के रूप में प्रस्तुत किया है। पंजाब के ग्रामीण, क़स्बाई और शहरी जीवन के पूँजीवादी रूपान्तरण के सूक्ष्म ब्योरों–तफ़सीलों को, दलित जीवन पर उनके प्रभाव को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत करने वाली ये हिन्दी की शायद अकेली औपन्यासिक कृतियाँ हैं। जाति–प्रश्न के प्रति जगदीशचन्द्र का रवैया वर्ग–विश्लेषणवादी है, लेकिन वर्ग–अपचयनवादी (क्लास–रिडक्शनिस्ट) नहीं है। ‘जुंकर टाइप बुर्जुआ भूमि.सुधारों’ के भारतीय संस्करण ने काश्तकार किसानों को मालिक बनाकर उनकी स्थिति में बदलाव किया और सामन्ती भूस्वामियों को बुर्जुआ भूस्वामी बन जाने का भरपूर अवसर दिया, लेकिन तमाम संवैधानिक “गारण्टियों” और प्रावधानों के बावजूद भूमिहीन दलितों की बहुसंख्यक आबादी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। पंजाब के गाँवों की पृष्ठभूमि में इस नंगी सच्चाई को जगदीशचन्द्र ने अत्यन्त कुशल ढंग से प्रस्तुत किया है। कभी–कभी अफ़सोस होता है कि देश के जिन इलाक़ों में ज़मीन्दारी प्रथा का भूमि.बन्दोबस्त लागू था (जैसे कि उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में) और जहाँ दलितों की जीवन स्थितियाँ सर्वाधिक नारकीय थीं, वहाँ की पृष्ठभूमि पर किसी उपन्यासकार ने दलित–जीवन को केन्द्र में रखकर इस तरह का कोई उपन्यास नहीं लिखा।
जातिगत उत्पीड़न के आर्थिक आधारों की अत्यन्त सूक्ष्मग्राही पड़ताल करने के साथ ही जगदीशचन्द्र बुर्जुआ वर्ग–विभेदीकरण के दलित–समाज की संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों की क़तई अनदेखी नहीं करते। वे इस सच्चाई से मुँह नहीं चुराते कि दलितों के बीच से जो एक मध्यवर्गीय बौद्धिक तबका पैदा हुआ है, वह स्वयं को बहुसंख्यक दलित आबादी से काटकर अलग कर चुका है और एक नये अभिजन तबके में तबदील हो चुका है। इन्हीं में कुलतार सिंह जैसे भ्रष्ट दलित अफ़सर हैं जो अपने ही भाइयों का हक़ छीनकर फ़ार्म हाउस का मालिक बन चुका है। दूसरी ओर काली के बेटे (कलक्टर) ज्ञान प्रकाश और (डॉक्टर) सतप्रकाश भी इन्हीं में शामिल हैं, जो स्वयं दलितों के सामाजिक जीवन के अन्धकारमय जीवन से बाहर निकल आने के बाद अब उधर मुड़कर भी नहीं देखना चाहते जहाँ अभी भी बहुसंख्यक दलित आबादी पड़ी हुई है। इसी प्रक्रिया में जगदीशचन्द्र दलित राजनीति की वास्तविकता को भी उजागर करते हैं जो मात्र दलित हितों की सौदेबाज़ी और वोटों की राजनीति करती है। सत्ता से नाभिनालबद्ध ऐसे राजनीतिज्ञों की पुरानी पीढ़ी की नुमाइन्दगी चौधरी शिंगाराराम करता है तो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व सेठ रामप्रकाश जैसे लोग करते हैं जो दलित राजनीति के नाम पर मात्र कुलतार सिंह जैसे दलित अफ़सरों के वर्गहितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कई मायनों में ‘गोदान’ की परम्परा का वास्तविक विस्तार जगदीशचन्द्र की इन कृतियों में देखा जा सकता है। ‘गोदान’ में मुख्यत: चौथे दशक के हिन्दुस्तान के गाँवों की गाथा है। वहाँ दलितों की जीवन स्थितियों का चित्रण भी है, लेकिन केन्द्र में ज़मीन्दारी प्रथा के जुए तले पिसते पूर्वी उत्तर प्रदेश के काश्तकार किसानों की दुरवस्था है। जगदीशचन्द्र की यह उपन्यासत्रयी मुख्यत: दशक के संक्रमणशील भारत के गाँवों की कथा है, लेकिन यहाँ केन्द्र में दलितों का जीवन है और विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियाँ पंजाब की हैं। साथ ही, जगदीशचन्द्र गाँवों से उजड़कर शहरों में आए दलितों की त्रासदी भी ग्राफ़िक विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं।
प्रेमचन्द की ही तरह, जगदीशचन्द्र के भी सन्दर्भ में “यथार्थवाद की विजय” मुख्यत: यह है कि उपस्थित किए गए मूलभूत जीवन–प्रश्न का समाधान वे कृत्रिम या आरोपित ढंग से कथावृत्त की चौहद्दी में घटित होते हुए नहीं दिखलाते। इस सतही विकल्प के द्वारा पाठक को राहत या चैन तो मिल सकता था, लेकिन यह “यथार्थवाद की पराजय” की शर्त पर ही सम्भव होता! ‘गोदान’ की ही तरह जगदीशचन्द्र की उपन्यासत्रयी का त्रासद अन्त पाठक को उस बेचैनी तक पहुँचाकर छोड़ देता है जहाँ से समाधान की तलाश की चिन्ताएँ उगना–पनपना शुरू करती हैं।
जगदीशचन्द्र हिन्दी कथा–साहित्य में यथार्थवाद के महान पुरस्कर्ताओं के समर्थ उत्तराधिकारी की अपनी योग्यता निर्विवाद रूप से सिद्ध कर चुके थे। हिन्दी साहित्य को अभी उनसे बहुत कुछ पाना था। उनके असामयिक निधन ने हिन्दी साहित्य को सचमुच अपूरणीय क्षति पहुँचाई है। काश कि अपनी उपन्यास–त्रयी की दलित महागाथा को वे बीसवीं सदी के अन्त तक विस्तार दे पाते! आशा की जानी चाहिए कि उनका कृतित्व नई पीढ़ी के कुछ साहसी, अध्यवसायी लेखकों को ऐसे प्रयासों के लिए प्रेरित करेगा!
ज़मीन अपनी तो थी (2001) नरककुण्ड में बास (1994 ) धरती धन न अपना (1972)
तीनों उपन्यासों के प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- सृजन परिप्रेक्ष्य, जनवरी-अप्रैल 2002