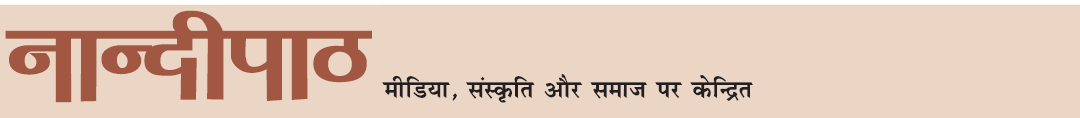Author Archives: नान्दीपाठ पत्रिका
ग्याँर्गी लुकाच का एक उद्दरण
गुजरात नरसंहार और “महान भारतीय मध्यवर्ग” का फ़ासीवादी चेहरा
 गुजरात के क़त्लेआम में मध्यवर्ग की भूमिका एक प्रातिनिधिक घटना है। कमोबेश उसमें पूरे भारतीय मध्यवर्ग की भूमिका की शिनाख्त की जा सकती है। यह सांस्कृतिक आन्दोलन के समक्ष उपस्थित गम्भीर चुनौतियों का अहसास कराती है और साम्प्रदायिकता–विरोध की पूरी रणनीति पर नये सिरे से सोचने के लिए बाध्य भी करती है। read more
गुजरात के क़त्लेआम में मध्यवर्ग की भूमिका एक प्रातिनिधिक घटना है। कमोबेश उसमें पूरे भारतीय मध्यवर्ग की भूमिका की शिनाख्त की जा सकती है। यह सांस्कृतिक आन्दोलन के समक्ष उपस्थित गम्भीर चुनौतियों का अहसास कराती है और साम्प्रदायिकता–विरोध की पूरी रणनीति पर नये सिरे से सोचने के लिए बाध्य भी करती है। read more मार्क ट्वेन की अमर कहानी : वह शख़्स जिसने हैडलेबर्ग को भ्रष्ट कर दिया

हैडलेबर्ग आसपास के सारे इलाक़े में सबसे ईमानदार और दयानतदार क़स्बा था। उसने पीढ़ियों से इस नेकनामी को बेदाग़ बनाए रखा था और उसे इस पर अपनी किसी भी दूसरी चीज़ से बढ़कर नाज़ था। उसे इस पर इस क़दर नाज़ था और वह इसे क़ायम रखने के लिए इतना बेताब था कि क़स्बे के लोग पालने में ही बच्चों को ईमानदारी की घुट्टी पिलाने लगते थे और उनकी शिक्षा के वर्षों के दौरान यही सबक उनकी पढ़ाई–लिखाई का मुख्य विषय होता था। read more
इक्कीसवीं सदी में बाल्ज़ाक

बाल्जाक की कालजयी महानता इस बात में निहित है कि उन्होंने मनुष्य को सामाजिक रूप से सक्रिय प्राणी के रूप में और अपने भाग्य के नियन्ता के रूप में, और अपने नैतिक आग्रहों और आदर्शों के लिए जूझते हुए दिखलाया। अपने अनगढ़–अधूरे वैज्ञानिक विचारों तथा अपने विचारों और आस्था के बीच के अन्तरविरोध के बावजूद, बाल्जाक के सामाजिक मानव के प्रकृत इतिहास–सम्बन्धी सिद्धान्त और फ्लॉबेयर के इस सिद्धान्त में कि कलाकार को देवता के समान तटस्थ होना चाहिए, भारी अन्तर है। राल्फ़ फॉक्स के शब्दों में, “…जीवन को देखने का उनका दृष्टिकोण सच्चे अर्थ में यथार्थवादी था। वह मानव समाज को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, एक ऐसी वस्तु के रूप में देखते थे, जो संघर्ष करती है और संघर्ष के दौरान विकसित होती है। फ्लॉबेयर में जीवन जैसे आम और स्थिर हो गया है। 1848 के बाद जीवन को उसके विकास–क्रम में देखना और चित्रित करना सम्भव न रहा, कारण कि वह विकास–क्रम अत्यन्त पीड़ामय था। सो, जीवन उनके लिए एक जमी हुई झील बन गया।” (‘उपन्यास और लोकजीवन’)
read moreहमारे समय का यथार्थ और जगदीशचन्द्र के उपन्यास
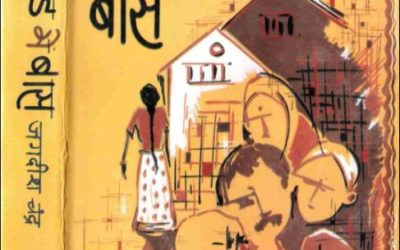
प्रेमचन्द की ही तरह, जगदीशचन्द्र के भी सन्दर्भ में “यथार्थवाद की विजय” मुख्यत: यह है कि उपस्थित किए गए मूलभूत जीवन–प्रश्न का समाधान वे कृत्रिम या आरोपित ढंग से कथावृत्त की चौहद्दी में घटित होते हुए नहीं दिखलाते। इस सतही विकल्प के द्वारा पाठक को राहत या चैन तो मिल सकता था, लेकिन यह “यथार्थवाद की पराजय” की शर्त पर ही सम्भव होता! ‘गोदान’ की ही तरह जगदीशचन्द्र की उपन्यासत्रयी का त्रासद अन्त पाठक को उस बेचैनी तक पहुँचाकर छोड़ देता है जहाँ से समाधान की तलाश की चिन्ताएँ उगना–पनपना शुरू करती हैं।
read moreभाषा–विज्ञान के इतिहास में मार्क्सवाद और वोलोशिनोव
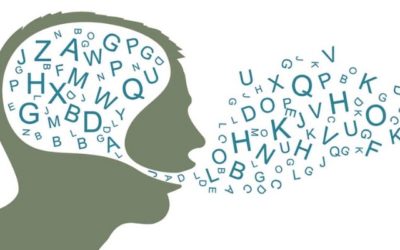
मानव–चिन्तन और संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों की खोज में आगे बढ़ते हुए, भाषा के प्रश्न से दर्शन की मुठभेड़ प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। मानव–समाज की समस्त भौतिक और आत्मिक गतिविधियों के दौरान संज्ञानात्मक और संसर्गात्मक प्रकार्यों (Function) की पूर्ति करनेवाली आधारभूत संकेत–प्रणाली के रूप में भाषा के विकास, उसकी प्रकृति और संरचना के अध्ययन के साथ–साथ, अव्यवस्थित ढंग से ही सही, पर शताब्दियों तक, दार्शनिक इन प्रश्नों से भी जूझते रहे कि भाषा किस हद तक मनुष्य की अन्य प्राणियों से इतर, प्राकृतिक–जैविक विशिष्टता की उपज है और किस हद तक यह एक सामाजिक परिघटना है। read more
ब्रेष्ट और स्तानिस्लाव्स्की-साथ–साथ और आमने–सामने

हमारे थिएटर को चीज़ों को समझने में होने वाले रोमाँच को प्रोत्साहित करना चाहिए और लोगों को यथास्थिति को बदलने में आनन्द लेने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हमारे दर्शकों को केवल यही नहीं सुनना चाहिए कि प्रोमीथियस कैसे मुक्त हुआ, बल्कि उन्हें उसे मुक्त कराने के आनन्द में स्वयं को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि वह हमारे थिएटर में आविष्कारक और अन्वेषक द्वारा अनुभव किए जाने वाले सन्तोष व आनन्द को महसूस करें, मुक्तिदायक के विजय के गौरव को महसूस करें। read more
सौन्दर्यीकरण के बारे में कुछ नोट्स
अपने व्यक्तित्व को भी सुन्दर बनाने का अतिरिक्त आग्रह एक आत्मरति है, जो इन्सान को चीज़ बना देता है। या फिर केंचुआ। या शायद, गम्भीरता–सुन्दरता का स्वाँग रचने वाला एक विदूषक। read more
कूर्बे की कला और उसकी ज़मीन

आज जब चित्रकला की यथार्थवादी परम्परा की कला–इतिहास और सैद्धान्तिकी के बुर्जुआ हलकों में चर्चा होती है तो प्राय: कूर्बे का नाम या तो चलताऊ ढंग से लिया जाता है या फिर उसके वैचारिक पक्षों और प्रतिबद्धता की अनदेखी की जाती है। उसके कृतित्व के कुछ प्रखर–प्रदीप्त पक्ष आज भी बुर्जुआ कलावन्तों की आँखों में चुभते हैं, उनके सुकोमल सौन्दर्य–बोध को घायल करते हैं। कूर्बे अपने समय में भी ऐसे लोगों को सदमा और झटका देता था और आज भी देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रश थामने वाले हाथों में बन्दूक थामकर सर्वहारा सत्ता के पक्ष में बैरिकेड्स के पीछे जा डटने वाले तथा जेल और निर्वासन से भी न टूटने वाले कलाकार को भला वे कलावन्त लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो कला के “बाज़ार” में महज़ कोठे के दलालों की भूमिका निभाते हैं?
read more